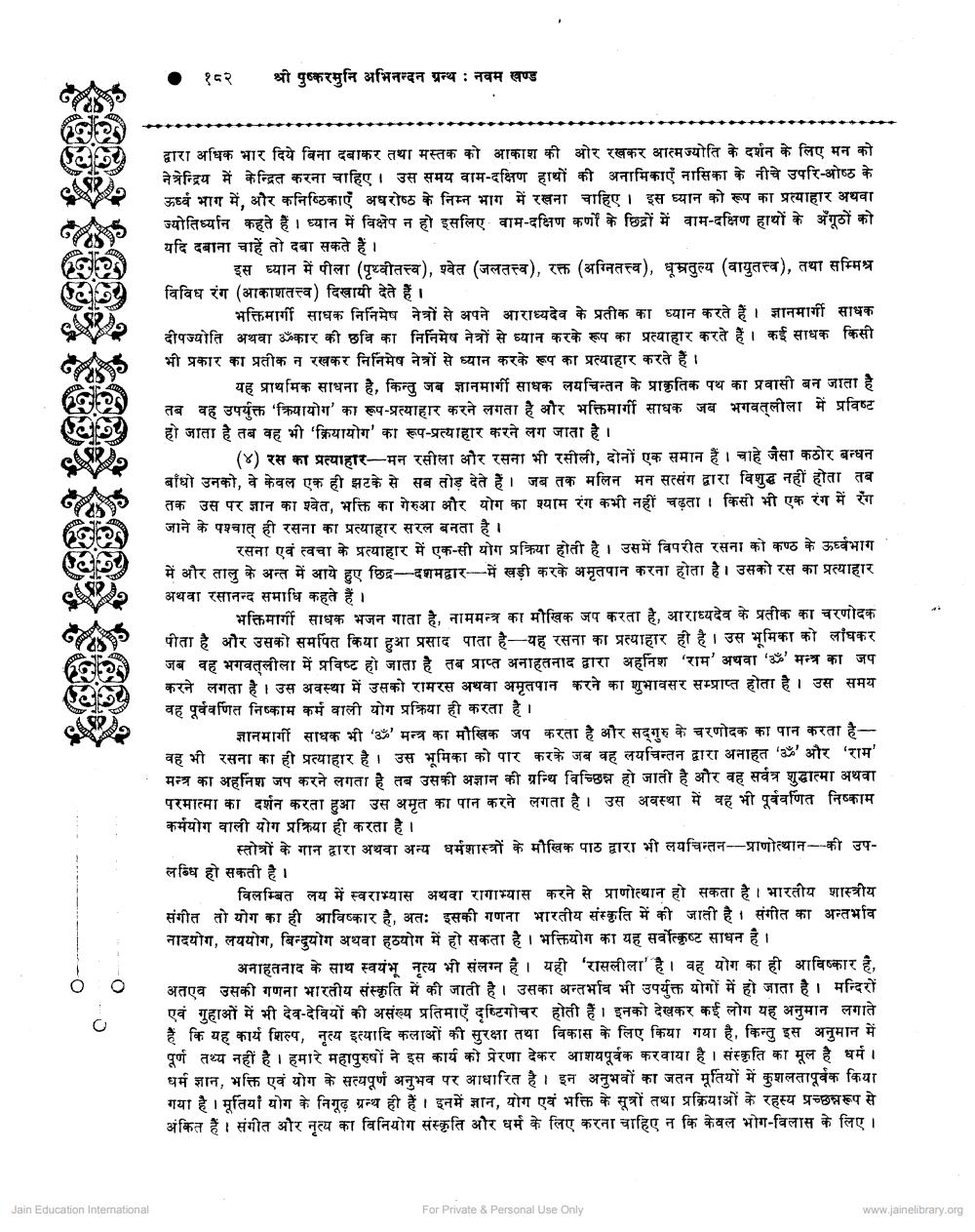________________
.
१८२
श्री पुष्करमुनि अभिनन्दन ग्रन्थ : नवम खण्ड
द्वारा अधिक भार दिये बिना दबाकर तथा मस्तक को आकाश की ओर रखकर आत्मज्योति के दर्शन के लिए मन को नेत्रेन्द्रिय में केन्द्रित करना चाहिए। उस समय वाम-दक्षिण हाथों की अनामिकाएँ नासिका के नीचे उपरि-ओष्ठ के ऊर्ध्व भाग में, और कनिष्ठिकाएँ अधरोष्ठ के निम्न भाग में रखना चाहिए। इस ध्यान को रूप का प्रत्याहार अथवा ज्योतिर्ध्यान कहते हैं । ध्यान में विक्षेप न हो इसलिए वाम-दक्षिण कर्णों के छिद्रों में वाम-दक्षिण हाथों के अँगूठों को यदि दबाना चाहें तो दबा सकते हैं।
इस ध्यान में पीला (पृथ्वीतत्त्व), श्वेत (जलतत्त्व), रक्त (अग्नितत्त्व), धूम्रतुल्य (वायुतत्त्व), तथा सम्मिश्र विविध रंग (आकाशतत्त्व) दिखायी देते हैं।
भक्तिमार्गी साधक निनिमेष नेत्रों से अपने आराध्यदेव के प्रतीक का ध्यान करते हैं। ज्ञानमार्गी साधक दीपज्योति अथवा ॐकार की छवि का निनिमेष नेत्रों से ध्यान करके रूप का प्रत्याहार करते हैं। कई साधक किसी भी प्रकार का प्रतीक न रखकर निनिमेष नेत्रों से ध्यान करके रूप का प्रत्याहार करते हैं।
यह प्राथमिक साधना है, किन्तु जब ज्ञानमार्गी साधक लयचिन्तन के प्राकृतिक पथ का प्रवासी बन जाता है तब वह उपर्युक्त 'क्रियायोग' का रूप-प्रत्याहार करने लगता है और भक्तिमार्गी साधक जब भगवत्लीला में प्रविष्ट हो जाता है तब वह भी 'क्रियायोग' का रूप-प्रत्याहार करने लग जाता है।
(४) रस का प्रत्याहार-मन रसीला और रसना भी रसीली, दोनों एक समान हैं। चाहे जैसा कठोर बन्धन बाँधो उनको, वे केवल एक ही झटके से सब तोड़ देते हैं। जब तक मलिन मन सत्संग द्वारा विशुद्ध नहीं होता तब तक उस पर ज्ञान का श्वेत, भक्ति का गेरुआ और योग का श्याम रंग कभी नहीं चढ़ता। किसी भी एक रंग में रंग जाने के पश्चात् ही रसना का प्रत्याहार सरल बनता है।
रसना एवं त्वचा के प्रत्याहार में एक-सी योग प्रक्रिया होती है। उसमें विपरीत रसना को कण्ठ के ऊर्ध्वभाग में और तालु के अन्त में आये हुए छिद्र-दशमद्वार-में खड़ी करके अमृतपान करना होता है। उसको रस का प्रत्याहार अथवा रसानन्द समाधि कहते हैं।
भक्तिमार्गी साधक भजन गाता है, नाममन्त्र का मौखिक जप करता है, आराध्यदेव के प्रतीक का चरणोदक पीता है और उसको समर्पित किया हुआ प्रसाद पाता है-यह रसना का प्रत्याहार ही है। उस भूमिका को लांघकर जब वह भगवत्लीला में प्रविष्ट हो जाता है तब प्राप्त अनाहतनाद द्वारा अहर्निश 'राम' अथवा 'ॐ' मन्त्र का जप करने लगता है। उस अवस्था में उसको रामरस अथवा अमृतपान करने का शुभावसर सम्प्राप्त होता है। उस समय वह पूर्ववणित निष्काम कर्म वाली योग प्रक्रिया ही करता है।
ज्ञानमार्गी साधक भी 'ॐ' मन्त्र का मौखिक जप करता है और सद्गुरु के चरणोदक का पान करता हैवह भी रसना का ही प्रत्याहार है। उस भूमिका को पार करके जब वह लयचिन्तन द्वारा अनाहत 'ॐ' और 'राम' मन्त्र का अहर्निश जप करने लगता है तब उसकी अज्ञान की ग्रन्थि विच्छिन्न हो जाती है और वह सर्वत्र शुद्धात्मा अथवा परमात्मा का दर्शन करता हुआ उस अमृत का पान करने लगता है। उस अवस्था में वह भी पूर्ववणित निष्काम कर्मयोग वाली योग प्रक्रिया ही करता है।
स्तोत्रों के गान द्वारा अथवा अन्य धर्मशास्त्रों के मौखिक पाठ द्वारा भी लयचिन्तन-प्राणोत्थान--की उपलब्धि हो सकती है।
विलम्बित लय में स्वराभ्यास अथवा रागाभ्यास करने से प्राणोत्थान हो सकता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत तो योग का ही आविष्कार है, अतः इसकी गणना भारतीय संस्कृति में की जाती है। संगीत का अन्तर्भाव नादयोग, लययोग, बिन्दुयोग अथवा हठयोग में हो सकता है । भक्तियोग का यह सर्वोत्कृष्ट साधन है।
अनाहतनाद के साथ स्वयंभू नृत्य भी संलग्न है। यही 'रासलीला' है। वह योग का ही आविष्कार है, अतएव उसकी गणना भारतीय संस्कृति में की जाती है। उसका अन्तर्भाव भी उपर्युक्त योगों में हो जाता है। मन्दिरों एवं गुहाओं में भी देव-देवियों की असंख्य प्रतिमाएँ दृष्टिगोचर होती हैं। इनको देखकर कई लोग यह अनुमान लगाते हैं कि यह कार्य शिल्प, नृत्य इत्यादि कलाओं की सुरक्षा तथा विकास के लिए किया गया है, किन्तु इस अनुमान में पूर्ण तथ्य नहीं है । हमारे महापुरुषों ने इस कार्य को प्रेरणा देकर आशयपूर्वक करवाया है। संस्कृति का मूल है धर्म । धर्म ज्ञान, भक्ति एवं योग के सत्यपूर्ण अनुभव पर आधारित है। इन अनुभवों का जतन मूर्तियों में कुशलतापूर्वक किया गया है । मूर्तियां योग के निगूढ़ ग्रन्थ ही हैं। इनमें ज्ञान, योग एवं भक्ति के सूत्रों तथा प्रक्रियाओं के रहस्य प्रच्छन्नरूप से अंकित हैं। संगीत और नृत्य का विनियोग संस्कृति और धर्म के लिए करना चाहिए न कि केवल भोग-विलास के लिए।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org