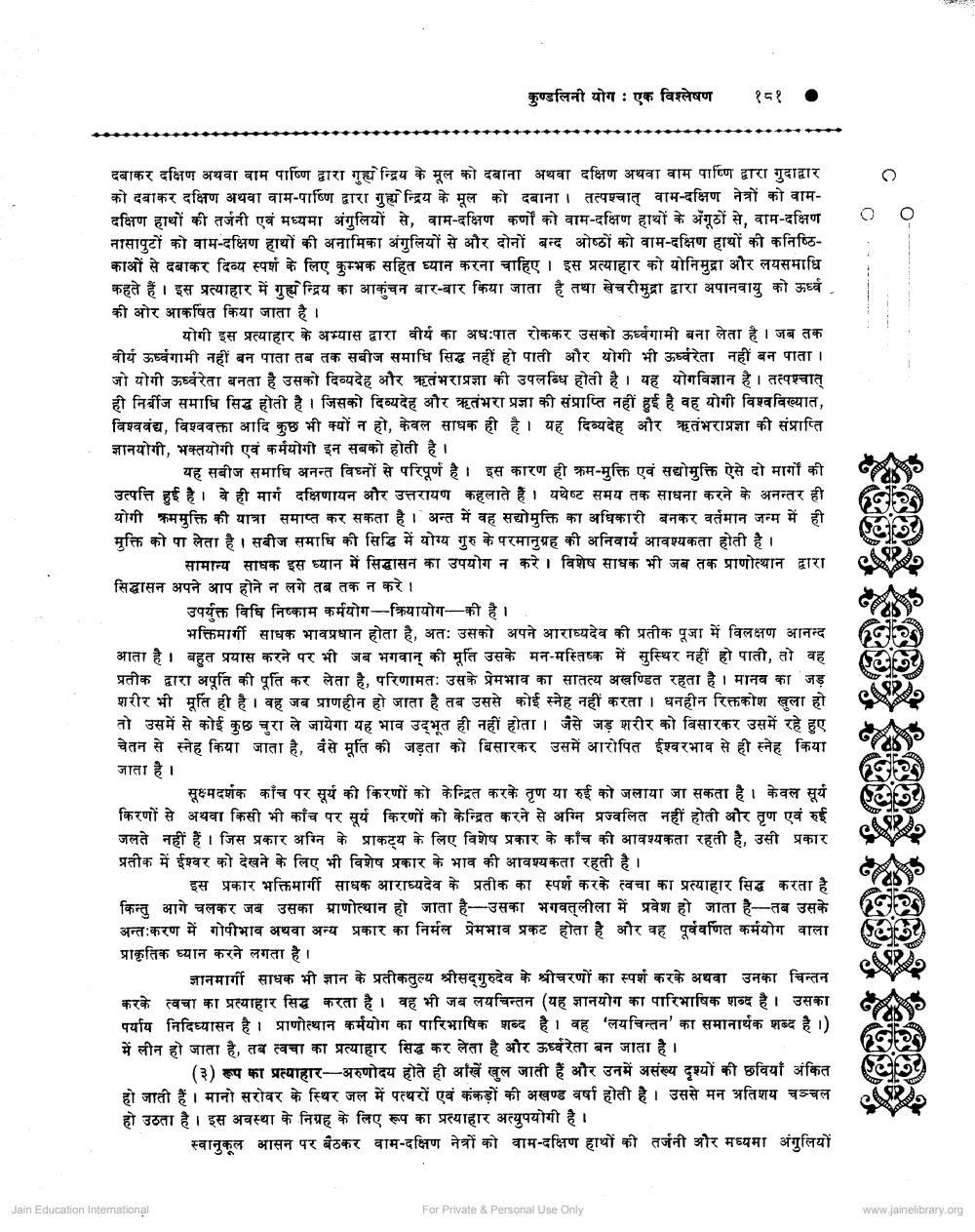________________
कुण्डलिनी योग : एक विश्लेषण
१८१ .
-
---------
दबाकर दक्षिण अथवा वाम पाष्णि द्वारा गुह्यन्द्रिय के मूल को दबाना अथवा दक्षिण अथवा वाम पाष्णि द्वारा गुदाद्वार को दबाकर दक्षिण अथवा वाम-पाष्णि द्वारा गुह्यन्द्रिय के मूल को दबाना। तत्पश्चात् वाम-दक्षिण नेत्रों को वामदक्षिण हाथों की तर्जनी एवं मध्यमा अंगुलियों से, वाम-दक्षिण कों को वाम-दक्षिण हाथों के अँगूठों से, वाम-दक्षिण नासापुटों को वाम-दक्षिण हाथों की अनामिका अंगुलियों से और दोनों बन्द ओष्ठों को वाम-दक्षिण हाथों की कनिष्ठिकाओं से दबाकर दिव्य स्पर्श के लिए कुम्भक सहित ध्यान करना चाहिए। इस प्रत्याहार को योनिमुद्रा और लयसमाधि कहते हैं । इस प्रत्याहार में गुह्य न्द्रिय का आकुंचन बार-बार किया जाता है तथा खेचरीमुद्रा द्वारा अपानवायु को ऊर्ध्व , की ओर आकर्षित किया जाता है ।
योगी इस प्रत्याहार के अभ्यास द्वारा वीर्य का अधःपात रोककर उसको ऊर्ध्वगामी बना लेता है । जब तक वीर्य ऊर्ध्वगामी नहीं बन पाता तब तक सबीज समाधि सिद्ध नहीं हो पाती और योगी भी ऊर्ध्वरेता नहीं बन पाता। जो योगी ऊर्ध्वरेता बनता है उसको दिव्यदेह और ऋतंभराप्रज्ञा की उपलब्धि होती है। यह योगविज्ञान है। तत्पश्चात् ही निर्बीज समाधि सिद्ध होती है । जिसको दिव्यदेह और ऋतंभरा प्रज्ञा की संप्राप्ति नहीं हुई है वह योगी विश्वविख्यात, विश्ववंद्य, विश्ववक्ता आदि कुछ भी क्यों न हो, केवल साधक ही है। यह दिव्यदेह और ऋतंभराप्रज्ञा की संप्राप्ति ज्ञानयोगी, भक्तयोगी एवं कर्मयोगी इन सबको होती है।
यह सबीज समाधि अनन्त विघ्नों से परिपूर्ण है। इस कारण ही क्रम-मुक्ति एवं सद्योमुक्ति ऐसे दो मार्गों की उत्पत्ति हुई है। वे ही मार्ग दक्षिणायन और उत्तरायण कहलाते हैं। यथेष्ट समय तक साधना करने के अनन्तर ही योगी क्रममुक्ति की यात्रा समाप्त कर सकता है। अन्त में वह सद्योमुक्ति का अधिकारी बनकर वर्तमान जन्म में ही मुक्ति को पा लेता है । सबीज समाधि की सिद्धि में योग्य गुरु के परमानुग्रह की अनिवार्य आवश्यकता होती है ।
__सामान्य साधक इस ध्यान में सिद्धासन का उपयोग न करे । विशेष साधक भी जब तक प्राणोत्थान द्वारा सिद्धासन अपने आप होने न लगे तब तक न करे।
उपर्युक्त विधि निष्काम कर्मयोग-क्रियायोग-की है।
भक्तिमार्गी साधक भावप्रधान होता है, अत: उसको अपने आराध्यदेव की प्रतीक पूजा में विलक्षण आनन्द आता है। बहुत प्रयास करने पर भी जब भगवान् की मूर्ति उसके मन-मस्तिष्क में सुस्थिर नहीं हो पाती, तो वह प्रतीक द्वारा अपूर्ति की पूर्ति कर लेता है, परिणामतः उसके प्रेमभाव का सातत्य अखण्डित रहता है। मानव का जड़ शरीर भी मूर्ति ही है। वह जब प्राणहीन हो जाता है तब उससे कोई स्नेह नहीं करता । धनहीन रिक्तकोश खुला हो तो उसमें से कोई कुछ चुरा ले जायेगा यह भाव उद्भूत ही नहीं होता। जैसे जड़ शरीर को बिसारकर उसमें रहे हुए चेतन से स्नेह किया जाता है, वैसे मूर्ति की जड़ता को बिसारकर उसमें आरोपित ईश्वरभाव से ही स्नेह किया जाता है।
सूक्ष्मदर्शक काँच पर सूर्य की किरणों को केन्द्रित करके तृण या रुई को जलाया जा सकता है। केवल सूर्य किरणों से अथवा किसी भी कांच पर सूर्य किरणों को केन्द्रित करने से अग्नि प्रज्वलित नहीं होती और तृण एवं रुई जलते नहीं हैं। जिस प्रकार अग्नि के प्राकट्य के लिए विशेष प्रकार के काँच की आवश्यकता रहती है, उसी प्रकार प्रतीक में ईश्वर को देखने के लिए भी विशेष प्रकार के भाव की आवश्यकता रहती है।
इस प्रकार भक्तिमार्गी साधक आराध्यदेव के प्रतीक का स्पर्श करके त्वचा का प्रत्याहार सिद्ध करता है किन्तु आगे चलकर जब उसका प्राणोत्थान हो जाता है-उसका भगवत्लीला में प्रवेश हो जाता है तब उसके अन्तःकरण में गोपीभाव अथवा अन्य प्रकार का निर्मल प्रेमभाव प्रकट होता है और वह पूर्ववर्णित कर्मयोग वाला प्राकृतिक ध्यान करने लगता है।
ज्ञानमार्गी साधक भी ज्ञान के प्रतीकतुल्य श्रीसद्गुरुदेव के श्रीचरणों का स्पर्श करके अथवा उनका चिन्तन करके त्वचा का प्रत्याहार सिद्ध करता है। वह भी जब लयचिन्तन (यह ज्ञानयोग का पारिभाषिक शब्द है। उसका पर्याय निदिध्यासन है। प्राणोत्थान कर्मयोग का पारिभाषिक शब्द है। वह 'लयचिन्तन' का समानार्थक शब्द है।) में लीन हो जाता है, तब त्वचा का प्रत्याहार सिद्ध कर लेता है और ऊर्ध्वरेता बन जाता है।
(३) रूप का प्रत्याहार-अरुणोदय होते ही आँखें खुल जाती हैं और उनमें असंख्य दृश्यों की छवियाँ अंकित हो जाती हैं। मानो सरोवर के स्थिर जल में पत्थरों एवं कंकड़ों की अखण्ड वर्षा होती है। उससे मन अतिशय चञ्चल हो उठता है । इस अवस्था के निग्रह के लिए रूप का प्रत्याहार अत्युपयोगी है ।
स्वानुकल आसन पर बैठकर वाम-दक्षिण नेत्रों को वाम-दक्षिण हाथों की तर्जनी और मध्यमा अंगुलियों
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org