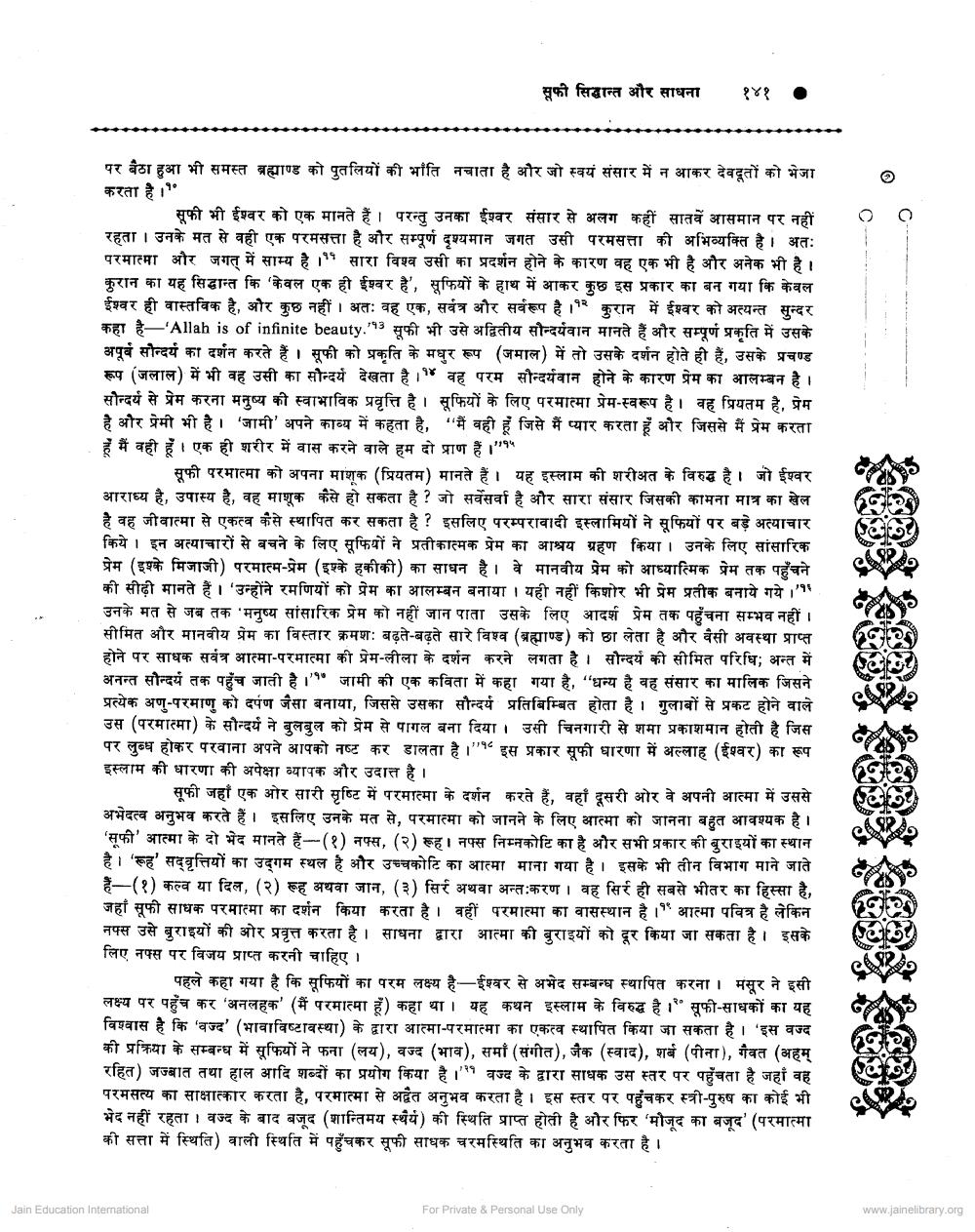________________
सूफी सिद्धान्त और साधना
१४१
.
पर बैठा हुआ भी समस्त ब्रह्माण्ड को पुतलियों की भाँति नचाता है और जो स्वयं संसार में न आकर देवदूतों को भेजा
करता है।
सारा विश्व उसीकयों के हाथ में है। मागत है और
सूफी भी ईश्वर को एक मानते हैं। परन्तु उनका ईश्वर संसार से अलग कहीं सातवें आसमान पर नहीं रहता । उनके मत से वही एक परमसत्ता है और सम्पूर्ण दृश्यमान जगत उसी परमसत्ता की अभिव्यक्ति है। अतः परमात्मा और जगत् में साम्य है ।" सारा विश्व उसी का प्रदर्शन होने के कारण वह एक भी है और अनेक भी है। कुरान का यह सिद्धान्त कि केवल एक ही ईश्वर है', सूफियों के हाथ में आकर कुछ इस प्रकार का बन गया कि केवल ईश्वर ही वास्तविक है, और कुछ नहीं। अतः वह एक, सर्वत्र और सर्वरूप है ।१२ कुरान में ईश्वर को अत्यन्त सुन्दर कहा है-'Allah is of infinite beauty.१3 सूफी भी उसे अद्वितीय सौन्दर्यवान मानते हैं और सम्पूर्ण प्रकृति में उसके अपूर्व सौन्दर्य का दर्शन करते हैं। सूफी को प्रकृति के मधुर रूप (जमाल) में तो उसके दर्शन होते ही हैं, उसके प्रचण्ड रूप (जलाल) में भी वह उसी का सौन्दर्य देखता है। वह परम सौन्दर्यवान होने के कारण प्रेम का आलम्बन है। सौन्दर्य से प्रेम करना मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। सूफियों के लिए परमात्मा प्रेम-स्वरूप है। वह प्रियतम है, प्रेम है और प्रेमी भी है। 'जामी' अपने काव्य में कहता है, "मैं वही हूँ जिसे मैं प्यार करता है और जिससे मैं प्रेम करता हूँ मैं वही हूँ। एक ही शरीर में वास करने वाले हम दो प्राण हैं ।"१५ ।
सूफी परमात्मा को अपना माशक (प्रियतम) मानते हैं। यह इस्लाम की शरीअत के विरुद्ध है। जो ईश्वर आराध्य है, उपास्य है, वह माशूक कैसे हो सकता है ? जो सर्वेसर्वा है और सारा संसार जिसकी कामना मात्र का खेल है वह जीवात्मा से एकत्व कैसे स्थापित कर सकता है ? इसलिए परम्परावादी इस्लामियों ने सूफियों पर बड़े अत्याचार किये। इन अत्याचारों से बचने के लिए सूफियों ने प्रतीकात्मक प्रेम का आश्रय ग्रहण किया। उनके लिए सांसारिक प्रेम (इश्के मिजाजी) परमात्म-प्रेम (इश्के हकीकी) का साधन है। वे मानवीय प्रेम को आध्यात्मिक प्रेम तक पहुँचने की सीढ़ी मानते हैं। उन्होंने रमणियों को प्रेम का आलम्बन बनाया। यही नहीं किशोर भी प्रेम प्रतीक बनाये गये ।११ उनके मत से जब तक 'मनुष्य सांसारिक प्रेम को नहीं जान पाता उसके लिए आदर्श प्रेम तक पहुँचना सम्भव नहीं। सीमित और मानवीय प्रेम का विस्तार क्रमश: बढ़ते-बढ़ते सारे विश्व (ब्रह्माण्ड) को छा लेता है और वैसी अवस्था प्राप्त होने पर साधक सर्वत्र आत्मा-परमात्मा की प्रेम-लीला के दर्शन करने लगता है। सौन्दर्य की सीमित परिधि; अन्त में अनन्त सौन्दर्य तक पहुँच जाती है ।१० जामी की एक कविता में कहा गया है, "धन्य है वह संसार का मालिक जिसने प्रत्येक अणु-परमाणु को दर्पण जैसा बनाया, जिससे उसका सौन्दर्य प्रतिबिम्बित होता है। गुलाबों से प्रकट होने वाले उस (परमात्मा) के सौन्दर्य ने बुलबुल को प्रेम से पागल बना दिया। उसी चिनगारी से शमा प्रकाशमान होती है जिस पर लुब्ध होकर परवाना अपने आपको नष्ट कर डालता है।"१८ इस प्रकार सूफी धारणा में अल्लाह (ईश्वर) का रूप इस्लाम की धारणा की अपेक्षा व्यापक और उदात्त है।
सूफी जहाँ एक ओर सारी सृष्टि में परमात्मा के दर्शन करते हैं, वहाँ दूसरी ओर वे अपनी आत्मा में उससे अभेदत्व अनुभव करते हैं। इसलिए उनके मत से, परमात्मा को जानने के लिए आत्मा को जानना बहुत आवश्यक है। 'सूफी' आत्मा के दो भेद मानते हैं-(१) नफ्स, (२) रूह। नफ्स निम्नकोटि का है और सभी प्रकार की बुराइयों का स्थान है। 'रूह' सद्वृत्तियों का उद्गम स्थल है और उच्चकोटि का आत्मा माना गया है। इसके भी तीन विभाग माने जाते हैं-(१) कल्व या दिल, (२) रूह अथवा जान, (३) सिरी अथवा अन्त:करण । वह सिर्र ही सबसे भीतर का हिस्सा है, जहाँ सूफी साधक परमात्मा का दर्शन किया करता है। वहीं परमात्मा का वासस्थान है। आत्मा पवित्र है लेकिन नफ्स उसे बुराइयों की ओर प्रवृत्त करता है। साधना द्वारा आत्मा की बुराइयों को दूर किया जा सकता है। इसके लिए नफ्स पर विजय प्राप्त करनी चाहिए।
पहले कहा गया है कि सूफियों का परम लक्ष्य है-ईश्वर से अभेद सम्बन्ध स्थापित करना। मसूर ने इसी लक्ष्य पर पहुँच कर 'अनलहक' (मैं परमात्मा हूँ) कहा था। यह कथन इस्लाम के विरुद्ध है।" सूफी-साधकों का यह विश्वास है कि 'वज्द' (भावाविष्टावस्था) के द्वारा आत्मा-परमात्मा का एकत्व स्थापित किया जा सकता है। इस वज्द की प्रक्रिया के सम्बन्ध में सूफियों ने फना (लय), वज्द (भाव), समाँ (संगीत), जैक (स्वाद), शर्ब (पीना), गैवत (अहम् रहित) जज्बात तथा हाल आदि शब्दों का प्रयोग किया है ।१ बज्द के द्वारा साधक उस स्तर पर पहुँचता है जहाँ वह परमसत्य का साक्षात्कार करता है, परमात्मा से अद्वैत अनुभव करता है। इस स्तर पर पहुंचकर स्त्री-पुरुष का कोई भी भेद नहीं रहता। वज्द के बाद बजूद (शान्तिमय स्थैर्य) की स्थिति प्राप्त होती है और फिर 'मौजूद का बजूद' (परमात्मा की सत्ता में स्थिति) वाली स्थिति में पहुँचकर सूफी साधक चरमस्थिति का अनुभव करता है।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org