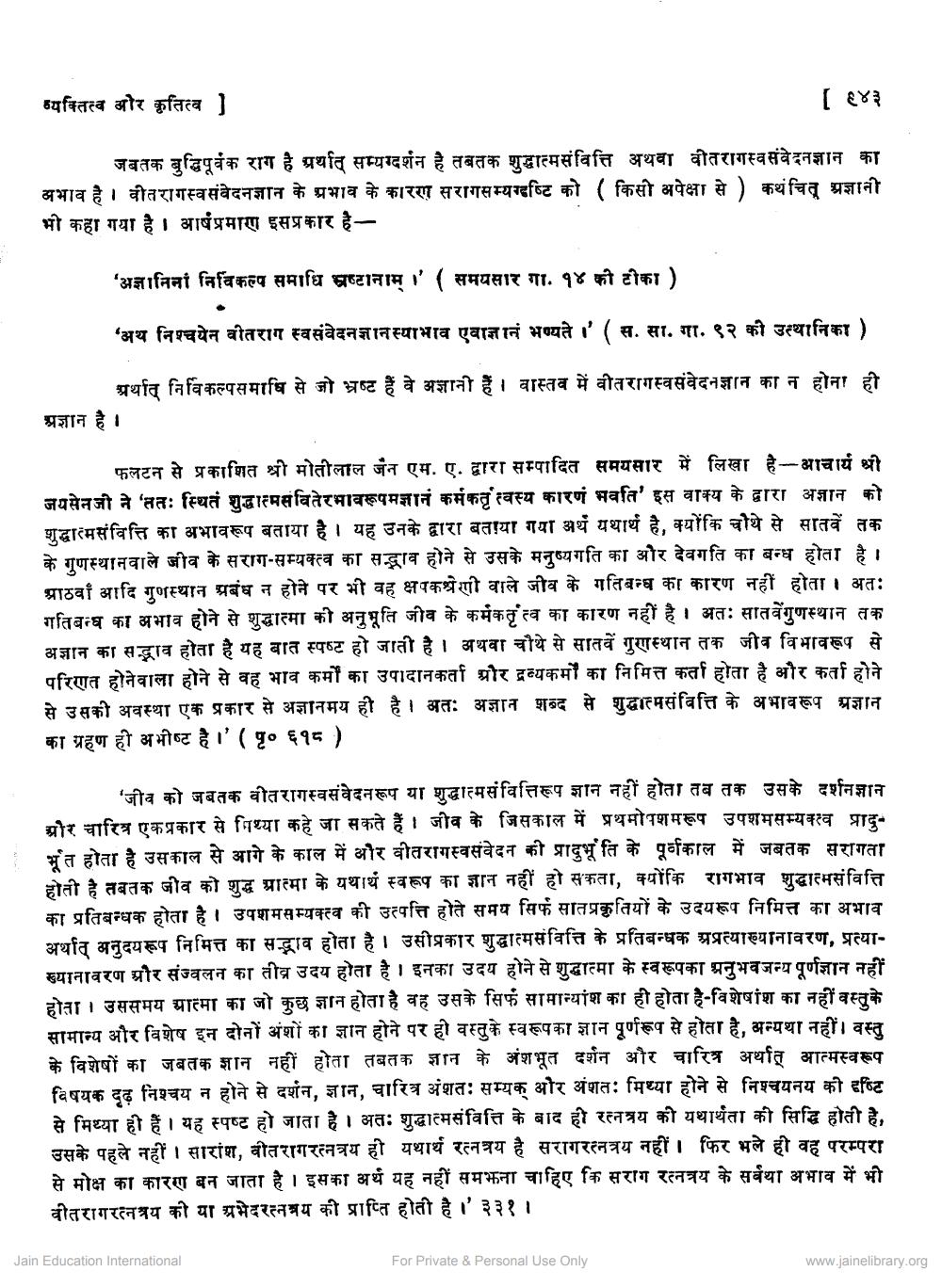________________
व्यक्तित्व और कृतित्व ]
[ ९४३
जबतक बुद्धिपूर्वक राग है अर्थात् सम्यग्दर्शन है तबतक शुद्धात्मसंवित्ति अथवा वीतरागस्वसंवेदनज्ञान का अभाव है । वीतरागस्वसंवेदनज्ञान के प्रभाव के कारण सरागसम्यग्दष्टि को ( किसी अपेक्षा से ) कथंचितू अज्ञानी भी कहा गया है । आर्षप्रमाण इसप्रकार है
'अज्ञानिना निर्विकल्प समाधि भ्रष्टानाम् ।' ( समयसार गा. १४ की टीका )
'अथ निश्चयेन वीतराग स्वसंवेदनज्ञानस्याभाव एवाजानं भव्यते ।' ( स. सा. गा. ९२ की उत्थानिका)
अर्थात् निविकल्पसमाधि से जो भ्रष्ट हैं वे अज्ञानी हैं। वास्तव में वीतरागस्वसंवेदनज्ञान का न होना ही प्रज्ञान है।
फलटन से प्रकाशित श्री मोतीलाल जैन एम. ए. द्वारा सम्पादित समयसार में लिखा है-आचार्य श्री जयसेनजी ने 'ततः स्थितं शुद्धात्मसंवितेरभावरूपमज्ञानं कर्मकर्तृत्वस्य कारणं भवति' इस वाक्य के द्वारा अज्ञान को शुद्धात्मसंवित्ति का अभावरूप बताया है। यह उनके द्वारा बताया गया अर्थ यथार्थ है, क्योंकि चौथे से सातवें तक के गुणस्थानवाले जीव के सराग-सम्यक्त्व का सद्भाव होने से उसके मनुष्य गति का और देवगति का बन्ध होता है। पाठवाँ आदि गुणस्थान प्रबंध न होने पर भी वह क्षपकश्रेणी वाले जीव के गतिबन्ध का कारण नहीं होता। अतः गतिबन्ध का अभाव होने से शुद्धात्मा की अनुभूति जीव के कर्मकर्तृत्व का कारण नहीं है। अतः सातवेंगुणस्थान तक अज्ञान का सद्भाव होता है यह बात स्पष्ट हो जाती है। अथवा चौथे से सातवें गुरणस्थान तक जीव विभावरूप से परिणत होनेवाला होने से वह भाव कर्मों का उपादानकर्ता और द्रव्यकर्मों का निमित्त कर्ता होता है और कर्ता होने से उसकी अवस्था एक प्रकार से अज्ञानमय ही है। अतः अज्ञान शब्द से शुद्धात्मसंवित्ति के अभावरूप प्रज्ञान का ग्रहण ही अभीष्ट है।' (पृ० ६१८ )
'जीव को जबतक वीतरागस्वसंवेदनरूप या शुद्धात्मसंवित्तिरूप ज्ञान नहीं होता तब तक उसके दर्शन ज्ञान और चारित्र एकप्रकार से मिथ्या कहे जा सकते हैं। जीव के जिसकाल में प्रथमोपशमरूप उपशमसम्यक्त्व भूत होता है उसकाल से आगे के काल में और वीतरागस्वसंवेदन की प्रादुर्भूति के पूर्वकाल में जबतक सरागता होती है तबतक जीव को शुद्ध प्रात्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि रागभाव शुद्धात्मसंवित्ति का प्रतिबन्धक होता है। उपशमसम्यक्त्व की उत्पत्ति होते समय सिर्फ सातप्रकृतियों के उदयरूप निमित्त का अभाव अर्थात अनदयरूप निमित्त का सद्भाव होता है। उसीप्रकार शूद्धात्मसंवित्ति के प्रतिबन्धक अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन का तीव्र उदय होता है। इनका उदय होने से शुद्धात्मा के स्वरूपका अनभवजन्य पर्णज्ञान नहीं होता। उससमय आत्मा का जो कुछ ज्ञान होता है वह उसके सिर्फ सामान्यांश का ही होता है-विशेषांश का नहीं वस्तुके सामान्य और विशेष इन दोनों अंशों का ज्ञान होने पर ही वस्तु के स्वरूपका ज्ञान पूर्णरूप से होता है, अन्यथा नहीं। वस्तु के विशेषों का जबतक ज्ञान नहीं होता तबतक ज्ञान के अंशभूत दर्शन और चारित्र अर्थात् आत्मस्वरूप विषयक दढ निश्चय न होने से दर्शन, ज्ञान, चारित्र अंशतः सम्यक और अंशत: मिथ्या होने से निश्चयनय की दृष्टि से मिथ्या ही हैं। यह स्पष्ट हो जाता है। अतः शुद्धात्मसंवित्ति के बाद ही रत्नत्रय को यथार्थता की सिद्धि होती है, उसके पहले नहीं। सारांश, वीतरागरत्नत्रय ही यथार्थ रत्नत्रय है सरागरत्नत्रय नहीं। फिर भले ही वह परम्परा से मोक्ष का कारण बन जाता है । इसका अर्थ यह नहीं समझना चाहिए कि सराग रत्नत्रय के सर्वथा अभाव में भी वीतरागरत्नत्रय की या अभेदरत्नत्रय की प्राप्ति होती है।' ३३१ ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org