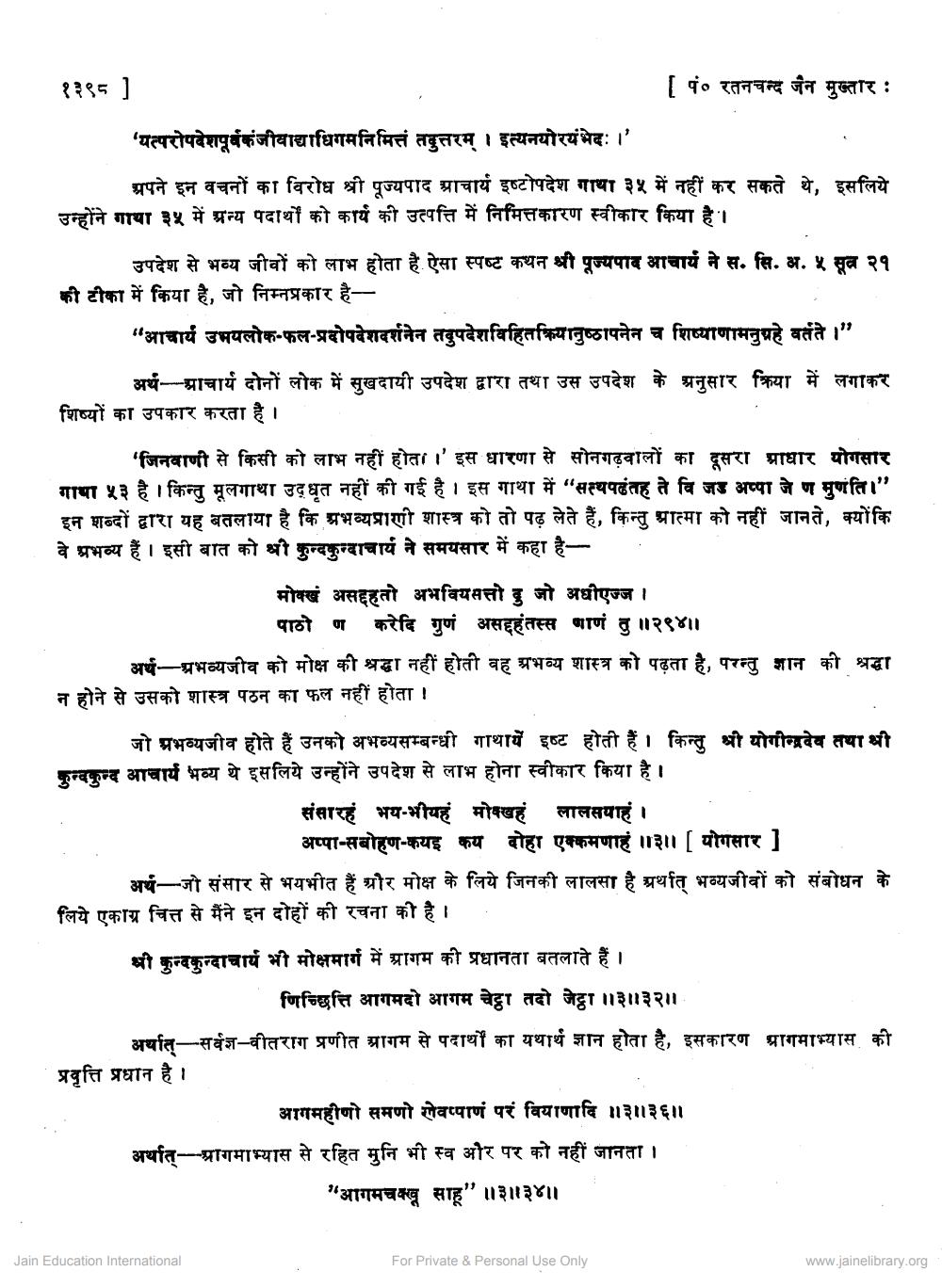________________
१३९८ ]
[ पं० रतनचन्द जैन मुख्तार : 'यत्परोपदेशपूर्वकंजीवाद्याधिगमनिमित्तं तदुत्तरम् । इत्यनयोरयंभेदः ।'
अपने इन वचनों का विरोध श्री पूज्यपाद आचार्य इष्टोपदेश गाथा ३५ में नहीं कर सकते थे, इसलिये उन्होंने गाया ३५ में अन्य पदार्थों को कार्य की उत्पत्ति में निमित्तकारण स्वीकार किया है।
उपदेश से भव्य जीवों को लाभ होता है ऐसा स्पष्ट कथन श्री पूज्यपाद आचार्य ने स. सि. अ. ५ सूत्र २१ की टीका में किया है, जो निम्नप्रकार है
"आचार्य उभयलोक-फल-प्रदोपदेशदर्शनेन तदुपदेशविहितक्रियानुष्ठापनेन च शिष्याणामनुग्रहे वर्तते।"
अर्थ-प्राचार्य दोनों लोक में सुखदायी उपदेश द्वारा तथा उस उपदेश के अनुसार क्रिया में लगाकर शिष्यों का उपकार करता है ।
"जिनवाणी से किसी को लाभ नहीं होता।' इस धारणा से सोनगढ़वालों का दूसरा प्राधार योगसार गाथा ५३ है । किन्तु मूलगाथा उद्धृत नहीं की गई है । इस गाथा में "सत्यपढंतह ते वि जड अप्पा जे ण मुणति।" इन शब्दों द्वारा यह बतलाया है कि अभव्यप्राणी शास्त्र को तो पढ़ लेते हैं, किन्तु प्रात्मा को नहीं जानते, क्योंकि वे अभव्य हैं । इसी बात को श्री कुन्दकुन्दाचार्य ने समयसार में कहा है
मोक्खं असद्दहतो अभवियसत्तो दु जो अधीएज्ज ।
पाठो ण करेदि गुणं असद्दहंतस्स गाणं तु ॥२९४॥ अर्थ-अभव्यजीव को मोक्ष की श्रद्धा नहीं होती वह अभव्य शास्त्र को पढ़ता है, परन्तु शान की श्रद्धा न होने से उसको शास्त्र पठन का फल नहीं होता।
जो प्रभव्यजीव होते हैं उनको अभव्यसम्बन्धी गाथायें इष्ट होती हैं। किन्तु श्री योगीन्द्रदेव तथा श्री कुन्दकुन्द आचार्य भव्य थे इसलिये उन्होंने उपदेश से लाभ होना स्वीकार किया है।
संसारहं भय-भीयहं मोक्खहं लालसयाहं।
अप्पा-सबोहण-कयइ कय दोहा एक्कमणाहं ॥३॥ [ योगसार ] अर्थ-जो संसार से भयभीत हैं और मोक्ष के लिये जिनकी लालसा है अर्थात् भव्यजीवों को संबोधन के लिये एकाग्र चित्त से मैंने इन दोहों की रचना की है। श्री कुन्दकुन्दाचार्य भी मोक्षमार्ग में प्रागम की प्रधानता बतलाते हैं ।
___णिच्छित्ति आगमदो आगम चेट्ठा तदो जेट्ठा ॥३॥३२॥ अर्थात्-सर्वज्ञ-वीतराग प्रणीत आगम से पदार्थों का यथार्थ ज्ञान होता है, इसकारण प्रागमाभ्यास की प्रवृत्ति प्रधान है।
आगमहीणो समणो णेवप्पाणं परं वियाणादि ॥३॥३६॥ अर्थात्-पागमाभ्यास से रहित मुनि भी स्व और पर को नहीं जानता।
"आगमचक्खू साहू" ॥३॥३४॥
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org