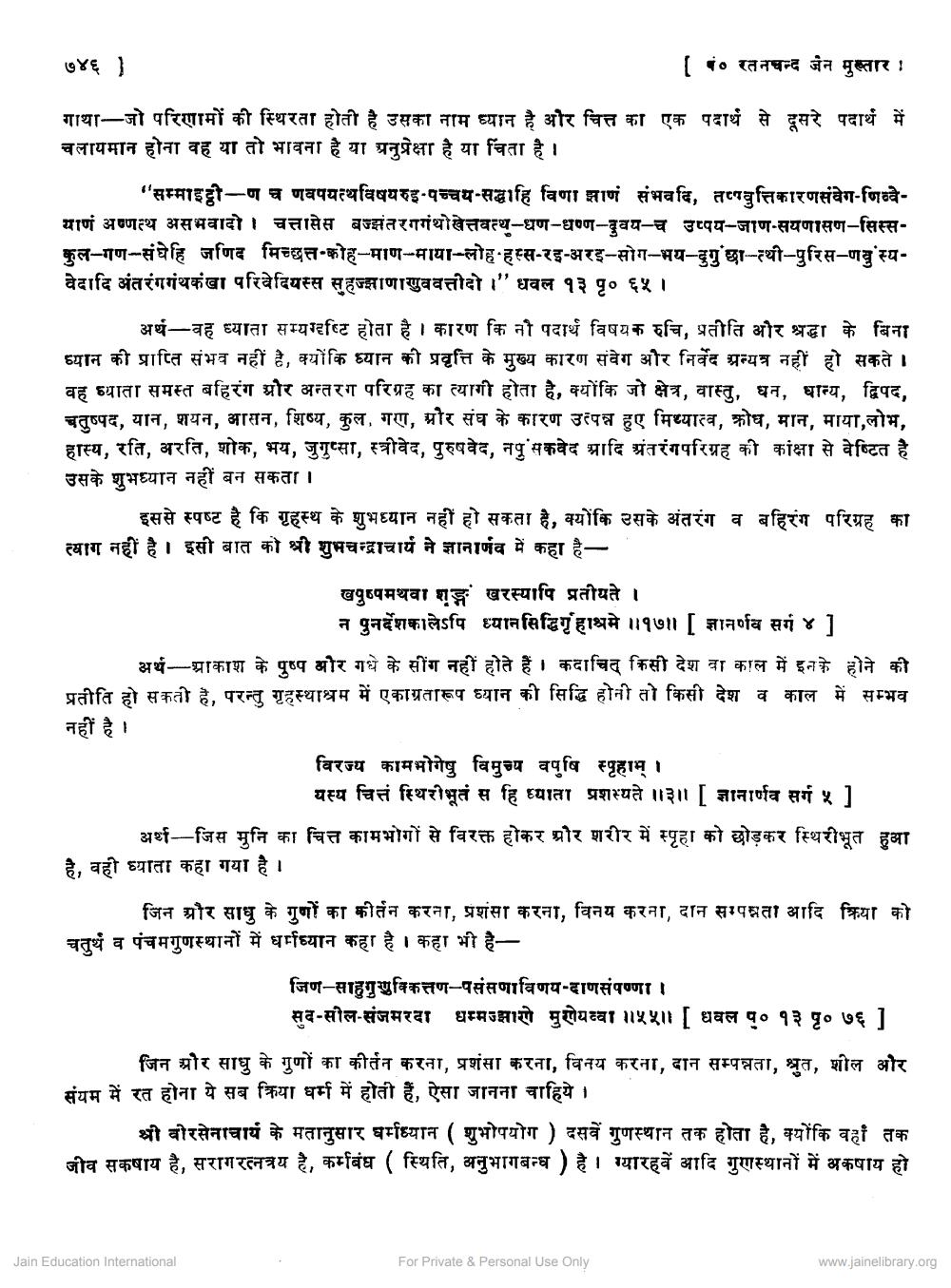________________
७४६ }
[ पं० रतनचन्द जैन मुख्तार ! गाथा - जो परिणामों की स्थिरता होती है उसका नाम ध्यान है और चित्त का एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में चलायमान होना वह या तो भावना है या अनुप्रेक्षा है या चिंता है ।
" सम्माइट्ठी - ण च णवपयत्यविषय रुइ-पच्चय-सद्धाहि विणा झाणं संभवदि, तवृत्तिकारणसंवेग- णिब्वेया अण्णत्थ असभवादो । चत्तासेस बज्झतरगगंथो खेत्तवत्थु - धन - धण्ण-वय-च उप्पय- जाण सयणासण- सिस्सकुल - गण - संघेहि जणिद मिच्छत्त कोह-माण - माया - लोह · हस्स रइ अरइ- सोग-भय-दुगु छा-त्थी - पुरिस - णस्यवेदादि अंतरंगगंथखा परिवेदियस्स सुहज्झाणाणुववत्तोदो ।" धवल १३ पृ० ६५ ।
अर्थ - वह ध्याता सम्यग्दृष्टि होता है । कारण कि तो पदार्थ विषयक रुचि प्रतीति और श्रद्धा के बिना ध्यान की प्राप्ति संभव नहीं है, क्योंकि ध्यान की प्रवृत्ति के मुख्य कारण संवेग और निर्वेद अन्यत्र नहीं हो सकते । वह ध्याता समस्त बहिरंग और अन्तरंग परिग्रह का त्यागी होता है, क्योंकि जो क्षेत्र, वास्तु, धन, धान्य, द्विपद, चतुष्पद, यान, शयन, आसन, शिष्य, कुल, गरण, और संघ के कारण उत्पन्न हुए मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद आदि अंतरंगपरिग्रह की कक्षा से वेष्टित है उसके शुभध्यान नहीं बन सकता ।
इससे स्पष्ट है कि गृहस्थ के शुभध्यान नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके अंतरंग व बहिरंग परिग्रह का त्याग नहीं है । इसी बात को श्री शुभचन्द्राचार्य ने ज्ञानार्णव में कहा है
खपुष्पमथवा शृङ्गः खरस्यापि प्रतीयते ।
न पुनर्देशकालेsपि ध्यान सिद्धिगृहाश्रमे ॥१७॥ [ ज्ञानर्णव सर्ग ४ ]
अर्थ - श्राकाश के पुष्प और गधे के सींग नहीं होते हैं । कदाचित् किसी देश वा काल में इनके होने की प्रतीति हो सकती है, परन्तु गृहस्थाश्रम में एकाग्रतारूप ध्यान की सिद्धि होनी तो किसी देश व काल में सम्भव नहीं है ।
विरज्य कामभोगेषु विमुच्य वपुषि स्पृहाम् ।
यस्य चित्तं स्थिरीभूतं स हि ध्याता प्रशस्यते ॥ ३॥ [ ज्ञानार्णव सर्ग ५ ]
अर्थ - जिस मुनि का चित्त कामभोगों से विरक्त होकर और शरीर में स्पृहा को छोड़कर स्थिरीभूत हुआ है, वही ध्याता कहा गया है ।
जिन और साधु के गुणों का कीर्तन करना, प्रशंसा करना, विनय करना, दान सम्पन्नता आदि क्रिया को चतुर्थं व पंचमगुणस्थानों में धर्मध्यान कहा है । कहा भी है
Jain Education International
जिण - साहुगुणुवित्तण-पसंसणाविणय- दाणसंपण्णा ।
सुव- सील- संजमरदा धम्मज्झारो मुलेयव्वा ॥५५॥ [ धवल ० १३ पृ० ७६ ]
जिन और साधु के गुणों का कीर्तन करना, प्रशंसा करना, विनय करना, दान सम्पन्नता, श्रुत, शील और संयम में रत होना ये सब क्रिया धर्म में होती हैं, ऐसा जानना चाहिये ।
श्री वीरसेनाचार्य के मतानुसार धर्मध्यान ( शुभोपयोग ) दसवें गुणस्थान तक होता है, क्योंकि वहाँ तक जीव सकषाय है, सराग रत्नत्रय है, कर्मबंध ( स्थिति, अनुभागबन्ध ) है । ग्यारहवें आदि गुणस्थानों में अकषाय हो
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org