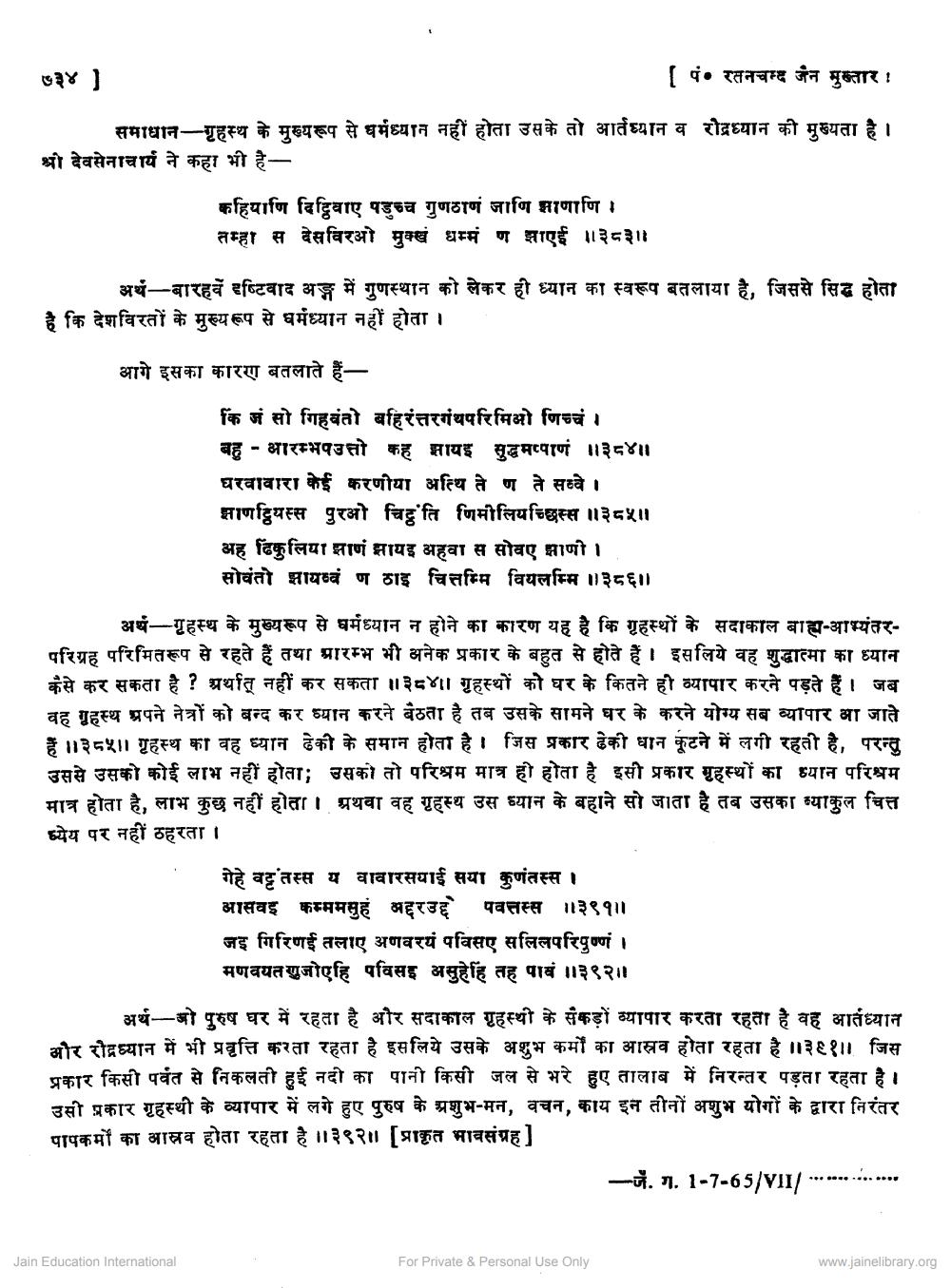________________
७३४ ]
समाधान-गृहस्थ के मुख्यरूप
श्री देवसेनाचार्य ने कहा भी है
[ पं० रतनचन्द जैन मुख्तार !
से धर्मध्यान नहीं होता उसके तो आर्तध्यान व रौद्रध्यान की मुख्यता है ।
कहियाणि दिट्टिवाए पडुच्च गुणठाणं जाणि झाणाणि । तम्हा स देसविरओ मुक्खं धम्मं ण झाई ॥ ३८३ ॥
अर्थ - बारहवें दृष्टिवाद अङ्ग में गुणस्थान को लेकर ही ध्यान का स्वरूप बतलाया है, जिससे सिद्ध होता है कि देश विरतों के मुख्यरूप से घमंध्यान नहीं होता ।
आगे इसका कारण बतलाते हैं
Jain Education International
कि जं सो गिवंतो बहिरंत्तरगंथपरिमिओ णिच्चं । बहु - आरम्भपउतो कह झाय सुद्धमप्पाणं ॥ ३८४ ॥ घरवावारा केई करणीया अत्थि ते ण ते सब्वे । झाट्रियस्स पुरओ चिट्ठति णिमीलियच्छिस्स ॥ ३८५ ॥ अह टिकुलिया झाणं झायइ अहवा स सोवए झाणी | सोवंतो झायब्वं ण ठाइ चित्तम्मि वियलम्मि ॥ ३८६ ॥
अर्थ – गृहस्थ के मुख्यरूप से धर्मध्यान न होने का कारण यह है कि गृहस्थों के सदाकाल बाह्य आभ्यंतरपरिग्रह परिमितरूप से रहते हैं तथा प्रारम्भ भी अनेक प्रकार के बहुत से होते हैं । इसलिये वह शुद्धात्मा का ध्यान कैसे कर सकता है ? अर्थात् नहीं कर सकता ॥ ३८४ ॥ गृहस्थों को घर के कितने ही व्यापार करने पड़ते हैं । जब वह गृहस्थ अपने नेत्रों को बन्द कर ध्यान करने बैठता है तब उसके सामने घर के करने योग्य सब व्यापार आ जाते हैं ।।३८५।। गृहस्थ का वह ध्यान ढेकी के समान होता है। जिस प्रकार ढेकी धान कूटने में लगी रहती है, परन्तु उससे उसको कोई लाभ नहीं होता; उसको तो परिश्रम मात्र ही होता है इसी प्रकार गृहस्थों का ध्यान परिश्रम मात्र होता है, लाभ कुछ नहीं होता । श्रथवा वह गृहस्थ उस ध्यान के बहाने सो जाता है तब उसका ब्याकुल चित्त ध्येय पर नहीं ठहरता ।
गेहे व तस् य वावारसयाई सया कुणंतस्स । आसवई कम्ममसुहं अद्दरउद्द पवत्तस्स ॥३९१ ॥ जई गिरिणई तलाए अणवरयं पविसए सलिलपरिपुष्णं । मणवयत जोएहि पविसद्द असुहेहि तह पावं ॥ ३९२ ॥
अर्थ- जो पुरुष घर में रहता है और सदाकाल गृहस्थी के सैकड़ों व्यापार करता रहता है वह आर्तध्यान और रौद्रध्यान में भी प्रवृत्ति करता रहता है इसलिये उसके अशुभ कर्मों का आस्रव होता रहता है || ३६१ ॥ जिस प्रकार किसी पर्वत से निकलती हुई नदी का पानी किसी जल से भरे हुए तालाब में निरन्तर पड़ता रहता है । उसी प्रकार गृहस्थी के व्यापार में लगे हुए पुरुष के अशुभ- मन, वचन, काय इन तीनों अशुभ योगों के द्वारा निरंतर पापकर्मों का आस्रव होता रहता है ।। ३९२॥ [ प्राकृत भावसंग्रह ]
For Private & Personal Use Only
- जै. ग. 1-7-65/ VII /
*******........
www.jainelibrary.org