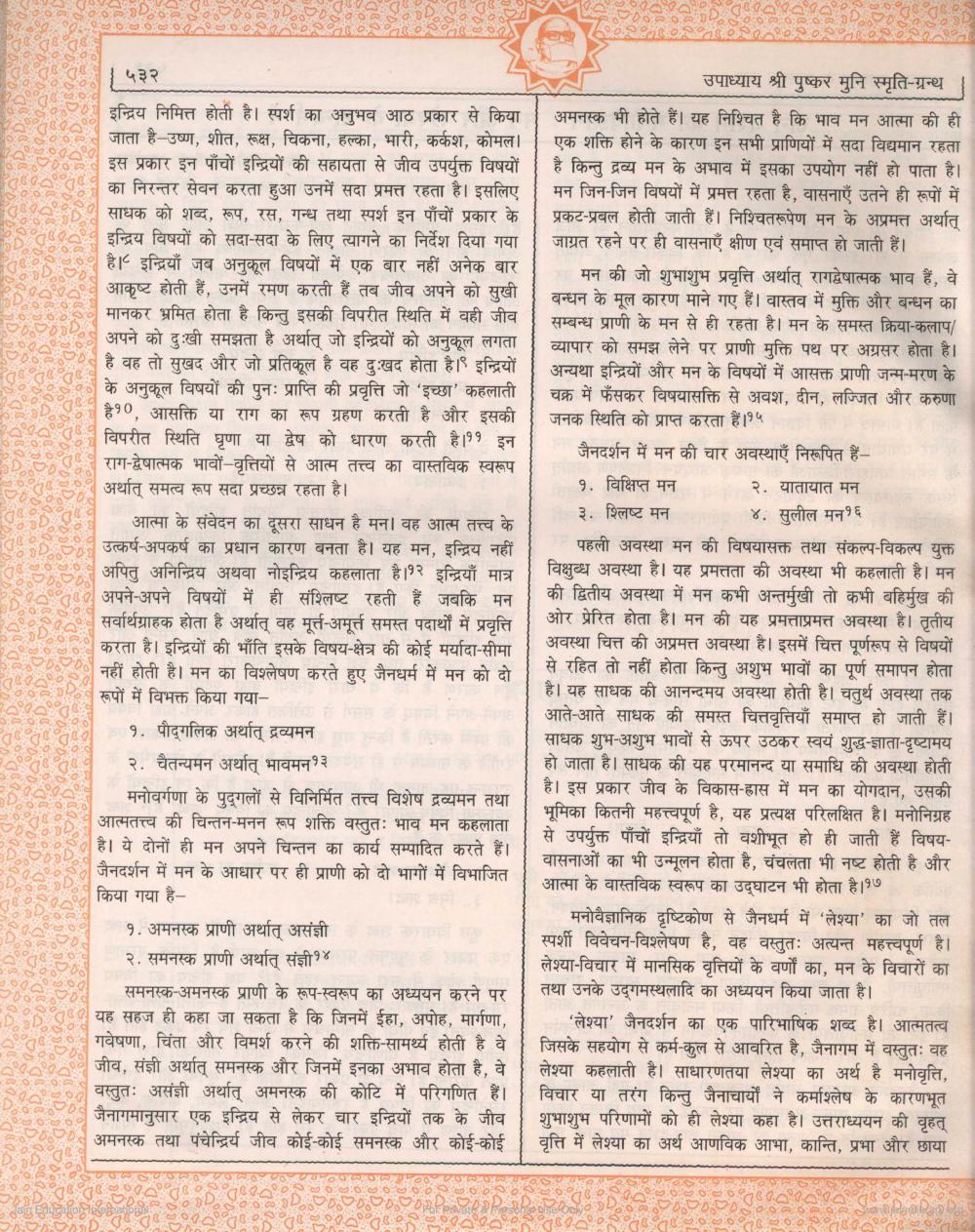________________
TRO8999.00000000000DPaar
00000000000000Ratopati
HORORD
1 ५३२
उपाध्याय श्री पुष्कर मुनि स्मृति-ग्रन्थ इन्द्रिय निमित्त होती है। स्पर्श का अनुभव आठ प्रकार से किया । अमनस्क भी होते हैं। यह निश्चित है कि भाव मन आत्मा की ही जाता है-उष्ण, शीत, रूक्ष, चिकना, हल्का, भारी, कर्कश, कोमल।। एक शक्ति होने के कारण इन सभी प्राणियों में सदा विद्यमान रहता इस प्रकार इन पाँचों इन्द्रियों की सहायता से जीव उपर्युक्त विषयों है किन्तु द्रव्य मन के अभाव में इसका उपयोग नहीं हो पाता है। का निरन्तर सेवन करता हुआ उनमें सदा प्रमत्त रहता है। इसलिए । मन जिन-जिन विषयों में प्रमत्त रहता है, वासनाएँ उतने ही रूपों में साधक को शब्द, रूप, रस, गन्ध तथा स्पर्श इन पाँचों प्रकार के प्रकट-प्रबल होती जाती हैं। निश्चितरूपेण मन के अप्रमत्त अर्थात् इन्द्रिय विषयों को सदा-सदा के लिए त्यागने का निर्देश दिया गया । जाग्रत रहने पर ही वासनाएँ क्षीण एवं समाप्त हो जाती हैं। है।८ इन्द्रियाँ जब अनुकूल विषयों में एक बार नहीं अनेक बार
मन की जो शुभाशुभ प्रवृत्ति अर्थात् रागद्वेषात्मक भाव हैं, वे आकृष्ट होती हैं, उनमें रमण करती हैं तब जीव अपने को सुखी
बन्धन के मूल कारण माने गए हैं। वास्तव में मुक्ति और बन्धन का मानकर भ्रमित होता है किन्तु इसकी विपरीत स्थिति में वही जीव । सम्बन्ध प्राणी के मन से ही रहता है। मन के समस्त क्रिया-कलाप/ अपने को दुःखी समझता है अर्थात् जो इन्द्रियों को अनुकूल लगता व्यापार को समझ लेने पर प्राणी मुक्ति पथ पर अग्रसर होता है। है वह तो सुखद और जो प्रतिकूल है वह दुःखद होता है। इन्द्रियों अन्यथा इन्द्रियों और मन के विषयों में आसक्त प्राणी जन्म-मरण के के अनुकूल विषयों की पुनः प्राप्ति की प्रवृत्ति जो 'इच्छा' कहलाती चक्र में फँसकर विषयासक्ति से अवश, दीन, लज्जित और करुणा है१०, आसक्ति या राग का रूप ग्रहण करती है और इसकी । जनक स्थिति को प्राप्त करता हैं।१५ विपरीत स्थिति घृणा या द्वेष को धारण करती है।११ इन
जैनदर्शन में मन की चार अवस्थाएँ निरूपित हैंराग-द्वेषात्मक भावों-वृत्तियों से आत्म तत्त्व का वास्तविक स्वरूप अर्थात् समत्व रूप सदा प्रच्छन्न रहता है।
१. विक्षिप्त मन२. यातायात मन
३. श्लिष्ट मन आत्मा के संवेदन का दूसरा साधन है मन। वह आत्म तत्त्व के ।
४. सुलील मन१६ उत्कर्ष-अपकर्ष का प्रधान कारण बनता है। यह मन, इन्द्रिय नहीं
पहली अवस्था मन की विषयासक्त तथा संकल्प-विकल्प युक्त अपितु अनिन्द्रिय अथवा नोइन्द्रिय कहलाता है।१२ इन्द्रियाँ मात्र ।
विक्षुब्ध अवस्था है। यह प्रमत्तता की अवस्था भी कहलाती है। मन अपने-अपने विषयों में ही संश्लिष्ट रहती हैं जबकि मन
की द्वितीय अवस्था में मन कभी अन्तर्मुखी तो कभी बहिर्मुख की सर्वार्थग्राहक होता है अर्थात् वह मूर्त-अमूर्त समस्त पदार्थों में प्रवृत्ति
ओर प्रेरित होता है। मन की यह प्रमत्ताप्रमत्त अवस्था है। तृतीय करता है। इन्द्रियों की भाँति इसके विषय-क्षेत्र की कोई मर्यादा-सीमा
अवस्था चित्त की अप्रमत्त अवस्था है। इसमें चित्त पूर्णरूप से विषयों नहीं होती है। मन का विश्लेषण करते हुए जैनधर्म में मन को दो
से रहित तो नहीं होता किन्तु अशुभ भावों का पूर्ण समापन होता रूपों में विभक्त किया गया
है। यह साधक की आनन्दमय अवस्था होती है। चतुर्थ अवस्था तक
आते-आते साधक की समस्त चित्तवृत्तियाँ समाप्त हो जाती हैं। १. पीद्गलिक अर्थात् द्रव्यमन
साधक शुभ-अशुभ भावों से ऊपर उठकर स्वयं शुद्ध-ज्ञाता-दृष्टामय २. चैतन्यमन अर्थात् भावमन१३
हो जाता है। साधक की यह परमानन्द या समाधि की अवस्था होती
है। इस प्रकार जीव के विकास-हास में मन का योगदान, उसकी मनोवर्गणा के पुद्गलों से विनिर्मित तत्त्व विशेष द्रव्यमन तथा
भूमिका कितनी महत्त्वपूर्ण है, यह प्रत्यक्ष परिलक्षित है। मनोनिग्रह आत्मतत्त्व की चिन्तन-मनन रूप शक्ति वस्तुतः भाव मन कहलाता
से उपर्युक्त पाँचों इन्द्रियाँ तो वशीभूत हो ही जाती हैं विषयहै। ये दोनों ही मन अपने चिन्तन का कार्य सम्पादित करते हैं।
वासनाओं का भी उन्मूलन होता है, चंचलता भी नष्ट होती है और जैनदर्शन में मन के आधार पर ही प्राणी को दो भागों में विभाजित
आत्मा के वास्तविक स्वरूप का उद्घाटन भी होता है।१७ । किया गया है
मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से जैनधर्म में 'लेश्या' का जो तल १. अमनस्क प्राणी अर्थात् असंज्ञी
स्पर्शी विवेचन-विश्लेषण है, वह वस्तुतः अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। २. समनस्क प्राणी अर्थात् संज्ञी१४
लेश्या-विचार में मानसिक वृत्तियों के वर्गों का, मन के विचारों का समनस्क-अमनस्क प्राणी के रूप-स्वरूप का अध्ययन करने पर तथा उनके उद्गमस्थलादि का अध्ययन किया जाता है। यह सहज ही कहा जा सकता है कि जिनमें ईहा, अपोह, मार्गणा, _'लेश्या' जैनदर्शन का एक पारिभाषिक शब्द है। आत्मतत्व गवेषणा, चिंता और विमर्श करने की शक्ति-सामर्थ्य होती है वे जिसके सहयोग से कर्म-कुल से आवरित है, जैनागम में वस्तुतः वह जीव, संज्ञी अर्थात् समनस्क और जिनमें इनका अभाव होता है, वे / लेश्या कहलाती है। साधारणतया लेश्या का अर्थ है मनोवृत्ति, वस्तुतः असंज्ञी अर्थात् अमनस्क की कोटि में परिगणित हैं। विचार या तरंग किन्तु जैनाचार्यों ने कर्माश्लेष के कारणभूत जैनागमानुसार एक इन्द्रिय से लेकर चार इन्द्रियों तक के जीव शुभाशुभ परिणामों को ही लेश्या कहा है। उत्तराध्ययन की वृहत् अमनस्क तथा पंचेन्द्रिय जीव कोई-कोई समनस्क और कोई-कोई वृत्ति में लेश्या का अर्थ आणविक आभा, कान्ति, प्रभा और छाया
390
यापन
प
5:00:00:00:0ANDAVDO
100%
060
3-06-D
26-C