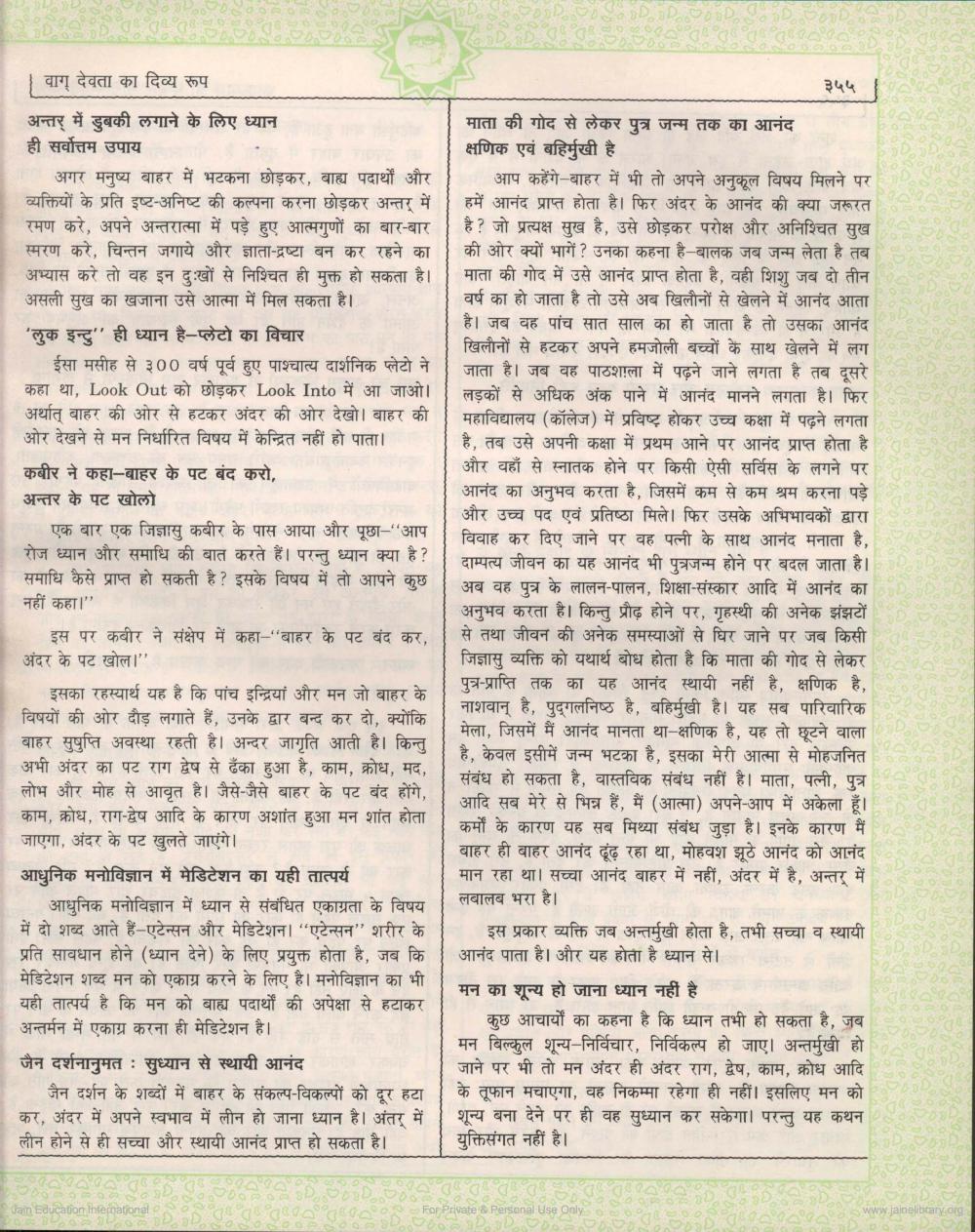________________
वाग देवता का दिव्य रूप
अन्तर में डुबकी लगाने के लिए ध्यान ही सर्वोत्तम उपाय
अगर मनुष्य बाहर में भटकना छोड़कर, बाह्य पदार्थों और व्यक्तियों के प्रति इष्ट-अनिष्ट की कल्पना करना छोड़कर अन्तर में रमण करे, अपने अन्तरात्मा में पड़े हुए आत्मगुणों का बार-बार स्मरण करे, चिन्तन जगाये और ज्ञाता द्रष्टा बन कर रहने का अभ्यास करे तो वह इन दुःखों से निश्चित ही मुक्त हो सकता है। असली सुख का खजाना उसे आत्मा में मिल सकता है। 'लुक इन्टु" ही ध्यान है-प्लेटो का विचार
ईसा मसीह से ३०० वर्ष पूर्व हुए पाश्चात्य दार्शनिक प्लेटो ने कहा था, Look Out को छोड़कर Look Into में आ जाओ। अर्थात् बाहर की ओर से हटकर अंदर की ओर देखो। बाहर की ओर देखने से मन निर्धारित विषय में केन्द्रित नहीं हो पाता।
कबीर ने कहा- बाहर के पट बंद करो, अन्तर के पट खोलो
एक बार एक जिज्ञासु कबीर के पास आया और पूछा - "आप रोज ध्यान और समाधि की बात करते हैं। परन्तु ध्यान क्या है ? समाधि कैसे प्राप्त हो सकती है ? इसके विषय में तो आपने कुछ नहीं कहा।"
इस पर कबीर ने संक्षेप में कहा- "बाहर के पट बंद कर, अंदर के पट खोल ।"
इसका रहस्यार्थ यह है कि पांच इन्द्रियां और मन जो बाहर के विषयों की ओर दौड़ लगाते हैं, उनके द्वार बन्द कर दो, क्योंकि बाहर सुषुप्ति अवस्था रहती है। अन्दर जागृति आती है। किन्तु अभी अंदर का पट राग द्वेष से ढँका हुआ है, काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह से आवृत है। जैसे-जैसे बाहर के पट बंद होंगे, काम, क्रोध, राग-द्वेष आदि के कारण अशांत हुआ मन शांत होता जाएगा, अंदर के पट खुलते जाएंगे।
आधुनिक मनोविज्ञान में मेडिटेशन का यही तात्पर्य
आधुनिक मनोविज्ञान में ध्यान से संबंधित एकाग्रता के विषय में दो शब्द आते हैं- एटेन्सन और मेडिटेशन। “एटेन्सन" शरीर के प्रति सावधान होने (ध्यान देने) के लिए प्रयुक्त होता है, जब कि मेडिटेशन शब्द मन को एकाग्र करने के लिए है। मनोविज्ञान का भी यही तात्पर्य है कि मन को बाह्य पदार्थों की अपेक्षा से हटाकर अन्तर्मन में एकाग्र करना ही मेडिटेशन है।
जैन दर्शनानुमत: सुध्यान से स्थायी आनंद
जैन दर्शन के शब्दों में बाहर के संकल्प-विकल्पों को दूर हटा कर, अंदर में अपने स्वभाव में लीन हो जाना ध्यान है। अंतर् में लीन होने से ही सच्चा और स्थायी आनंद प्राप्त हो सकता है।
Jan Education International
माता की गोद से लेकर पुत्र जन्म तक का आनंद क्षणिक एवं बहिर्मुखी है
३५५
आप कहेंगे-बाहर में भी तो अपने अनुकूल विषय मिलने पर हमें आनंद प्राप्त होता है। फिर अंदर के आनंद की क्या जरूरत है ? जो प्रत्यक्ष सुख है, उसे छोड़कर परोक्ष और अनिश्चित सुख की ओर क्यों भागें ? उनका कहना है-बालक जब जन्म लेता है तब माता की गोद में उसे आनंद प्राप्त होता है, वही शिशु जब दो तीन वर्ष का हो जाता है तो उसे अब खिलौनों से खेलने में आनंद आता है। जब वह पांच सात साल का हो जाता है तो उसका आनंद खिलौनों से हटकर अपने हमजोली बच्चों के साथ खेलने में लग जाता है। जब वह पाठशाला में पढ़ने जाने लगता है तब दूसरे लड़कों से अधिक अंक पाने में आनंद मानने लगता है। फिर महाविद्यालय (कॉलेज) में प्रविष्ट होकर उच्च कक्षा में पढ़ने लगता है, तब उसे अपनी कक्षा में प्रथम आने पर आनंद प्राप्त होता है। और वहाँ से स्नातक होने पर किसी ऐसी सर्विस के लगने पर आनंद का अनुभव करता है, जिसमें कम से कम श्रम करना पड़े और उच्च पद एवं प्रतिष्ठा मिले। फिर उसके अभिभावकों द्वारा विवाह कर दिए जाने पर वह पत्नी के साथ आनंद मनाता है, दाम्पत्य जीवन का यह आनंद भी पुत्रजन्म होने पर बदल जाता है। अब वह पुत्र के लालन-पालन, शिक्षा-संस्कार आदि में आनंद का अनुभव करता है। किन्तु प्रौढ़ होने पर गृहस्थी की अनेक झंझटों से तथा जीवन की अनेक समस्याओं से घिर जाने पर जब किसी जिज्ञासु व्यक्ति को यथार्थ बोध होता है कि माता की गोद से लेकर पुत्र-प्राप्ति तक का यह आनंद स्थायी नहीं है, क्षणिक है, नाशवान् है, पुद्गलनिष्ठ है, बहिर्मुखी है यह सब पारिवारिक मेला, जिसमें मैं आनंद मानता था क्षणिक है, यह तो छूटने वाला है केवल इसीमें जन्म भटका है, इसका मेरी आत्मा से मोहजनित संबंध हो सकता है, वास्तविक संबंध नहीं है। माता, पत्नी, पुत्र आदि सब मेरे से भिन्न हैं, मैं (आत्मा) अपने-आप में अकेला हूँ। कर्मों के कारण यह सब मिथ्या संबंध जुड़ा है। इनके कारण मैं बाहर ही बाहर आनंद ढूंढ़ रहा था, मोहवश झूठे आनंद को आनंद मान रहा था। सच्चा आनंद बाहर में नहीं, अंदर में है, अन्तर् में लबालब भरा है।
इस प्रकार व्यक्ति जय अन्तर्मुखी होता है, तभी सच्चा व स्थायी आनंद पाता है। और यह होता है ध्यान से।
मन का शून्य हो जाना ध्यान नहीं है
जब
कुछ आचार्यों का कहना है कि ध्यान तभी हो सकता है, मन बिल्कुल शून्य- निर्विचार, निर्विकल्प हो जाए। अन्तर्मुखी हो जाने पर भी तो मन अंदर ही अंदर राग, द्वेष, काम, क्रोध आदि के तूफान मचाएगा, वह निकम्मा रहेगा ही नहीं। इसलिए मन को शून्य बना देने पर ही वह सुध्यान कर सकेगा। परन्तु यह कथन युक्तिसंगत नहीं है।
For Private & Personal Use Only DDOA
www.jainelibrary.org