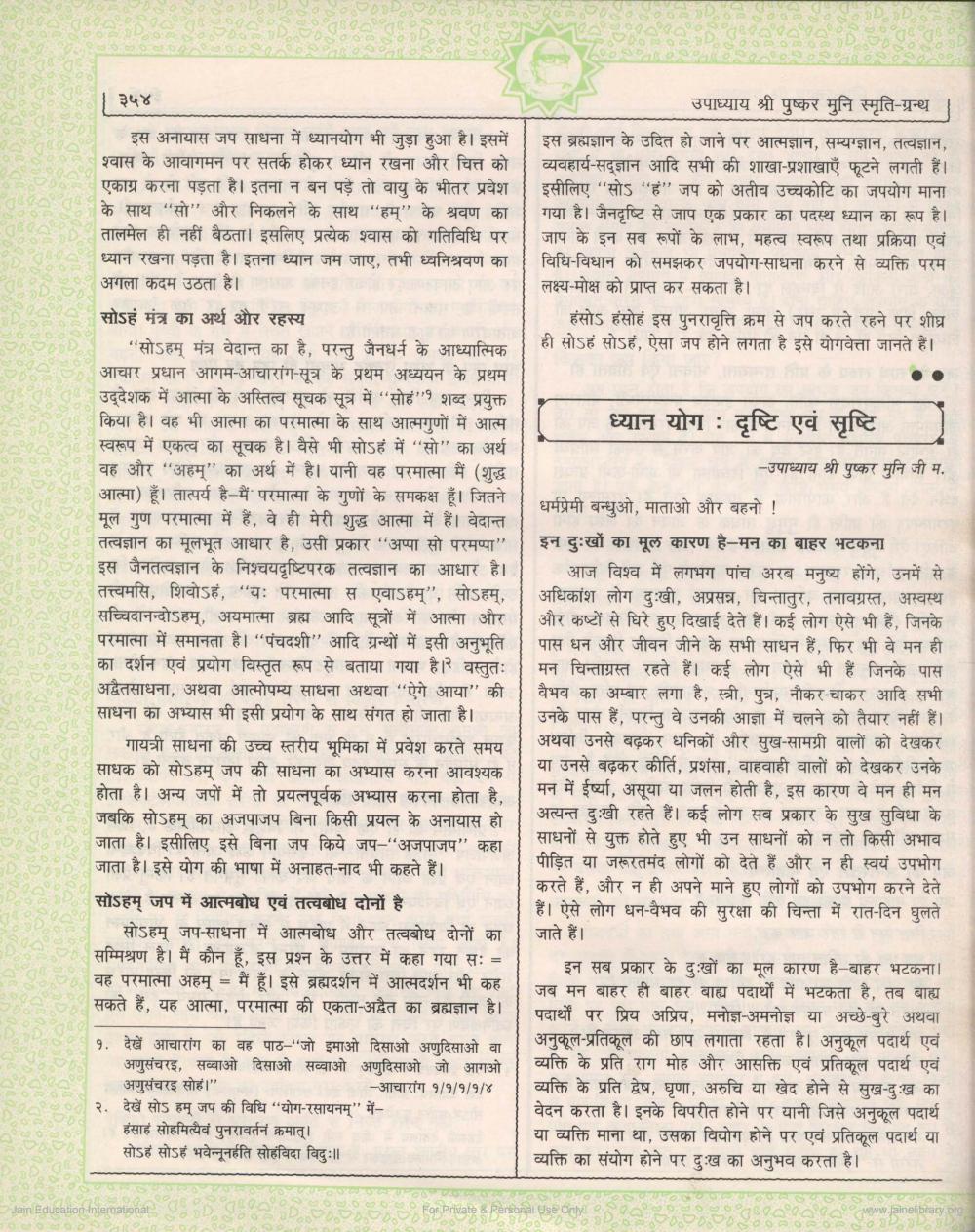________________
३५४
इस अनायास जप साधना में ध्यानयोग भी जुड़ा हुआ है। इसमें श्वास के आवागमन पर सतर्क होकर ध्यान रखना और चित्त को एकाग्र करना पड़ता है। इतना न बन पड़े तो वायु के भीतर प्रवेश के साथ "सो" और निकलने के साथ "हम्" के श्रवण का तालमेल ही नहीं बैठता। इसलिए प्रत्येक श्वास की गतिविधि पर ध्यान रखना पड़ता है। इतना ध्यान जम जाए, तभी ध्वनिश्रवण का अगला कदम उठता है।
सोऽहं मंत्र का अर्थ और रहस्य
"सोऽहम् मंत्र वेदान्त का है, परन्तु जैनधर्न के आध्यात्मिक आचार प्रधान आगम- आचारांग सूत्र के प्रथम अध्ययन के प्रथम उद्देशक में आत्मा के अस्तित्व सूचक सूत्र में "सोहं शब्द प्रयुक्त किया है। वह भी आत्मा का परमात्मा के साथ आत्मगुणों में आत्म स्वरूप में एकत्व का सूचक है। वैसे भी सोऽहं में "सो" का अर्थ यह और "अहम्" का अर्थ में है। यानी यह परमात्मा में (शुद्ध आत्मा) हूँ। तात्पर्य है- मैं परमात्मा के गुणों के समकक्ष हूँ। जितने मूल गुण परमात्मा में हैं, वे ही मेरी शुद्ध आत्मा में हैं। वेदान्त तत्वज्ञान का मूलभूत आधार है, उसी प्रकार "अप्पा सो परमप्पा" इस जैनतत्वज्ञान के निश्चयदृष्टिपरक तत्वज्ञान का आधार है। तत्त्वमसि शिवोऽहं यः परमात्मा स एवाऽहम् सोऽहम् सच्चिदानन्दोऽहम्, अयमात्मा ब्रह्म आदि सूत्रों में आत्मा और परमात्मा में समानता है "पंचदशी" आदि ग्रन्थों में इसी अनुभूति का दर्शन एवं प्रयोग विस्तृत रूप से बताया गया है। वस्तुतः अद्वैतसाधना, अथवा आत्मोपम्य साधना अथवा "ऐगे आया" की साधना का अभ्यास भी इसी प्रयोग के साथ संगत हो जाता है।
3
गायत्री साधना की उच्च स्तरीय भूमिका में प्रवेश करते समय साधक को सोऽहम् जप की साधना का अभ्यास करना आवश्यक होता है अन्य जपों में तो प्रयत्नपूर्वक अभ्यास करना होता है, जबकि सोऽहम् का अजपाजप बिना किसी प्रयत्न के अनायास हो जाता है। इसीलिए इसे बिना जप किये जप- "अजपाजप" कहा जाता है। इसे योग की भाषा में अनाहत नाद भी कहते हैं।
सोऽहम् जप में आत्मबोध एवं तत्वबोध दोनों है
सोऽहम् जप साधना में आत्मबोध और तत्वबोध दोनों का सम्मिश्रण है। मैं कौन हूँ, इस प्रश्न के उत्तर में कहा गया सः वह परमात्मा अहम् = मैं हूँ। इसे ब्रह्मदर्शन में आत्मदर्शन भी कह सकते हैं, यह आत्मा, परमात्मा की एकता-अद्वैत का ब्रह्मज्ञान है।
१. देखें आचारांग का वह पाठ "जो इमाओ दिसाओ अणुदिसाओ वा अणुसंचरइ, सव्वाओ दिसाओ सव्वाओ अणुदिसाओ जो आगओ अणुसंचरइ सोहं ।" - आचारांग १/१/१/१/४
२. देखें सोऽहम् जप की विधि “योग रसायनम्" मेंहंसाहं सोहमित्यैवं पुनरावर्तनं क्रमात्।
सोऽहं सोऽहं भवेन्नूनर्हति सोहंविदा विदुः ॥
Jain Education International
उपाध्याय श्री पुष्कर मुनि स्मृति ग्रन्थ
इस ब्रह्मज्ञान के उदित हो जाने पर आत्मज्ञान, सम्यग्ज्ञान, तत्वज्ञान, व्यवहार्य सज्ञान आदि सभी की शाखा प्रशाखाएँ फूटने लगती हैं। इसीलिए "सोऽ "हं" जप को अतीव उच्चकोटि का जपयोग माना गया है। जैनदृष्टि से जाप एक प्रकार का पदस्थ ध्यान का रूप है। जाप के इन सब रूपों के लाभ, महत्व स्वरूप तथा प्रक्रिया एवं विधि-विधान को समझकर जपयोग-साधना करने से व्यक्ति परम लक्ष्य-मोक्ष को प्राप्त कर सकता है।
हंसो हंसोहं इस पुनरावृत्ति क्रम से जप करते रहने पर शीघ्र ही सोऽहं सोऽहं, ऐसा जप होने लगता है इसे योगवेत्ता जानते हैं।
ध्यान योग : दृष्टि एवं सृष्टि
-उपाध्याय श्री पुष्कर मुनि जी म.
धर्मप्रेमी बन्धुओ, माताओ और बहनो !
इन दुःखों का मूल कारण है-मन का बाहर भटकना
आज विश्व में लगभग पांच अरब मनुष्य होंगे, उनमें से अधिकांश लोग दुःखी, अप्रसन्न, चिन्तातुर तनावग्रस्त, अस्वस्थ और कष्टों से घिरे हुए दिखाई देते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं, जिनके पास धन और जीवन जीने के सभी साधन हैं, फिर भी वे मन ही मन चिन्ताग्रस्त रहते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जिनके पास वैभव का अम्बार लगा है, स्त्री, पुत्र, नौकर-चाकर आदि सभी उनके पास हैं, परन्तु वे उनकी आज्ञा में चलने को तैयार नहीं हैं। अथवा उनसे बढ़कर धनिकों और सुख-सामग्री वालों को देखकर या उनसे बढ़कर कीर्ति, प्रशंसा, वाहवाही वालों को देखकर उनके मन में ईर्ष्या, असूया या जलन होती है, इस कारण वे मन ही मन अत्यन्त दुःखी रहते हैं। कई लोग सब प्रकार के सुख सुविधा के साधनों से युक्त होते हुए भी उन साधनों को न तो किसी अभाव पीड़ित या जरूरतमंद लोगों को देते हैं और न ही स्वयं उपभोग करते हैं, और न ही अपने माने हुए लोगों को उपभोग करने देते हैं ऐसे लोग धन-वैभव की सुरक्षा की चिन्ता में रात-दिन घुलते जाते हैं।
For Private & Personal Use Only!
इन सब प्रकार के दुःखों का मूल कारण है-बाहर भटकना । जब मन बाहर ही बाहर बाह्य पदार्थों में भटकता है, तब बाह्य पदार्थों पर प्रिय अप्रिय, मनोज्ञ-अमनोज्ञ या अच्छे-बुरे अथवा अनुकूल-प्रतिकूल की छाप लगाता रहता है। अनुकूल पदार्थ एवं व्यक्ति के प्रति राग मोह और आसक्ति एवं प्रतिकूल पदार्थ एवं व्यक्ति के प्रति द्वेष, घृणा, अरुचि या खेद होने से सुख-दुःख का वेदन करता है। इनके विपरीत होने पर यानी जिसे अनुकूल पदार्थ या व्यक्ति माना था, उसका वियोग होने पर एवं प्रतिकूल पदार्थ या व्यक्ति का संयोग होने पर दुःख का अनुभव करता है।
www.jainelibrary.org D