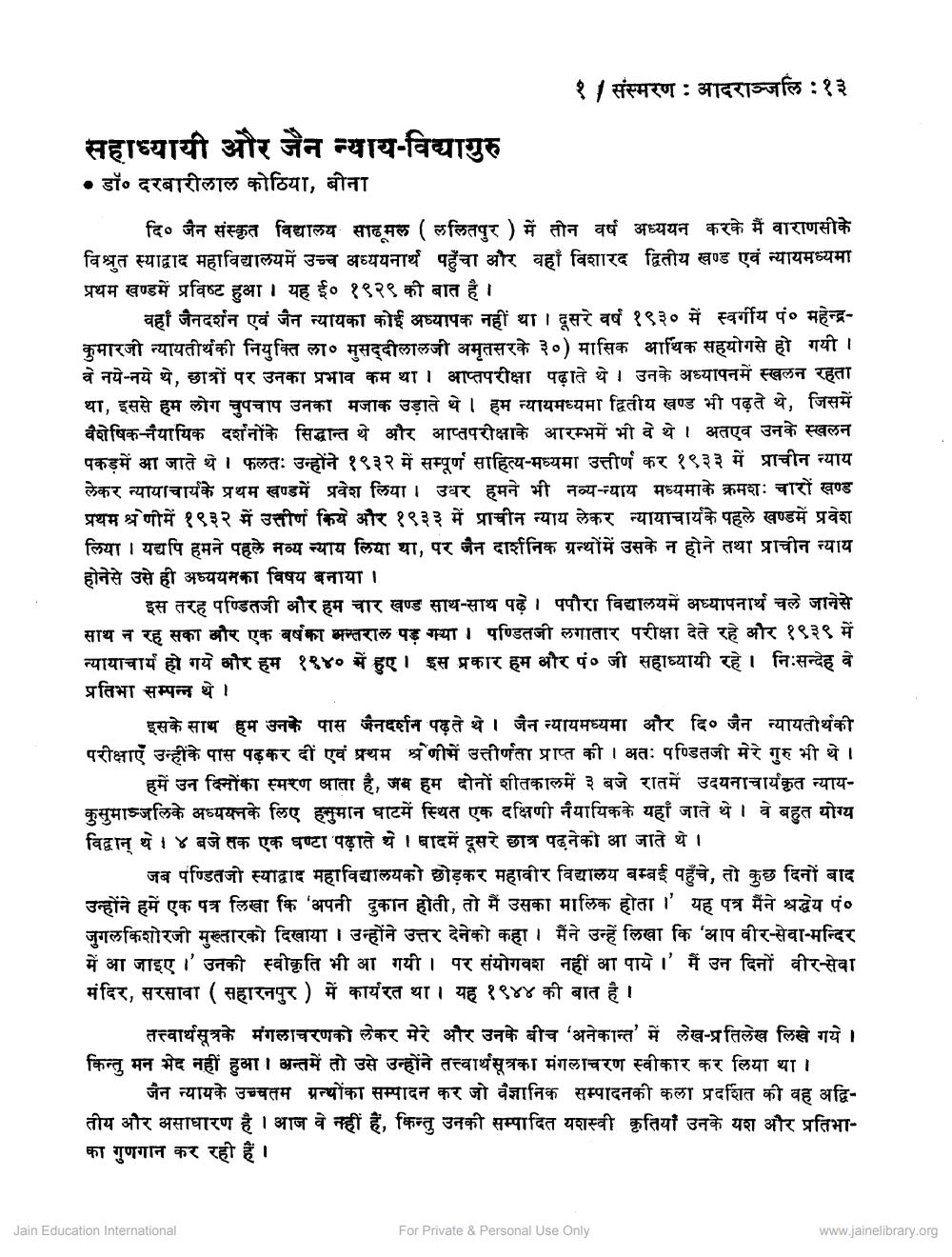________________
१/ संस्मरण : आदराञ्जलि : १३
सहाध्यायी और जैन न्याय-विद्यागुरु • डॉ० दरबारीलाल कोठिया, बीना
दि० जैन संस्कृत विद्यालय साढ़मल ( ललितपुर ) में तीन वर्ष अध्ययन करके मैं वाराणसीके विश्रुत स्याद्वाद महाविद्यालयमें उच्च अध्ययनार्थ पहुँचा और वहाँ विशारद द्वितीय खण्ड एवं न्यायमध्यमा प्रथम खण्डमें प्रविष्ट हुआ। यह ई० १९२९ की बात है।
वहाँ जैनदर्शन एवं जैन न्यायका कोई अध्यापक नहीं था। दूसरे वर्ष १९३० में स्वर्गीय पं० महेन्द्रकुमारजी न्यायतीर्थकी नियुक्ति ला० मसददीलालजी अमतसरके ३०) मासिक आर्थिक सहयोगसे हो गयी। वे नये-नये थे, छात्रों पर उनका प्रभाव कम था। आप्तपरीक्षा पढाते थे। उनके अध्यापनमें स्खलन रहता था, इससे हम लोग चुपचाप उनका मजाक उड़ाते थे । हम न्यायमध्यमा द्वितीय खण्ड भी पढ़ते थे, जिसमें वैशेषिक-नैयायिक दर्शनोंके सिद्धान्त थे और आप्तपरीक्षाके आरम्भमें भी वे थे । अतएव उनके स्खलन पकड़में आ जाते थे। फलतः उन्होंने १९३२ में सम्पूर्ण साहित्य-मध्यमा उत्तीर्ण कर १९३३ में प्राचीन न्याय लेकर न्यायाचार्यके प्रथम खण्डमें प्रवेश लिया। उधर हमने भी नव्य-न्याय मध्यमाके क्रमशः चारों खण्ड प्रथम श्रेणीमें १९३२ में उत्तीर्ण किये और १९३३ में प्राचीन न्याय लेकर न्यायाचार्यके पहले खण्डमें प्रवेश लिया । यद्यपि हमने पहले नव्य न्याय लिया था, पर जैन दार्शनिक ग्रन्थोंमें उसके न होने तथा प्राचीन न्याय होनेसे उसे ही अध्ययनका विषय बनाया।
इस तरह पण्डितजी और हम चार खण्ड साथ-साथ पढ़े। पपौरा विद्यालयमें अध्यापनार्थ चले जानेसे साथ न रह सका और एक बर्षका अन्तराल पड़ गया। पण्डितजी लगातार परीक्षा देते रहे और १९३९ में न्यायाचार्य हो गये और हम १९४० में हुए। इस प्रकार हम और पं० जी सहाध्यायी रहे। निःसन्देह वे प्रतिभा सम्पन्न थे।
इसके साथ हम उनके पास जैनदर्शन पढ़ते थे। जैन न्यायमध्यमा और दि० जैन न्यायतीर्थकी परीक्षाएँ उन्हीं के पास पड़कर दी एवं प्रथम श्रेणीमें उत्तीर्णता प्राप्त की । अतः पण्डितजी मेरे गुरु भी थे ।
हमें उन दिनोंका स्मरण आता है, जब हम दोनों शीतकालमें ३ बजे रातमें उदयनाचार्यकृत न्यायकुसुमाञ्जलिके अध्ययनके लिए हनुमान घाटमें स्थित एक दक्षिणी नैयायिकके यहाँ जाते थे। वे बहत योग्य विद्वान् थे। ४ बजे तक एक घण्टा पढ़ाते थे । बादमें दूसरे छात्र पढ़नेको आ जाते थे ।
जब पण्डितजी स्याद्वाद महाविद्यालयको छोड़कर महावीर विद्यालय बम्बई पहुँचे, तो कुछ दिनों बाद उन्होंने हमें एक पत्र लिखा कि 'अपनी दुकान होती, तो मैं उसका मालिक होता।' यह पत्र मैंने श्रद्धेय पं० जुगलकिशोरजी मुख्तारको दिखाया । उन्होंने उत्तर देनेको कहा। मैंने उन्हें लिखा कि 'आप वीर-सेवा-मन्दिर में आ जाइए।' उनकी स्वीकृति भी आ गयी। पर संयोगवश नहीं आ पाये।' मैं उन दिनों वीर-सेवा मंदिर, सरसावा (सहारनपुर) में कार्यरत था। यह १९४४ की बात है।
तत्त्वार्थसूत्रके मंगलाचरणको लेकर मेरे और उनके बीच 'अनेकान्त' में लेख-प्रतिलेख लिखे गये। किन्तु मन भेद नहीं हुआ। अन्तमें तो उसे उन्होंने तत्त्वार्थसूत्रका मंगलाचरण स्वीकार कर लिया था।
जैन न्यायके उच्चतम ग्रन्थोंका सम्पादन कर जो वैज्ञानिक सम्पादनकी कला प्रदर्शित की वह अद्वितीय और असाधारण है । आज वे नहीं हैं, किन्तु उनकी सम्पादित यशस्वी कृतियाँ उनके यश और प्रतिभाका गुणगान कर रही हैं।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org