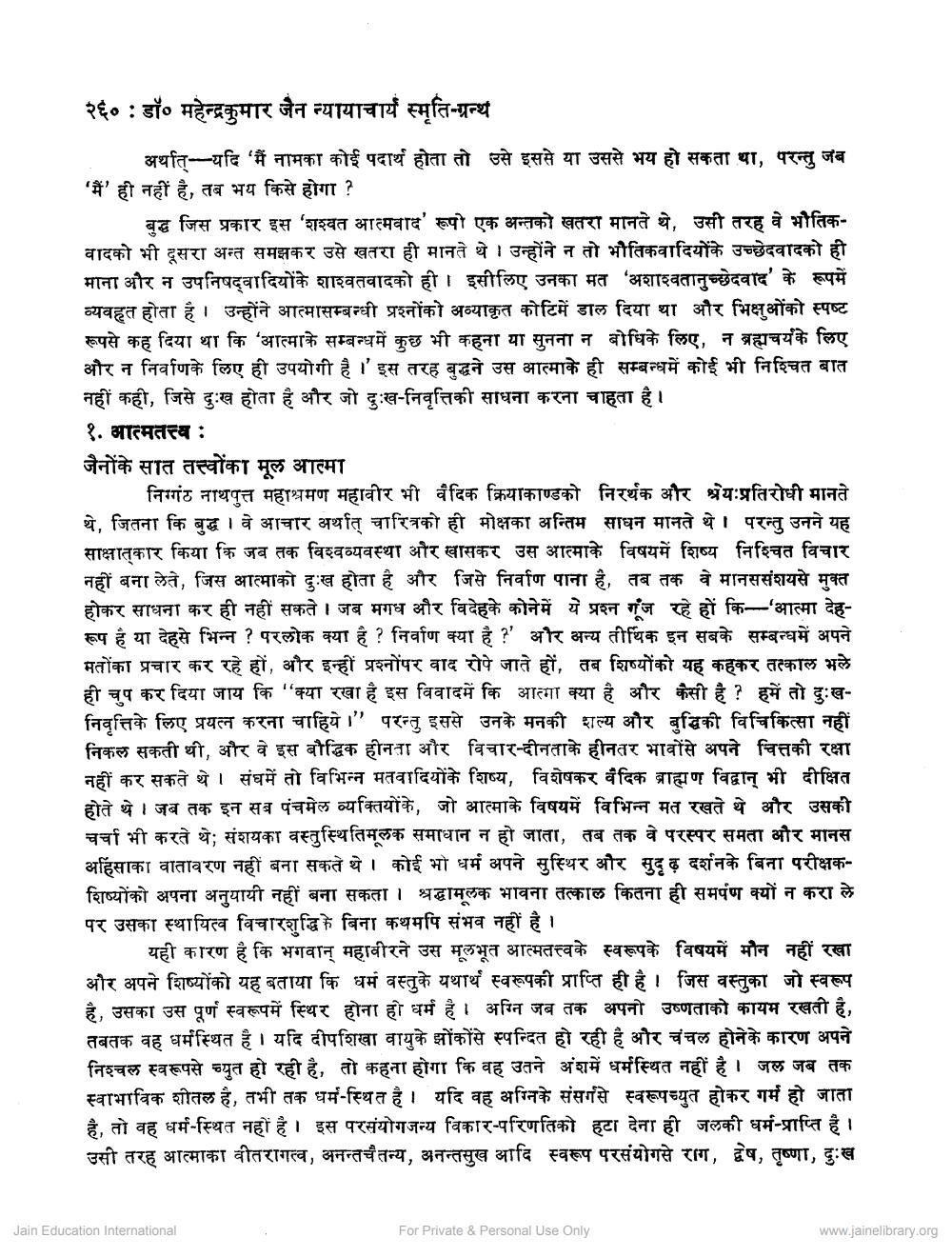________________
२६० : डॉ० महेन्द्रकुमार जैन न्यायाचार्य स्मृति ग्रन्थ
अर्थात् - यदि 'मैं नामका कोई पदार्थ होता तो उसे इससे या उससे भय हो सकता था, परन्तु जब 'मैं' ही नहीं है, तब भय किसे होगा ?
बुद्ध जिस प्रकार इस 'शश्वत आत्मवाद' रूपो एक अन्तको खतरा मानते थे, उसी तरह वे भौतिकवादको भी दूसरा अन्त समझकर उसे खतरा ही मानते थे । उन्होंने न तो भौतिकवादियोंके उच्छेदवादको ही माना और न उपनिषद्वादियोंके शाश्वतवादको ही । इसीलिए उनका मत 'अशाश्वतानुच्छेदवाद' के रूपमें व्यवहृत होता है । उन्होंने आत्मासम्बन्धी प्रश्नोंको अव्याकृत कोटिमें डाल दिया था और भिक्षुओंको स्पष्ट रूपसे कह दिया था कि 'आत्मा के सम्बन्ध में कुछ भी कहना या सुनना न बोधिके लिए, न ब्रह्मचर्यं के लिए और न निर्वाणके लिए ही उपयोगी है।' इस तरह बुद्धने उस आत्माके ही सम्बन्ध में कोई भी निश्चित बात नहीं कही, जिसे दुःख होता है और जो दुःख निवृत्तिकी साधना करना चाहता है ।
१. आत्मतत्व :
जैनों के सात तत्वोंका मूल आत्मा
निग्गंठ नाथपुत्त महाश्रमण महावीर भी वैदिक क्रियाकाण्डको निरर्थक और श्रेयः प्रतिरोधी मानते थे, जितना कि बुद्ध । वे आचार अर्थात् चारित्रको ही मोक्षका अन्तिम साधन मानते थे । परन्तु उनने यह साक्षात्कार किया कि जब तक विश्वव्यवस्था और खासकर उस आत्माके विषय में शिष्य निश्चित विचार नहीं बना लेते, जिस आत्माको दुःख होता है और जिसे निर्वाण पाना है, तब तक वे मानससंशयसे मुक्त होकर साधना कर ही नहीं सकते । जब मगध और विदेहके कोने में ये प्रश्न गूंज रहे हों कि - 'आत्मा देहरूप है या देहसे भिन्न ? परलोक क्या है ? निर्वाण क्या है ?' और अन्य तीर्थिक इन सबके सम्बन्धमें अपने मतोंका प्रचार कर रहे हों, और इन्हीं प्रश्नोंपर वाद रोपे जाते हों, तब शिष्यों को यह कहकर तत्काल भले ही चुप कर दिया जाय कि "क्या रखा है इस विवाद में कि आत्मा क्या है और कैसी है ? हमें तो दुःखनिवृत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिये।" परन्तु इससे उनके मनकी शल्य और बुद्धिकी विचिकित्सा नहीं निकल सकती थी, और वे इस बौद्धिक हीनता और विचार- दीनताके हीनतर भावोंसे अपने चित्तकी रक्षा नहीं कर सकते थे । संघ में तो विभिन्न मतवादियोंके शिष्य, विशेषकर वैदिक ब्राह्मण विद्वान् भी दीक्षित होते थे । जब तक इन सब पंचमेल व्यक्तियोंके, जो आत्माके विषयमें विभिन्न मत रखते थे और उसकी चर्चा भी करते थे; संशयका वस्तुस्थितिमूलक समाधान न हो जाता, तब तक वे परस्पर समता और मानस अहिंसाका वातावरण नहीं बना सकते थे । कोई भो धर्म अपने सुस्थिर और सुदृढ़ दर्शनके बिना परीक्षकशिष्योंको अपना अनुयायी नहीं बना सकता । श्रद्धामूलक भावना तत्काल कितना ही समर्पण क्यों न करा ले पर उसका स्थायित्व विचारशुद्धि के बिना कथमपि संभव नहीं है ।
यही कारण है कि भगवान् महावीरने उस मूलभूत आत्मतत्त्व के स्वरूपके विषयमें मौन नहीं रखा और अपने शिष्योंको यह बताया कि धर्म वस्तुके यथार्थं स्वरूपकी प्राप्ति ही है । जिस वस्तुका जो स्वरूप है, उसका उस पूर्ण स्वरूपमें स्थिर होना हो धर्म है। अग्नि जब तक अपनी उष्णताको कायम रखती है, तबतक वह धर्मस्थित है। यदि दीपशिखा वायुके झोंकोंसे स्पन्दित हो रही है और चंचल होनेके कारण अपने निश्चल स्वरूपसे च्युत हो रही है, तो कहना होगा कि वह उतने अंशमें धर्मस्थित नहीं है । जल जब तक स्वाभाविक शीतल है, तभी तक धर्म-स्थित है। यदि वह अग्निके संसर्गसे स्वरूपच्युत होकर गर्म हो जाता है, तो वह धर्म-स्थित नहीं है । इस परसंयोगजन्य विकार परिणतिको हटा देना ही जलकी धर्म-प्राप्ति है । उसी तरह आत्माका वीतरागत्व, अनन्तचैतन्य, अनन्तसुख आदि स्वरूप परसंयोगसे राग, द्वेष, तृष्णा, दुःख
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org