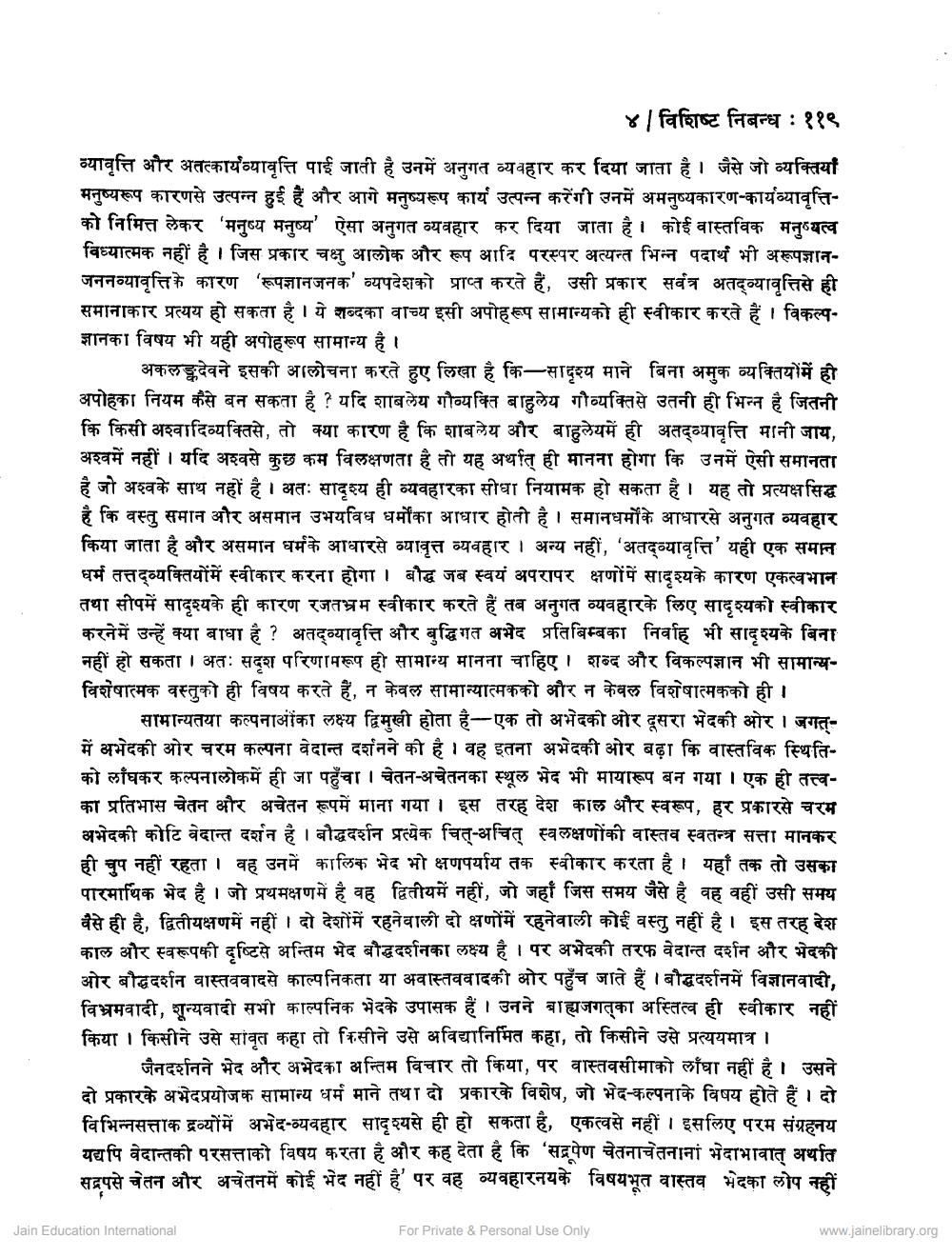________________
४ / विशिष्ट निबन्ध : ११९
व्यावृत्ति और अतत्कार्यव्यावृत्ति पाई जाती है उनमें अनुगत व्यवहार कर दिया जाता है। जैसे जो व्यक्तियाँ मनुष्यरूप कारणसे उत्पन्न हुई है और आगे मनुष्यरूप कार्य उत्पन्न करेंगी उनमें अमनुष्यकारण-कार्यव्यावृत्तिको निमित्त लेकर 'मनुष्य मनुष्य' ऐसा अनुगत व्यवहार कर दिया जाता है। कोई वास्तविक मनुष्यत्व विध्यात्मक नहीं है । जिस प्रकार चक्षु आलोक और रूप आदि परस्पर अत्यन्त भिन्न पदार्थ भी अरूपज्ञानजननव्यावृत्ति के कारण 'रूपज्ञानजनक' व्यपदेशको प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार सर्वत्र अतव्यावृत्तिसे ही समानाकार प्रत्यय हो सकता है । ये शब्दका वाच्य इसी अपोहरूप सामान्यको ही स्वीकार करते हैं । विकल्पज्ञानका विषय भी यही अपोहरूप सामान्य है।
____ अकलङ्कदेवने इसकी आलोचना करते हुए लिखा है कि-सादृश्य माने बिना अमुक व्यक्तियोंमें ही अपोहका नियम कैसे बन सकता है ? यदि शाबलेय गौव्यक्ति बाहुलेय गौव्यक्तिसे उतनी ही भिन्न है जितनी कि किसी अश्वादिव्यक्तिसे, तो क्या कारण है कि शाबलेय और बाहुलेयमें ही अतद्व्यावृत्ति मानी जाय, अश्वमें नहीं । यदि अश्वसे कुछ कम विलक्षणता है तो यह अर्थात् ही मानना होगा कि उनमें ऐसी समानता है जो अश्वके साथ नहीं है । अतः सादृश्य ही व्यवहारका सीधा नियामक हो सकता है। यह तो प्रत्यक्षसिद्ध है कि वस्तु समान और असमान उभयविध धर्मोका आधार होती है । समानधर्मों के आधारसे अनुगत व्यवहार किया जाता है और असमान धर्मके आधारसे व्यावृत्त व्यवहार । अन्य नहीं, 'अतव्यावृत्ति' यही एक समान धर्म तत्तद्व्यक्तियों में स्वीकार करना होगा। बौद्ध जब स्वयं अपरापर क्षणों में सादृश्यके कारण एकत्वभान तथा सीपमें सादृश्यके ही कारण रजतभ्रम स्वीकार करते हैं तब अनुगत व्यवहारके लिए सादृश्यको स्वीकार करने में उन्हें क्या बाधा है ? अतव्यावृत्ति और बुद्धि गत अभेद प्रतिबिम्बका निर्वाह भी सादृश्यके बिना नहीं हो सकता । अतः सदृश परिणामरूप हो सामान्य मानना चाहिए । शब्द और विकल्पज्ञान भी सामान्यविशेषात्मक वस्तुको ही विषय करते हैं, न केवल सामान्यात्मकको और न केवल विशेषात्मकको ही।
सामान्यतया कल्पनाओंका लक्ष्य द्विमुखी होता है-एक तो अभेदको ओर दूसरा भेदकी ओर । जगतमें अभेदकी ओर चरम कल्पना वेदान्त दर्शनने की है। वह इतना अभेदकी ओर बढ़ा कि वास्तविक स्थितिको लाँधकर कल्पनालोकमें ही जा पहुँचा । चेतन-अचेतनका स्थूल भेद भी मायारूप बन गया। एक ही तत्त्वका प्रतिभास चेतन और अचेतन रूपमें माना गया। इस तरह देश काल और स्वरूप, हर प्रकारसे चरम अभेदकी कोटि वेदान्त दर्शन है । बौद्धदर्शन प्रत्येक चित्-अचित् स्वलक्षणोंकी वास्तव स्वतन्त्र सत्ता मानकर ही चुप नहीं रहता। वह उनमें कालिक भेद भो क्षणपर्याय तक स्वीकार करता है। यहाँ तक तो उसका पारमार्थिक भेद है । जो प्रथमक्षणमें है वह द्वितीयमें नहीं, जो जहाँ जिस समय जैसे है वह वहीं उसी समय वैसे ही है. द्वितीयक्षणमें नहीं । दो देशोंमें रहनेवाली दो क्षणोंमें रहनेवाली कोई वस्तु नहीं है। इस तरह देश काल और स्वरूपकी दृष्टिसे अन्तिम भेद बौद्धदर्शनका लक्ष्य है । पर अभेदकी तरफ वेदान्त दर्शन और भेदकी
ओर बौद्धदर्शन वास्तववादसे काल्पनिकता या अवास्तववादकी ओर पहुँच जाते हैं । बौद्धदर्शनमें विज्ञानवादी, विभ्रमवादी, शुन्यवादी सभी काल्पनिक भेदके उपासक हैं । उनने बाह्यजगत्का अस्तित्व ही स्वीकार नहीं किया । किसीने उसे सांवत कहा तो किसीने उसे अविद्यानिर्मित कहा, तो किसीने उसे प्रत्ययमात्र ।
जैनदर्शनने भेद और अभेदका अन्तिम विचार तो किया, पर वास्तवसीमाको लाँघा नहीं है। उसने दो प्रकारके अभेदप्रयोजक सामान्य धर्म माने तथा दो प्रकारके विशेष, जो भेद-कल्पनाके विषय होते हैं। दो विभिन्नसत्ताक द्रव्योंमें अभेद-व्यवहार सादृश्यसे ही हो सकता है, एकत्वसे नहीं । इसलिए परम संग्रहनय यद्यपि वेदान्तकी परसत्ताको विषय करता है और कह देता है कि 'सद्रपेण चेतनाचेतनानां भेदाभावात अर्थात सद्रपसे चेतन और अचेतनमें कोई भेद नहीं है' पर वह व्यवहारनयके विषयभूत वास्तव भेदका लोप नहीं
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org