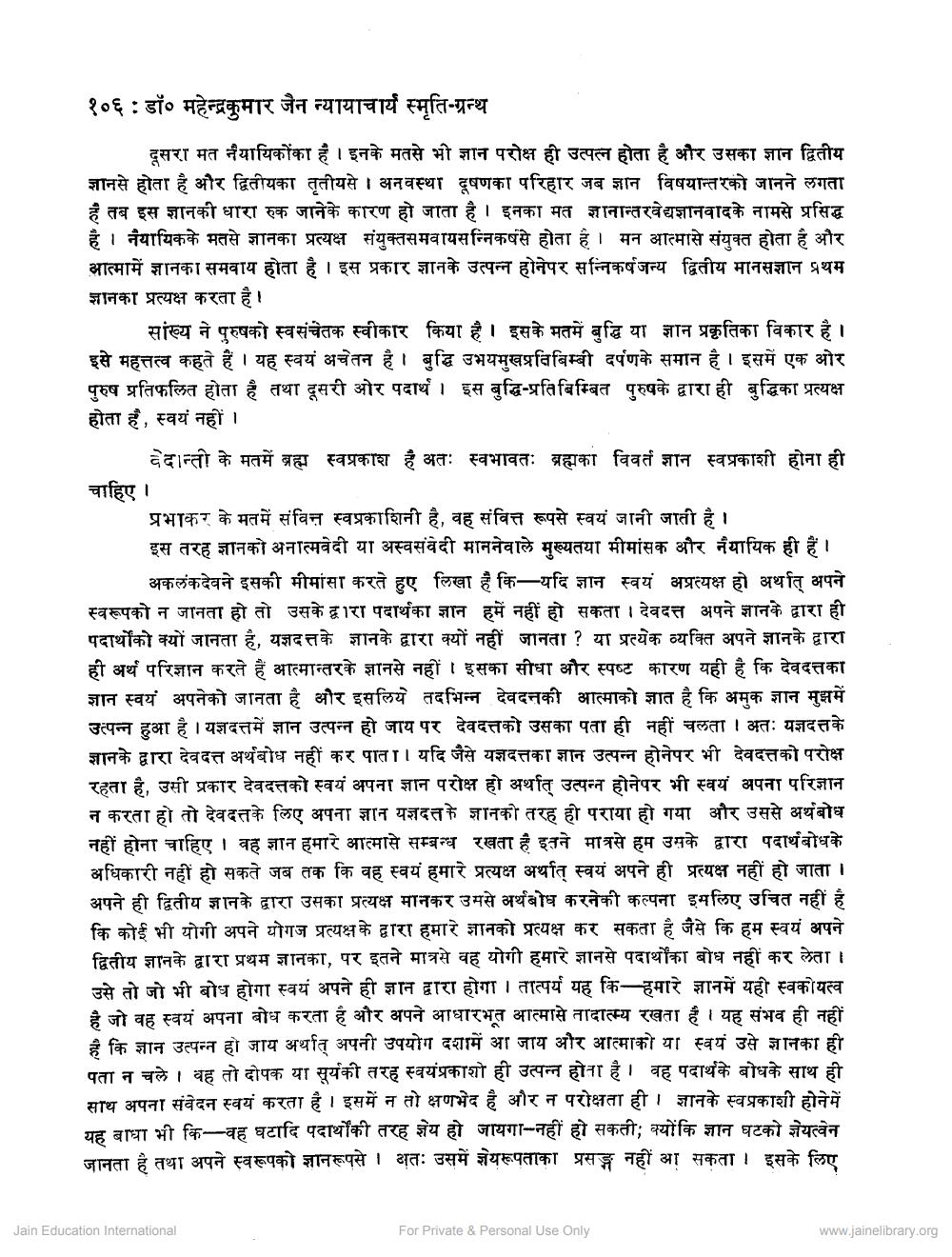________________
१०६ : डॉ० महेन्द्रकुमार जैन न्यायाचार्य स्मृति-ग्रन्थ
दुसरा मत नैयायिकोंका है। इनके मतसे भी ज्ञान परोक्ष ही उत्पत्न होता है और उसका ज्ञान द्वितीय ज्ञानसे होता है और द्वितीयका तृतीयसे । अनवस्था दूषणका परिहार जब ज्ञान विषयान्तरको जानने लगता है तब इस ज्ञानकी धारा रुक जानेके कारण हो जाता है। इनका मत ज्ञानान्तरवेद्यज्ञानवादके नामसे प्रसिद्ध है। नैयायिकके मतसे ज्ञानका प्रत्यक्ष संयुक्तसमवायसन्निकर्षसे होता है। मन आत्मासे संयुक्त होता है और आत्मामें ज्ञानका समवाय होता है । इस प्रकार ज्ञानके उत्पन्न होनेपर सन्निकर्षजन्य द्वितीय मानसज्ञान प्रथम ज्ञानका प्रत्यक्ष करता है।
सांख्य ने पुरुषको स्वसंचेतक स्वीकार किया है। इसके मतमें बुद्धि या ज्ञान प्रकृतिका विकार है। इसे महत्तत्व कहते हैं । यह स्वयं अचेतन है। बुद्धि उभयमुखप्रतिबिम्बी दर्पणके समान है । इसमें एक ओर पुरुष प्रतिफलित होता है तथा दूसरी ओर पदार्थ। इस बुद्धि-प्रतिबिम्बित पुरुषके द्वारा ही बुद्धिका प्रत्यक्ष होता है, स्वयं नहीं।
वेदान्ती के मतमें ब्रह्म स्वप्रकाश है अतः स्वभावतः ब्रह्मका विवर्त ज्ञान स्वप्रकाशी होना ही चाहिए।
प्रभाकर के मतमें संविन स्वप्रकाशिनी है, वह संवित्त रूपसे स्वयं जानी जाती है। इस तरह ज्ञानको अनात्मवेदी या अस्वसंवेदी माननेवाले मख्यतया मीमांसक और नैयायिक ही हैं।
अकलंकदेवने इसकी मीमांसा करते हुए लिखा है कि यदि ज्ञान स्वयं अप्रत्यक्ष हो अर्थात् अपने स्वरूपको न जानता हो तो उसके द्वारा पदार्थका ज्ञान हमें नहीं हो सकता । देवदत्त अपने ज्ञानके द्वारा ही पदार्थोंको क्यों जानता है, यज्ञदत्तके ज्ञानके द्वारा क्यों नहीं जानता ? या प्रत्येक व्यक्ति अपने ज्ञानके द्वारा ही अर्थ परिज्ञान करते हैं आत्मान्तरके ज्ञानसे नहीं । इसका सीधा और स्पष्ट कारण यही है कि देवदत्तका ज्ञान स्वयं अपनेको जानता है और इसलिये तदभिन्न देवदनकी आत्माको ज्ञात है कि अमुक ज्ञान मुझमें उत्पन्न हआ है । यज्ञदत्तमें ज्ञान उत्पन्न हो जाय पर देवदत्तको उसका पता ही नहीं चलता । अतः यज्ञदत्तके ज्ञानके द्वारा देवदत्त अर्थबोध नहीं कर पाता। यदि जैसे यज्ञदत्तका ज्ञान उत्पन्न होनेपर भी देवदत्तको परोक्ष रहता है, उसी प्रकार देवदत्तको स्वयं अपना ज्ञान परोक्ष हो अर्थात् उत्पन्न होनेपर भी स्वयं अपना परिज्ञान न करता हो तो देवदत्तके लिए अपना ज्ञान यज्ञदत्तके ज्ञानको तरह ही पराया हो गया और उससे अर्थबोध नहीं होना चाहिए। वह ज्ञान हमारे आत्मासे सम्बन्ध रखता है इतने मात्रसे हम उसके द्वारा पदार्थबोधके अधिकारी नहीं हो सकते जब तक कि वह स्वयं हमारे प्रत्यक्ष अर्थात् स्वयं अपने ही प्रत्यक्ष नहीं हो जाता । अपने ही द्वितीय ज्ञानके द्वारा उसका प्रत्यक्ष मानकर उमसे अर्थबोध करनेकी कल्पना इसलिए उचित नहीं है कि कोई भी योगी अपने योगज प्रत्यक्ष के द्वारा हमारे ज्ञानको प्रत्यक्ष कर सकता है जैसे कि हम स्वयं अपने द्वितीय ज्ञानके द्वारा प्रथम ज्ञानका, पर इतने मात्रसे वह योगी हमारे ज्ञानसे पदार्थों का बोध नहीं कर लेता। उसे तो जो भी बोध होगा स्वयं अपने ही ज्ञान द्वारा होगा । तात्पर्य यह कि हमारे ज्ञानमें यही स्वकोयत्व है जो वह स्वयं अपना बोध करता है और अपने आधारभत आत्मासे तादात्म्य रखता है । यह संभव ही नहीं है कि ज्ञान उत्पन्न हो जाय अर्थात् अपनी उपयोग दशामें आ जाय और आत्माको या स्वयं उसे ज्ञानका ही पता न चले। वह तो दोपक या सूर्यकी तरह स्वयंप्रकाशो ही उत्पन्न होता है। वह पदार्थके बोधके साथ ही साथ अपना संवेदन स्वयं करता है । इसमें न तो क्षणभेद है और न परोक्षता ही। ज्ञानके स्वप्रकाशी होने में यह बाधा भी कि-वह घटादि पदार्थोकी तरह ज्ञेय हो जायगा-नहीं हो सकती; क्योंकि ज्ञान घटको ज्ञेयत्वेन जानता है तथा अपने स्वरूपको ज्ञानरूपसे । अतः उसमें ज्ञेयरूपताका प्रसङ्ग नहीं आ सकता। इसके लिए
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org