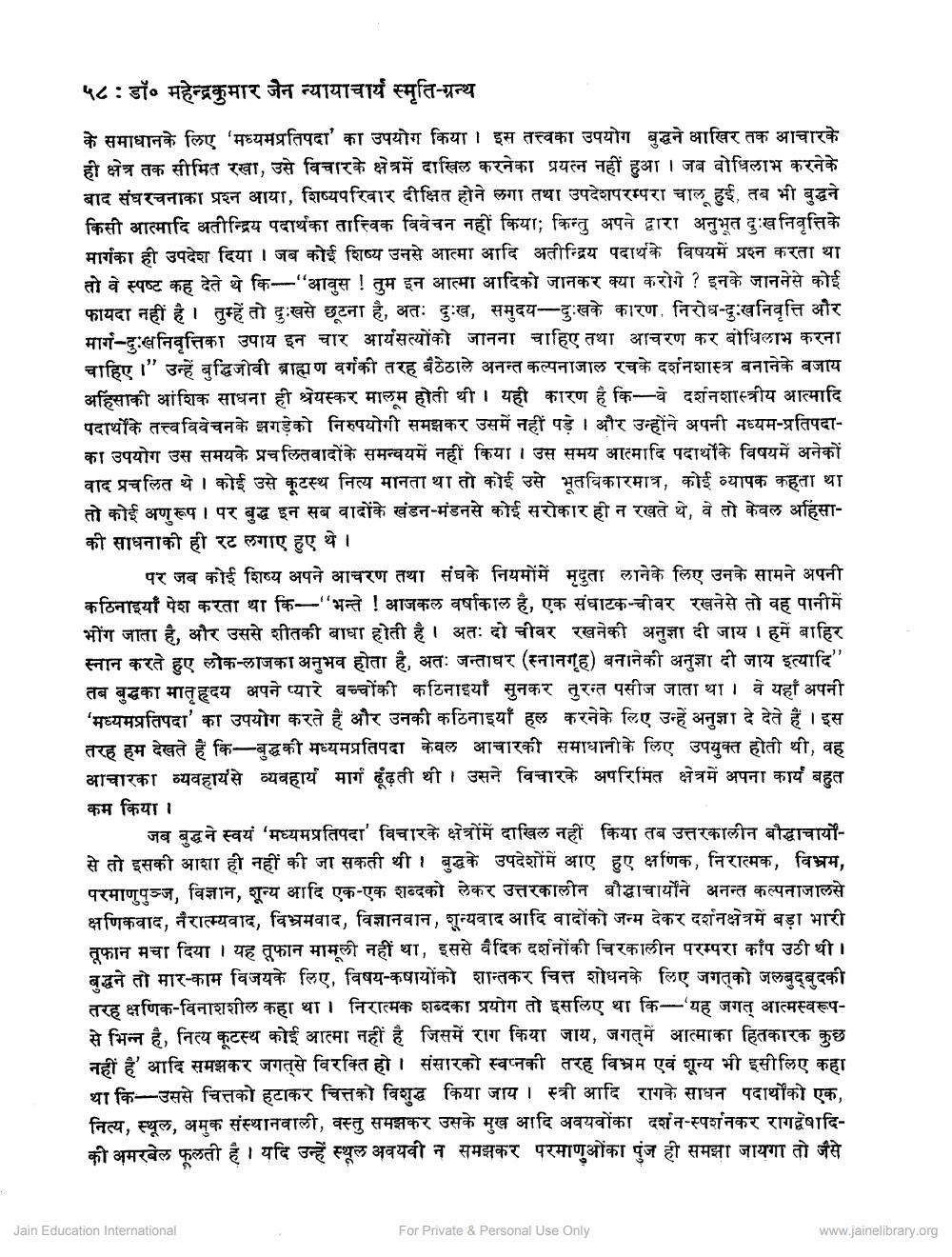________________
५८ : डॉ० महेन्द्रकुमार जैन न्यायाचार्य स्मृति ग्रन्थ
के समाधान के लिए 'मध्यमप्रतिपदा' का उपयोग किया। इस तत्त्वका उपयोग बुद्धने आखिर तक आचारके ही क्षेत्र तक सीमित रखा, उसे विचारके क्षेत्रमें दाखिल करनेका प्रयत्न नहीं हुआ । जब बोधिलाभ करने के बाद संघरचनाका प्रश्न आया, शिष्यपरिवार दीक्षित होने लगा तथा उपदेशपरम्परा चालू हुई, तब भी बुद्धने किसी आत्मादि अतीन्द्रिय पदार्थका तात्त्विक विवेचन नहीं किया; किन्तु अपने द्वारा अनुभूत दुःख निवृत्ति के मार्गका ही उपदेश दिया । जब कोई शिष्य उनसे आत्मा आदि अतीन्द्रिय पदार्थ के विषयमें प्रश्न करता था तो वे स्पष्ट कह देते थे कि - " आवुस ! तुम इन आत्मा आदिको जानकर क्या करोगे ? इनके जानने से कोई फायदा नहीं है । तुम्हें तो दुःखसे छूटना है, अतः दुःख, समुदय - दुःखके कारण निरोध-दुःखनिवृत्ति और मार्ग - दुःखनिवृत्तिका उपाय इन चार आर्यसत्योंको जानना चाहिए तथा आचरण कर बोधिलाभ करना चाहिए।" उन्हें बुद्धिजीवी ब्राह्मण वर्गकी तरह बैठेठाले अनन्त कल्पनाजाल रचके दर्शनशास्त्र बनानेके बजाय अहिंसा आशिक साधना ही श्रेयस्कर मालूम होती थी । यही कारण है कि वे दर्शनशास्त्रीय आत्मादि पदार्थोंके तत्त्व विवेचनके झगड़ेको निरुपयोगी समझकर उसमें नहीं पड़े । और उन्होंने अपनी नध्यम - प्रतिपदाका उपयोग उस समयके प्रचलितवादों के समन्वयमें नहीं किया । उस समय आत्मादि पदार्थोंके विषय में अनेकों वाद प्रचलित थे । कोई उसे कूटस्थ नित्य मानता था तो कोई उसे भूतविकारमात्र, कोई व्यापक कहता था तो कोई अणुरूप । पर बुद्ध इन सब वादोंके खंडन-मंडनसे कोई सरोकार ही न रखते थे, वे तो केवल अहिंसाकी साधना की ही रट लगाए हुए थे 1
पर जब कोई शिष्य अपने आचरण तथा संघके नियमोंमें मृदुता लानेके लिए उनके सामने अपनी कठिनाइयाँ पेश करता था कि-- "भन्ते ! आजकल वर्षाकाल है, एक संघाटक-चीवर रखने से तो वह पानी में भोंग जाता है, और उससे शीतकी बाधा होती है । अतः दो चीवर रखनेकी अनुज्ञा दी जाय । हमें बाहिर स्नान करते हुए लोक-लाजका अनुभव होता है, अतः जन्ताघर (स्नानगृह) बनानेकी अनुज्ञा दी जाय इत्यादि' तब बुद्धका मातृहृदय अपने प्यारे बच्चोंकी कठिनाइयाँ सुनकर तुरन्त पसीज जाता था। वे यहाँ अपनी 'मध्यमप्रतिपदा' का उपयोग करते हैं और उनकी कठिनाइयाँ हल करनेके लिए उन्हें अनुज्ञा दे देते हैं । इस तरह हम देखते हैं कि - बुद्धकी मध्यमप्रतिपदा केवल आचारकी समाधानी के लिए उपयुक्त होती थी, वह आचारका व्यवहायसे व्यवहार्य मार्ग ढूंढ़ती थी । उसने विचारके अपरिमित क्षेत्रमें अपना कार्यं बहुत कम किया ।
जब बुद्ध ने स्वयं 'मध्यमप्रतिपदा' विचारके क्षेत्रोंमें दाखिल नहीं किया तब उत्तरकालीन बौद्धाचार्योसे तो इसकी आशा ही नहीं की जा सकती थी । बुद्धके उपदेशोंमें आए हुए क्षणिक, निरात्मक, विभ्रम, परमाणुपुञ्ज, विज्ञान, शून्य आदि एक-एक शब्दको लेकर उत्तरकालीन बौद्धाचार्योंने अनन्त कल्पनाजालसे क्षणिकवाद, नैरात्म्यवाद, विभ्रमवाद, विज्ञानवान, शून्यवाद आदि वादोंको जन्म देकर दर्शनक्षेत्र में बड़ा भारी तूफान मचा दिया । यह तुफान मामूली नहीं था, इससे वैदिक दर्शनोंकी चिरकालीन परम्परा काँप उठी थी । बुद्धने तो मार-काम विजयके लिए, विषय-कषायोंको शान्तकर चित्त शोधन के लिए जगत्को जलबुद्बुदकी तरह क्षणिक-विनाशशील कहा था । निरात्मक शब्दका प्रयोग तो इसलिए था कि - 'यह जगत् आत्मस्वरूपसे भिन्न है, नित्य कूटस्थ कोई आत्मा नहीं है जिसमें राग किया जाय, जगत् में आत्माका हितकारक कुछ नहीं है' आदि समझकर जगत्से विरक्ति हो । संसारको स्वप्नकी तरह विभ्रम एवं शून्य भी इसीलिए कहा था कि उससे चित्तको हटाकर चित्तको विशुद्ध किया जाय । स्त्री आदि रागके साधन पदार्थोंको एक, नित्य, स्थूल, अमुक संस्थानवाली, वस्तु समझकर उसके मुख आदि अवयवोंका दर्शन- स्पर्शनकर रागद्वेषादिकी अमरबेल फूलती है । यदि उन्हें स्थूल अवयवी न समझकर परमाणुओं का पुंज ही समझा जायगा तो जैसे
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org