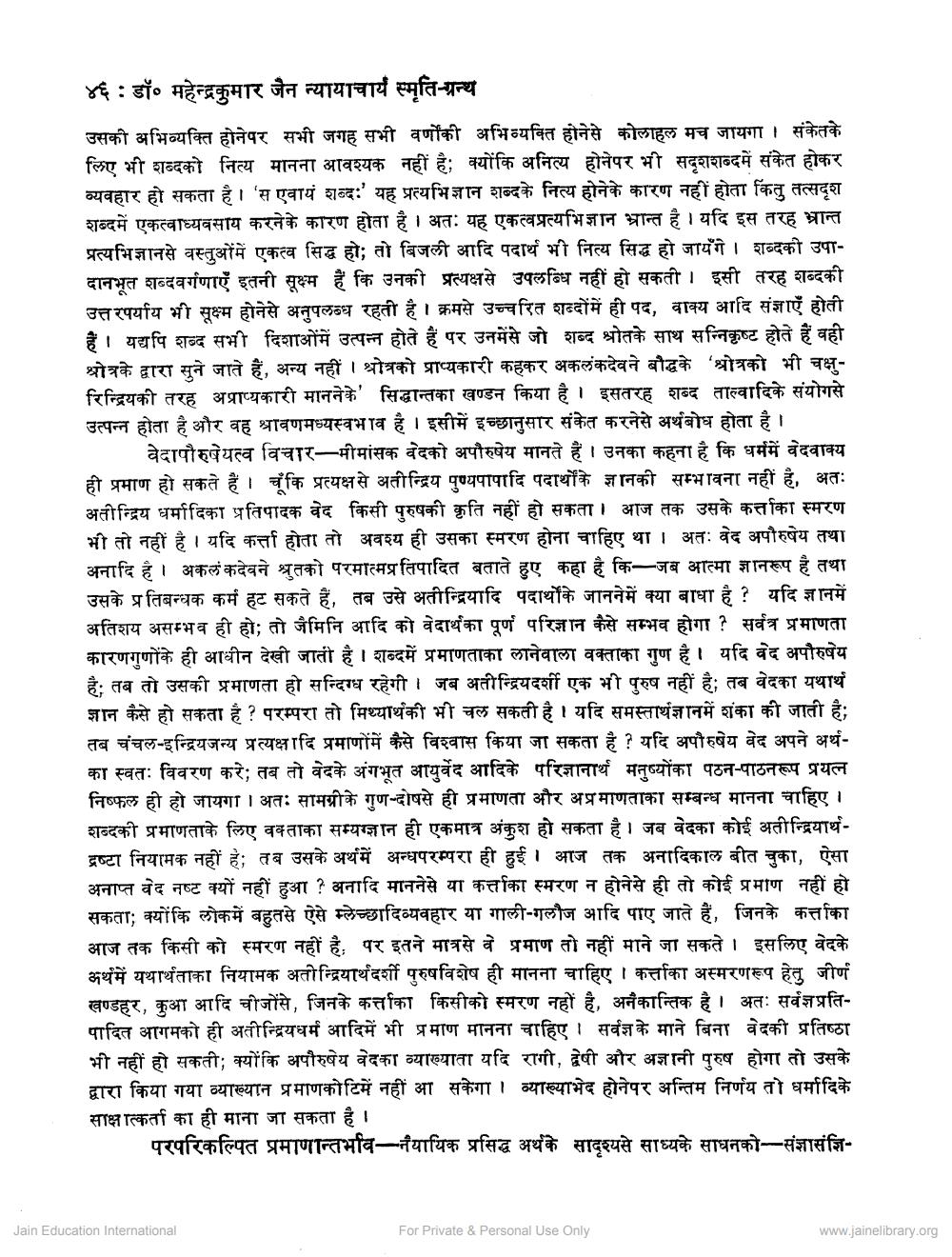________________
४६ : डॉ. महेन्द्रकुमार जैन न्यायाचार्य स्मृति-ग्रन्थ उसकी अभिव्यक्ति होनेपर सभी जगह सभी वर्गोंकी अभिव्यक्ति होनेसे कोलाहल मच जायगा। संतके लिए भी शब्दको नित्य मानना आवश्यक नहीं है; क्योंकि अनित्य होनेपर भी सदशशब्दमें संकेत होकर व्यवहार हो सकता है। स एवायं शब्दः' यह प्रत्यभिज्ञान शब्दके नित्य होनेके कारण नहीं होता किंतु तत्सदृश शब्दमें एकत्वाध्यवसाय करने के कारण होता है । अतः यह एकत्वप्रत्यभिज्ञान भ्रान्त है । यदि इस तरह भ्रान्त प्रत्यभिज्ञानसे वस्तुओंमें एकत्व सिद्ध हो; तो बिजली आदि पदार्थ भी नित्य सिद्ध हो जायेंगे। शब्दको उपादानभूत शब्दवर्गणाएँ इतनी सूक्ष्म हैं कि उनकी प्रत्यक्षसे उपलब्धि नहीं हो सकती। इसी तरह शब्दकी उत्तरपर्याय भी सूक्ष्म होनेसे अनुपलब्ध रहती है। क्रमसे उच्चरित शब्दोंमें ही पद, वाक्य आदि संज्ञाएँ होती हैं । यद्यपि शब्द सभी दिशाओंमें उत्पन्न होते हैं पर उनमेंसे जो शब्द श्रोतके साथ सन्निकृष्ट होते हैं वही श्रोत्रके द्वारा सुने जाते हैं, अन्य नहीं । श्रोत्रको प्राप्यकारी कहकर अकलंकदेवने बौद्धके 'श्रोत्रको भी चक्षुरिन्द्रियकी तरह अप्राप्यकारी माननेके' सिद्धान्तका खण्डन किया है । इसतरह शब्द ताल्वादिके संयोगसे उत्पन्न होता है और वह श्रावणमध्यस्वभाव है । इसीमें इच्छानुसार संकेत करनेसे अर्थबोध होता है।
वेदापौरुषेयत्व विचार-मीमांसक वेदको अपौरुषेय मानते हैं। उनका कहना है कि धर्ममें वेदवाक्य ही प्रमाण हो सकते हैं। चूंकि प्रत्यक्षसे अतीन्द्रिय पुण्यपापादि पदार्थों के ज्ञानकी सम्भावना नहीं है, अतः अतीन्द्रिय धर्मादिका प्रतिपादक वेद किसी पुरुषकी कृति नहीं हो सकता। आज तक उसके कर्ताका स्मरण भी तो नहीं है । यदि कर्ता होता तो अवश्य ही उसका स्मरण होना चाहिए था। अतः वेद अपौरुषेय तथा अनादि है। अकलंकदेवने श्रुतको परमात्मप्रतिपादित बताते हुए कहा है कि जब आत्मा ज्ञानरूप है तथा उसके प्रतिबन्धक कर्म हट सकते हैं, तब उसे अतीन्द्रियादि पदार्थों के जानने में क्या बाधा है ? यदि ज्ञानमें अतिशय असम्भव ही हो; तो जैमिनि आदि को वेदार्थका पूर्ण परिज्ञान कैसे सम्भव होगा? सर्वत्र प्रमाणता कारणगुणोंके ही आधीन देखी जाती है। शब्दमें प्रमाणताका लानेवाला वक्ताका गुण है। यदि वेद अपौरुषेय है; तब तो उसकी प्रमाणता हो सन्दिग्ध रहेगी। जब अतीन्द्रियदर्शी एक भी पुरुष नहीं है; तब वेदका यथार्थ ज्ञान कैसे हो सकता है ? परम्परा तो मिथ्यार्थकी भी चल सकती है। यदि समस्तार्थज्ञानमें शंका की जाती है; तब चंचल-इन्द्रियजन्य प्रत्यक्षादि प्रमाणोंमें कैसे विश्वास किया जा सकता है ? यदि अपौरुषेय वेद अपने अर्थका स्वतः विवरण करे; तब तो वेदके अंगभूत आयुर्वेद आदिके परिज्ञानार्थ मनुष्योंका पठन-पाठनरूप प्रयत्न निष्फल ही हो जायगा । अतः सामग्रीके गुण-दोषसे ही प्रमाणता और अप्रमाणताका सम्बन्ध मानना चाहिए। शब्दकी प्रमाणताके लिए वक्ताका सम्यग्ज्ञान ही एकमात्र अंकुश हो सकता है। जब वेदका कोई अतीन्द्रियार्थद्रष्टा नियामक नहीं है; तब उसके अर्थमें अन्धपरम्परा ही हुई। आज तक अनादिकाल बीत चुका, ऐसा अनाप्त वेद नष्ट क्यों नहीं हुआ? अनादि माननेसे या कर्ताका स्मरण न होनेसे ही तो कोई प्रमाण नहीं हो सकता; क्योंकि लोकमें बहुतसे ऐसे म्लेच्छादिव्यवहार या गाली-गलौज आदि पाए जाते हैं, जिनके कर्ताका आज तक किसी को स्मरण नहीं है, पर इतने मात्रसे वे प्रमाण तो नहीं माने जा सकते । इसलिए वेदके अर्थमें यथार्थताका नियामक अतीन्द्रियार्थदर्शी पुरुषविशेष ही मानना चाहिए । कर्ताका अस्मरणरूप हेतु जीर्ण खण्डहर, कुआ आदि चीजोंसे, जिनके कर्ताका किसीको स्मरण नहीं है, अनैकान्तिक है। अतः सर्वज्ञप्रतिपादित आगमको ही अतीन्द्रियधर्म आदिमें भी प्रमाण मानना चाहिए। सर्वज्ञ के माने बिना वेदकी प्रतिष्ठा भी नहीं हो सकती; क्योंकि अपौरुषेय वेदका व्याख्याता यदि रागी, द्वेषी और अज्ञानी पुरुष होगा तो उसके द्वारा किया गया व्याख्यान प्रमाणकोटिमें नहीं आ सकेगा। व्याख्याभेद होनेपर अन्तिम निर्णय तो धर्मादिके साक्षात्कर्ता का ही माना जा सकता है।
परपरिकल्पित प्रमाणान्तर्भाव-नैयायिक प्रसिद्ध अर्थके सादृश्यसे साध्यके साधनको-संज्ञासंज्ञि
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org