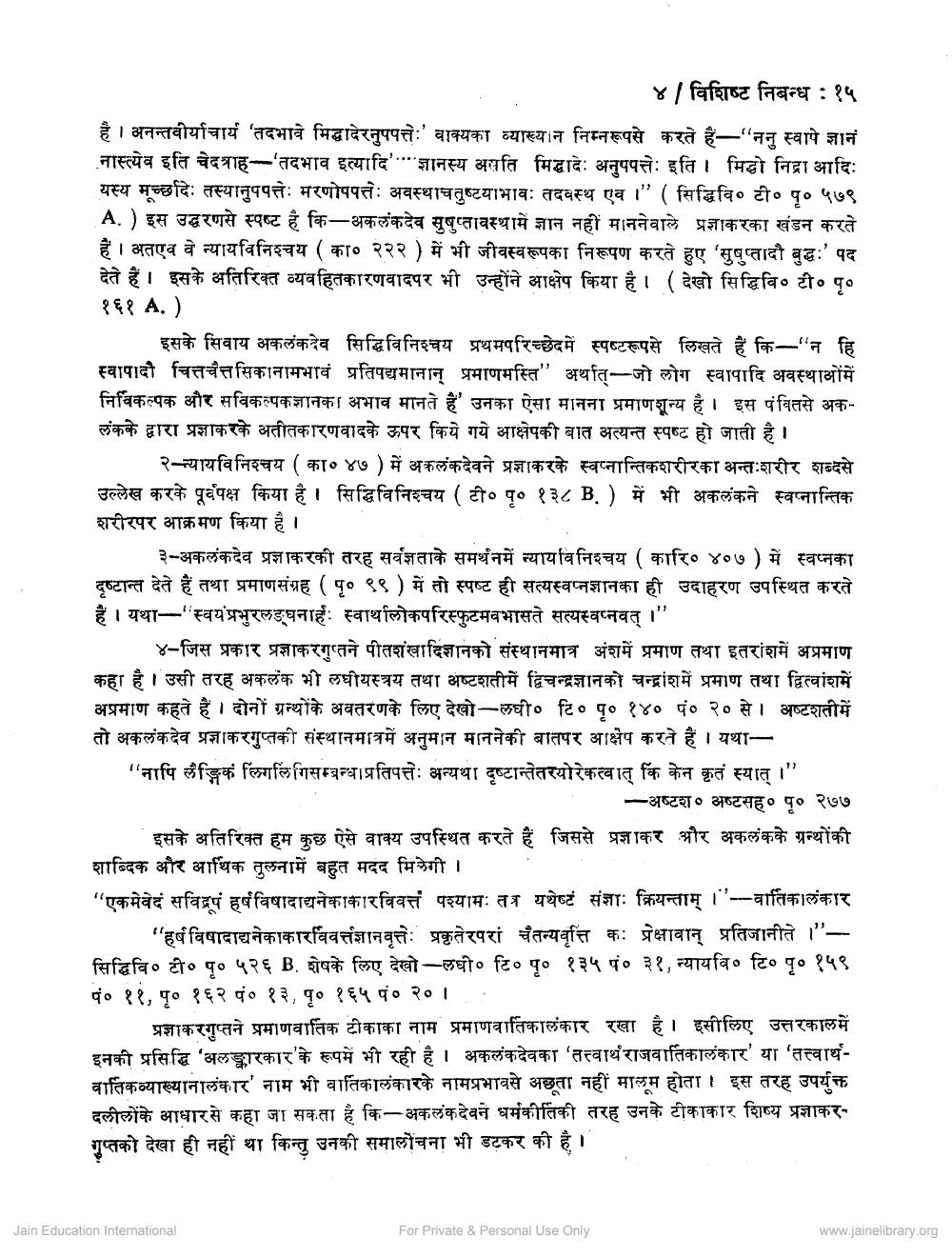________________
४ / विशिष्ट निबन्ध : १५ है । अनन्तवीर्याचार्य 'तदभावे मिद्धादेरनुपपत्तेः' वाक्यका व्याख्यान निम्नरूपसे करते हैं- " ननु स्वापे ज्ञानं नास्त्येव इति चेदाह - 'तदभाव इत्यादि' ज्ञानस्य असति मिद्धादेः अनुपपत्तेः इति । मिठो निद्रा आदिः यस्य मूर्च्छादेः तस्यानुपपत्तेः मरणोपपत्तेः अवस्थाचतुष्टयाभावः तदवस्थ एव ।" ( सिद्धिवि० टी० पृ० ५७९ A. ) इस उद्धरणसे स्पष्ट है कि - अकलंकदेव सुषुप्तावस्थामें ज्ञान नहीं माननेवाले प्रज्ञाकरका खंडन करते हैं । अतएव वे न्यायविनिश्चय ( का० २२२ ) में भी जीवस्वरूपका निरूपण करते हुए 'सुषुप्तादी बुद्ध:' पद देते हैं । इसके अतिरिक्त व्यवहितकारणवादपर भी उन्होंने आक्षेप किया है । ( देखो सिद्धिवि० टी० पृ० १६१ A. )
इसके सिवाय अकलंकदेव सिद्धिविनिश्चय प्रथमपरिच्छेद में स्पष्टरूपसे लिखते हैं कि- "न हि स्वापादौ चित्तचत्तसिकानामभावं प्रतिपद्यमानान् प्रमाणमस्ति" अर्थात् - जो लोग स्वापादि अवस्थाओं में निर्विकल्पक और सविकल्पकज्ञानका अभाव मानते हैं उनका ऐसा मानना प्रमाणशून्य है । इस पंक्तिसे अकलंकके द्वारा प्रज्ञाकरके अतीतकारणवादके ऊपर किये गये आक्षेपकी बात अत्यन्त स्पष्ट हो जाती है ।
२ - न्यायविनिश्चय ( का० ४७ ) में अकलंकदेवने प्रज्ञाकरके स्वप्नान्तिकशरीरका अन्तःशरीर शब्दसे उल्लेख करके पूर्वपक्ष किया है । सिद्धिविनिश्चय ( टी० पृ० १३८ B. ) में भी अकलंकने स्वप्नान्तिक शरीरपर आक्रमण किया है ।
३- अकलंकदेव प्रज्ञाकरकी तरह सर्वज्ञताके समर्थनमें न्यायविनिश्चय ( कारि० ४०७ ) में स्वप्नका दृष्टान्त देते हैं तथा प्रमाण संग्रह ( पृ० ९९ ) में तो स्पष्ट ही सत्यस्वप्नज्ञानका ही उदाहरण उपस्थित करते हैं । यथा - "स्वयंप्रभुरलङ्घनार्हः स्वार्थालोकपरिस्फुटमवभासते सत्यस्वप्नवत् । "
४- जिस प्रकार प्रज्ञाकरगुप्तने पीतशंखादिज्ञानको संस्थानमात्र अंशमें प्रमाण तथा इतरांशमें अप्रमाण कहा है । उसी तरह अकलंक भी लघीयस्त्रय तथा अष्टशती में द्विचन्द्रज्ञानको चन्द्रांश में प्रमाण तथा द्वित्वांश में अप्रमाण कहते हैं । दोनों ग्रन्थोंके अवतरणके लिए देखो - लघी० टि० पृ० १४० पं० २० से । अष्टशती में तो अकलंकदेव प्रज्ञाकरगुप्तकी संस्थानमात्रमें अनुमान माननेकी बातपर आक्षेप करते हैं । यथा
"नापि लैङ्गिक लिगलिगसम्बन्धाप्रतिपत्तेः अन्यथा दृष्टान्तेतरयोरेकत्वात् कि केन कृतं स्यात् । "
- अष्टश ० अष्टसह ० पृ० २७७
इसके अतिरिक्त हम कुछ ऐसे वाक्य उपस्थित करते हैं जिससे प्रज्ञाकर और अकलंकके ग्रन्थोंकी शाब्दिक और आर्थिक तुलना में बहुत मदद मिलेगी ।
" एकमेवेदं सविद्रूपं हर्षविषादाद्यनेकाकारविवत्तं पश्यामः तत्र यथेष्टं संज्ञाः क्रियन्ताम् ।" - वार्तिकालंकार "हर्ष विषादाद्यनेकाकारविवर्त्तज्ञानवृत्तेः प्रकृतेरपरां चैतन्यवृत्ति कः प्रेक्षावान् प्रतिजानीते । "सिद्धिवि० टी० पृ० ५२६ B. शेषके लिए देखो - लघी० टि० पृ० १३५ पं० ३१, न्यायवि० टि० पृ० १५९ पं० ११, पृ० १६२ पं० १३, पृ० १६५ पं० २० ।
प्रज्ञाकरगुप्तने प्रमाणवार्तिक टीकाका नाम प्रमाणवार्तिकालंकार रखा है । इसीलिए उत्तरकाल में इनकी प्रसिद्धि 'अलङ्कारकार के रूपमें भी रही है । अकलंकदेवका 'तत्त्वार्थ राजवार्तिकालंकार' या 'तत्त्वार्थवार्तिकव्याख्यानालंकार' नाम भी वार्तिकालंकारके नामप्रभावसे अछूता नहीं मालूम होता । इस तरह उपर्युक्त दलीलोंके आधार से कहा जा सकता है कि - अकलंक देवने धर्मकीर्तिकी तरह उनके टीकाकार शिष्य प्रज्ञाकरगुप्तको देखा ही नहीं था किन्तु उनकी समालोचना भी डटकर की है।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org