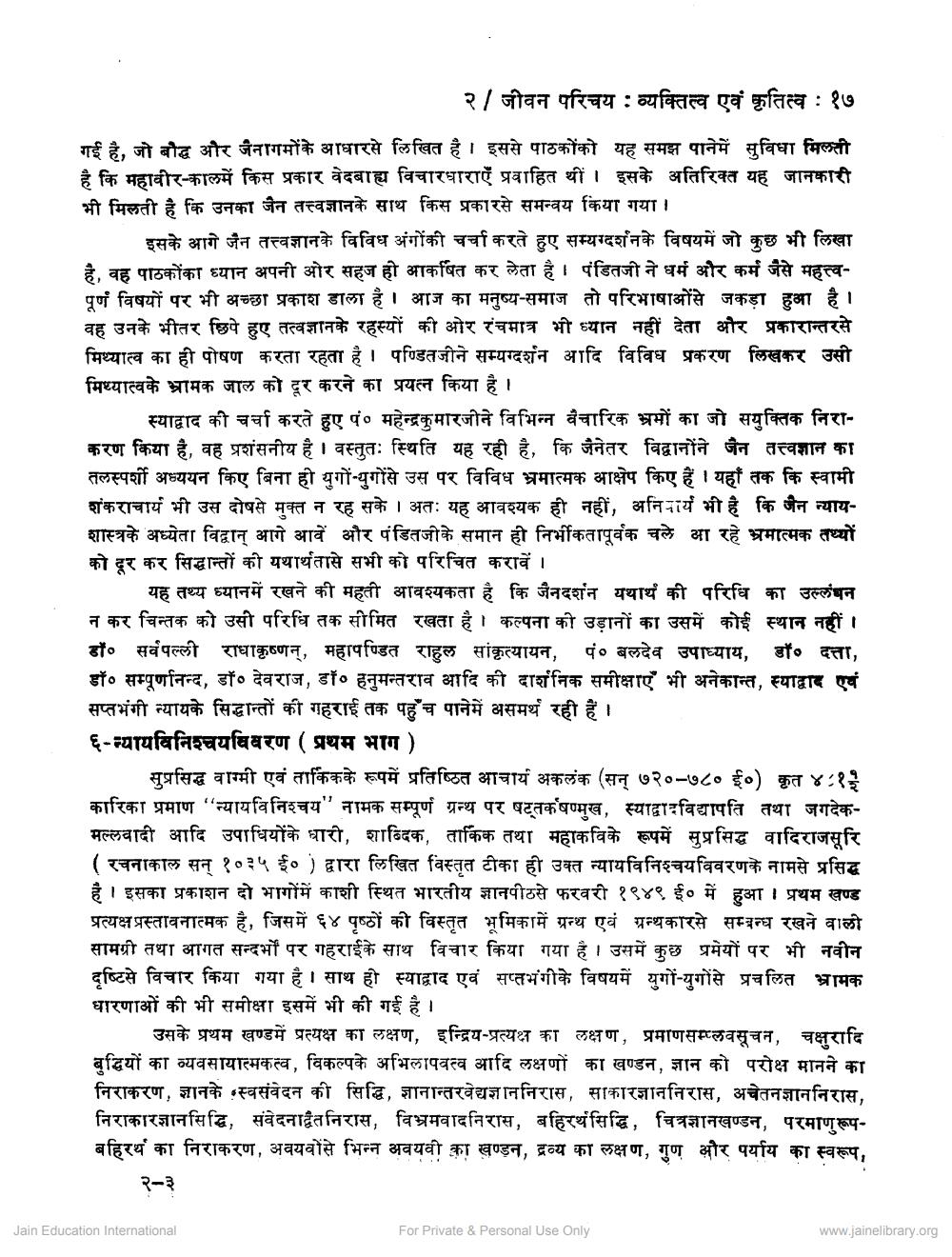________________
२ / जीवन परिचय : व्यक्तित्व एवं कृतित्व : १७ गई है, जो बौद्ध और जैनागमों के आधारसे लिखित है । इससे पाठकोंको यह समझ पानेमें सुविधा मिलती है कि महावीर - कालमें किस प्रकार वेदबाह्य विचारधाराएँ प्रवाहित थीं । इसके अतिरिक्त यह जानकारी भी मिलती है कि उनका जैन तत्त्वज्ञानके साथ किस प्रकारसे समन्वय किया गया ।
इसके आगे जैन तत्त्वज्ञान के विविध अंगोंकी चर्चा करते हुए सम्यग्दर्शनके विषयमें जो कुछ भी लिखा है, वह पाठकों का ध्यान अपनी ओर सहज हो आकर्षित कर लेता है। पंडितजी ने धर्म और कर्म जैसे महत्त्वपूर्ण विषयों पर भी अच्छा प्रकाश डाला है । आज का मनुष्य-समाज तो परिभाषाओंसे जकड़ा हुआ है । वह उनके भीतर छिपे हुए तत्वज्ञानके रहस्यों की ओर रंचमात्र भी ध्यान नहीं देता और प्रकारान्तरसे मिथ्यात्व का ही पोषण करता रहता है । पण्डितजीने सम्यग्दर्शन आदि विविध प्रकरण लिखकर उसी मिथ्यात्वके भ्रामक जाल को दूर करने का प्रयत्न किया है ।
स्याद्वाद की चर्चा करते हुए पं० महेन्द्रकुमारजीने विभिन्न वैचारिक भ्रमों का जो सयुक्तिक निराकरण किया है, वह प्रशंसनीय है । वस्तुतः स्थिति यह रही है, कि जैनेतर विद्वानोंने जैन तत्त्वज्ञान का तलस्पर्शी अध्ययन किए बिना ही युगों-युगों से उस पर विविध भ्रमात्मक आक्षेप किए हैं । यहाँ तक कि स्वामी शंकराचार्य भी उस दोष से मुक्त न रह सके । अतः यह आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी है कि जैन न्यायशास्त्र के अध्येता विद्वान् आगे आवें और पंडितजी के समान ही निर्भीकतापूर्वक चले आ रहे भ्रमात्मक तथ्यों को दूर कर सिद्धान्तों की यथार्थतासे सभी को परिचित करावें ।
यह तथ्य ध्यान में रखने की महती आवश्यकता है कि जैनदर्शन यथार्थ की परिधि न कर चिन्तक को उसी परिधि तक सीमित रखता है। कल्पना की उड़ानों का उसमें कोई डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन्, महापण्डित राहुल सांकृत्यायन, पं० बलदेव उपाध्याय, डॉ० सम्पूर्णानन्द, डॉ० देवराज, डॉ० हनुमन्तराव आदि की दार्शनिक समीक्षाएँ भी अनेकान्त, स्याद्वाद एवं सप्तभंगी न्यायके सिद्धान्तों की गहराई तक पहुँच पानेमें असमर्थ रही हैं ।
का उल्लंघन स्थान नहीं । डॉ० दत्ता,
६- न्यायविनिश्चयविवरण (प्रथम भाग )
सुप्रसिद्ध वाग्मी एवं तार्किक के रूपमें प्रतिष्ठित आचार्य अकलंक (सन् ७२०-७८० ई०) कृत ४ : १३ कारिका प्रमाण " न्यायविनिश्चय' नामक सम्पूर्ण ग्रन्थ पर षट्तर्कषण्मुख, स्याद्वादविद्यापति तथा जगदेकमल्लवादी आदि उपाधियोंके धारी, शाब्दिक, तार्किक तथा महाकविके रूपमें सुप्रसिद्ध वादिराजसूरि ( रचनाकाल सन् १०३५ ई० ) द्वारा लिखित विस्तृत टीका ही उक्त न्यायविनिश्चयविवरणके नामसे प्रसिद्ध है । इसका प्रकाशन दो भागों में काशी स्थित भारतीय ज्ञानपीठसे फरवरी १९४९ ई० में हुआ । प्रथम खण्ड प्रत्यक्ष प्रस्तावनात्मक है, जिसमें ६४ पृष्ठों की विस्तृत भूमिका में ग्रन्थ एवं ग्रन्थकार से सम्बन्ध रखने वाली सामग्री तथा आगत सन्दर्भों पर गहराई के साथ विचार किया गया है। उसमें कुछ प्रमेयों पर भी नवीन दृष्टिसे विचार किया गया है । साथ ही स्याद्वाद एवं सप्तभंगीके विषय में युगों-युगों से प्रचलित भ्रामक धारणाओं की भी समीक्षा इसमें भी की गई है ।
उसके प्रथम खण्ड में प्रत्यक्ष का लक्षण, इन्द्रिय- प्रत्यक्ष का लक्षण, प्रमाणसम्प्लवसूचन, चक्षुरादि बुद्धियों का व्यवसायात्मकत्व, विकल्पके अभिलापवत्व आदि लक्षणों का खण्डन, ज्ञान को परोक्ष मानने का निराकरण, ज्ञानके (स्वसंवेदन की सिद्धि, ज्ञानान्तरवेद्यज्ञाननिरास साकारज्ञाननिरास, अचेतनज्ञाननिरास, निराकारज्ञानसिद्धि, संवेदनाद्वैत निरास, विभ्रमवादनिरास, बहिरर्थसिद्धि चित्रज्ञानखण्डन, परमाणुरूपबहिरर्थं का निराकरण, अवयवोंसे भिन्न अवयवी का खण्डन, द्रव्य का लक्षण, गुण और पर्याय का स्वरूप,
3
२-३
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org