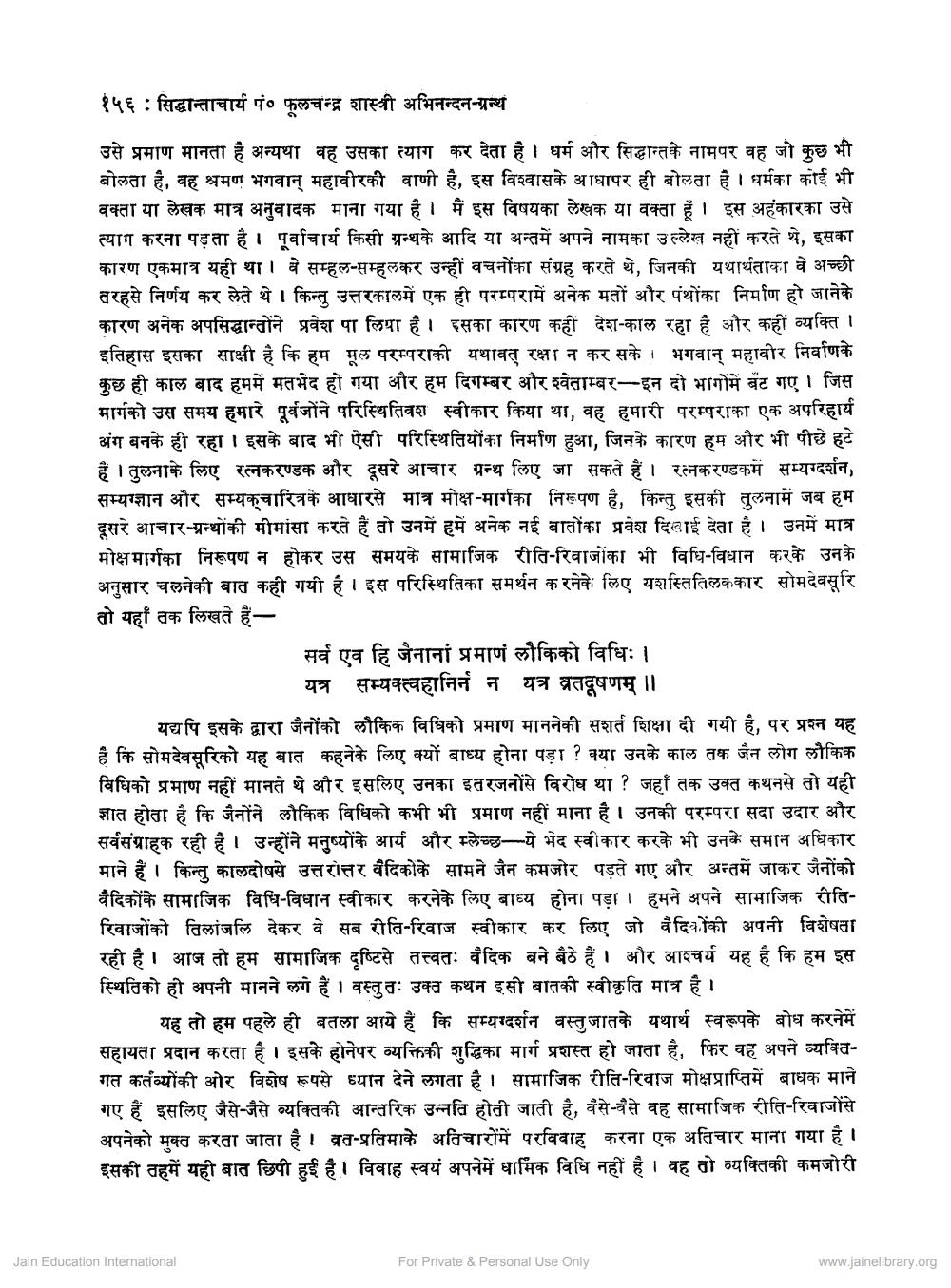________________
१५६ : सिद्धान्ताचार्य पं० फूलचन्द्र शास्त्री अभिनन्दन ग्रन्थ
उसे प्रमाण मानता है अन्यथा वह उसका त्याग कर देता है । धर्म और सिद्धान्त के नामपर वह जो कुछ भी बोलता है, वह श्रमण भगवान् महावीरकी वाणी है, इस विश्वासके आधापर ही बोलता है । धर्मका कोई भी वक्ता या लेखक मात्र अनुवादक माना गया है । मैं इस विषयका लेखक या वक्ता हूँ । इस अहंकारका उसे त्याग करना पड़ता है । पूर्वाचार्य किसी ग्रन्थके आदि या अन्तमें अपने नामका उल्लेख नहीं करते थे, इसका कारण एकमात्र यही था । वे सम्हल सम्हलकर उन्हीं वचनोंका संग्रह करते थे, जिनकी यथार्थताका वे अच्छी तरहसे निर्णय कर लेते थे । किन्तु उत्तरकालमें एक ही परम्परामें अनेक मतों और पंथोंका निर्माण हो जानेके कारण अनेक अपसिद्धान्तोंने प्रवेश पा लिया है। इसका कारण कहीं देश-काल रहा है और कहीं व्यक्ति । इतिहास इसका साक्षी है कि हम मूल परम्पराकी यथावत् रक्षा न कर सके। भगवान् महावीर निर्वाणके कुछ ही काल बाद हममें मतभेद हो गया और हम दिगम्बर और श्वेताम्बर- इन दो भागों में बँट गए । जिस मार्गको उस समय हमारे पूर्वजोंने परिस्थितिवश स्वीकार किया था, वह हमारी परम्पराका एक अपरिहार्य अंग बनके ही रहा । इसके बाद भी ऐसी परिस्थितियोंका निर्माण हुआ, जिनके कारण हम और भी पीछे हटे हैं । तुलना के लिए रत्नकरण्डक और दूसरे आचार ग्रन्थ लिए जा सकते हैं । रत्नकरण्डकमें सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र के आधारसे मात्र मोक्ष मार्गका निरूपण है, किन्तु इसकी तुलनामें जब हम दूसरे आचार-ग्रन्थोंकी मीमांसा करते हैं तो उनमें हमें अनेक नई बातोंका प्रवेश दिखाई देता है । उनमें मात्र मोक्षमार्गका निरूपण न होकर उस समय के सामाजिक रीति-रिवाजोंका भी विधि-विधान करके उनके अनुसार चलनेकी बात कही गयी है । इस परिस्थितिका समर्थन करनेके लिए यशस्तितिलककार सोमदेवसूरि तो यहाँ तक लिखते हैं
सर्व एव हि जैनानां प्रमाणं लौकिको विधिः । यत्र सम्यक्त्वहानिर्न न यत्र व्रतदूषणम् ॥
यद्यपि इसके द्वारा जैनोंको लौकिक विधिको प्रमाण माननेकी सशर्त शिक्षा दी गयी है, पर प्रश्न यह है कि सोमदेवसूरिको यह बात कहनेके लिए क्यों बाध्य होना पड़ा ? क्या उनके काल तक जैन लोग लौकिक विधिको प्रमाण नहीं मानते थे और इसलिए उनका इतरजनोंसे विरोध था ? जहाँ तक उक्त कथनसे तो यही ज्ञात होता है कि जैनोंने लौकिक विधिको कभी भी प्रमाण नहीं माना है । उनकी परम्परा सदा उदार और सर्वसंग्राहक रही है । उन्होंने मनुष्योंके आर्य और म्लेच्छ— ये भेद स्वीकार करके भी उनके समान अधिकार माने हैं । किन्तु कालदोषसे उत्तरोत्तर वैदिको के सामने जैन कमजोर पड़ते गए और अन्तमें जाकर जैनोंको वैदिकोंके सामाजिक विधि-विधान स्वीकार करनेके लिए बाध्य होना पड़ा। हमने अपने सामाजिक रीतिरिवाजोंको तिलांजलि देकर वे सब रीति-रिवाज स्वीकार कर लिए जो वैदिकों की अपनी विशेषता रही है । आज तो हम सामाजिक दृष्टिसे तत्त्वतः वैदिक बने बैठे हैं । और आश्चर्य यह है कि हम इस स्थितिको ही अपनी मानने लगे हैं । वस्तुतः उक्त कथन इसी बातकी स्वीकृति मात्र है ।
यह तो हम पहले ही बतला आये हैं कि सम्यग्दर्शन वस्तुजातके यथार्थ स्वरूपके बोध करनेमें सहायता प्रदान करता है । इसके होनेपर व्यक्तिकी शुद्धिका मार्ग प्रशस्त हो जाता है, फिर वह अपने व्यक्तिगत कर्तव्योंकी ओर विशेष रूपसे ध्यान देने लगता है । सामाजिक रीति-रिवाज मोक्षप्राप्ति में बाधक माने गए हैं इसलिए जैसे-जैसे व्यक्तिकी आन्तरिक उन्नति होती जाती है, वैसे-वैसे वह सामाजिक रीति-रिवाजों से अपनेको मुक्त करता जाता है । व्रत प्रतिमाके अतिचारोंमें परविवाह करना एक अतिचार माना गया है । इसकी तहमें यही बात छिपी हुई है। विवाह स्वयं अपनेमें धार्मिक विधि नहीं है । वह तो व्यक्तिकी कमजोरी
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org