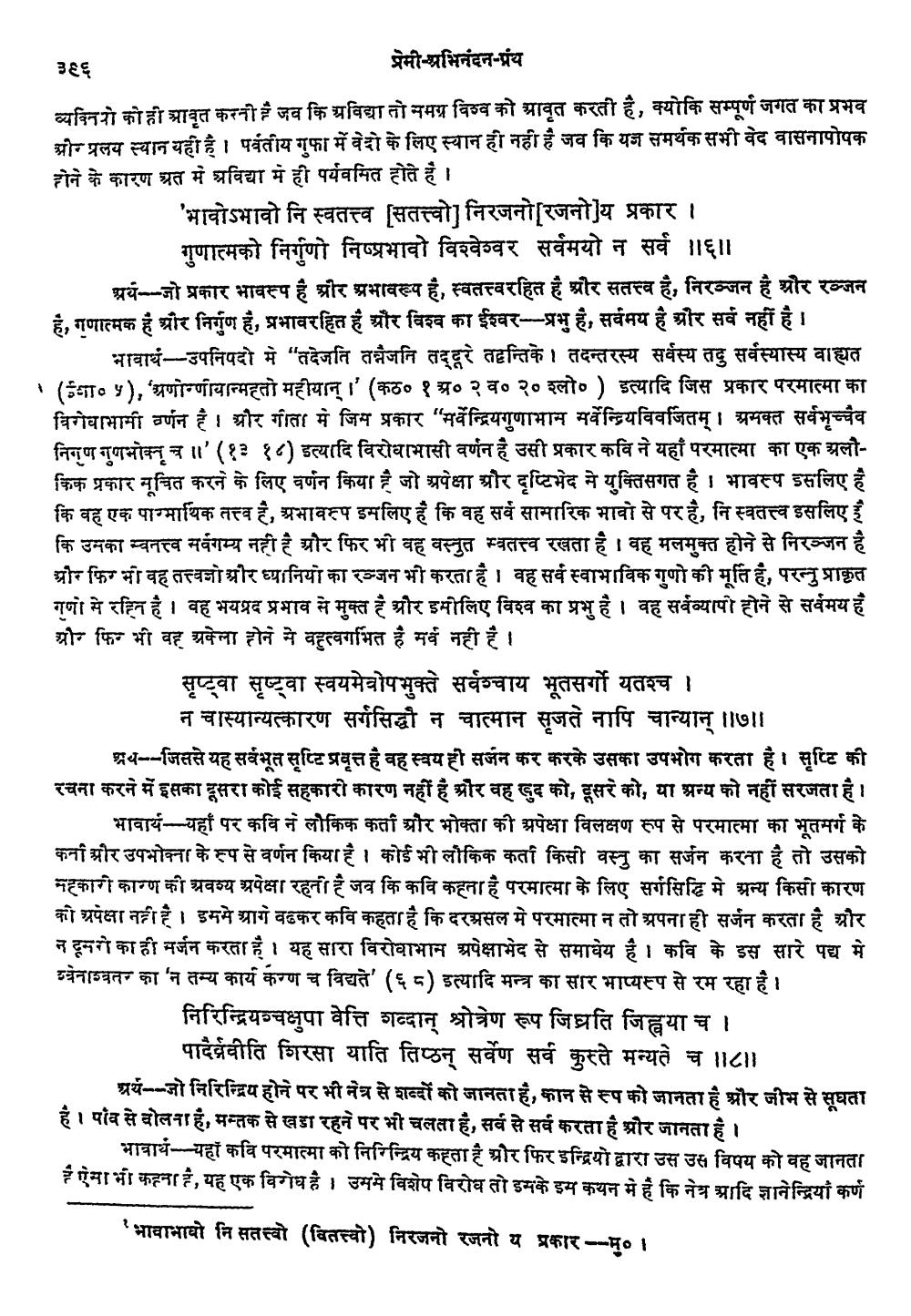________________
प्रेमी-अभिनंदन-प्रंय ३६६ व्यक्तियों को ही आवृत करनी है जब कि अविद्या तो समग्र विश्व को आवृत करती है, क्योकि सम्पूर्ण जगत का प्रभव
और प्रलय स्थान यही है । पर्वतीय गुफा में वेदो के लिए स्थान ही नहीं है जव कि यज समर्थक सभी वेद वासनापोपक होने के कारण अत में अविद्या में ही पर्यवमित होते है ।
'भावोऽभावो नि स्वतत्त्व [सतत्त्वो निरजनो[रजनो]य प्रकार ।
गुणात्मको निर्गुणो निष्प्रभावो विश्वेश्वर सर्वमयो न सर्व ॥६॥ अर्थ-जो प्रकार भावस्प है और प्रभावरूप है, स्वतत्त्वरहित है और सतत्त्व है, निरञ्जन है और रजन है, गणात्मक है और निर्गुण है, प्रभावरहित है और विश्व का ईश्वर-प्रभु है, सर्वमय है और सर्व नहीं है।
भावार्थ-उपनिपदो में "तदेजति तनैजनि तदरे तद्वन्तिके। तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य वाह्यत । (मा०५), 'अणोणीयान्महतो महीयान् ।' (कठ० १ अ० २ व० २० श्लो०) इत्यादि जिस प्रकार परमात्मा का विगेवाभामी वर्णन है । और गीता में जिस प्रकार “मन्द्रियगुणाभाम मन्द्रियविवर्जितम् । अमक्त सर्वभृच्चव निगण गुणभोक्तृ च ।।' (१३ १८) इत्यादि विरोधाभासी वर्णन है उसी प्रकार कवि ने यहां परमात्मा का एक अलौकिक प्रकार मूचित करने के लिए वर्णन किया है जो अपेक्षा और दृष्टिभेद ने युक्तिसगत है । भावस्प इसलिए है कि वह एक पारमार्थिक तत्त्व है, अभावस्प इमलिए है कि वह सर्व सामारिक भावो से पर है, नि स्वतत्त्व इसलिए है कि उनका स्वतत्त्व सर्वगम्य नहीं है और फिर भी वह वस्तुत स्वतत्त्व रखता है । वह मलमुक्त होने से निरञ्जन है और फिर भी वह तत्त्वज्ञो और ध्यानियो का रजन भी करता है। वह सर्व स्वाभाविक गुणो की मूर्ति है, परन्तुप्राकृत गुणों से रहित है। वह भयप्रद प्रभाव से मुक्त है और इमोलिए विश्व का प्रभु है । वह सर्वव्यापी होने से सर्वमय है और फिर भी वह अकेला होने ने वहुत्वभित है मर्व नहीं है।।
सृष्ट्वा सृष्ट्वा स्वयमेवोपभुक्ते सर्वश्चाय भूतसर्गो यतश्च ।
न चास्यान्यत्कारण सर्गसिद्धौ न चात्मान सृजते नापि चान्यान् ॥७॥ श्रय--जिससे यह सर्वभूत सृष्टि प्रवृत्त है वह स्वय ही सर्जन कर करके उसका उपभोग करता है। सृष्टि की रचना करने में इसका दूसरा कोई सहकारी कारण नहीं है और वह खुद को, दूसरे को, या अन्य को नहीं सरजता है।
भावार्य-यहाँ पर कवि ने लौकिक कर्ता और भोक्ता की अपेक्षा विलक्षण रूप से परमात्मा का भूतमर्ग के का और उपभोक्ता के रूप से वर्णन किया है। कोई भी लौकिक कर्ता किसी वस्तु का सर्जन करता है तो उसको नहकारी कारण की अवश्य अपेक्षा रहती है जब कि कवि कहता है परमात्मा के लिए सर्गसिद्धि मे अन्य किसी कारण को अपेक्षा नहीं है। इसमे आगे बढकर कवि कहता है कि दरअसल मे परमात्मा न तो अपना ही सर्जन करता है और न दूनगे का ही मर्जन करता है । यह सारा विरोधाभान अपेक्षाभेद से समाधेय है। कवि के इस सारे पद्य मे ग्वनाश्वतर का 'न तम्य कार्य कंग्ण च विद्यते' (६८) इत्यादि मन्त्र का सार भाप्यस्प से रम रहा है।
निरिन्द्रियश्चक्षुपा वेत्ति शब्दान् श्रोत्रेण रूप जिघ्रति जिह्वया च ।
पादैर्ब्रवीति शिरसा याति तिष्ठन् सर्वेण सर्व कुरते मन्यते च ॥८॥ अर्थ--जो निरिन्द्रिय होने पर भी नेत्र से शब्दों को जानता है, कान से स्प को जानता है और जीभ से सूघता है। पांव से बोलना है, मन्तक से खडा रहने पर भी चलता है, सर्व से सर्व करता है और जानता है।
भावार्थ-यहाँ कवि परमात्मा को निरिन्द्रिय कहता है और फिर इन्द्रियो द्वारा उस उस विषय को वह जानता है ऐमा भी कहना है, यह एक विरोध है । उममे विशेष विरोध तो इसके इस कथन मे है कि नेत्र आदि ज्ञानेन्द्रियां कर्ण
'भावाभायो नि सतत्त्वो (वितत्त्वो) निरजनो रजनो य प्रकार--म० ।