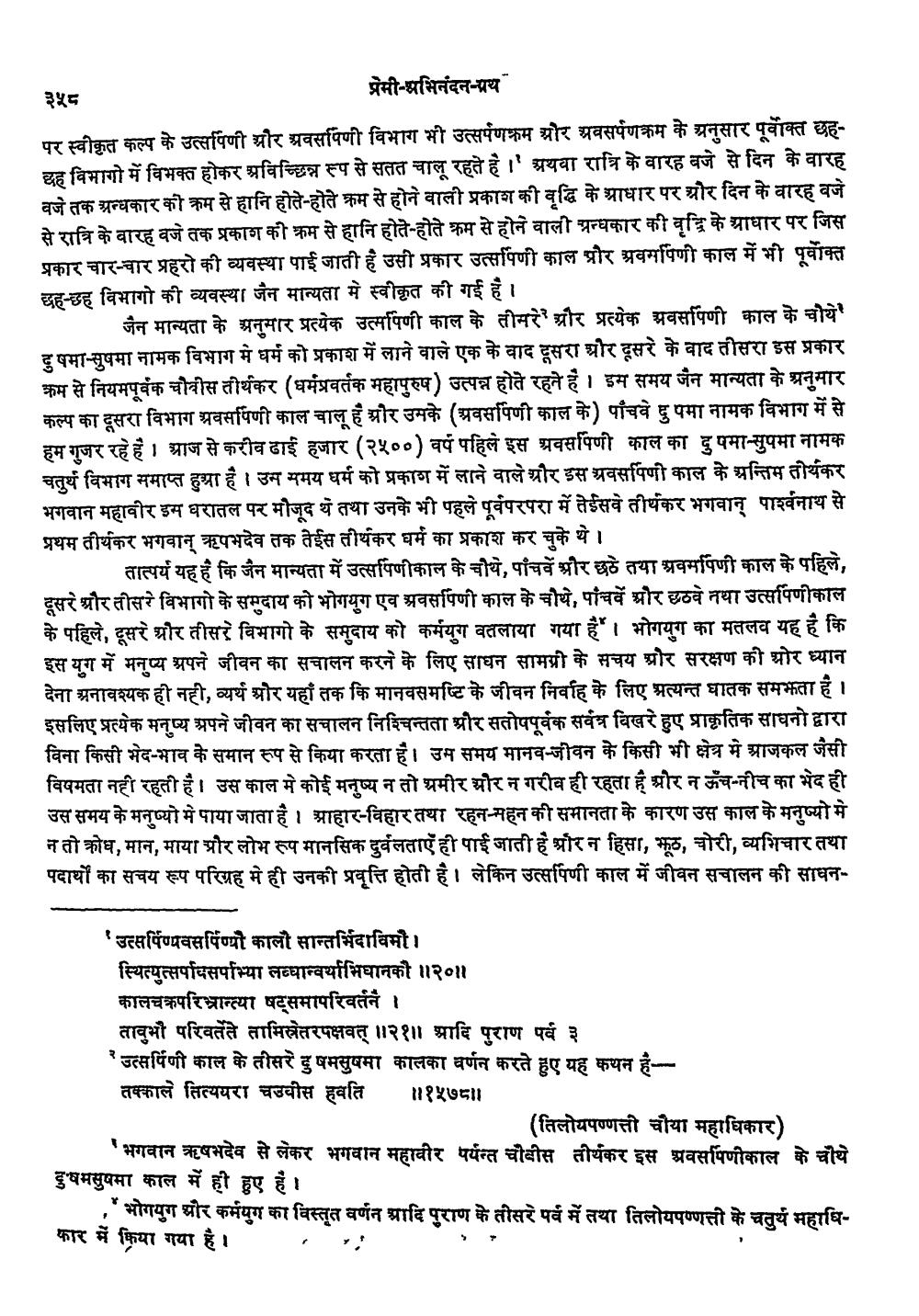________________
३५८
प्रेमी-अभिनंदन-प्रथ पर स्वीकृत कल्प के उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी विभाग भी उत्सर्पणक्रम और अवसर्पणक्रम के अनुसार पूर्वोक्त छहछह विभागो में विभक्त होकर अविच्छिन्न रूप से सतत चालू रहते है ।' अथवा रात्रि के वारह बजे से दिन के वारह वजे तक अन्धकार को क्रम से हानि होते-होते क्रम से होने वाली प्रकाश की वृद्धि के आधार पर और दिन के बारह बजे से रात्रि के वारह बजे तक प्रकाश की क्रम से हानि होते-होते क्रम से होने वाली अन्धकार की वृद्धि के आधार पर जिस प्रकार चार-चार प्रहरो की व्यवस्था पाई जाती है उसी प्रकार उत्सर्पिणी काल और अवपिणी काल में भी पूर्वोक्त छह-छह विभागो की व्यवस्था जैन मान्यता मे स्वीकृत की गई है।
जैन मान्यता के अनुसार प्रत्येक उमर्पिणी काल के तीसरे और प्रत्येक अवसर्पिणी काल के चौथे दुषमा-सुषमा नामक विभाग मे धर्म को प्रकाश में लाने वाले एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा इस प्रकार क्रम से नियमपूर्वक चौबीस तीर्थकर (धर्मप्रवर्तक महापुरुष) उत्पन्न होते रहते है। इस समय जैन मान्यता के अनुमार कल्प का दूसरा विभाग अवसर्पिणी काल चालू है और उसके (अवसर्पिणी काल के) पाँचवे दुपमा नामक विभाग में से हम गुजर रहे है। आज से करीब ढाई हजार (२५००) वर्ष पहिले इस अवसर्पिणी काल का दुपमा-सुपमा नामक चतुर्थ विभाग ममाप्त हुआ है । उस समय धर्म को प्रकाश में लाने वाले और इस अवसर्पिणी काल के अन्तिम तीर्थकर भगवान महावीर इस धरातल पर मौजूद थे तथा उनके भी पहले पूर्वपरपरा में तेईसवे तीर्थकर भगवान् पार्श्वनाथ से प्रथम तीर्थकर भगवान् ऋपभदेव तक तेईस तीर्थकर धर्म का प्रकाश कर चुके थे।
तात्पर्य यह है कि जैन मान्यता में उत्सर्पिणीकाल के चौथे, पांचवें और छठे तथा अवमर्पिणी काल के पहिले, दूसरे और तीसरे विभागो के समुदाय को भोगयुग एव अवसर्पिणी काल के चौथे, पांचवें और छठवे नथा उत्सर्पिणीकाल के पहिले, दूसरे और तीसरे विभागो के समुदाय को कर्मयुग वतलाया गया है। भोगयुग का मतलव यह है कि इस युग में मनुष्य अपने जीवन का सचालन करने के लिए साधन सामग्री के सचय और सरक्षण की ओर ध्यान देना अनावश्यक ही नहीं, व्यर्थ और यहां तक कि मानवसमष्टि के जीवन निर्वाह के लिए अत्यन्त घातक समझता है । इसलिए प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन का सचालन निश्चिन्तता और सतोपपूर्वक सर्वत्र विखरे हुए प्राकृतिक साधनो द्वारा विना किसी भेद-भाव के समान रूप से किया करता है। उस समय मानव-जीवन के किसी भी क्षेत्र मे आजकल जैसी विषमता नहीं रहती है। उस काल मे कोई मनुष्य न तो अमीर और न गरीब ही रहता है और न ऊंच-नीच का भेद ही उस समय के मनुष्यो मे पाया जाता है। आहार-विहार तथा रहन-महन की समानता के कारण उस काल के मनुष्यो मे न तो क्रोध, मान, माया और लोभ रूप मानसिक दुर्वलताएँ ही पाई जाती है और न हिसा, झूठ, चोरी, व्यभिचार तथा पदार्थों का सचय रूप परिग्रह मे ही उनकी प्रवृत्ति होती है। लेकिन उत्सर्पिणी काल में जीवन सचालन की साधन
'उत्सर्पिण्यवसर्पियो कालो सान्तर्भिदाविमौ। स्थित्युत्सयसभ्यिा लब्धान्वर्थाभिधानको ॥२०॥ कालचक्रपरिभ्रान्त्या षट्समापरिवर्तनै ।। तावुभौ परिवर्तेते तामिस्नेतरपक्षवत् ॥२॥ आदि पुराण पर्व ३ 'उत्सर्पिणी काल के तीसरे दुषमसुषमा कालका वर्णन करते हुए यह कथन हैतक्काले तित्ययरा चउवीस हवति ॥१५७८॥
(तिलोयपण्णत्ती चौया महाधिकार) 'भगवान ऋषभदेव से लेकर भगवान महावीर पर्यन्त चौबीस तीर्थकर इस अवसर्पिणीकाल के चौथे दुषमसुषमा काल में ही हुए है।
* भोगयुग और कर्मयुग का विस्तृत वर्णन आदि पुराण के तीसरे पर्व में तथा तिलोयपण्णत्तो के चतुर्य महाधिकार में किया गया है।