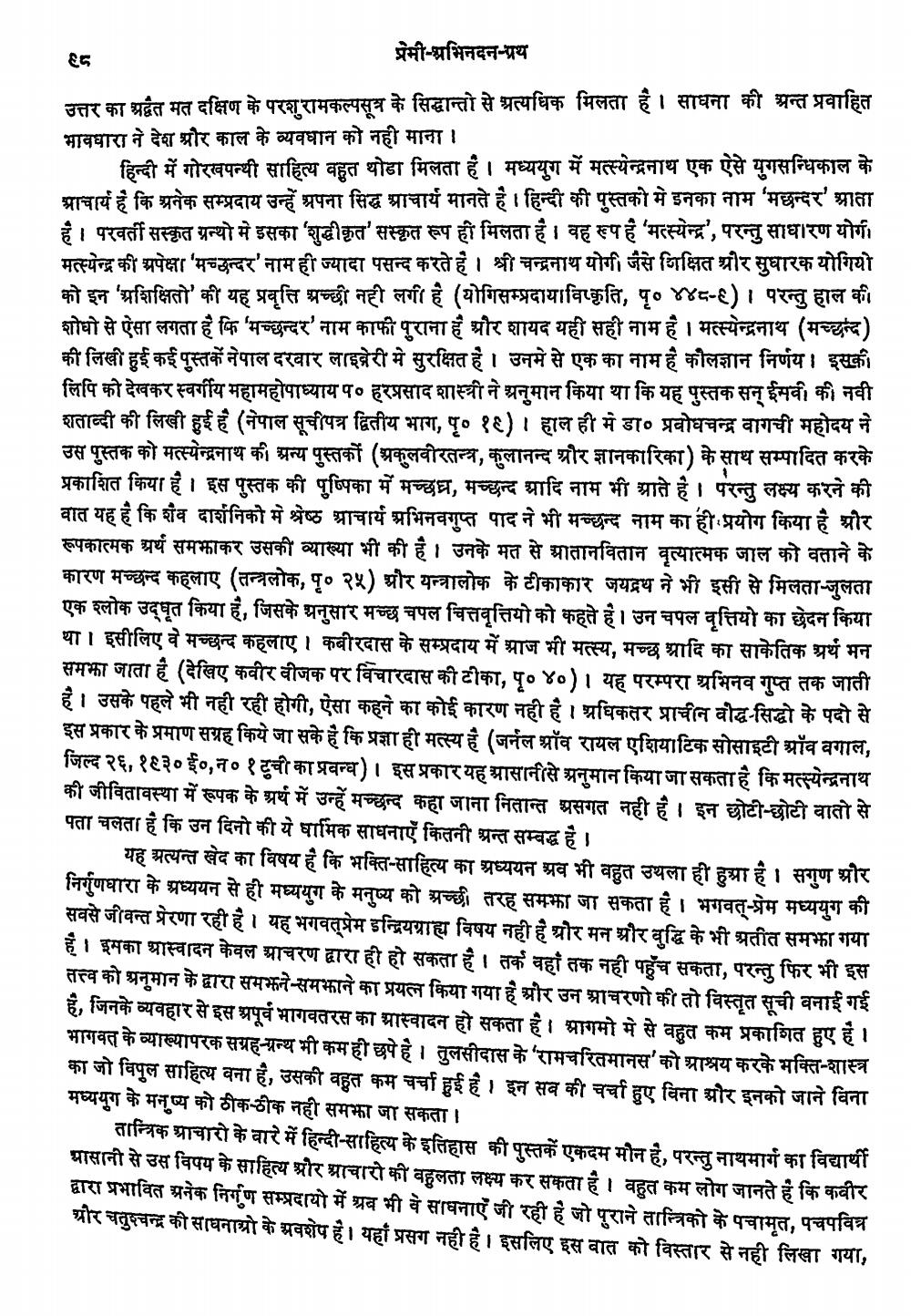________________
प्रेमी-अभिनदन-प्रथ ६८ उत्तर का अद्वैत मत दक्षिण के परशुरामकल्पसूत्र के सिद्धान्तो से अत्यधिक मिलता है। साधना की अन्त प्रवाहित भावधारा ने देश और काल के व्यवधान को नहीं माना।
हिन्दी में गोरखपन्थी साहित्य बहुत थोडा मिलता है। मध्ययुग में मत्स्येन्द्रनाथ एक ऐसे युगसन्धिकाल के आचार्य है कि अनेक सम्प्रदाय उन्हें अपना सिद्ध प्राचार्य मानते है । हिन्दी की पुस्तको मे इनका नाम 'मछन्दर' आता है। परवर्ती सस्कृत ग्रन्थो मे इसका शुद्धीकृत' सस्कृत रूप ही मिलता है । वह रूप है 'मत्स्येन्द्र', परन्तु साधारण योग मत्स्येन्द्र की अपेक्षा 'मच्छन्दर' नाम ही ज्यादा पसन्द करते है । श्री चन्द्रनाथ योगी जैसे गिक्षित और सुधारक योगियो को इन 'अशिक्षितो' की यह प्रवृत्ति अच्छी नहीं लगी है (योगिसम्प्रदायाविष्कृति, पृ० ४४८-९)। परन्तु हाल की शोधो से ऐसा लगता है कि मच्छन्दर' नाम काफी पुराना है और शायद यही सही नाम है । मत्स्येन्द्रनाथ (मच्छन्द) की लिखी हुई कई पुस्तकें नेपाल दरवार लाइब्रेरी मे सुरक्षित है । उनमे से एक का नाम है कौलज्ञान निर्णय। इसकी लिपि को देखकर स्वर्गीय महामहोपाध्याय प० हरप्रसाद शास्त्री ने अनुमान किया था कि यह पुस्तक सन् ईमवी की नवी शताब्दी की लिखी हुई है (नेपाल सूचीपत्र द्वितीय भाग, पृ० १९)। हाल ही में डा० प्रबोधचन्द्र वागची महोदय ने उस पुस्तक को मत्स्येन्द्रनाथ की अन्य पुस्तकों (अकुलवीरतन्त्र, कुलानन्द और ज्ञानकारिका) के साथ सम्पादित करके प्रकाशित किया है। इस पुस्तक की पुष्पिका में मच्छघ्र, मच्छन्द आदि नाम भी आते है। परन्तु लक्ष्य करने की वात यह है कि शव दार्शनिको मे श्रेष्ठ प्राचार्य अभिनवगुप्त पाद ने भी मच्छन्द नाम का ही प्रयोग किया है और रूपकात्मक अर्थ समझाकर उसकी व्याख्या भी की है। उनके मत से आतानवितान वृत्यात्मक जाल को बताने के कारण मच्छन्द कहलाए (तन्त्रलोक, पृ० २५) और यन्त्रालोक के टीकाकार जयद्रथ ने भी इसी से मिलता-जुलता एक श्लोक उद्धृत किया है, जिसके अनुसार मच्छ चपल चित्तवृत्तियो को कहते है। उन चपल वृत्तियो का छेदन किया था। इसीलिए वे मच्छन्द कहलाए। कबीरदास के सम्प्रदाय में आज भी मत्स्य, मच्छ आदि का साकेतिक अर्थ मन समझा जाता है (देखिए कवीर वीजक पर विचारदास की टीका, पृ० ४०)। यह परम्परा अभिनव गुप्त तक जाती है। उसके पहले भी नही रही होगी, ऐसा कहने का कोई कारण नही है। अधिकतर प्राचीन वौद्ध-सिद्धो के पदो से इस प्रकार के प्रमाण सग्रह किये जा सके है कि प्रज्ञा ही मत्स्य है (जर्नल ऑव रायल एशियाटिक सोसाइटी ऑव वगाल, जिल्द २६, १६३० ई०,न०१टुची का प्रबन्ध)। इस प्रकार यह आसानी से अनुमान किया जा सकता है कि मत्स्येन्द्रनाथ की जीवितावस्था में रूपक के अर्थ में उन्हें मच्छन्द कहा जाना नितान्त असगत नही है। इन छोटी-छोटी बातो से पता चलता है कि उन दिनो की ये धार्मिक साधनाएँ कितनी अन्त सम्बद्ध है।
यह अत्यन्त खेद का विषय है कि भक्ति-साहित्य का अध्ययन अव भी बहुत उथला ही हुआ है । सगुण और निर्गुणधारा के अध्ययन से ही मध्ययुग के मनुष्य को अच्छी तरह समझा जा सकता है। भगवत्-प्रेम मध्ययुग की सवसे जीवन्त प्रेरणा रही है। यह भगवत्प्रेम इन्द्रियग्राह्य विषय नही है और मन और बुद्धि के भी अतीत समझा गया है। इसका प्रास्वादन केवल आचरण द्वारा ही हो सकता है । तर्क वहां तक नही पहुंच सकता, परन्तु फिर भी इस तत्त्व को अनुमान के द्वारा समझने-समझाने का प्रयल किया गया है और उन पाचरणो की तो विस्तृत सूची बनाई गई है, जिनके व्यवहार से इस अपूर्व भागवतरस का पास्वादन हो सकता है। प्रागमो मे से बहुत कम प्रकाशित हुए है। भागवत के व्याख्यापरक सग्रह-ग्रन्थ भी कम ही छपे है। तुलसीदास के 'रामचरितमानस' को प्राश्रय करके भक्ति-शास्त्र का जो विपुल साहित्य बना है, उसकी वहुत कम चर्चा हुई है। इन सब की चर्चा हुए विना और इनको जाने विना मध्ययुग के मनुष्य को ठीक-ठीक नही समझा जा सकता।
तान्त्रिक प्राचारो के बारे में हिन्दी-साहित्य के इतिहास की पुस्तकें एकदम मौन है, परन्तु नाथमार्ग का विद्यार्थी मासानी से उस विषय के साहित्य और प्राचारो की बहुलता लक्ष्य कर सकता है। बहुत कम लोग जानते है कि कवीर द्वारा प्रभावित अनेक निर्गुण सम्प्रदायो में अब भी वे साधनाएं जी रही है जो पुराने तान्त्रिको के पचामृत, पचपवित्र और चतुश्चन्द्र की साधनायो के अवशेप है। यहां प्रसग नहीं है। इसलिए इस बात को विस्तार से नहीं लिखा गया,