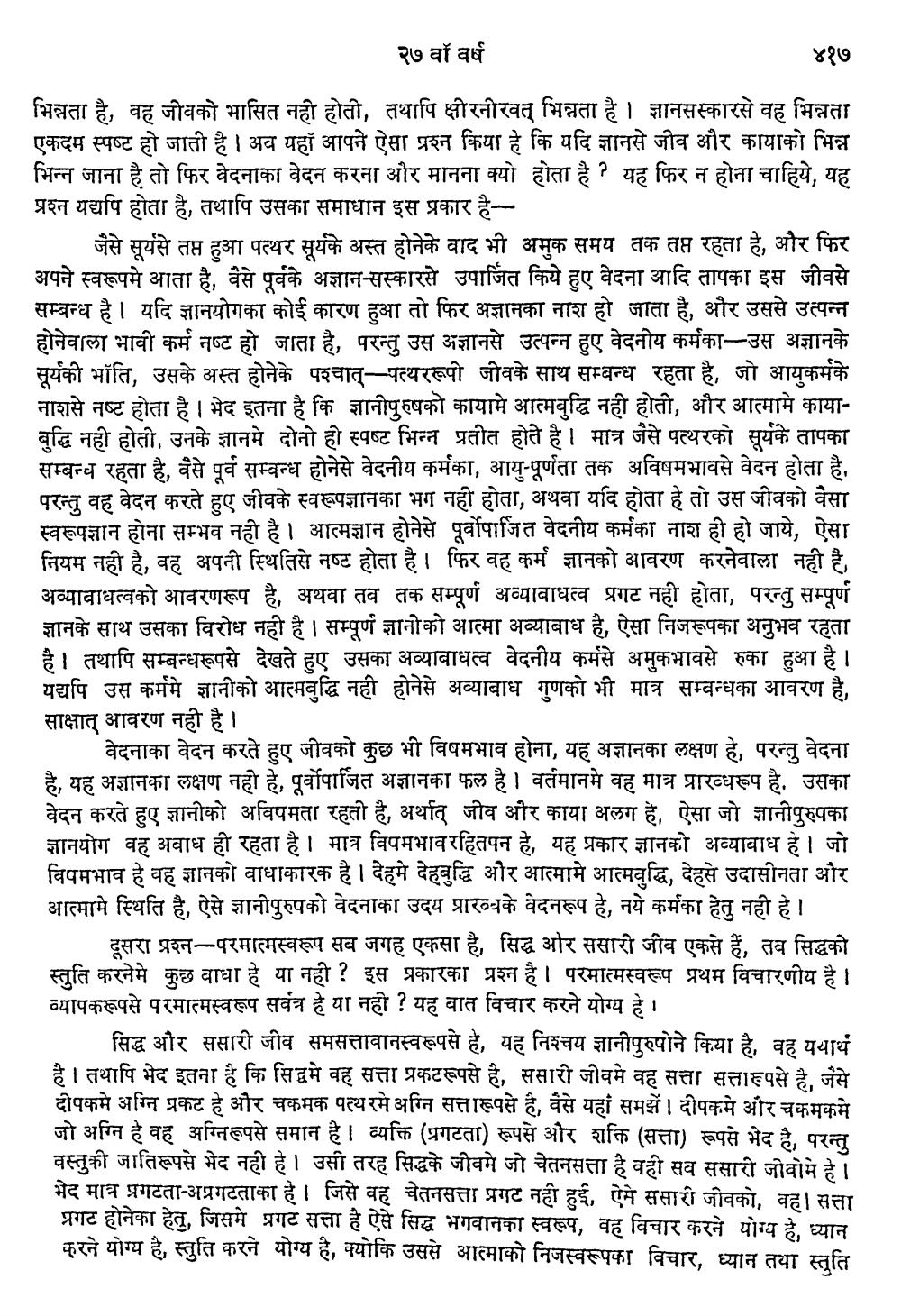________________
२७ वॉ वर्ष
४१७
भिन्नता है, वह जीवको भासित नही होती, तथापि क्षीरनीरवत् भिन्नता है। ज्ञानसस्कारसे वह भिन्नता एकदम स्पष्ट हो जाती है । अव यहाँ आपने ऐसा प्रश्न किया है कि यदि ज्ञानसे जीव और कायाको भिन्न भिन्न जाना है तो फिर वेदनाका वेदन करना और मानना क्यो होता है ? यह फिर न होना चाहिये, यह प्रश्न यद्यपि होता है, तथापि उसका समाधान इस प्रकार है
जैसे सूर्यसे तप्त हआ पत्थर सूर्यके अस्त होनेके बाद भी अमुक समय तक तप्त रहता है, और फिर अपने स्वरूपमे आता है, वैसे पूर्वके अज्ञान-सस्कारसे उपार्जित किये हुए वेदना आदि तापका इस जीवसे सम्बन्ध है। यदि ज्ञानयोगका कोई कारण हुआ तो फिर अज्ञानका नाश हो जाता है, और उससे उत्पन्न होनेवाला भावी कर्म नष्ट हो जाता है, परन्तु उस अज्ञानसे उत्पन्न हुए वेदनोय कर्मका-उस अज्ञानके सूर्यकी भाँति, उसके अस्त होनेके पश्चात्-पत्थररूपी जीवके साथ सम्बन्ध रहता है, जो आयुकर्मके नाशसे नष्ट होता है । भेद इतना है कि ज्ञानीपुरुषको कायामे आत्मबुद्धि नही होती, और आत्मामे कायाबुद्धि नही होती, उनके ज्ञानमे दोनो ही स्पष्ट भिन्न प्रतीत होते है। मात्र जैसे पत्थरको सूर्यके तापका सम्बन्ध रहता है, वैसे पूर्व सम्बन्ध होनेसे वेदनीय कर्मका, आयु-पूर्णता तक अविषमभावसे वेदन होता है, परन्तु वह वेदन करते हुए जीवके स्वरूपज्ञानका भग नही होता, अथवा यदि होता हे तो उस जीवको वैसा स्वरूपज्ञान होना सम्भव नही है। आत्मज्ञान होनेसे पूर्वोपार्जित वेदनीय कर्मका नाश ही हो जाये, ऐसा नियम नही है, वह अपनी स्थितिसे नष्ट होता है। फिर वह कर्म ज्ञानको आवरण करनेवाला नही है, अव्यावाधत्वको आवरणरूप है, अथवा तब तक सम्पूर्ण अव्यावाधत्व प्रगट नही होता, परन्तु सम्पूर्ण ज्ञानके साथ उसका विरोध नही है । सम्पूर्ण ज्ञानोको आत्मा अव्याबाध है, ऐसा निजरूपका अनुभव रहता है। तथापि सम्बन्धरूपसे देखते हुए उसका अव्यावाधत्व वेदनीय कर्मसे अमुकभावसे रुका हुआ है। यद्यपि उस कर्ममे ज्ञानीको आत्मबुद्धि नही होनेसे अव्यावाध गुणको भी मात्र सम्बन्धका आवरण है, साक्षात् आवरण नहीं है।
वेदनाका वेदन करते हुए जीवको कुछ भी विषमभाव होना, यह अज्ञानका लक्षण है, परन्तु वेदना है, यह अज्ञानका लक्षण नहीं है, पूर्वोपार्जित अज्ञानका फल है। वर्तमानमे वह मात्र प्रारब्धरूप है. उसका वेदन करते हुए ज्ञानीको अविषमता रहती है, अर्थात् जीव और काया अलग है, ऐसा जो ज्ञानीपुरुपका ज्ञानयोग वह अवाध ही रहता है। मात्र विपमभावरहितपन है, यह प्रकार ज्ञानको अव्यावाध है। जो विषमभाव हे वह ज्ञानको वाधाकारक है । देहमे देहबुद्धि और आत्मामे आत्मवुद्धि, देहसे उदासीनता और आत्मामे स्थिति है, ऐसे ज्ञानोपुरुपको वेदनाका उदय प्रारब्धके वेदनरूप है, नये कर्मका हेतु नही है।
दूसरा प्रश्न-परमात्मस्वरूप सब जगह एकसा है, सिद्ध ओर ससारी जीव एकसे हैं, तब सिद्धको स्तुति करनेमे कुछ बाधा हे या नहीं ? इस प्रकारका प्रश्न है। परमात्मस्वरूप प्रथम विचारणीय है। व्यापकरूपसे परमात्मस्वरूप सर्वत्र हे या नहीं ? यह बात विचार करने योग्य है ।
सिद्ध और ससारी जीव समसत्तावानस्वरूपसे है, यह निश्चय ज्ञानीपुरुषोने किया है, वह यथार्थ है। तथापि भेद इतना है कि सिद्वमे वह सत्ता प्रकटरूपसे है, ससारी जीवमे वह सत्ता सत्तारूपसे है, जैसे दीपकमे अग्नि प्रकट हे और चकमक पत्थरमे अग्नि सत्तारूपसे है, वैसे यहां समझें। दीपकमे और चकमकमे जो अग्नि हे वह अग्निरूपसे समान है। व्यक्ति (प्रगटता) रूपसे और शक्ति (सत्ता) रूपसे भेद है, परन्तु वस्तुकी जातिरूपसे भेद नही है । उसी तरह सिद्धके जीवमे जो चेतनसत्ता है वही सव ससारी जोवोमे हे । भेद मात्र प्रगटता-अप्रगटताका है । जिसे वह चेतनसत्ता प्रगट नहीं हुई, ऐसे ससारी जीवको, वह। सत्ता प्रगट होनेका हेतु, जिसमे प्रगट सत्ता है ऐसे सिद्ध भगवानका स्वरूप, वह विचार करने योग्य है, ध्यान करने योग्य है, स्तुति करने योग्य है, क्योकि उससे आत्माको निजस्वरूपका विचार, ध्यान तथा स्तुति