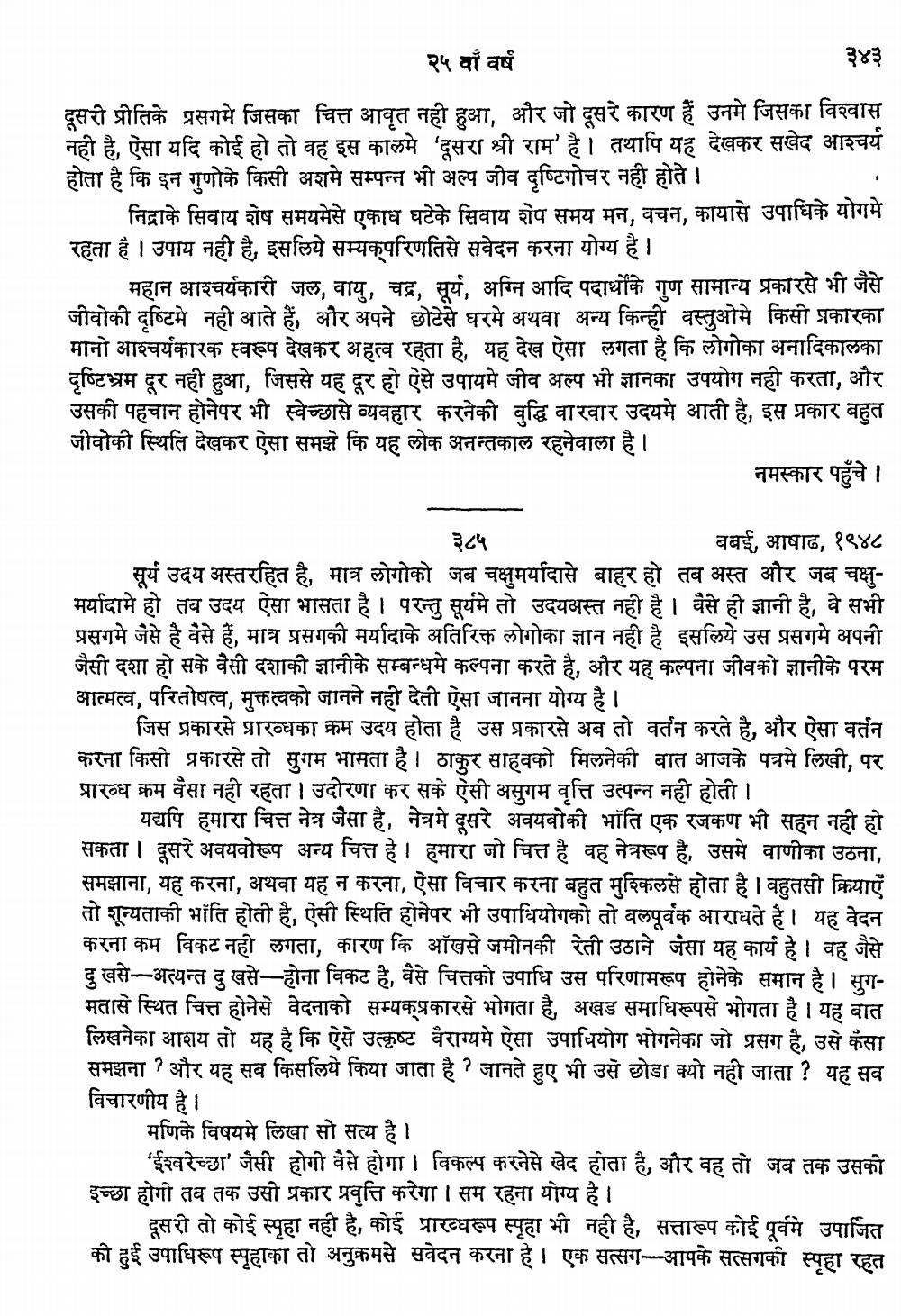________________
२५ वाँ वर्ष
३४३ दूसरी प्रीतिके प्रसगमे जिसका चित्त आवृत नही हुआ, और जो दूसरे कारण हैं उनमे जिसका विश्वास नही है, ऐसा यदि कोई हो तो वह इस कालमे 'दूसरा श्री राम' है। तथापि यह देखकर सखेद आश्चर्य होता है कि इन गुणोके किसी अशमे सम्पन्न भी अल्प जीव दृष्टिगोचर नही होते।
निद्राके सिवाय शेष समयमेसे एकाध घटेके सिवाय शेप समय मन, वचन, कायासे उपाधिके योगमे रहता है । उपाय नही है, इसलिये सम्यक्परिणतिसे सवेदन करना योग्य है।
महान आश्चर्यकारी जल, वायु, चद्र, सूर्य, अग्नि आदि पदार्थोंके गुण सामान्य प्रकारसे भी जैसे जीवोकी दृष्टिमे नही आते हैं, और अपने छोटेसे घरमे अथवा अन्य किन्ही वस्तुओमे किसी प्रकारका मानो आश्चर्यकारक स्वरूप देखकर अहत्व रहता है, यह देख ऐसा लगता है कि लोगोका अनादिकालका दृष्टिभ्रम दूर नहीं हुआ, जिससे यह दूर हो ऐसे उपायमे जीव अल्प भी ज्ञानका उपयोग नहीं करता, और उसकी पहचान होनेपर भी स्वेच्छासे व्यवहार करनेकी बुद्धि वारवार उदयमे आती है, इस प्रकार बहुत जीवोकी स्थिति देखकर ऐसा समझे कि यह लोक अनन्तकाल रहनेवाला है।
नमस्कार पहुंचे।
बबई, आषाढ, १९४८ सूर्य उदय अस्तरहित है, मात्र लोगोको जब चक्षुमर्यादासे बाहर हो तब अस्त और जब चक्षुमर्यादामे हो तब उदय ऐसा भासता है। परन्तु सूर्यमे तो उदयमस्त नही है। वैसे ही ज्ञानी है, वे सभी प्रसगमे जैसे है वैसे हैं, मात्र प्रसगकी मर्यादाके अतिरिक्त लोगोका ज्ञान नही है इसलिये उस प्रसगमे अपनी जैसी दशा हो सके वैसी दशाको ज्ञानीके सम्बन्धमे कल्पना करते है, और यह कल्पना जीवको ज्ञानीके परम आत्मत्व, परितोषत्व, मुक्तत्वको जानने नही देती ऐसा जानना योग्य है।
जिस प्रकारसे प्रारब्धका क्रम उदय होता है उस प्रकारसे अब तो वर्तन करते है, और ऐसा वर्तन करना किसी प्रकारसे तो सुगम भामता है। ठाकुर साहबको मिलनेकी बात आजके पत्रमे लिखी, पर प्रारब्ध क्रम वैसा नही रहता । उदोरणा कर सके ऐसी असुगम वृत्ति उत्पन्न नहीं होती।
यद्यपि हमारा चित्त नेत्र जैसा है, नेत्रमे दूसरे अवयवोकी भॉति एक रजकण भी सहन नही हो सकता। दूसरे अवयवोरूप अन्य चित्त है। हमारा जो चित्त है वह नेत्ररूप है, उसमे वाणीका उठना, समझाना, यह करना, अथवा यह न करना, ऐसा विचार करना बहुत मुश्किलसे होता है । वहुतसी क्रियाएँ तो शून्यताकी भाँति होती है, ऐसी स्थिति होनेपर भी उपाधियोगको तो बलपूर्वक आराधते है। यह वेदन करना कम विकट नही लगता, कारण कि आँखसे जमोनकी रेती उठाने जैसा यह कार्य है। वह जैसे दु खसे-अत्यन्त दु खसे-होना विकट है, वैसे चित्तको उपाधि उस परिणामरूप होनेके समान है। सुगमतासे स्थित चित्त होनेसे वेदनाको सम्यक्प्रकारसे भोगता है, अखड समाधिरूपसे भोगता है । यह बात लिखनेका आशय तो यह है कि ऐसे उत्कृष्ट वैराग्यमे ऐसा उपाधियोग भोगनेका जो प्रसग है, उसे कैसा समझना ? और यह सब किसलिये किया जाता है ? जानते हुए भी उसे छोडा क्यो नही जाता? यह सव विचारणीय है।
मणिके विषयमे लिखा सो सत्य है।
'ईश्वरेच्छा' जैसी होगी वैसे होगा। विकल्प करनेसे खेद होता है, और वह तो जब तक उसकी इच्छा होगी तब तक उसी प्रकार प्रवृत्ति करेगा । सम रहना योग्य है।
दूसरी तो कोई स्पृहा नही है, कोई प्रारब्धल्प स्पृहा भी नही है, सत्तारूप कोई पूर्वमे उपार्जित को हुई उपाधिरूप स्पृहाका तो अनुक्रमसे सवेदन करना है। एक सत्सग-आपके सत्सगकी स्पृहा रहत