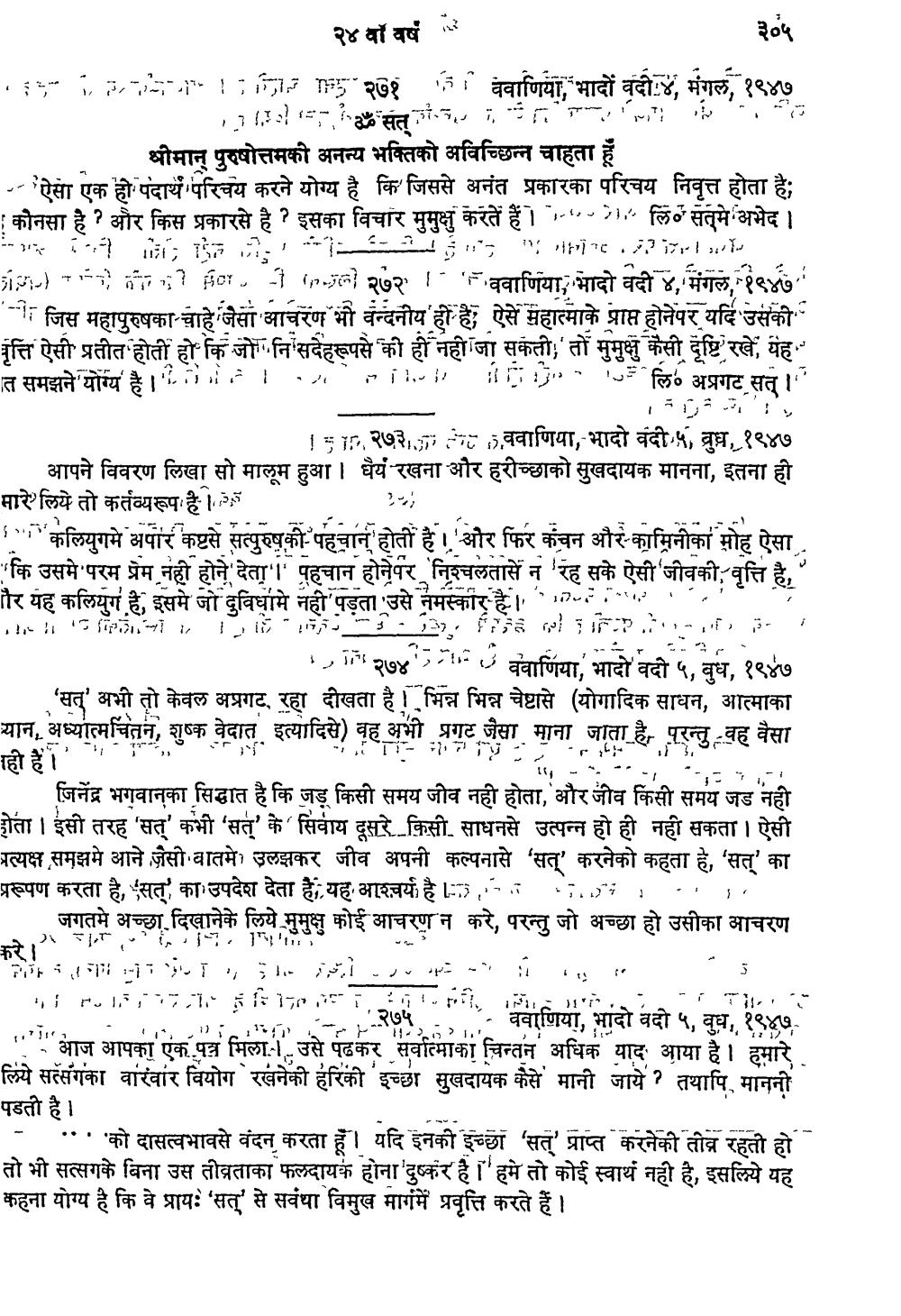________________
२४ वॉ वर्ष
२७१
pr
ॐ सत्
श्रीमान् पुरुषोत्तमकी अनन्य भक्तिको अविच्छिन्न चाहता हूँ
'ऐसा एक हो पदार्थ परिचय करने योग्य है कि जिससे अनंत प्रकारका परिचय निवृत्त होता है; कौनसा है ? और किस प्रकारसे है ? इसका विचार मुमुक्षु करते हैं । लि सत्मे अभेद । Ca Mo Ba A 12 for 1
1
AISH
Pine. T
२७२ । 'F'ववाणिया, भादो वदी ४, मंगल, १९४७ - जिस महापुरुषका चाहे जैसा आचरण भी वन्दनीय हो है; ऐसे महात्मा के प्राप्त होने पर यदि उसकी " वृत्ति ऐसी प्रतीत होती हो कि जो नि सदेहरूपसे की ही नही जा सकती, तो मुमुक्षु कैसी दृष्टि रखें, यह " त समझने योग्य है । लि० अप्रगट सत्
मे 1
1/
३०५
ववाणिया, भादों वदी ४, मंगल, १९४७
D
२७३ववाणिया, भादो वंदी ५, बुध, १९४७ आपने विवरण लिखा सो मालूम हुआ । धैर्य रखना और हरीच्छाको सुखदायक मानना, इतना ही मारे लिये तो कर्तव्य रूप है
22
'
“कलियुगमे अपार कष्टसे सत्पुरुष की पहचान होती है। और फिर कंचन और कामिनीका मोह ऐसा कि उसमे परम प्रेम नही होने देता।' पहचान होनेपर निश्चलतासें न रह सके ऐसी 'जीवकी, वृत्ति है, और यह कलियुग है, इसमे जो दुविधामे नही पड़ता उसे नमस्कार है ।
" }
18
"
करे ।
ܐ ܐ ܐ ܐ ܐ
17 २७४
वाणिया, भादो वदी ५, बुध, १९४७ (योगादिक साधन, आत्माका
'सत्' अभी तो केवल अप्रगढ़, रहा दीखता है। भिन्न भिन्न चेष्टासे यान, अध्यात्मचिंतन, शुष्क वेदात इत्यादिसे) वह अभी प्रगट जैसा माना जाता है, परन्तु वह वैसा ही हैं।
If
Ty
414141
יְז
--
2
t
fee की २७५
11
ار
7
जिनेंद्र भगवानका सिद्धात है कि जड़ किसी समय जीव नही होता, और जीव किसी समय जड नही होता । इसी तरह 'सत्' कभी 'सत्' के ' सिवाय दूसरे किसी साधनसे उत्पन्न हो ही नही सकता । ऐसी प्रत्यक्ष समझमे आने जैसी बातमे उलझकर जीव अपनी कल्पनासे 'सत्' करनेको कहता है, 'सत्' का प्ररूपण करता है, सत् का उपदेश देता है, यह आश्चर्य है -
3
17
7.07 3
जगतमे अच्छा दिखाने के लिये मुमुक्षु कोई आचरण न करे, परन्तु जो अच्छा हो उसीका आचरण
ASP
17
को
5
41
Ti
'ववाणिया, भादो वदी ५, बुध, १९४७'''' आज आपका एक पत्र मिला । उसे पढकर सर्वात्माका चिन्तन अधिक याद आया है । हमारे लिये सत्संगका वारंवार वियोग रखनेकी हरिकी इच्छा सुखदायक कैसे मानी जाये ? तथापि, माननी पडती है ।
'""
'को दासत्वभावसे वंदन करता हूँ । यदि इनकी इच्छा 'सत्' प्राप्त करनेकी तीव्र रहती हो तो भी सत्सगके बिना उस तीव्रताका फलदायक होना दुष्कर है।' हमे तो कोई स्वार्थ नही है, इसलिये यह कहना योग्य है कि वे प्रायः 'सत्' से सर्वथा विमुख मार्ग में प्रवृत्ति करते हैं ।