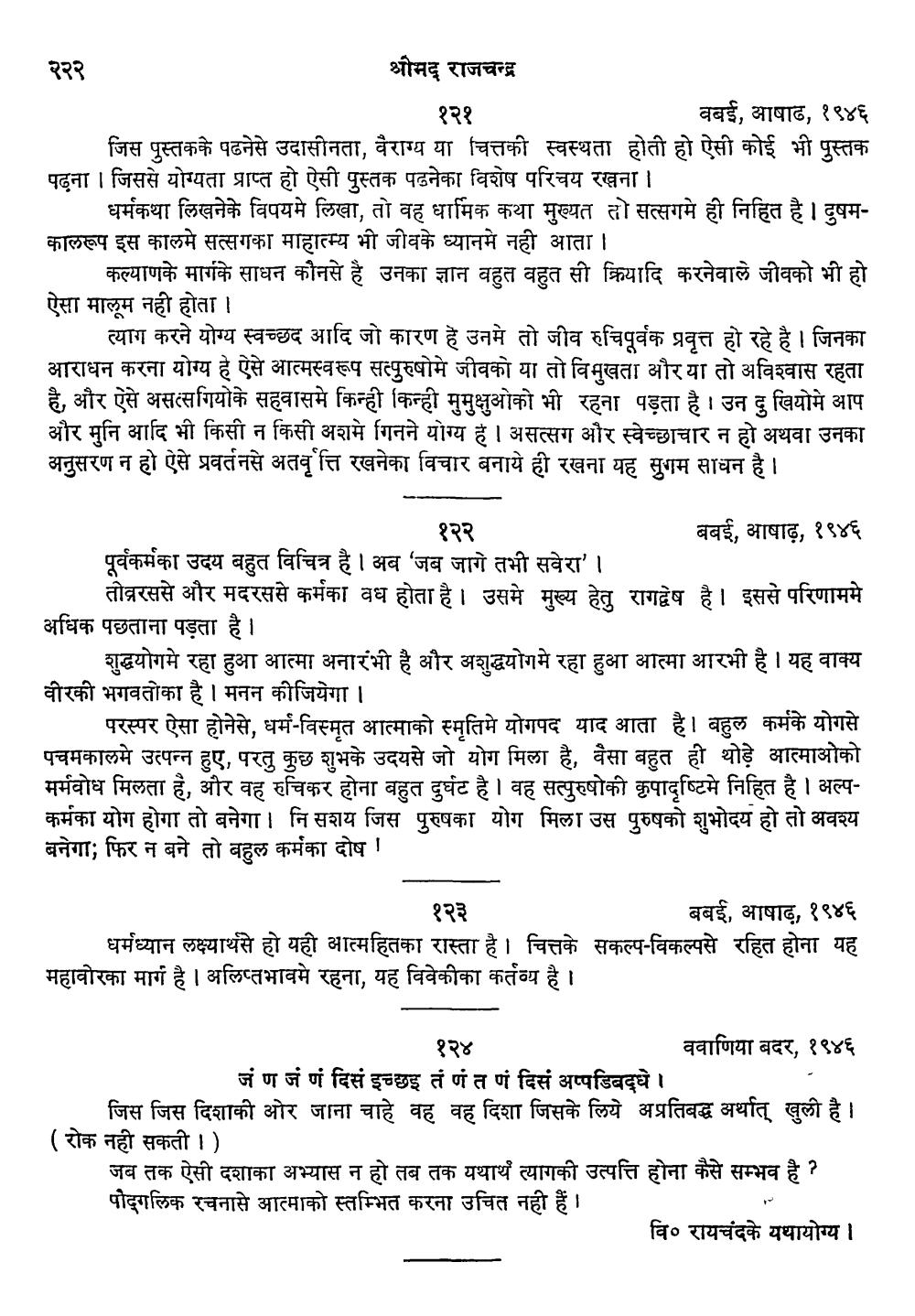________________
श्रीमद राजचन्द्र
१२१
बबई, आषाढ, १९४६ जिस पुस्तक के पढनेसे उदासीनता, वैराग्य या चित्तकी स्वस्थता होती हो ऐसी कोई भी पुस्तक पढ़ना । जिससे योग्यता प्राप्त हो ऐसी पुस्तक पढनेका विशेष परिचय रखना ।
धर्मकथा लिखनेके विपयमे लिखा, तो वह धार्मिक कथा मुख्यत तो सत्सगमे ही निहित है । दुषमकालरूप इस कालमे सत्सगका माहात्म्य भी जीवके ध्यानमे नही आता ।
कल्याणके मार्गके साधन कौनसे है उनका ज्ञान बहुत बहुत सी क्रियादि करनेवाले जीवको भी हो ऐसा मालूम नही होता |
२२२
त्याग करने योग्य स्वच्छद आदि जो कारण है उनमे तो जीव रुचिपूर्वक प्रवृत्त हो रहे है । जिनका आराधन करना योग्य हे ऐसे आत्मस्वरूप सत्पुरुषोमे जीवको या तो विमुखता और या तो अविश्वास रहता है, और ऐसे असत्सगियो के सहवासमे किन्ही किन्ही मुमुक्षुओको भी रहना पड़ता है। उन दुखियोमे आप और मुनि आदि भी किसी न किसी अशमे गिनने योग्य है । असत्सग और स्वेच्छाचार न हो अथवा उनका अनुसरण न हो ऐसे प्रवर्तनसे अतवृत्ति रखनेका विचार बनाये ही रखना यह सुगम साधन है ।
१२२
बबई, आषाढ़, १९४६
पूर्व कर्म का उदय बहुत विचित्र है । अब 'जब जागे तभी सवेरा' । तोव्ररससे और मदरससे कर्मका वध होता है । उसमे मुख्य हेतु रागद्वेष है । इससे परिणाममे अधिक पछताना पड़ता है ।
शुद्धयोगमे रहा हुआ आत्मा अनारंभी है और अशुद्धयोगमे रहा हुआ आत्मा आरभी है । यह वाक्य वीरकी भगवतो का है । मनन कीजियेगा ।
परस्पर ऐसा होनेसे, धर्म-विस्मृत आत्माको स्मृतिमे योगपद याद आता है । बहुल कर्मके योगसे पचमकालमे उत्पन्न हुए, परतु कुछ शुभके उदयसे जो योग मिला है, वैसा बहुत ही थोड़े आत्माओको मर्मबोध मिलता है, और वह रुचिकर होना बहुत दुर्घट है। वह सत्पुरुषोकी कृपादृष्टिमे निहित है । अल्पकर्मका योग होगा तो बनेगा । नि सशय जिस पुरुषका योग मिला उस पुरुषको शुभोदय हो तो अवश्य बनेगा; फिर न बने तो बहुल कर्मका दोष !
१२३
बबई, आषाढ़, १९४६
धर्मध्यान लक्ष्यार्थसे हो यही आत्महितका रास्ता है । चित्तके सकल्प-विकल्पसे रहित होना यह महावोरका मार्ग है । अलिप्तभावमे रहना, यह विवेकीका कर्तव्य है ।
१२४
ववाणिया बदर, १९४६
जंण णं दिसं इच्छइ तं णं त णं दिसं अप्पडिबधे ।
जिस जिस दिशाकी ओर जाना चाहे वह वह दिशा जिसके लिये अप्रतिबद्ध अर्थात् खुली है । ( रोक नही सकती । )
जब तक ऐसी दशाका अभ्यास न हो तब तक यथार्थं त्यागकी उत्पत्ति होना कैसे सम्भव है ? पोद्गलिक रचना से आत्माको स्तम्भित करना उचित नही हैं ।
वि० रायचंदके यथायोग्य |