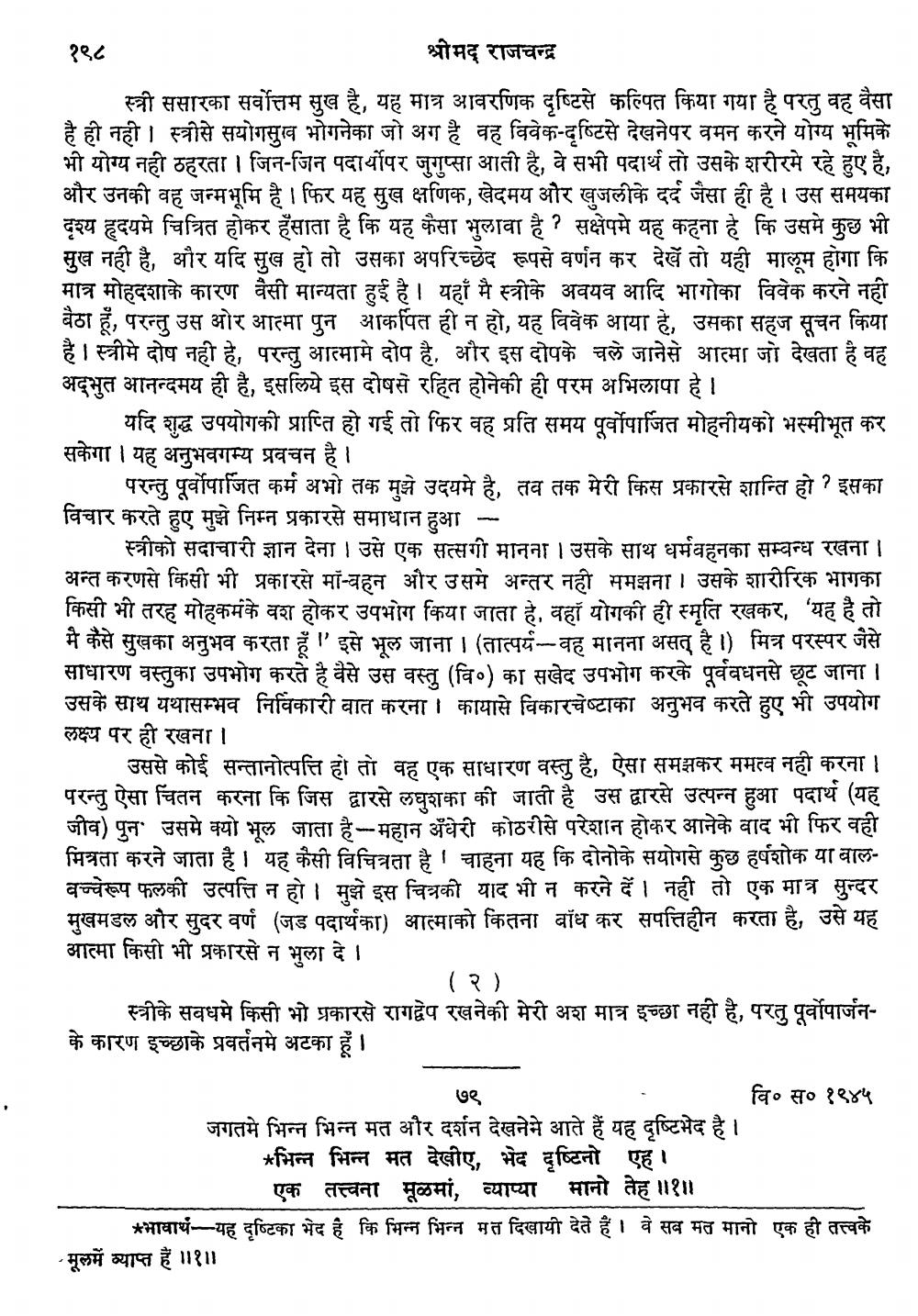________________
श्रीमद् राजचन्द्र
स्त्रीससारका सर्वोत्तम सुख है, यह मात्र आवरणिक दृष्टिसे कल्पित किया गया है परंतु वह वैसा है ही नही । स्त्रीसे सयोगसुख भोगनेका जो अग है वह विवेक - दृष्टिसे देखनेपर वमन करने योग्य भूमिके भी योग्य नही ठहरता । जिन-जिन पदार्थोपर जुगुप्सा आती है, वे सभी पदार्थ तो उसके शरीरमे रहे हुए है, और उनकी वह जन्मभूमि है । फिर यह सुख क्षणिक, खेदमय और खुजलीके दर्द जैसा ही है । उस समयका दृश्य हृदयमे चित्रित होकर हँसाता है कि यह कैसा भुलावा है ? सक्षेपमे यह कहना है कि उसमे कुछ भी सुख नही है, और यदि सुख हो तो उसका अपरिच्छेद रूपसे वर्णन कर देखें तो यही मालूम होगा कि मात्र मोहदशाके कारण वैसी मान्यता हुई है । यहाँ मै स्त्रीके अवयव आदि भागोका विवेक करने नही बैठा हूँ, परन्तु उस ओर आत्मा पुन आकर्षित ही न हो, यह विवेक आया है, उसका सहज सूचन किया है । स्त्री दोष नही है, परन्तु आत्मामे दोप है, और इस दोपके चले जानेसे आत्मा जो देखता है वह अद्भुत आनन्दमय ही है, इसलिये इस दोष से रहित होनेकी ही परम अभिलापा है ।
१९८
यदि शुद्ध उपयोगकी प्राप्ति हो गई तो फिर वह प्रति समय पूर्वोपार्जित मोहनीयको भस्मीभूत कर सकेगा । यह अनुभवगम्य प्रवचन है ।
परन्तु पूर्वोपार्जित कर्म अभी तक मुझे उदयमे है, तब तक मेरी किस प्रकारसे शान्ति हो ? इसका विचार करते हुए मुझे निम्न प्रकारसे समाधान हुआ
स्त्रीको सदाचारी ज्ञान देना । उसे एक सत्सगी मानना । उसके साथ धर्मवहनका सम्बन्ध रखना | अन्तकरणसे किसी भी प्रकारसे माँ-वहन और उसमे अन्तर नहीं समझना । उसके शारीरिक भागका किसी भी तरह मोहकर्मके वश होकर उपभोग किया जाता है, वहाँ योगकी ही स्मृति रखकर, 'यह है तो मे कैसे सुखका अनुभव करता हूँ ।" इसे भूल जाना । (तात्पर्य - वह मानना असत् है ।) मित्र परस्पर जैसे साधारण वस्तुका उपभोग करते है वैसे उस वस्तु (वि०) का सखेद उपभोग करके पूर्वबधनसे छूट जाना । उसके साथ यथासम्भव निर्विकारी बात करना । कायासे विकारचेष्टाका अनुभव करते हुए भी उपयोग लक्ष्य पर ही रखना ।
उससे कोई सन्तानोत्पत्ति हो तो वह एक साधारण वस्तु है, ऐसा समझकर ममत्व नही करना । परन्तु ऐसा चिंतन करना कि जिस द्वारसे लघुशका की जाती है उस द्वारसे उत्पन्न हुआ पदार्थ (यह जीव) पुन उसमे क्यो भूल जाता है - महान अँधेरी कोठरीसे परेशान होकर आनेके बाद भी फिर वही मित्रता करने जाता है । यह कैसी विचित्रता है । चाहना यह कि दोनोके सयोगसे कुछ हर्षशोक या बालबच्चेरूप फलकी उत्पत्ति न हो। मुझे इस चित्रकी याद भी न करने दें। नहीं तो एक मात्र सुन्दर मुखमडल और सुदर वर्ण (जड पदार्थका ) आत्माको कितना बाँध कर सपत्तिहीन करता है, उसे यह आत्मा किसी भी प्रकारसे न भुला दे ।
( २ )
स्त्रीके सबधमे किसी भी प्रकारसे रागद्वेप रखनेकी मेरी अश मात्र इच्छा नही है, परतु पूर्वोपार्जन - के कारण इच्छाके प्रवर्तनमे अटका हूँ ।
७९
जगतमे भिन्न भिन्न मत और दर्शन देखनेने आते हैं यह दृष्टिभेद है । * भिन्न भिन्न मत देखीए, भेद दृष्टिनो एह ।
एक तत्त्वना मूळमां, व्याप्या मानो तेह ॥ १॥ *भावार्थ - यह दृष्टिका भेद है कि भिन्न भिन्न मत दिखायी देते - मूलमें व्याप्त है ||१||
वि० स० १९४५
। वे सब मत मानो एक ही तत्त्वके