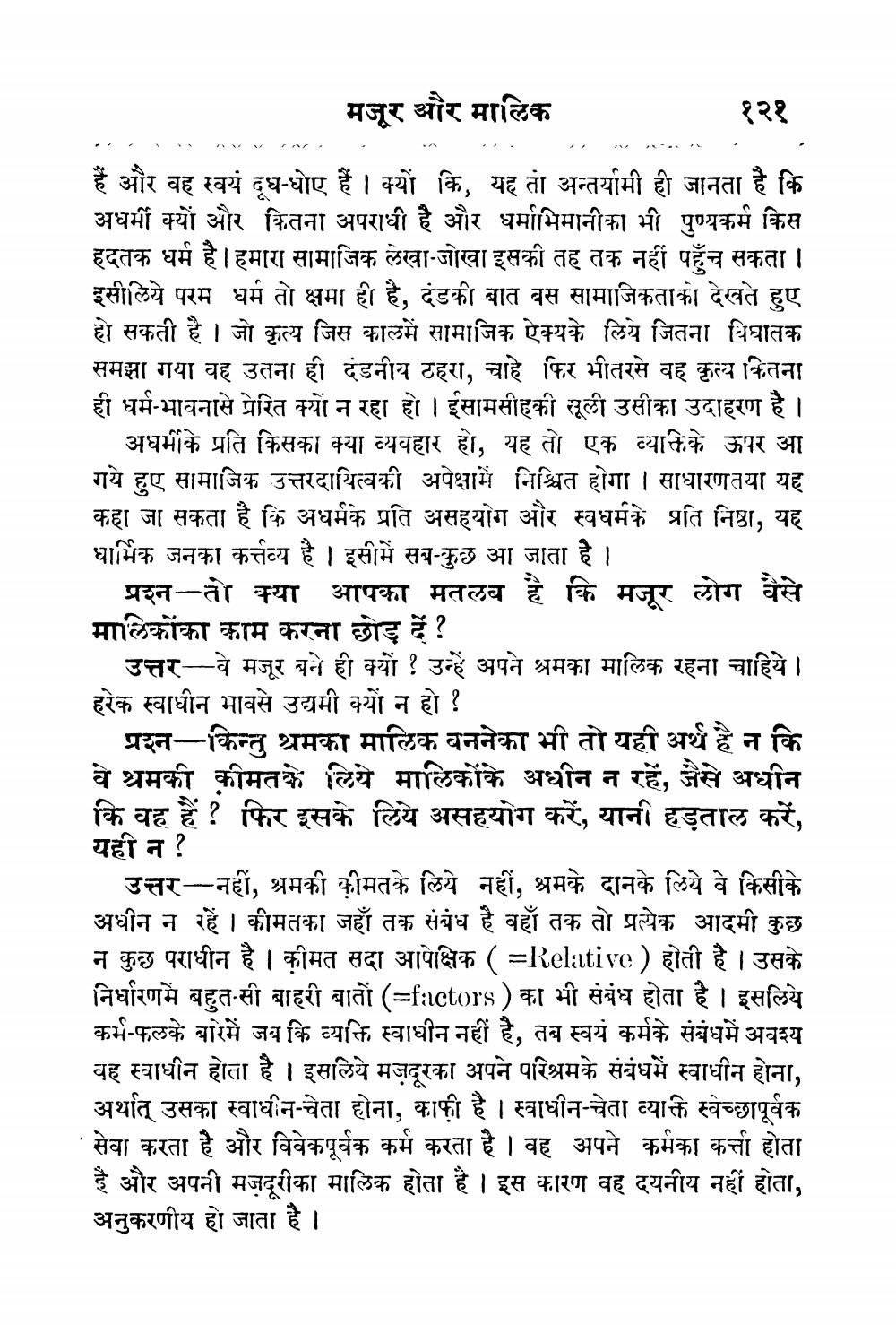________________
मजूर और मालिक
१२१ हैं और वह स्वयं दूध-धोए हैं। क्यों कि, यह तो अन्तर्यामी ही जानता है कि अधर्मी क्यों और कितना अपराधी है और धर्माभिमानीका भी पुण्यकर्म किस हदतक धर्म है । हमारा सामाजिक लेखा-जोखा इसकी तह तक नहीं पहुँच सकता । इसीलिये परम धर्म तो क्षमा ही है, दंडकी बात बस सामाजिकताको देखते हुए हो सकती है । जो कृत्य जिस कालमें सामाजिक ऐक्यके लिये जितना विघातक समझा गया वह उतना ही दंडनीय ठहरा, चाहे फिर भीतरसे वह कृत्य कितना ही धर्म-भावनासे प्रेरित क्यों न रहा हो । ईसामसीहकी सूली उसीका उदाहरण है ।
अधर्मी प्रति किसका क्या व्यवहार हो, यह तो एक व्यक्तिके ऊपर आ गये हुए सामाजिक उत्तरदायित्व की अपेक्षा में निश्चित होगा । साधारणतया यह कहा जा सकता है कि अधर्म के प्रति असहयोग और स्वधर्म के प्रति निष्ठा, यह धार्मिक जनका कर्त्तव्य है । इसी में सब कुछ आ जाता है । प्रश्न - तो क्या आपका मतलब है कि मजूर लोग वैसे मालिकोंका काम करना छोड़ दें ?
उत्तर—वे मजूर बने ही क्यों ? उन्हें अपने श्रमका मालिक रहना चाहिये । हरेक स्वाधीन भावसे उद्यमी क्यों न हो ?
प्रश्न - किन्तु श्रमका मालिक बननेका भी तो यही अर्थ है न कि वे श्रमकी कीमत के लिये मालिकोंके अधीन न रहें, जैसे अर्धान कि वह हैं ? फिर इसके लिये असहयोग करें, यानी हड़ताल करें, यही न ?
उत्तर— नहीं, श्रमकी कीमत के लिये नहीं, श्रमके दानके लिये वे किसीके अधीन न रहें | कीमतका जहाँ तक संबंध है वहाँ तक तो प्रत्येक आदमी कुछ न कुछ पराधीन है । क़ीमत सदा आपेक्षिक ( = Relative ) होती है । उसके निर्धारण में बहुत-सी बाहरी बातों (= factors) का भी संबंध होता है । इसलिये कर्म-फलके बारेमें जब कि व्यक्ति स्वाधीन नहीं है, तब स्वयं कर्मके संबंध में अवश्य वह स्वाधीन होता है । इसलिये मज़दूरका अपने परिश्रम के संबंध में स्वाधीन होना, अर्थात् उसका स्वाधीन-चेता होना, काफी है । स्वाधीन चेता व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक 'सेवा करता है और विवेकपूर्वक कर्म करता है । वह अपने कर्मका कर्त्ता होता है और अपनी मज़दूरीका मालिक होता है । इस कारण वह दयनीय नहीं होता, अनुकरणीय हो जाता है ।
1