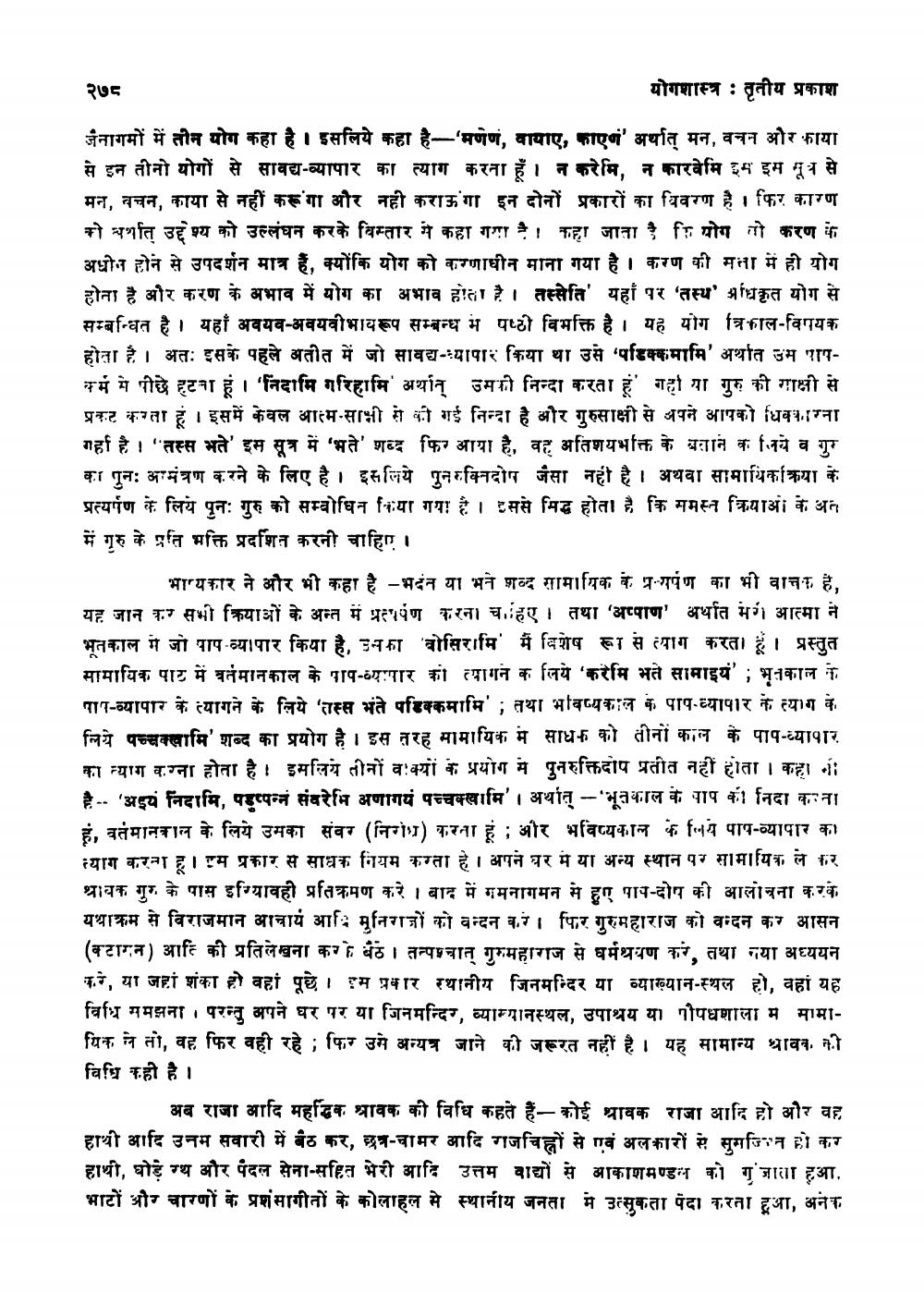________________
२७०
योगशास्त्र : तृतीय प्रकाश
जनागमों में तीन योग कहा है । इसलिये कहा है-'मणेणं, वायाए, कारण' अर्थात् मन, वचन और काया से इन तीनो योगों से सावद्य-व्यापार का त्याग करता हूँ। न करेमि, न कारवेमि इम इम मूत्र से मन, वचन, काया से नहीं करूंगा और नही कराऊंगा इन दोनों प्रकारों का विवरण है । फिर कारण को अर्थात उद्देश्य को उल्लंघन करके विस्तार में कहा गया है। कहा जाता है कि योग को करण के अधीन होने से उपदर्शन मात्र हैं, क्योंकि योग को करणाधीन माना गया है। करण की मना में ही योग होता है और करण के अभाव में योग का अभाव होता है। तस्सेति' यहाँ पर 'तस्थ' अधिकृत योग से सम्बन्धित है। यहाँ अवयव-अवयवीभावरूप सम्बन्ध म पष्ठी विभक्ति है। यह योग त्रिकाल-विषयक होता है। अतः इसके पहले अतीत में जो सावद्य-न्यापार किया था उसे 'पडिक्कमामि' अर्थात उम पापकम से पीछे हटना हूं । निदामि गरिहामि' अर्थात् उमको निन्दा करता हूं' गहाँ या गुरु की गाक्षी से प्रकट करता हूं । इसमें केवल आत्म-साक्षी से की गई निन्दा है और गुरुसाक्षी से अपने आपको धिक्कारना गर्दा है । "तस्स भते' इस सूत्र में 'भते' शब्द फिर आया है, वह अतिशयक्ति के बताने क लिये व गुर का पुन: आमंत्रण करने के लिए है। इसलिये पुनरुक्निदोष जैसा नहीं है । अथवा सामायिकक्रिया के प्रत्यर्पण के लिये पुनः गुरु को सम्बोधिन किया गया है। इससे सिद्ध होता है कि ममस्न क्रियाओं के अन में गुरु के प्रति भक्ति प्रदर्शित करनी चाहिए।
भाग्यकार ने और भी कहा है -भदंन या भने शब्द सामायिक के प्र-गपंण का भी वाता है. यह जान कर सभी क्रियाओं के अन्त में प्राण करना चाहिए। तथा 'अप्पाण' अर्थात मी आत्मा ने भूतकाल में जो पाप व्यापार किया है, उसका 'बोसिरामि' में विशेष रूप से त्याग करता हूँ। प्रस्तुत मामायिक पाट में वर्तमानकाल के पाप-व्यापार को त्यागन क लिये 'करेमि भते सामाइयं ; भूतकाल में पाप-व्यापार के त्यागने के लिये 'तस्स भंते पडिक्कमामि' ; तथा भविष्यकाल के पाप-व्यापार के त्याग के लिये पच्चक्खामि' शब्द का प्रयोग है। इस तरह मामायिक में साधक को तीनों काल के पाप-व्यापार का त्याग क.ग्ना होता है। इमलिये तीनों वाक्यों के प्रयोग में पुनरुक्तिदोप प्रतीत नहीं होता। कहानी है -- 'अइयं निदामि, पड़प्पन्न संवरेमि अणागयं पच्चक्खामि' । अर्थात् -'भूतकाल के पाप की निदा करना हैं, वर्तमानकाल के लिये उमका संवर (निगेध) करता हूं ; और भविष्यकाल के लिये पाप-व्यापार का त्याग करना है। एम प्रकार स साधक नियम करता है। अपने घर में या अन्य स्थान पर सामायिक ले कर थावक गुरु के पास इग्यिावही प्रतिक्रमण करे । बाद में गमनागमन में हए पाप-दोष की आलोचना करके यथाक्रम से विराजमान आचार्य आदि मुनिगजों को वन्दन करें। फिर गुरुमहाराज को वन्दन कर आसन (क्टागन) आदि की प्रतिलेखना करके बैठे। तत्पश्चात् गुरुमहागज से धर्मश्रवण करे, तथा नया अध्ययन करे, या जहां शंका हो वहां पूछे । म प्रकार स्थानीय जिनमन्दिर या व्याख्यान-स्थल हो, वहां यह विधि समझना । परन्तु अपने घर पर या जिनमन्दिर, व्याम्यानस्थल, उपाश्रय या गौपधशाला म मामायिक ले तो, वह फिर वही रहे ; फिर उसे अन्यत्र जाने की जरूरत नहीं है। यह सामान्य श्रावक की विधि कही है।
अब राजा आदि महर्दिक श्रावक की विधि कहते हैं-कोई श्रावक राजा आदि हो और वह हाथी आदि उनम सवारी में बैठ कर, छत्र-चामर आदि गजचिह्नों से एवं अलकारों में सुमति हो कर हाथी, घोड़े रथ और पंदल सेना-सहित भेरी आदि उत्तम वाद्यों से आकाशमण्डल को गुजाता हुआ. भाटों और चारणों के प्रशंमागीतों के कोलाहल मे स्थानीय जनता में उत्सुकता पैदा करता हुआ, अनेक