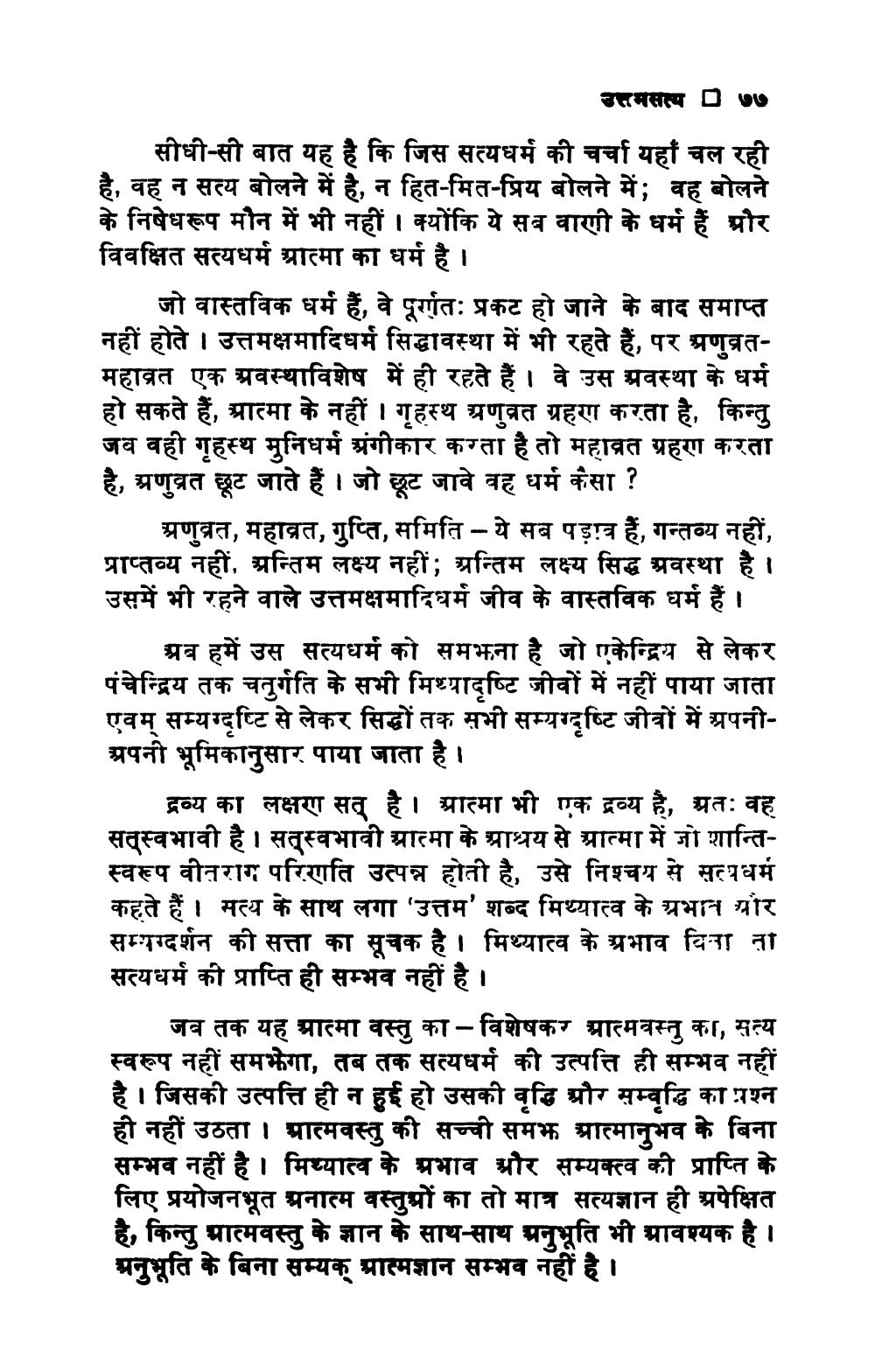________________
उत्तमसत्य D७७ सीधी-सी बात यह है कि जिस सत्यधर्म की चर्चा यहां चल रही है, वह न सत्य बोलने में है, न हित-मित-प्रिय बोलने में; वह बोलने के निषेधरूप मौन में भी नहीं । क्योंकि ये सब वाणी के धर्म हैं और विवक्षित सत्यधर्म आत्मा का धर्म है ।
जो वास्तविक धर्म हैं, वे पूर्णतः प्रकट हो जाने के बाद समाप्त नहीं होते । उत्तमक्षमादिधर्म सिद्धावस्था में भी रहते हैं, पर अणुव्रतमहाव्रत एक अवस्थाविशेष में ही रहते हैं। वे उस अवस्था के धर्म हो सकते हैं, आत्मा के नहीं । गृहस्थ प्रणवत ग्रहण करता है, किन्तु जब वही गृहस्थ मुनिधर्म अंगीकार करता है तो महावत ग्रहण करता है, अणुव्रत छूट जाते हैं। जो छूट जावे वह धर्म कैसा?
अणुव्रत, महाव्रत, गुप्ति, समिति - ये सब पड़ाव हैं, गन्तव्य नहीं, प्राप्तव्य नहीं, अन्तिम लक्ष्य नहीं; अन्तिम लक्ष्य सिद्ध अवस्था है। उसमें भी रहने वाले उत्तमक्षमादिधर्म जीव के वास्तविक धर्म हैं।
अब हमें उस सत्यधर्म को समझना है जो एकेन्द्रिय से लेकर पंचेन्द्रिय तक चतुर्गति के सभी मिथ्यादृष्टि जीवों में नहीं पाया जाता एवम् सम्यग्दृष्टि से लेकर सिद्धों तक सभी सम्यग्दृष्टि जीवों में अपनीअपनी भूमिकानुसार पाया जाता है।
द्रव्य का लक्षण सत् है। आत्मा भी एक द्रव्य है, अत: वह सत्स्वभावी है। सत्स्वभावी आत्मा के आश्रय से प्रात्मा में जो शान्तिस्वरूप वीतराग परिणति उत्पन्न होती है, उसे निश्चय से सत्यधर्म कहते हैं। मत्य के साथ लगा 'उत्तम' शब्द मिथ्यात्व के अभात पौर सम्पग्दर्शन की सत्ता का सूचक है। मिथ्यात्व के प्रभाव विना ना सत्यधर्म की प्राप्ति ही सम्भव नहीं है।
जब तक यह आत्मा वस्तु का-विशेषकर आत्मवस्तु का, सत्य स्वरूप नहीं समझेगा, तब तक सत्यधर्म की उत्पत्ति ही सम्भव नहीं है। जिसकी उत्पत्ति ही न हुई हो उसकी वृद्धि और सम्वृद्धि का प्रश्न ही नहीं उठता। आत्मवस्तु की सच्ची समझ आत्मानुभव के बिना सम्भव नहीं है। मिथ्यात्व के प्रभाव और सम्यक्त्व की प्राप्ति के लिए प्रयोजनभूत अनात्म वस्तुओं का तो मात्र सत्यज्ञान ही अपेक्षित है, किन्तु पात्मवस्तु के ज्ञान के साथ-साथ अनुभूति भी आवश्यक है। अनुभूति के बिना सम्यक् प्रात्मज्ञान सम्भव नहीं है।