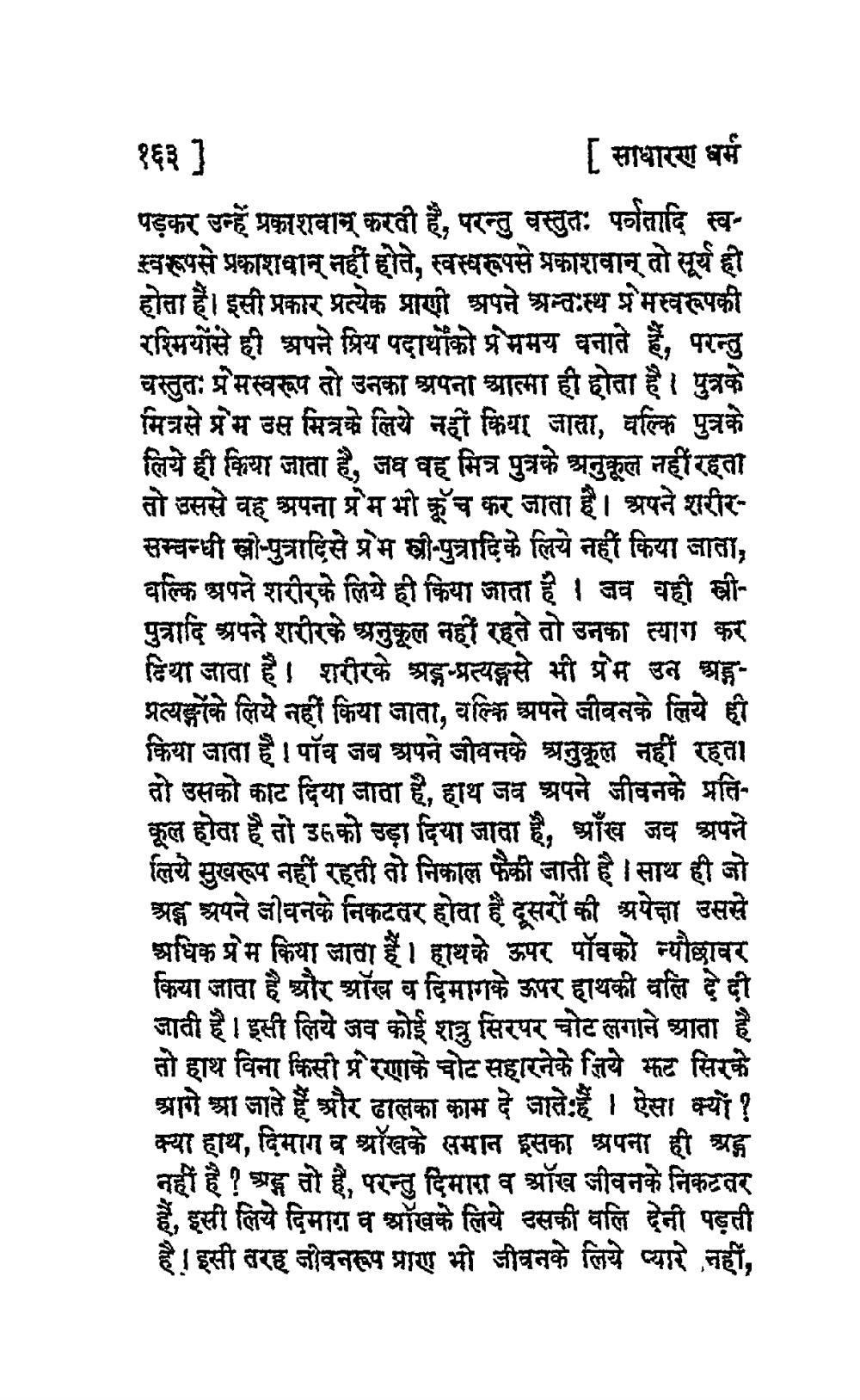________________
१६३ ]
[साधारण धर्म पड़कर उन्हें प्रकाशवान करती है, परन्तु वस्तुतः पर्वतादि स्वस्वरूपसे प्रकाशवान नहीं होते, स्वस्वरूपसे प्रकाशवान तो सूर्य ही होता है। इसी प्रकार प्रत्येक प्राणी अपने अन्तःस्थ प्रेमस्वरूपकी रश्मियोंसे ही अपने प्रिय पदार्थोंको प्रेममय बनाते हैं, परन्तु चस्तुतः प्रेमस्वरूप तो उनका अपना आत्मा ही होता है। पुत्रके मित्रसे प्रेम उस मित्र के लिये नहीं किया जाता, बल्कि पुत्रके लिये ही किया जाता है, जब वह मित्र पुत्रके अनुकूल नहींरहता तो उससे वह अपना प्रेम भी कुँच कर जाता है। अपने शरीरसम्बन्धी खो-पुत्रादिसे प्रेम त्री-पुत्रादिके लिये नहीं किया जाता, बल्कि अपने शरीरके लिये ही किया जाता है । जब वही स्त्रीपुत्रादि अपने शरीरके अनुकूल नहीं रहते तो उनका त्याग कर दिया जाता है। शरीरके अङ्ग-प्रत्यङ्गसे भी प्रेम उन अङ्गप्रत्यङ्गोंके लिये नहीं किया जाता, बल्कि अपने जीवन के लिये ही किया जाता है । पॉव जब अपने जीवनके अनुकूल नहीं रहता तो उसको काट दिया जाता है, हाथ जब अपने जीवनके प्रतिकूल होता है तो उसको उड़ा दिया जाता है, आँख जव अपने लिये सुखरूप नहीं रहती तो निकाल फैकी जाती है। साथ ही जो अझ अपने जीवनके निकटतर होता है दूसरों की अपेक्षा उससे अधिक प्रेम किया जाता है। हाथके ऊपर पॉवको न्यौछावर किया जाता है और आँख व दिमागके पर हाथकी बलि दे दी जाती है। इसी लिये जब कोई शत्रु सिरपर चोट लगाने आता है तो हाथ विना किसी प्रेरणाके चोट सहारनेके लिये झट सिरके आगे आ जाते हैं और ढालका काम दे जाते हैं । ऐसा क्यों? क्या हाथ, दिमाग व श्रॉखके समान इसका अपना ही अङ्ग नहीं है ? अङ्ग तो है, परन्तु दिमारा व ऑख जीवनके निकटतर हैं, इसी लिये दिमाग व बाखके लिये उसकी बलि देनी पड़ती है। इसी तरह जीवनरूप प्राण भी जीवनके लिये प्यारे नहीं,