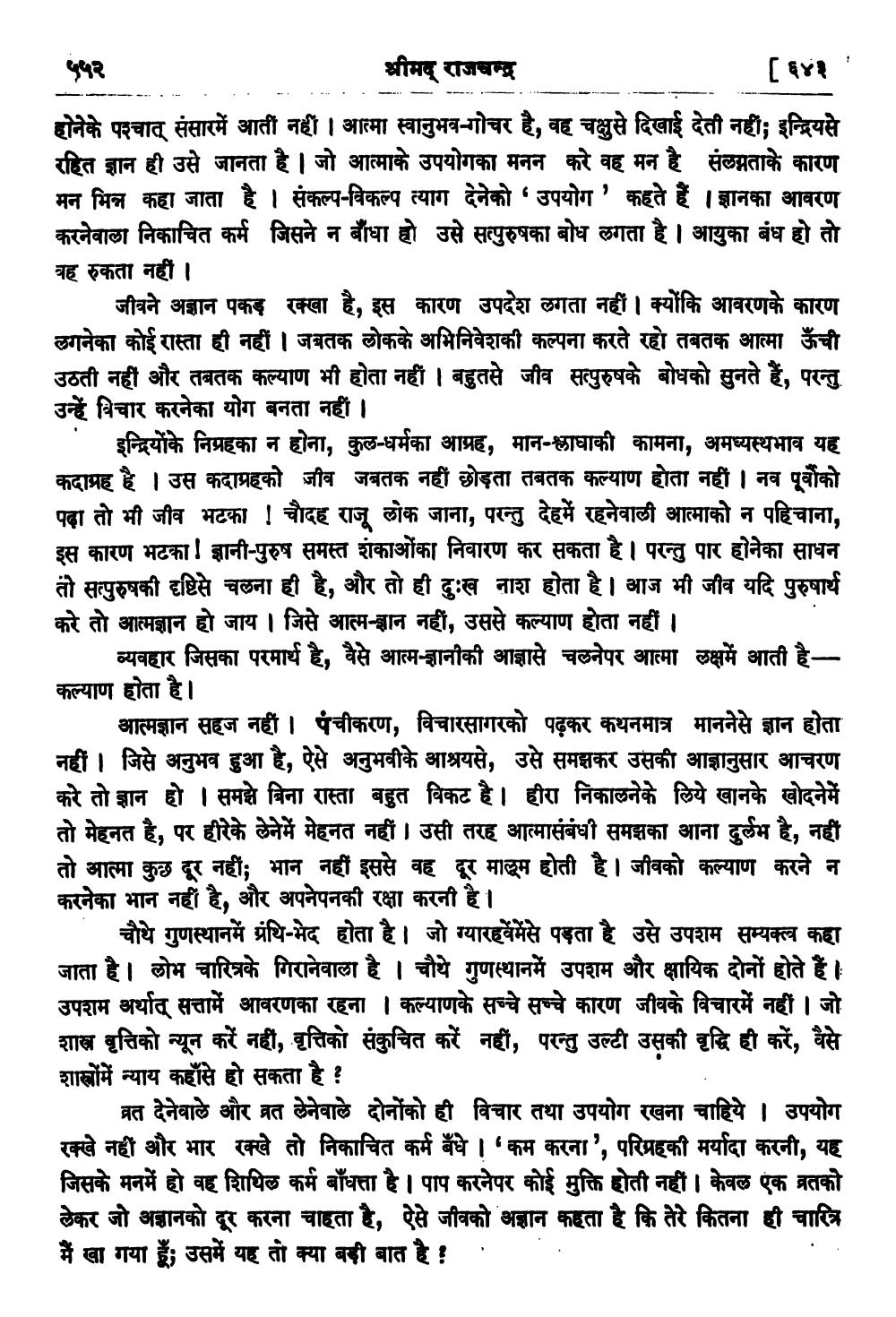________________
५५२ श्रीमद् राजचन्द्र
[६४१ होनेके पश्चात् संसारमें आती नहीं । आत्मा स्वानुभव-गोचर है, वह चक्षुसे दिखाई देती नहीं; इन्द्रियसे रहित ज्ञान ही उसे जानता है । जो आत्माके उपयोगका मनन करे वह मन है संलग्नताके कारण मन भिन्न कहा जाता है । संकल्प-विकल्प त्याग देनेको ' उपयोग' कहते हैं । ज्ञानका आवरण करनेवाला निकाचित कर्म जिसने न बाँधा हो उसे सत्पुरुषका बोध लगता है । आयुका बंध हो तो वह रुकता नहीं।
जीवने अज्ञान पकड़ रक्खा है, इस कारण उपदेश लगता नहीं। क्योंकि आवरणके कारण लगनेका कोई रास्ता ही नहीं । जबतक लोकके अभिनिवेशकी कल्पना करते रहो तबतक आत्मा ऊँची उठती नहीं और तबतक कल्याण भी होता नहीं । बहुतसे जीव सत्पुरुषके बोधको सुनते हैं, परन्तु उन्हें विचार करनेका योग बनता नहीं।
- इन्द्रियोंके निग्रहका न होना, कुल-धर्मका आग्रह, मान-श्लाघाकी कामना, अमध्यस्थभाव यह कदाग्रह है । उस कदाग्रहको जीव जबतक नहीं छोड़ता तबतक कल्याण होता नहीं । नव पूर्वोको पढ़ा तो भी जीव भटका ! चौदह राजू लोक जाना, परन्तु देहमें रहनेवाली आत्माको न पहिचाना, इस कारण भटका! ज्ञानी-पुरुष समस्त शंकाओंका निवारण कर सकता है। परन्तु पार होनेका साधन तो सत्पुरुषकी दृष्टिसे चलना ही है, और तो ही दुःख नाश होता है। आज भी जीव यदि पुरुषार्थ करे तो आत्मज्ञान हो जाय । जिसे आत्म-ज्ञान नहीं, उससे कल्याण होता नहीं।
व्यवहार जिसका परमार्थ है, वैसे आत्म-ज्ञानीकी आज्ञासे चलनेपर आत्मा लक्षमें आती हैकल्याण होता है।
__ आत्मज्ञान सहज नहीं। पंचीकरण, विचारसागरको पढ़कर कथनमात्र माननेसे ज्ञान होता नहीं। जिसे अनुभव हुआ है, ऐसे अनुभवीके आश्रयसे, उसे समझकर उसकी आज्ञानुसार आचरण करे तो ज्ञान हो । समझे बिना रास्ता बहुत विकट है। हीरा निकालनेके लिये खानके खोदनेमें तो मेहनत है, पर हीरेके लेनेमें मेहनत नहीं। उसी तरह आत्मासंबंधी समझका आना दुर्लभ है, नहीं तो आत्मा कुछ दूर नहीं; भान नहीं इससे वह दूर मालूम होती है। जीवको कल्याण करने न करनेका भान नहीं है, और अपनेपनकी रक्षा करनी है।
चौथे गुणस्थानमें ग्रंथि-भेद होता है। जो ग्यारहवेंमेंसे पड़ता है उसे उपशम सम्यक्त्व कहा जाता है। लोभ चारित्रके गिरानेवाला है । चौथे गुणस्थानमें उपशम और क्षायिक दोनों होते हैं। उपशम अर्थात् सत्तामें आवरणका रहना । कल्याणके सच्चे सच्चे कारण जीवके विचारमें नहीं । जो शास्त्र वृत्तिको न्यून करें नहीं, वृत्तिको संकुचित करें नहीं, परन्तु उल्टी उसकी वृद्धि ही करें, वैसे शास्त्रोंमें न्याय कहाँसे हो सकता है ?
व्रत देनेवाले और व्रत लेनेवाले दोनोंको ही विचार तथा उपयोग रखना चाहिये । उपयोग रक्खे नहीं और भार रक्खे तो निकाचित कर्म बँधे । 'कम करना', परिग्रहकी मर्यादा करनी, यह जिसके मनमें हो वह शिथिल कर्म बाँधत्ता है। पाप करनेपर कोई मुक्ति होती नहीं। केवल एक व्रतको लेकर जो अज्ञानको दूर करना चाहता है, ऐसे जीवको अज्ञान कहता है कि तेरे कितना ही चारित्र मैं खा गया है उसमें यह तो क्या बड़ी बात है! '