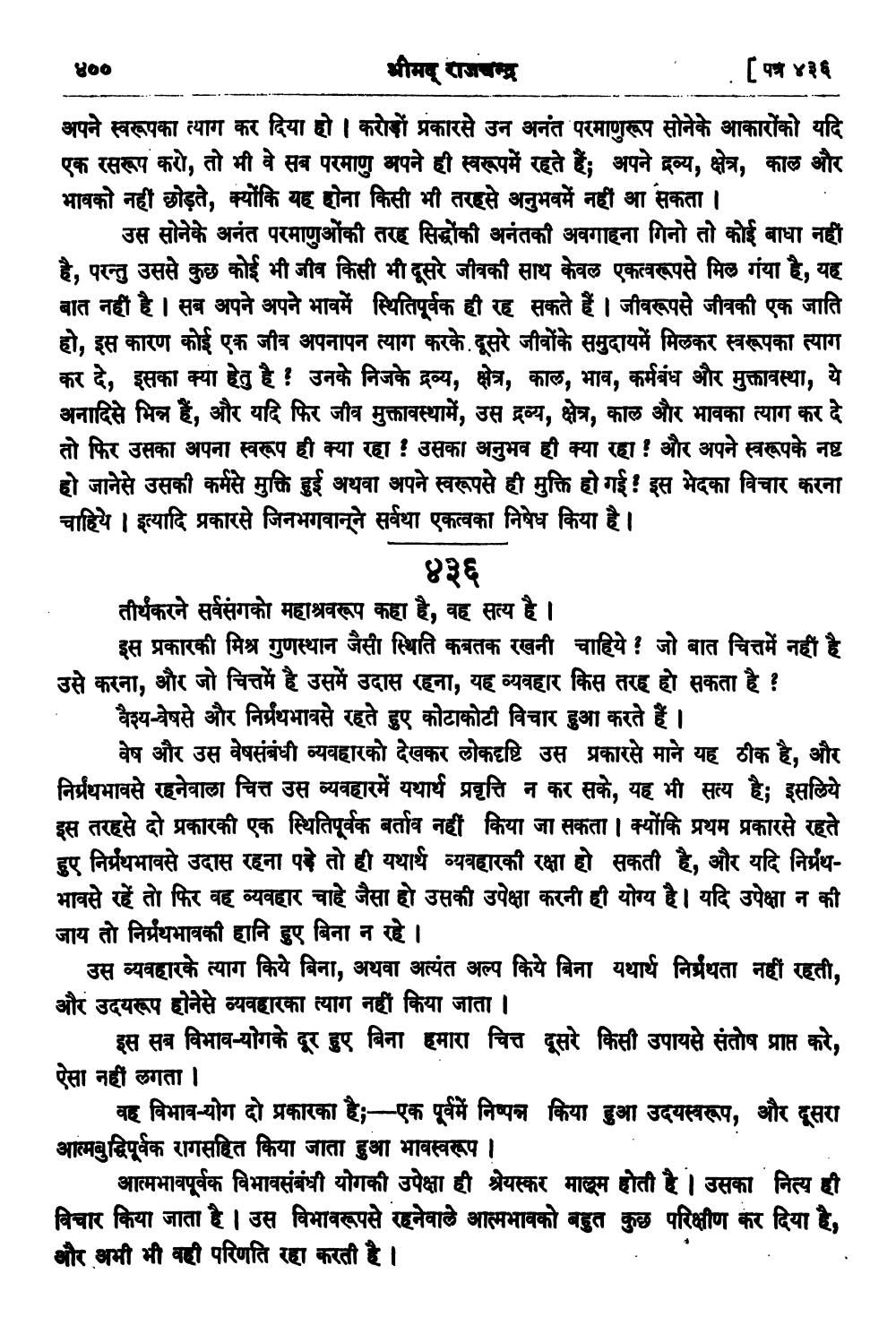________________
४००
भीमद् राजचन्द्र
- [पत्र ४३६ अपने स्वरूपका त्याग कर दिया हो । करोड़ों प्रकारसे उन अनंत परमाणुरूप सोनेके आकारोंको यदि एक रसरूप करो, तो भी वे सब परमाणु अपने ही स्वरूपमें रहते हैं; अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावको नहीं छोड़ते, क्योंकि यह होना किसी भी तरहसे अनुभवमें नहीं आ सकता।
उस सोनेके अनंत परमाणुओंकी तरह सिद्धोंकी अनंतकी अवगाहना गिनो तो कोई बाधा नहीं है, परन्तु उससे कुछ कोई भी जीव किसी भी दूसरे जीवकी साथ केवल एकत्वरूपसे मिल गया है, यह बात नहीं है । सब अपने अपने भावमें स्थितिपूर्वक ही रह सकते हैं । जीवरूपसे जीवकी एक जाति हो, इस कारण कोई एक जीव अपनापन त्याग करके.दूसरे जीवोंके समुदायमें मिलकर स्वरूपका त्याग कर दे, इसका क्या हेतु है ! उनके निजके द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, कर्मबंध और मुक्तावस्था, ये अनादिसे भिन्न हैं, और यदि फिर जीव मुक्तावस्थामें, उस द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावका त्याग कर दे तो फिर उसका अपना स्वरूप ही क्या रहा ! उसका अनुभव ही क्या रहा ! और अपने स्वरूपके नष्ट हो जानेसे उसकी कर्मसे मुक्ति हुई अथवा अपने स्वरूपसे ही मुक्ति हो गई ! इस भेदका विचार करना चाहिये । इत्यादि प्रकारसे जिनभगवान्ने सर्वथा एकत्वका निषेध किया है।
तीर्थकरने सर्वसंगको महाश्रवरूप कहा है, वह सत्य है।।
इस प्रकारकी मिश्र गुणस्थान जैसी स्थिति कबतक रखनी चाहिये ! जो बात चित्तमें नहीं है उसे करना, और जो चित्तमें है उसमें उदास रहना, यह व्यवहार किस तरह हो सकता है !
वैश्य-वेषसे और निग्रंथभावसे रहते हुए कोटाकोटी विचार हुआ करते हैं।
वेष और उस वेषसंबंधी व्यवहारको देखकर लोकदृष्टि उस प्रकारसे माने यह ठीक है, और निग्रंथभावसे रहनेवाला चित्त उस व्यवहारमें यथार्थ प्रवृत्ति न कर सके, यह भी सत्य है; इसलिये इस तरहसे दो प्रकारकी एक स्थितिपूर्वक बर्ताव नहीं किया जा सकता। क्योंकि प्रथम प्रकारसे रहते हुए निग्रंथमावसे उदास रहना पड़े तो ही यथार्थ व्यवहारकी रक्षा हो सकती है, और यदि निग्रंथभावसे रहें तो फिर वह व्यवहार चाहे जैसा हो उसकी उपेक्षा करनी ही योग्य है। यदि उपेक्षा न की जाय तो निग्रंथभावकी हानि हुए बिना न रहे ।
उस व्यवहारके त्याग किये बिना, अथवा अत्यंत अल्प किये बिना यथार्थ निग्रंथता नहीं रहती. और उदयरूप होनेसे व्यवहारका त्याग नहीं किया जाता।
इस सब विभाव-योगके दूर हुए बिना हमारा चित्त दूसरे किसी उपायसे संतोष प्राप्त करे, ऐसा नहीं लगता।
वह विभाव-योग दो प्रकारका है-एक पूर्वमें निष्पन्न किया हुआ उदयस्वरूप, और दूसरा आत्मबुद्धिपूर्वक रागसहित किया जाता हुआ भावस्वरूप ।
आत्मभावपूर्वक विभावसंबंधी योगकी उपेक्षा ही श्रेयस्कर मालूम होती है। उसका नित्य ही विचार किया जाता है । उस विभावरूपसे रहनेवाले आत्मभावको बहुत कुछ परिक्षीण कर दिया है, और अभी भी वही परिणति रहा करती है।