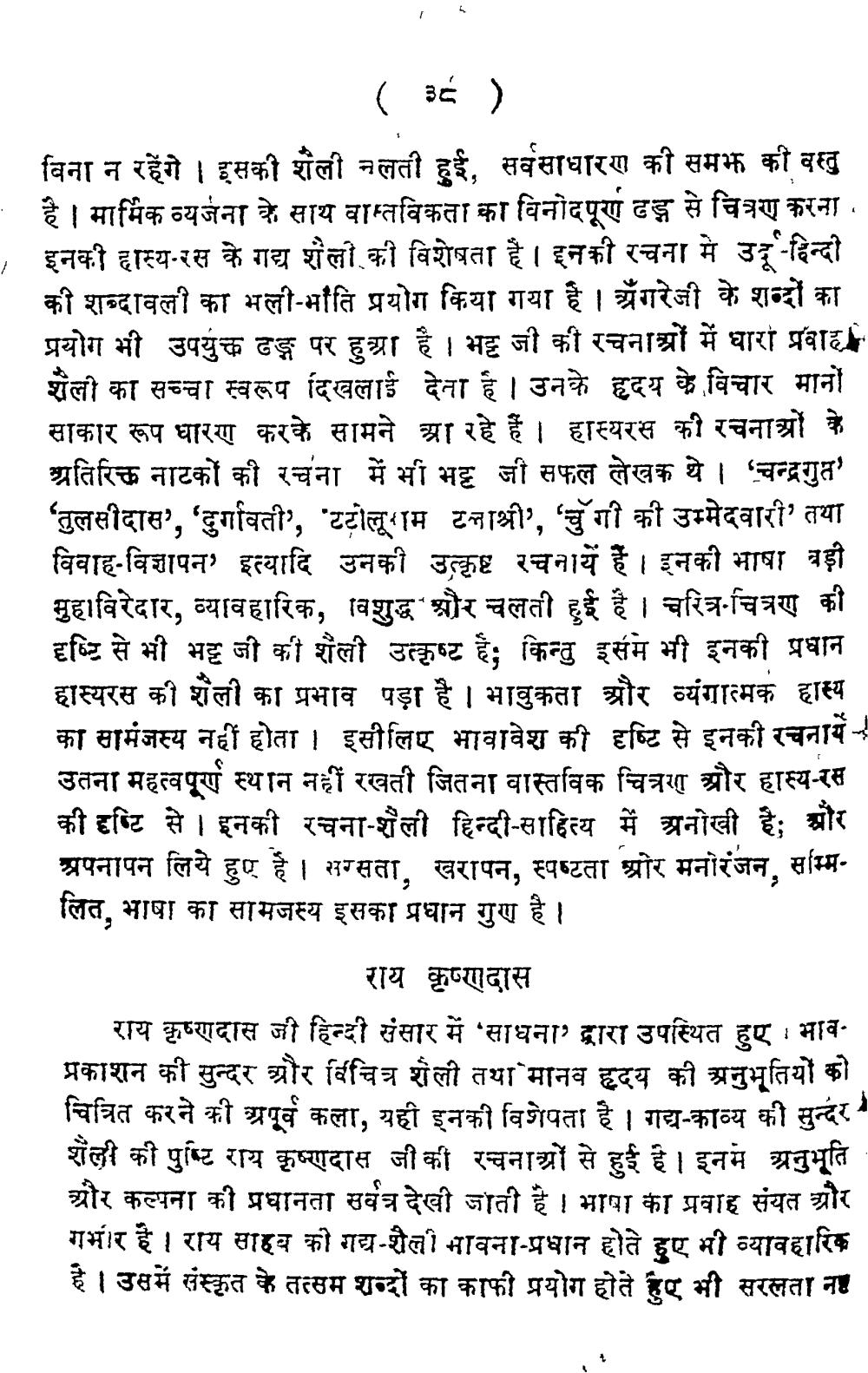________________
( ३८ ) बिना न रहेंगे। इसकी शैली नलती हुई, सर्वसाधारण की समझ की वस्तु है । मार्मिक व्यजना के साथ वास्तविकता का विनोदपूर्ण ढङ्ग से चित्रण करना . इनकी हास्य रस के गद्य शैली की विशेषता है । इनकी रचना मे उर्दू-हिन्दी की शब्दावली का भली-भांति प्रयोग किया गया है । अँगरेजी के शब्दों का । प्रयोग भी उपयुक्त ढङ्ग पर हुआ है । भट्ट जी की रचनाओं में धारा प्रवाह शैली का सच्चा स्वरूप दिखलाई देता है । उनके हृदय के विचार मानों साकार रूप धारण करके सामने आ रहे हैं । हास्यरस की रचनाओं के अतिरिक्त नाटकों की रचना में भी भट्ट जी सफल लेखक थे । 'चन्द्रगुप्त' 'तुलसीदास', 'दुर्गावती', 'टटोलू गम टनाश्री', 'चुंगी की उम्मेदवारी' तथा विवाह-विज्ञापन' इत्यादि उनकी उत्कृष्ट रचनायें हैं । इनकी भाषा बड़ी मुहाविरेदार, व्यावहारिक, विशुद्ध और चलती हुई है। चरित्र-चित्रण की दृष्टि से भी भट्ट जी की शैली उत्कृष्ट हैं; किन्तु इसमे भी इनकी प्रधान हास्यरस की शैली का प्रभाव पड़ा है । भावुकता और व्यंगात्मक हास्य का सामंजस्य नहीं होता। इसीलिए भावावेश की दृष्टि से इनकी रचनाये। उतना महत्वपूर्ण स्थान नहीं रखती जितना वास्तविक चित्रण और हास्य-रस की दृष्टि से । इनकी रचना-शैली हिन्दी-साहित्य में अनोखी है; और अपनापन लिये हुए हैं । सरसता, खरापन, स्पष्टता श्रोर मनोरंजन, सम्मि. लित, भाषा का सामजस्य इसका प्रधान गुण है।
राय कृष्णदास राय कृष्णदास जी हिन्दी संसार में 'साधना द्वारा उपस्थित हुए । भाव प्रकाशन की सुन्दर और विचित्र शैली तथा मानव हृदय की अनुभूतियों का. चित्रित करने की अपूर्व कला, यही इनकी विशेपता है । गद्य-काव्य की सुन्दर शैली की पुष्टि राय कृष्णदास जी की रचनाओं से हुई है। इनमें अनुभूति । और कल्पना की प्रधानता सर्वत्र देखी जाती है । भाषा का प्रवाह संयत और गार है । राय साहब को गद्य-शैली भावना-प्रधान होते हुए भी व्यावहारिक है । उसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों का काफी प्रयोग होते हुए भी सरलता नह