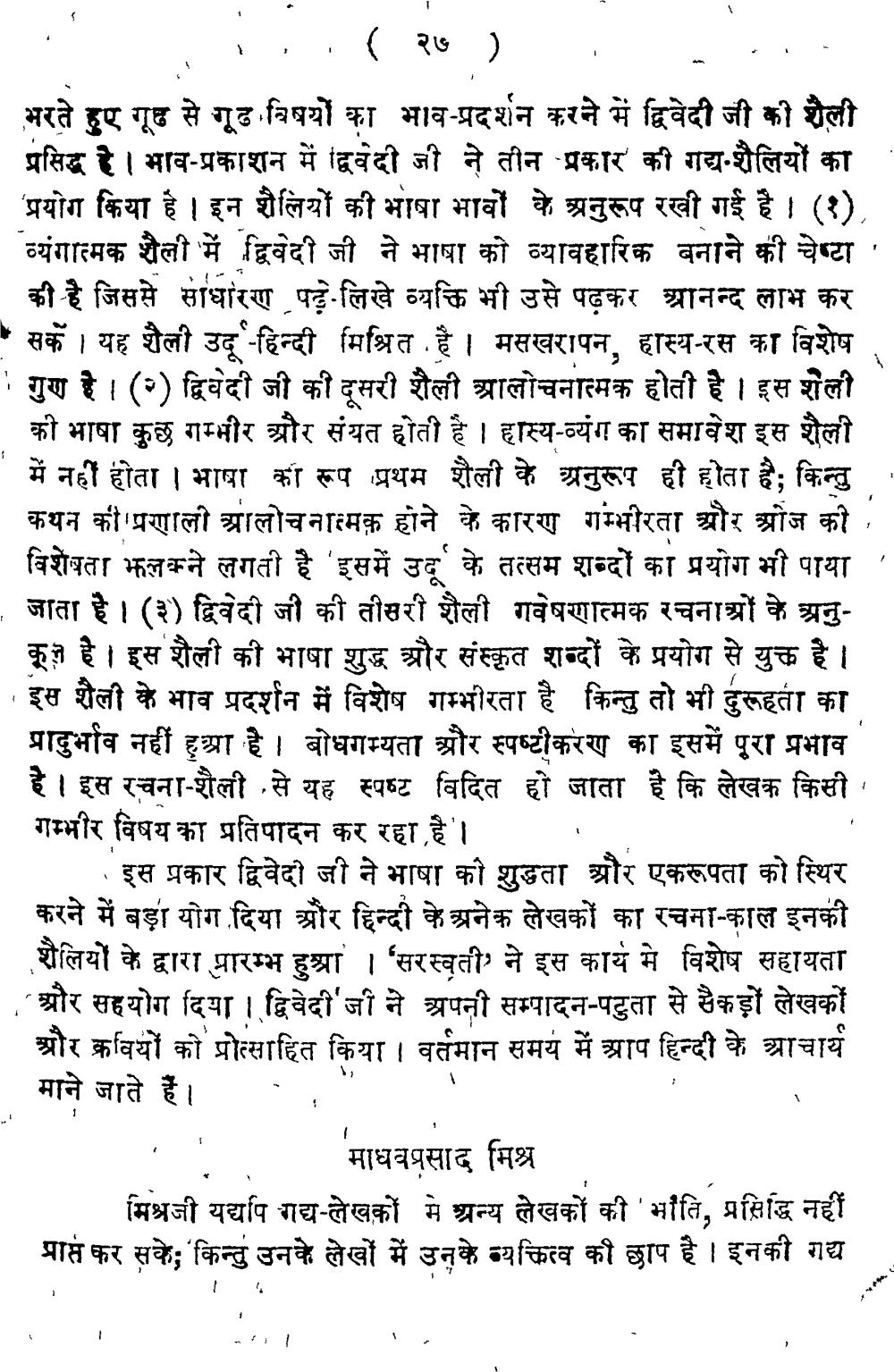________________
.
-
। . . ( २७ )
. . . भरते हुए गूढ से गूढ विषयों का भाव-प्रदर्शन करने में द्विवेदी जी की शैली प्रसिद्ध है। भाव-प्रकाशन में द्विवेदी जी ने तीन प्रकार की गद्य-शैलियों का 'प्रयोग किया है । इन शैलियों की भाषा भावों के अनुरूप रखी गई है । (१), व्यंगात्मक शैली में द्विवेदी जी ने भाषा को व्यावहारिक बनाने की चेष्टा ।
की है जिससे साधारण पढ़े-लिखे व्यक्ति भी उसे पढ़कर अानन्द लाभ कर • सकें । यह शैली उर्दू-हिन्दी मिश्रित है । मसखरापन, हास्य-रस का विशेष . 'गुण है । (२) द्विवेदी जी की दूसरी शैली अालोचनात्मक होती है । इस शैली ___ की भाषा कुछ गम्भीर और संयत होती है । हास्य-व्यंग का समावेश इस शैली ' में नहीं होता । भाषा का रूप प्रथम शैली के अनुरूप ही होता है; किन्तु ।
कथन को प्रणाली आलोचनात्मक होने के कारण गम्भीरता और प्रोज की , विशेषता झलकने लगती है 'इसमें उर्दू के तत्सम शब्दों का प्रयोग भी पाया । जाता है । (३) द्विवेदी जी की तीसरी शैली गवेषणात्मक रचनात्रों के अनुकूल है। इस शैली की भाषा शुद्ध और संस्कृत शब्दों के प्रयोग से युक्त है। • इस शैली के भाव प्रदर्शन में विशेष गम्भीरता है किन्तु तो भी दुरूहता का प्रादुर्भाव नहीं हुआ है। बोधगम्यता और स्पष्टीकरण का इसमें पूरा प्रभाव है। इस रचना-शैली से यह स्पष्ट विदित हो जाता है कि लेखक किसी। गम्भीर विषय का प्रतिपादन कर रहा है।
इस प्रकार द्विवेदी जी ने भाषा को शुद्धता और एकरूपता को स्थिर करने में बड़ा योग दिया और हिन्दी के अनेक लेखकों का रचना-काल इनकी
शैलियों के द्वारा प्रारम्भ हुश्रा । 'सरस्वती' ने इस कार्य मे विशेष सहायता . और सहयोग दिया। द्विवेदी जी ने अपनी सम्पादन-पटुता से सैकड़ों लेखकों
और कवियों को प्रोत्साहित किया। वर्तमान समय में आप हिन्दी के प्राचार्य ___ माने जाते हैं।
माधवप्रसाद मिश्र मिश्रजी यद्यपि गद्य-लेखकों मे अन्य लेखकों की भांति, प्रसिद्धि नहीं प्राप्त कर सके; किन्तु उनके लेखों में उनके व्यक्तित्व की छाप है । इनकी गद्य