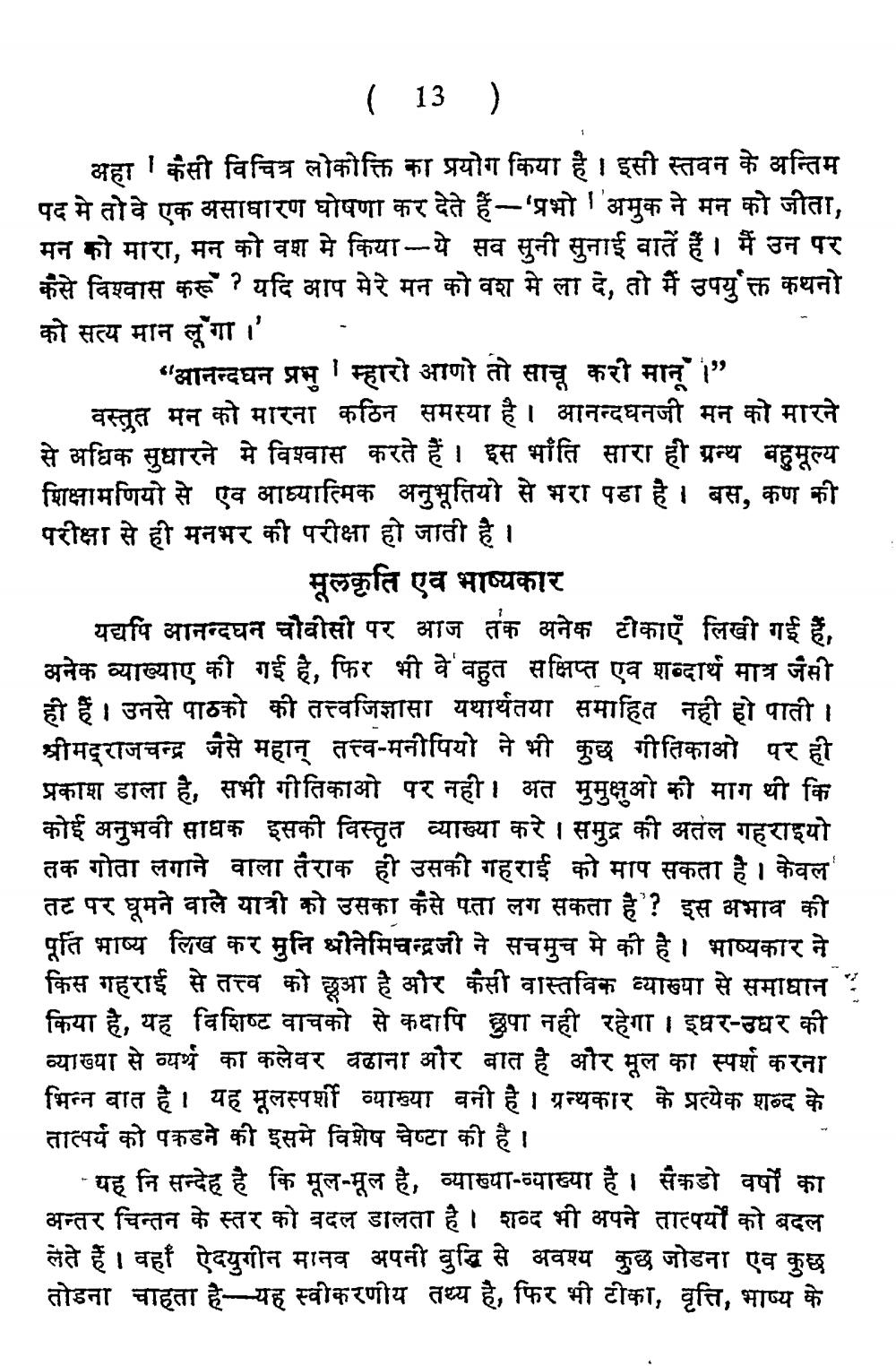________________
( 13 )
महा | कैसी विचित्र लोकोक्ति का प्रयोग किया है। इसी स्तवन के अन्तिम पद मे तोवे एक असाधारण घोषणा कर देते हैं-'प्रभो । 'अमुक ने मन को जीता, मन को मारा, मन को वश मे किया-ये सव सुनी सुनाई बातें हैं। मैं उन पर कैसे विश्वास करू ? यदि आप मेरे मन को वश मे ला दे, तो मैं उपर्युक्त कथनो को सत्य मान लूंगा।'
"आनन्दघन प्रभु | म्हारो आणो तो साचू करी मानू।" वस्तुत मन को मारना कठिन समस्या है। आनन्दघनजी मन को मारने से अधिक सुधारने मे विश्वास करते हैं। इस भांति सारा ही ग्रन्थ बहुमूल्य शिक्षामणियो से एव आध्यात्मिक अनुभूतियो से भरा पड़ा है। बस, कण की परीक्षा से ही मनभर की परीक्षा हो जाती है ।
मूलकृति एव भाष्यकार यद्यपि आनन्दघन चौवीसी पर आज तक अनेक टीकाएँ लिखी गई हैं, अनेक व्याख्याए की गई है, फिर भी वे बहुत सक्षिप्त एव शब्दार्थ मात्र जैसी ही हैं। उनसे पाठको की तत्त्वजिज्ञासा यथार्थतया समाहित नही हो पाती। श्रीमद्राजचन्द्र जैसे महान् तत्त्व-मनीपियो ने भी कुछ गीतिकाओ पर ही प्रकाश डाला है, सभी गीतिकाओ पर नही। अत मुमुक्षुओ की माग थी कि कोई अनुभवी साधक इसकी विस्तृत व्याख्या करे । समुद्र की अतल गहराइयो तक गोता लगाने वाला तैराक ही उसकी गहराई को माप सकता है। केवल तट पर घूमने वाले यात्री को उसका कैसे पता लग सकता है? इस अभाव की पूर्ति भाष्य लिख कर मुनि श्रीनेमिचन्द्रजी ने सचमुच मे की है। भाष्यकार ने किस गहराई से तत्त्व को छुआ है और कैसी वास्तविक व्याख्या से समाधान : किया है, यह विशिष्ट वाचको से कदापि छुपा नही रहेगा। इधर-उधर की व्याख्या से व्यर्थ का कलेवर बढाना और बात है और मूल का स्पर्श करना भिन्न बात है। यह मूलस्पर्शी व्याख्या बनी है। ग्रन्थकार के प्रत्येक शब्द के तात्पर्य को पकडने की इसमे विशेष चेष्टा की है।
“यह नि सन्देह है कि मूल-मूल है, व्याख्या-व्याख्या है। सैकडो वर्षों का अन्तर चिन्तन के स्तर को बदल डालता है। शब्द भी अपने तात्पर्यों को बदल लेते हैं। वहीं ऐदयुगीन मानव अपनी बुद्धि से अवश्य कुछ जोडना एव कुछ तोडना चाहता है-यह स्वीकरणीय तथ्य है, फिर भी टीका, वृत्ति, भाष्य के