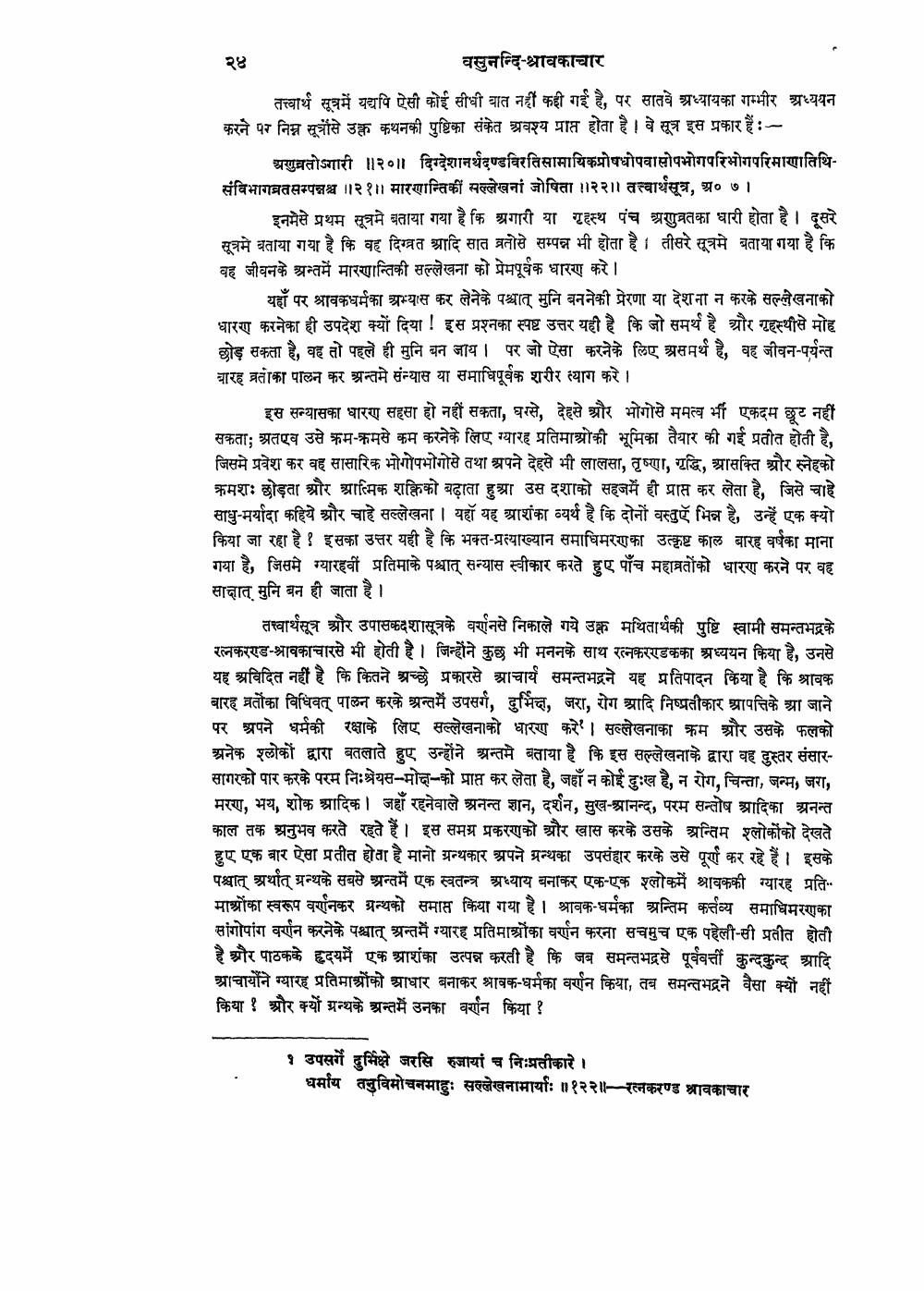________________
वसुनन्दि-श्रावकाचार तत्त्वार्थ सूत्रमें यद्यपि ऐसी कोई सीधी बात नहीं कही गई है, पर सातवे अध्यायका गम्भीर अध्ययन करने पर निम्न सूत्रोंसे उक्त कथनकी पुष्टिका संकेत अवश्य प्राप्त होता है। वे सूत्र इस प्रकार हैं:
अणुव्रतोऽगारी ॥२०॥ दिग्देशानर्थदण्डविरतिसामायिकपोषधोपवासोपभोगपरिभोगपरिमाणातिथिसंविभागवतसम्पन्नश्च ॥२१॥ मारणान्तिकीं सल्लेखनां जोषिता ॥२२॥ तत्वार्थसूत्र, अ०७।
इनमेसे प्रथम सूत्रमे बताया गया है कि अगारी या गृहस्थ पंच अणुव्रतका धारी होता है। दूसरे सूत्रमे बताया गया है कि वह दिग्वत आदि सात व्रतोसे सम्पन्न भी होता है। तीसरे सूत्रमे बताया गया है कि वह जीवन के अन्तमें मारणान्तिकी सल्लेखना को प्रेमपूर्वक धारण करे।
यहाँ पर श्रावकधर्मका अभ्यास कर लेनेके पश्चात् मुनि बननेकी प्रेरणा या देशना न करके सल्लेखनाको धारण करनेका ही उपदेश क्यों दिया ! इस प्रश्नका सष्ट उत्तर यही है कि जो समर्थ है और गृहस्थीसे मोह छोड़ सकता है, वह तो पहले ही मुनि बन जाय । पर जो ऐसा करनेके लिए असमर्थ है, वह जीवन-पर्यन्त बारह व्रतोका पालन कर अन्तमे संन्यास या समाधिपूर्वक शरीर त्याग करे ।
___ इस सन्यासका धारण सहसा हो नहीं सकता, घरसे, देहसे और भोगोसे ममत्व भी एकदम छुट नहीं सकता; अतएव उसे क्रम-क्रमसे कम करनेके लिए ग्यारह प्रतिमाश्रोकी भूमिका तैयार की गई प्रतीत होती है, जिसमे प्रवेश कर वह सासारिक भोगोपभोगोसे तथा अपने देहसे भी लालसा, तृष्णा, गृद्धि, आसक्ति और स्नेहको क्रमशः छोड़ता और अात्मिक शक्तिको बढ़ाता हुआ उस दशाको सहजमें ही प्राप्त कर लेता है, जिसे चाहे साधु-मर्यादा कहिये और चाहे सल्लेखना । यहाँ यह आशंका व्यर्थ है कि दोनों वस्तुएँ भिन्न है, उन्हें एक क्यो किया जा रहा है ? इसका उत्तर यही है कि भक्त-प्रत्याख्यान समाधिमरणका उत्कृष्ट काल बारह वर्षका माना गया है, जिसमे ग्यारहवीं प्रतिमाके पश्चात् सन्यास स्वीकार करते हुए पाँच महाव्रतोंको धारण करने पर वह साक्षात् मुनि बन ही जाता है।
तस्वार्थसूत्र और उपासकदशासूत्रके वर्णनसे निकाले गये उक्त मथितार्थकी पुष्टि स्वामी समन्तभद्रके रत्नकरण्ड-श्रावकाचारसे भी होती है। जिन्होंने कुछ भी मननके साथ रत्नकरण्डकका अध्ययन किया है, उनसे यह अविदित नहीं है कि कितने अच्छे प्रकारसे प्राचार्य समन्तभद्रने यह प्रतिपादन किया है कि श्रावक बारह व्रतोंका विधिवत् पालन करके अन्तमें उपसर्ग, दुर्भिक्ष, जरा, रोग आदि निष्प्रतीकार श्रापत्तिके श्रा जाने पर अपने धर्मकी रक्षाके लिए सल्लेखनाको धारण करें। सल्लेखनाका क्रम और उसके फलको अनेक श्लोकों द्वारा बतलाते हुए उन्होंने अन्तमे बताया है कि इस सल्लेखनाके द्वारा वह दुस्तर संसारसागरको पार करके परम निःश्रेयस-मोक्ष-को प्राप्त कर लेता है, जहाँ न कोई दुःख है, न रोग, चिन्ता, जन्म, जरा, मरण, भय, शोक श्रादिक । जहाँ रहनेवाले अनन्त ज्ञान, दर्शन, सुख-श्रानन्द, परम सन्तोष श्रादिका अनन्त काल तक अनुभव करते रहते हैं। इस समग्र प्रकरणको और खास करके उसके अन्तिम श्लोकोंको देखते हुए एक बार ऐसा प्रतीत होता है मानो ग्रन्थकार अपने ग्रन्थका उपसंहार करके उसे पूर्ण कर रहे हैं। इसके पश्चात् अर्थात् ग्रन्थके सबसे अन्तमें एक स्वतन्त्र अध्याय बनाकर एक-एक श्लोकमें श्रावककी ग्यारह प्रतिमाओंका स्वरूप वर्णनकर ग्रन्थको समाप्त किया गया है। श्रावक-धर्मका अन्तिम कर्त्तव्य समाधिमरणका सांगोपांग वर्णन करनेके पश्चात् अन्तमें ग्यारह प्रतिमाओंका वर्णन करना सचमुच एक पहेली-सी प्रतीत होती है और पाठकके हृदयमें एक श्राशंका उत्पन्न करती है कि जब समन्तभद्रसे पूर्ववर्ती कुन्दकुन्द आदि प्राचार्योंने ग्यारह प्रतिमाओंको श्राधार बनाकर श्रावक-धर्मका वर्णन किया, तब समन्तभद्रने वैसा क्यों नहीं किया ? और क्यों ग्रन्थके अन्तमें उनका वर्णन किया ?
१ उपसर्गे दुर्मिक्षे जरसि रुजायां च निःप्रतीकारे । धर्माय तनुविमोचनमाहुः सल्लेखनामार्याः ॥१२२॥-रत्नकरण्ड श्रावकाचार