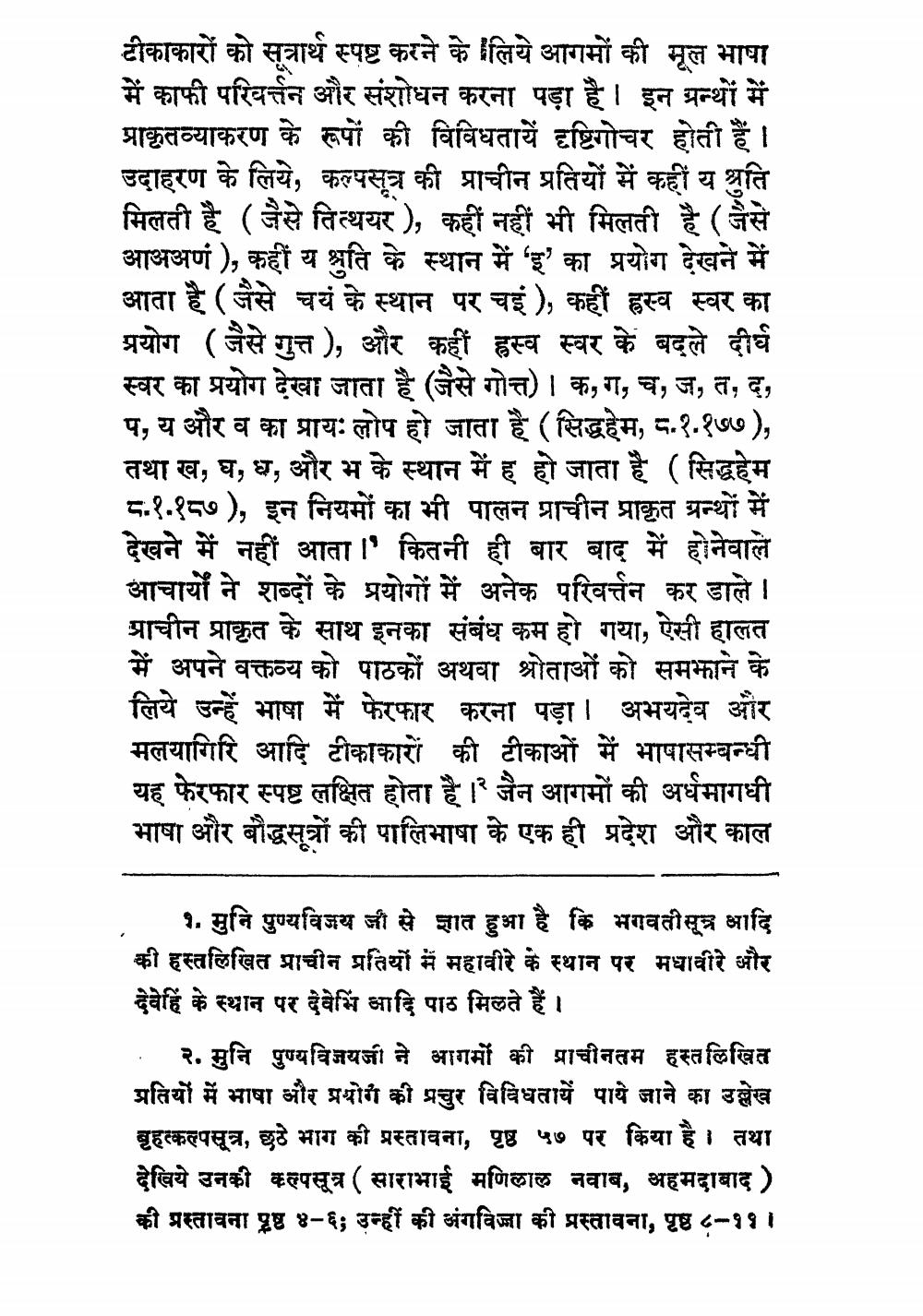________________
टीकाकारों को सूत्रार्थ स्पष्ट करने के लिये आगमों की मूल भाषा में काफी परिवर्तन और संशोधन करना पड़ा है। इन ग्रन्थों में प्राकृतव्याकरण के रूपों की विविधतायें दृष्टिगोचर होती हैं। उदाहरण के लिये, कल्पसूत्र की प्राचीन प्रतियों में कहीं य श्रुति मिलती है (जैसे तित्थयर ), कहीं नहीं भी मिलती है (जैसे आअअणं), कहीं य श्रुति के स्थान में 'इ' का प्रयोग देखने में आता है (जैसे चयं के स्थान पर चई), कहीं ह्रस्व स्वर का प्रयोग (जैसे गुत्त), और कहीं ह्रस्व स्वर के बदले दीर्घ स्वर का प्रयोग देखा जाता है (जैसे गोत्त) । क, ग, च, ज, त, द, प, य और व का प्रायः लोप हो जाता है (सिद्धहेम, ८.१.१७७), तथा ख, घ, ध, और भ के स्थान में ह हो जाता है (सिद्धहेम ८.१.१८७), इन नियमों का भी पालन प्राचीन प्राकृत ग्रन्थों में देखने में नहीं आता।' कितनी ही बार बाद में होनेवाले आचार्यों ने शब्दों के प्रयोगों में अनेक परिवर्तन कर डाले । प्राचीन प्राकृत के साथ इनका संबंध कम हो गया, ऐसी हालत में अपने वक्तव्य को पाठकों अथवा श्रोताओं को समझाने के लिये उन्हें भाषा में फेरफार करना पड़ा। अभयदेव और मलयागिरि आदि टीकाकारों की टीकाओं में भाषासम्बन्धी यह फेरफार स्पष्ट लक्षित होता है। जैन आगमों की अर्धमागधी भाषा और बौद्धसूत्रों की पालिभाषा के एक ही प्रदेश और काल
. .. मुनि पुण्यविजय जी से ज्ञात हुआ है कि भगवतीसूत्र आदि की हस्तलिखित प्राचीन प्रतियों में महावीरे के स्थान पर मधावीरे और देवेहिं के स्थान पर देवेभिं आदि पाठ मिलते हैं। .. २. मुनि पुण्यविजयजी ने आगमों की प्राचीनतम हस्तलिखित प्रतियों में भाषा और प्रयोग की प्रचुर विविधतायें पाये जाने का उल्लेख बृहत्कल्पसूत्र, छठे भाग की प्रस्तावना, पृष्ठ ५७ पर किया है। तथा देखिये उनकी कल्पसूत्र ( साराभाई मणिलाल नवाब, अहमदाबाद) की प्रस्तावना पृष्ठ ४-६, उन्हीं की अंगविज्जा की प्रस्तावना, पृष्ठ ८-११।