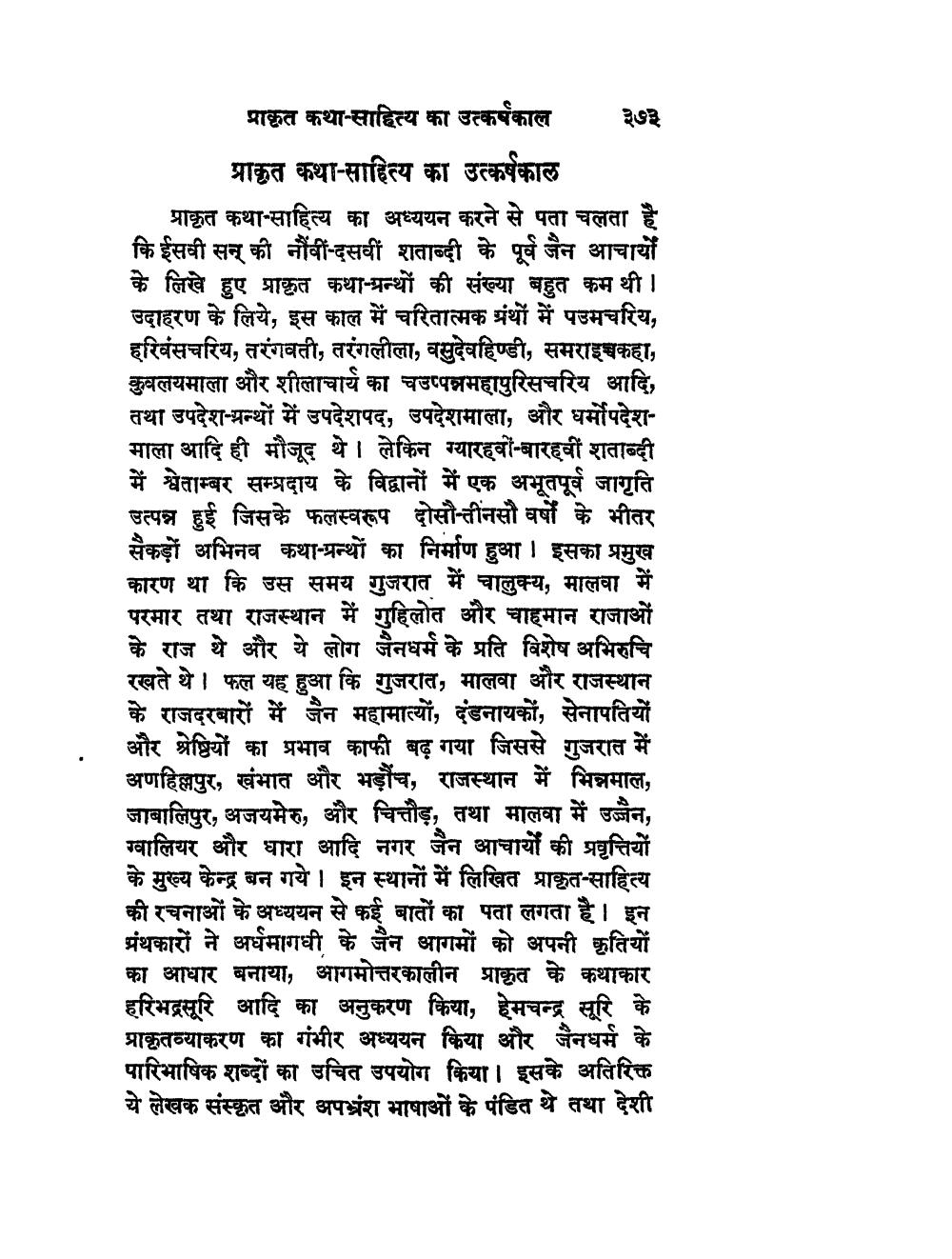________________
प्राकृत कथा-साहित्य का उत्कर्षकाल ३७३
प्राकृत कथा-साहित्य का उत्कर्षकाल प्राकृत कथा-साहित्य का अध्ययन करने से पता चलता है कि ईसवी सन की नौंवीं-दसवीं शताब्दी के पूर्व जैन आचार्यों के लिखे हुए प्राकृत कथा-ग्रन्थों की संख्या बहुत कम थी। उदाहरण के लिये, इस काल में चरितात्मक ग्रंथों में पउमचरिय, हरिवंसचरिय, तरंगवती, तरंगलीला, वसुदेवहिण्डी, समराइचकहा, कुवलयमाला और शीलाचार्य का चउप्पन्नमहापुरिसचरिय आदि, तथा उपदेश-ग्रन्थों में उपदेशपद, उपदेशमाला, और धर्मोपदेशमाला आदि ही मौजूद थे। लेकिन ग्यारहवीं-बारहवीं शताब्दी में श्वेताम्बर सम्प्रदाय के विद्वानों में एक अभूतपूर्व जागृति उत्पन्न हुई जिसके फलस्वरूप दोसौ-तीनसौ वर्षों के भीतर सैकड़ों अभिनव कथा-ग्रन्थों का निर्माण हुआ | इसका प्रमुख कारण था कि उस समय गुजरात में चालुक्य, मालवा में परमार तथा राजस्थान में गुहिलोत और चाहमान राजाओं के राज थे और ये लोग जैनधर्म के प्रति विशेष अभिरुचि रखते थे। फल यह हुआ कि गुजरात, मालवा और राजस्थान के राजदरबारों में जैन महामात्यों, दंडनायकों, सेनापतियों
और श्रेष्टियों का प्रभाव काफी बढ़ गया जिससे गुजरात में अणहिल्लपुर, खंभात और भडौंच, राजस्थान में भिन्नमाल, जाबालिपुर, अजयमेरु, और चित्तौड़, तथा मालवा में उज्जैन, ग्वालियर और धारा आदि नगर जैन आचार्यों की प्रवृत्तियों के मुख्य केन्द्र बन गये। इन स्थानों में लिखित प्राकृत-साहित्य की रचनाओं के अध्ययन से कई बातों का पता लगता है। इन ग्रंथकारों ने अर्धमागधी के जैन आगमों को अपनी कृतियों का आधार बनाया, आगमोत्तरकालीन प्राकृत के कथाकार हरिभद्रसूरि आदि का अनुकरण किया, हेमचन्द्र सूरि के प्राकृतव्याकरण का गंभीर अध्ययन किया और जैनधर्म के पारिभाषिक शब्दों का उचित उपयोग किया। इसके अतिरिक्त ये लेखक संस्कृत और अपभ्रंश भाषाओं के पंडित थे तथा देशी