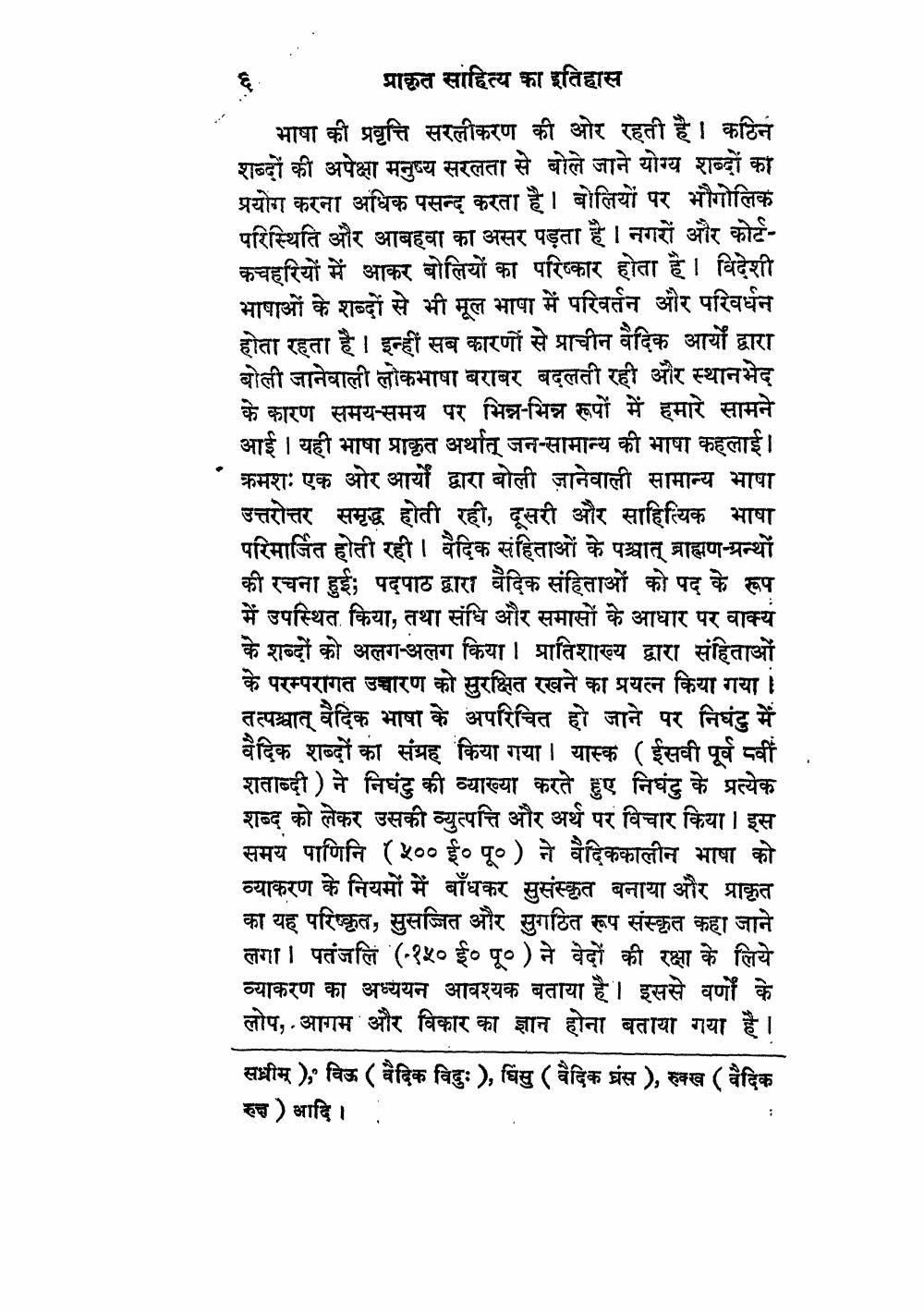________________
प्राकृत साहित्य का इतिहास भाषा की प्रवृत्ति सरलीकरण की ओर रहती है। कठिन शब्दों की अपेक्षा मनुष्य सरलता से बोले जाने योग्य शब्दों का प्रयोग करना अधिक पसन्द करता है। बोलियों पर भौगोलिक परिस्थिति और आबहवा का असर पड़ता है। नगरों और कोर्टकचहरियों में आकर बोलियों का परिष्कार होता है। विदेशी भाषाओं के शब्दों से भी मूल भाषा में परिवर्तन और परिवर्धन होता रहता है। इन्हीं सब कारणों से प्राचीन वैदिक आर्यों द्वारा बोली जानेवाली लोकभाषा बराबर बदलती रही और स्थानभेद के कारण समय-समय पर भिन्न-भिन्न रूपों में हमारे सामने आई । यही भाषा प्राकृत अर्थात् जन-सामान्य की भाषा कहलाई। क्रमशः एक ओर आर्यों द्वारा बोली जानेवाली सामान्य भाषा उत्तरोत्तर समृद्ध होती रही, दूसरी और साहित्यिक भाषा परिमार्जित होती रही। वैदिक संहिताओं के पश्चात् ब्राह्मण-अन्थों की रचना हुई; पदपाठ द्वारा वैदिक संहिताओं को पद के रूप में उपस्थित किया, तथा संधि और समासों के आधार पर वाक्य के शब्दों को अलग-अलग किया। प्रातिशाख्य द्वारा संहिताओं के परम्परागत उच्चारण को सुरक्षित रखने का प्रयत्न किया गया। तत्पश्चात् वैदिक भाषा के अपरिचित हो जाने पर निघंटु में वैदिक शब्दों का संग्रह किया गया। यास्क ( ईसवी पूर्व पवीं शताब्दी) ने निघंटु की व्याख्या करते हुए निघंटु के प्रत्येक शब्द को लेकर उसकी व्युत्पत्ति और अर्थ पर विचार किया। इस समय पाणिनि ( ५०० ई० पू०) ने वैदिककालीन भाषा को व्याकरण के नियमों में बाँधकर सुसंस्कृत बनाया और प्राकृत का यह परिष्कृत, सुसज्जित और सुगठित रूप संस्कृत कहा जाने लगा। पतंजलि (-१५० ई० पू०) ने वेदों की रक्षा के लिये व्याकरण का अध्ययन आवश्यक बताया है। इससे वर्णों के लोप, आगम और विकार का ज्ञान होना बताया गया है। सधीम् ); विऊ (वैदिक विदुः), प्रिंसु (वैदिक घंस), रुक्ख (वैदिक रुक्ष) आदि।