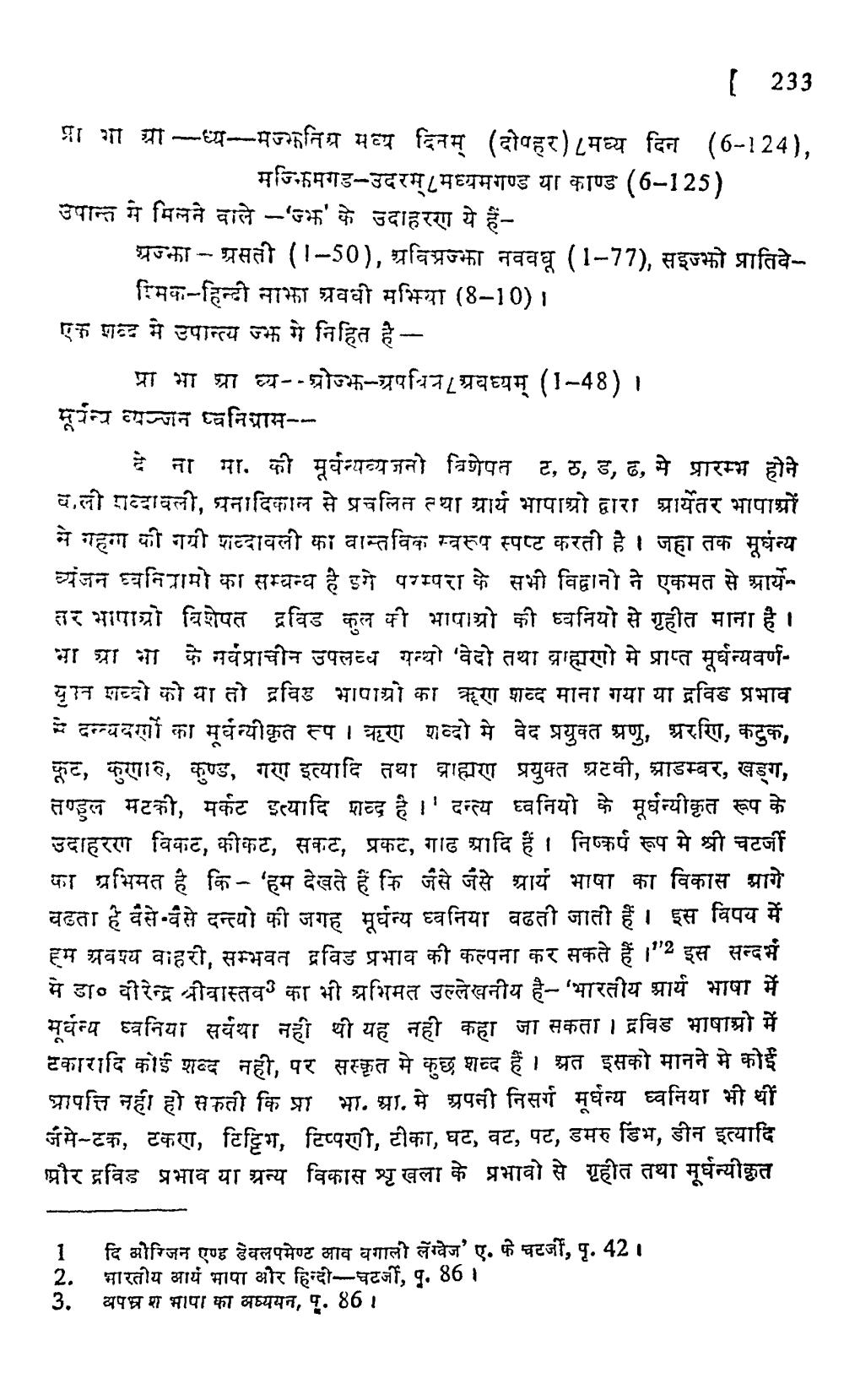________________
[ 233 प्रा मा या -~-ध्य-मज्झनिय मध्य दिनम् (दोपहर) मध्य दिन (6-124),
मजिक्रमगड-उदरम।मध्यमगण्ड या काण्ड (6-125) उपान्त मे मिलने वाले -'झ' के उदाहरण ये हैं
अज्झा - असती (1-50), अविप्रज्झा नववधू (1-77), सइज्झो प्रातिवे
निमक-हिन्दी नाझा अवधी मझ्यिा (8-10)। एक शब्द मे उपान्त्य ज्झ में निहित है
प्रा भा या ध्य-- प्रोझ-अपवित्र/अवध्यम् (1-48)। मूर्यन्त्र व्यञ्जन ध्वनिग्राम---
दे ना मा. की मूर्धन्यव्य जनो विपत ट, ठ, ड, ढ, मे प्रारम्भ होने वाली शब्दावली, घनादिकाल से प्रचलित तथा प्रार्य भापात्रो द्वारा प्रार्येतर भापायों ने गहण की गयी शब्दावली का वास्तविक स्वरूप स्पष्ट करती है । जहा तक मूर्धन्य व्यंजन ध्वनियामो का सम्बन्ध है इगे परम्परा के सभी विद्वानो ने एकमत से आर्यतर भापायो विशेषत द्रविड कल की भापायो की ध्वनियो से गृहीत माना है। भा या भा के मर्वप्राचीन उपलव्य यन्यो 'वेदो तथा ब्राह्मणो मे प्राप्त मूर्धन्यवर्णयुात शब्दो को या तो द्रविड भाषाम्रो का ऋण शब्द माना गया या द्रविड प्रभाव में दन्यदों का मूर्वन्यीकृत प । ऋण शब्दो मे वेद प्रयुक्त अणु, अरणि, कटुक, कूट, कुणाल, कुण्ड, गण इत्यादि तथा ब्राह्मण प्रयुक्त अटवी, आडम्बर, खड्ग, तण्डुल मटकी, मर्कट इत्यादि शब्द है । ' दन्त्य ध्वनियो के मूर्धन्यीकृत रूप के उदाहरण विकट, कीकट, सकट, प्रकट, गाढ आदि हैं। निष्कर्ष रूप मे श्री चटर्जी का अभिमत है कि- 'हम देखते हैं कि जैसे जैसे प्रार्य भाषा का विकास आगे बढता है वैसे-वैसे दन्त्यो की जगह मूर्धन्य ध्वनिया बढती जाती हैं। इस विपय में हम अवश्य बाहरी, सम्भवत द्रविड प्रभाव की कल्पना कर सकते हैं ।"2 इस सन्दर्भ में डा० वीरेन्द्र श्रीवास्तव का भी अभिमत उल्लेखनीय है- 'भारतीय आर्य भाषा में मूर्धन्य ध्वनिया सर्वथा नही थी यह नहीं कहा जा सकता। द्रविड भाषामो में टकारादि कोई शब्द नही, पर सस्कृत मे कुछ शब्द हैं । अत इसको मानने में कोई प्रापत्ति नहीं हो सकती कि प्रा भा. प्रा. मे अपनी निसर्ग मूर्धन्य ध्वनिया भी थीं जमे-टक, टकरण, टिट्रिम, टिप्पणी, टीका, घट, वट, पट, डमरु डिंभ, डीन इत्यादि पौर द्रविड प्रभाव या अन्य विकास शृखला के प्रभावो से गृहीत तथा मूर्धन्यीकृत
दि मोरिजन एण्ड डेवलपमेण्ट भाव वगाली लेंग्वेज' ए. फे चटर्जी, पृ. 42। 2. भारतीय आर्य भापा और हिन्दी-चटर्जी, पृ. 861 3. अपभ्र श भाषा का अध्ययन, पृ. 861