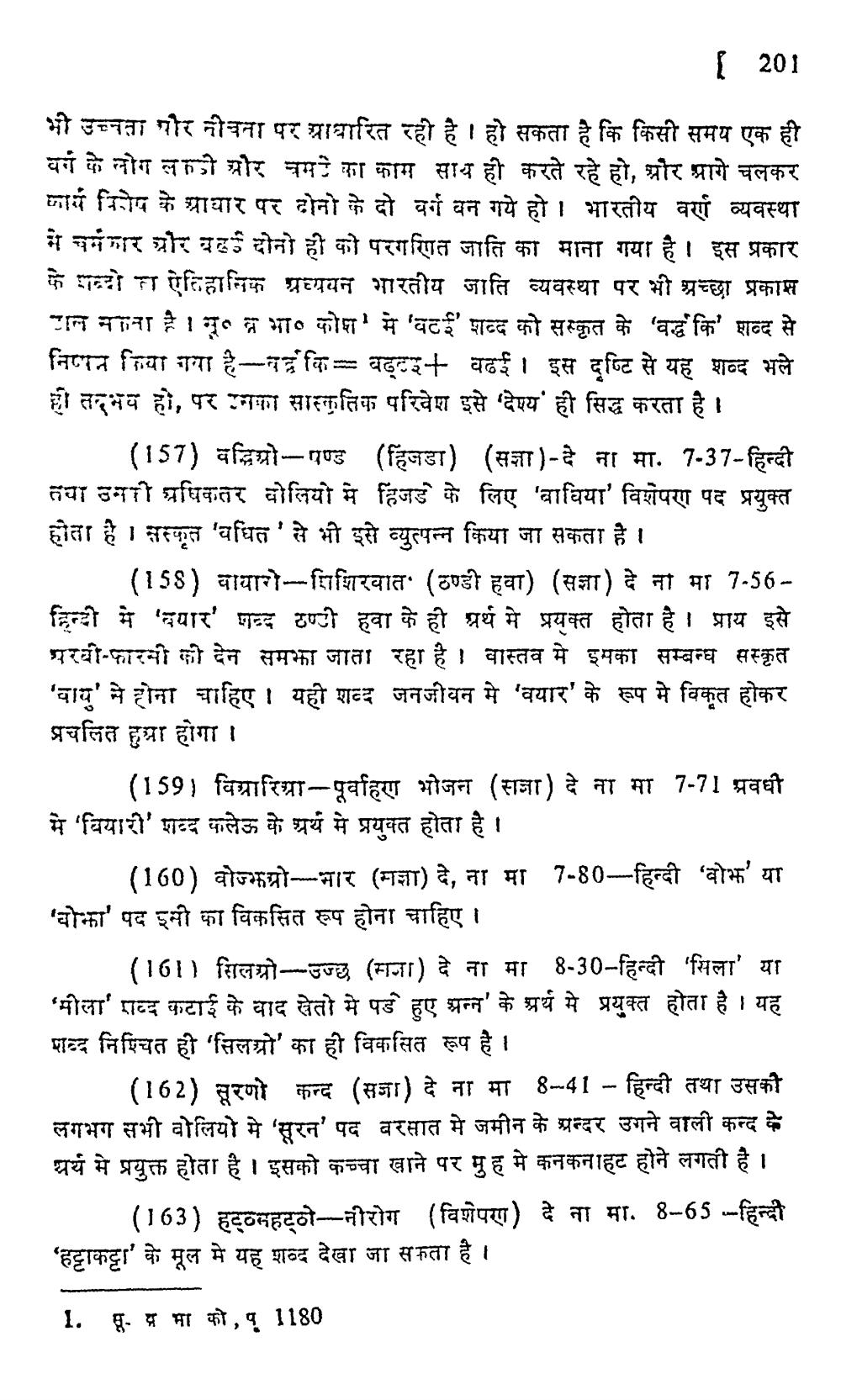________________
।
201
भी उच्नता गौर नीचता पर आधारित रही है । हो सकता है कि किसी समय एक ही वर्ग के लोग लककी और चमटे का काम साय ही करते रहे हो, और आगे चलकर मार्ग निरोप के आधार पर दोनो के दो वर्ग बन गये हो। भारतीय वर्ण व्यवस्था में चमगार और वह दोनो ही को परगणित जाति का माना गया है। इस प्रकार फे शब्दो ऐतिहानिक अध्ययन भारतीय जाति व्यवस्था पर भी अच्छा प्रकाश पाल नाता है । मूलद्र भा० कोश में 'वटई' शब्द को सस्कृत के 'वर्द्ध कि' शब्द से निप्पन किया गया है-पकि= बढ्द+ वढई। इस दृष्टि से यह शब्द भले ही तदभव हो, पर ममा सास्कृतिक परिवेश इसे 'देश्य ही सिद्ध करता है ।
(157) वद्धियो- पण्ड (हिंजडा) (सज्ञा)-दे ना मा. 7-37- हिन्दी तथा उनी अधिकतर बोलियो में हिजडे के लिए 'वाधिया' विशेपण पद प्रयुक्त होता है । सस्कृत 'वधित ' से भी इसे व्युत्पन्न किया जा सकता है ।
(158) वायागे-शिशिरवात: (ठण्डी हवा) (सज्ञा) दे ना मा 7-56 - हिन्दी में 'क्यार' शब्द ठण्डी हवा के ही प्रर्थ मे प्रयक्त होता है। प्राय इसे घरबी-फारनी की देन समझा जाता रहा है। वास्तव में इसका सम्बन्ध सस्कृत 'वायु मे होना चाहिए । यही शब्द जनजीवन मे 'वयार' के रूप मे विकृत होकर प्रचलित हुअा होगा।
(1591 विनारिया-पूर्वाहण भोजन (सजा) दे ना मा 7-71 अवधी मे 'बियारी' शब्द कालेऊ के अर्थ मे प्रयुक्त होता है ।
(160) वोज्झनो-भार (मज्ञा) दे, ना मा 7-80-हिन्दी 'वोझ' या 'वोझा' पद इसी का विकसित रूप होना चाहिए।
(161) सिलग्रो-उज्छ (मजा) दे ना मा 8-30-हिन्दी 'सिला' या 'मोला' शब्द कटाई के बाद खेतो मे पड़े हुए अन्न' के अर्थ मे प्रयुक्त होता है । यह मान्द निश्चित ही 'सिलयो' का ही विकसित रूप है ।
(162) सूरणो कन्द (सजा) दे ना मा 8-41 - हिन्दी तथा उसकी लगभग सभी बोलियो मे 'सूरन' पद बरसात मे जमीन के अन्दर उगने वाली कन्द के अर्थ मे प्रयुक्त होता है । इसको कच्चा खाने पर मुह मे कनकनाहट होने लगती है ।
(163) हमहो -नीरोग (विशेपण) दे ना मा. 8-65 --हिन्दी 'हट्टाकट्टा' के मूल मे यह शब्द देखा जा सकता है ।
1.
पू. ५ मा को, ५ 1180