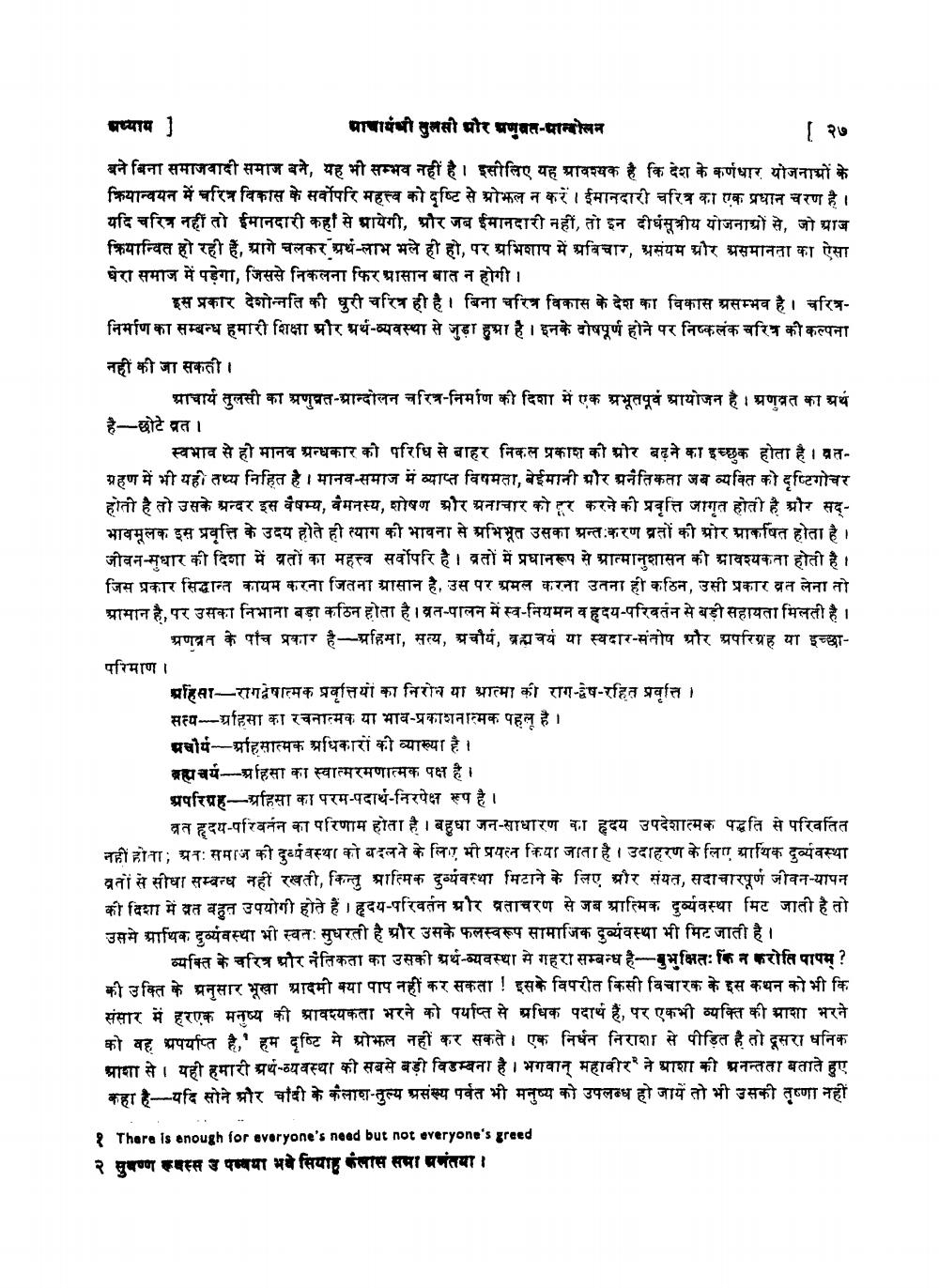________________
अध्याय प्राचार्यश्री तुलसी पौर प्रणवत-पादोलन
[ २७ बने बिना समाजवादी समाज बने, यह भी सम्भव नहीं है। इसीलिए यह आवश्यक है कि देश के कर्णधार योजनामों के क्रियान्वयन में चरित्र विकास के सर्वोपरि महत्त्व को दृष्टि से ओझल न करें। ईमानदारी चरित्र का एक प्रधान चरण है। यदि चरित्र नहीं तो ईमानदारी कहाँ से पायेगी, और जब ईमानदारी नहीं, तो इन दीर्घसूत्रीय योजनाओं से, जो ग्राज क्रियान्वित हो रही हैं, आगे चलकर अर्थ-लाभ भले ही हो, पर अभिशाप में अविचार, असंयम और असमानता का ऐसा घेरा समाज में पड़ेगा, जिससे निकलना फिर प्रासान बात न होगी।
इस प्रकार देशोन्नति की धुरी चरित्र ही है। बिना चरित्र विकास के देश का विकास असम्भव है। चरित्रनिर्माण का सम्बन्ध हमारी शिक्षा और अर्थ-व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। इनके दोषपूर्ण होने पर निष्कलंक चरित्र की कल्पना नहीं की जा सकती।
प्राचार्य तुलसी का अणुव्रत-आन्दोलन चरित्र-निर्माण की दिशा में एक अभूतपूर्व प्रायोजन है । अणुव्रत का अर्थ है-छोटे व्रत।
स्वभाव से ही मानव अन्धकार को परिधि से बाहर निकल प्रकाश की ओर बढ़ने का इच्छुक होता है। प्रतग्रहण में भी यही तथ्य निहित है। मानव-समाज में व्याप्त विषमता, बेईमानी और अनैतिकता जब व्यक्ति को दृष्टिगोचर होती है तो उसके अन्दर इस वैषम्य, वैमनस्य, शोषण और अनाचार को दूर करने की प्रवृत्ति जागृत होती है और सद्भावमूलक इस प्रवृत्ति के उदय होते ही त्याग की भावना से अभिभूत उसका अन्तःकरण व्रतों की ओर आकर्षित होता है। जीवन-मधार की दिशा में प्रतों का महत्त्व सर्वोपरि है। व्रतों में प्रधानरूप से प्रात्मानुशासन की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार सिद्धान्त कायम करना जितना आसान है, उस पर अमल करना उतना ही कठिन, उसी प्रकार व्रत लेना तो प्रामान है, पर उसका निभाना बड़ा कठिन होता है। व्रत-पालन में स्व-नियमन व हृदय-परिवर्तन से बड़ी सहायता मिलती है।
प्रणवत के पांच प्रकार है-हिमा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य या स्वदार-संतोष और अपरिग्रह या इच्छापरिमाण।
अहिंसा-रागद्वेषात्मक प्रवृत्तियों का निरोच या प्रात्मा की राग-द्वेष-रहित प्रवृत्ति । सत्य-हिसा का रचनात्मक या भाव-प्रकाशनात्मक पहलू है। प्रचौर्य-हिसात्मक अधिकारों की व्याख्या है। ब्रह्मचर्य-अहिसा का स्वात्मरमणात्मक पक्ष है। अपरिग्रह-हिसा का परम-पदार्थ-निरपेक्ष रूप है।
व्रत हृदय-परिवर्तन का परिणाम होता है । बहुधा जन-साधारण का हृदय उपदेशात्मक पद्धति से परिवर्तित नहीं होता; अतः समाज की दुर्व्यवस्था को बदलने के लिए भी प्रयत्न किया जाता है। उदाहरण के लिए आर्थिक दुर्व्यवस्था व्रतों से सीधा सम्बन्ध नहीं रखती, किन्तु पात्मिक दुव्यवस्था मिटाने के लिए और संयत, सदाचारपूर्ण जीवन-यापन की दिशा में व्रत बहुत उपयोगी होते हैं । हृदय-परिवर्तन और व्रताचरण से जब आत्मिक दुर्व्यवस्था मिट जाती है तो उसमे आथिक दृव्यवस्था भी स्वत: सुधरती है और उसके फलस्वरूप सामाजिक दुर्व्यवस्था भी मिट जाती है।
व्यक्ति के चरित्र और नैतिकता का उसकी अर्थ-व्यवस्था से गहरा सम्बन्ध है-भक्षितःकिन करोति पापम? की उक्ति के अनुसार भूखा पादमी क्या पाप नहीं कर सकता ! इसके विपरीत किसी विचारक के इस कथन को भी कि संसार में हरएक मनष्य की आवश्यकता भरने को पर्याप्त से अधिक पदार्थ हैं, पर एकभी व्यक्ति की भाशा भरने को वह अपर्याप्त है, हम दृष्टि मे प्रोझल नहीं कर सकते। एक निर्धन निराशा से पीड़ित है तो दूसरा धनिक आशा से। यही हमारी अर्थ-व्यवस्था की सबसे बड़ी विडम्बना है । भगवान् महावीर ने पाशा की अनन्तता बताते हुए कहा है-यदि सोने और चांदी के कैलाश-तुल्य प्रसंस्य पर्वत भी मनुष्य को उपलब्ध हो जाये तो भी उसकी तृष्णा नहीं
There is enough for everyone's need but not everyone's greed २ सुबण्ण बस्स उपन्यया भवे सियाह फैलास समाप्रतया।