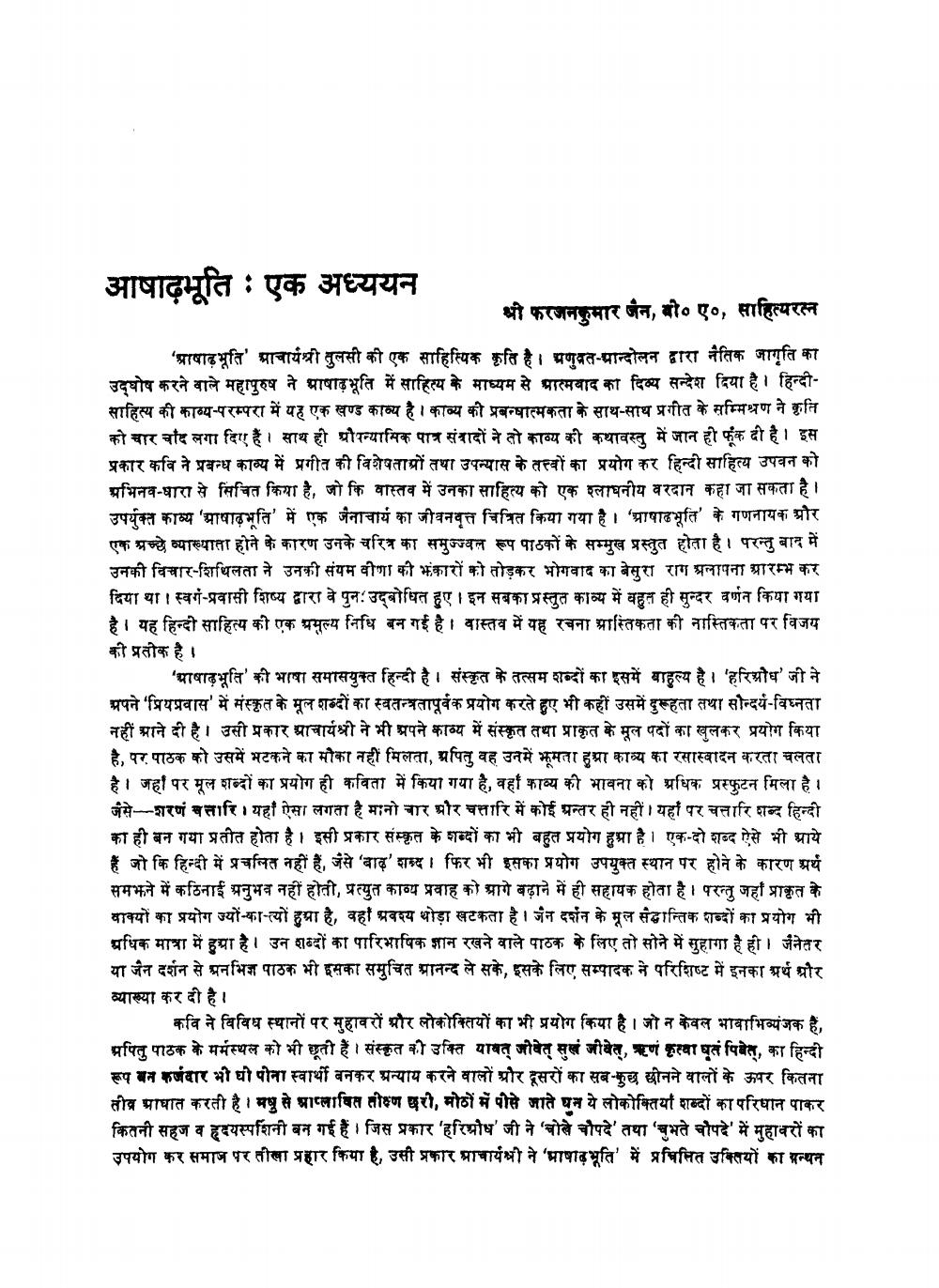________________
आषाढभूति : एक अध्ययन
श्री फरजनकुमार जैन, बी० ए०, साहित्यरत्न
'प्राषाढ़भूति' प्राचार्यश्री तुलसी की एक साहिस्यिक कृति है। प्रणवत-पान्दोलन द्वारा नैतिक जागृति का उद्घोष करने वाले महापुरुष ने भाषाढ़भूति में साहित्य के माध्यम से प्रात्मवाद का दिव्य सन्देश दिया है। हिन्दीसाहित्य की काव्य-परम्परा में यह एक खण्ड काव्य है। काव्य की प्रबन्धात्मकता के साथ-साथ प्रगीत के सम्मिश्रण ने कृति को चार चांद लगा दिए हैं। साथ ही प्रौपन्यामिक पात्र संवादों ने तो काव्य की कथावस्तु में जान ही फूंक दी है। इस प्रकार कवि ने प्रबन्ध काव्य में प्रगीत की विशेषतामों तथा उपन्यास के तत्त्वों का प्रयोग कर हिन्दी साहित्य उपवन को अभिनव-धारा से सिंचित किया है, जो कि वास्तव में उनका साहित्य को एक श्लाघनीय वरदान कहा जा सकता है। उपर्युक्त काव्य 'आषाढभूति' में एक जैनाचार्य का जीवनवृत्त चित्रित किया गया है। 'आषाढभूति' के गणनायक और एक अच्छे व्याख्याता होने के कारण उनके चरित्र का समुज्ज्वल रूप पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत होता है। परन्तु बाद में उनकी विचार-शिथिलता ने उनकी संयम वीणा की झंकारों को तोड़कर भोगवाद का बेसुरा राग अलापना प्रारम्भ कर दिया था। स्वर्ग-प्रवासी शिष्य द्वारा वे पुनः उद्बोधित हुए। इन सबका प्रस्तुत काव्य में बहुत ही सुन्दर वर्णन किया गया है। यह हिन्दी साहित्य की एक अमुल्य निधि बन गई है। वास्तव में यह रचना आस्तिकता की नास्तिकता पर विजय की प्रतीक है।
'आषाढ़भूति' की भाषा समासयुक्त हिन्दी है। संस्कृत के तत्सम शब्दों का इसमें बाहुल्य है। 'हरिऔध' जी ने अपने 'प्रियप्रवास' में संस्कृत के मूल शब्दों का स्वतन्त्रतापूर्वक प्रयोग करते हुए भी कहीं उसमें दुरूहता तथा सौन्दर्य-विघ्नता नहीं आने दी है। उसी प्रकार प्राचार्यश्री ने भी अपने काव्य में संस्कृत तथा प्राकृत के मूल पदों का खुलकर प्रयोग किया है, पर पाठक को उसमें भटकने का मौका नहीं मिलता, अपितु वह उनमें झूमता हुमा काव्य का रसास्वादन करता चलता है। जहां पर मूल शब्दों का प्रयोग ही कविता में किया गया है, वहाँ काव्य की भावना को अधिक प्रस्फुटन मिला है। जैसे-शरणं बत्तारि। यहाँ ऐसा लगता है मानो चार और चत्तारि में कोई अन्तर ही नहीं। यहाँ पर चत्तारि शब्द हिन्दी का ही बन गया प्रतीत होता है। इसी प्रकार संस्कृत के शब्दों का भी बहुत प्रयोग हुमा है। एक-दो शब्द ऐसे भी आये हैं जो कि हिन्दी में प्रचलित नहीं हैं, जैसे 'बाढ़' शब्द । फिर भी इसका प्रयोग उपयुक्त स्थान पर होने के कारण अर्थ समझने में कठिनाई अनुभव नहीं होती, प्रत्युत काव्य प्रवाह को आगे बढ़ाने में ही सहायक होता है। परन्तु जहाँ प्राकृत के वाक्यों का प्रयोग ज्यों-का-त्यों हुआ है, वहाँ अवश्य थोड़ा खटकता है । जैन दर्शन के मूल सैद्धान्तिक शब्दों का प्रयोग भी अधिक मात्रा में हुआ है। उन शब्दों का पारिभाषिक ज्ञान रखने वाले पाठक के लिए तो सोने में सुहागा है ही। जनेतर या जैन दर्शन से अनभिज्ञ पाठक भी इसका समुचित प्रानन्द ले सके, इसके लिए सम्पादक ने परिशिष्ट में इनका अर्थ और व्याख्या कर दी है।
कवि ने विविध स्थानों पर मुहावरों और लोकोक्तियों का भी प्रयोग किया है। जो न केवल भावाभिव्यंजक है, अपितु पाठक के मर्मस्थल को भी छूती हैं । संस्कृत की उक्ति यावत् जोवेत् सुखं जीवेत, ऋणं कृत्वातं पिबेत, का हिन्दी रूप बन कर्जदार भी घी पीना स्वार्थी बनकर अन्याय करने वालों और दूसरों का सब-कुछ छीनने वालों के ऊपर कितना तीव्र प्राघात करती है। मधु से प्राप्लाषित तीक्ष्ण छरी, मोठों में पीसे जाते घन ये लोकोक्तियाँ शब्दों का परिधान पाकर कितनी सहज व हृदयस्पशिनी बन गई हैं। जिस प्रकार 'हरिऔध' जी ने 'चोखे चौपदे' तथा 'चुभते चौपदे' में मुहावरों का उपयोग कर समाज पर तीखा प्रहार किया है, उसी प्रकार प्राचार्यश्री ने 'भाषाढ़भूति' में प्रचिलित उक्तियों का मन्थन