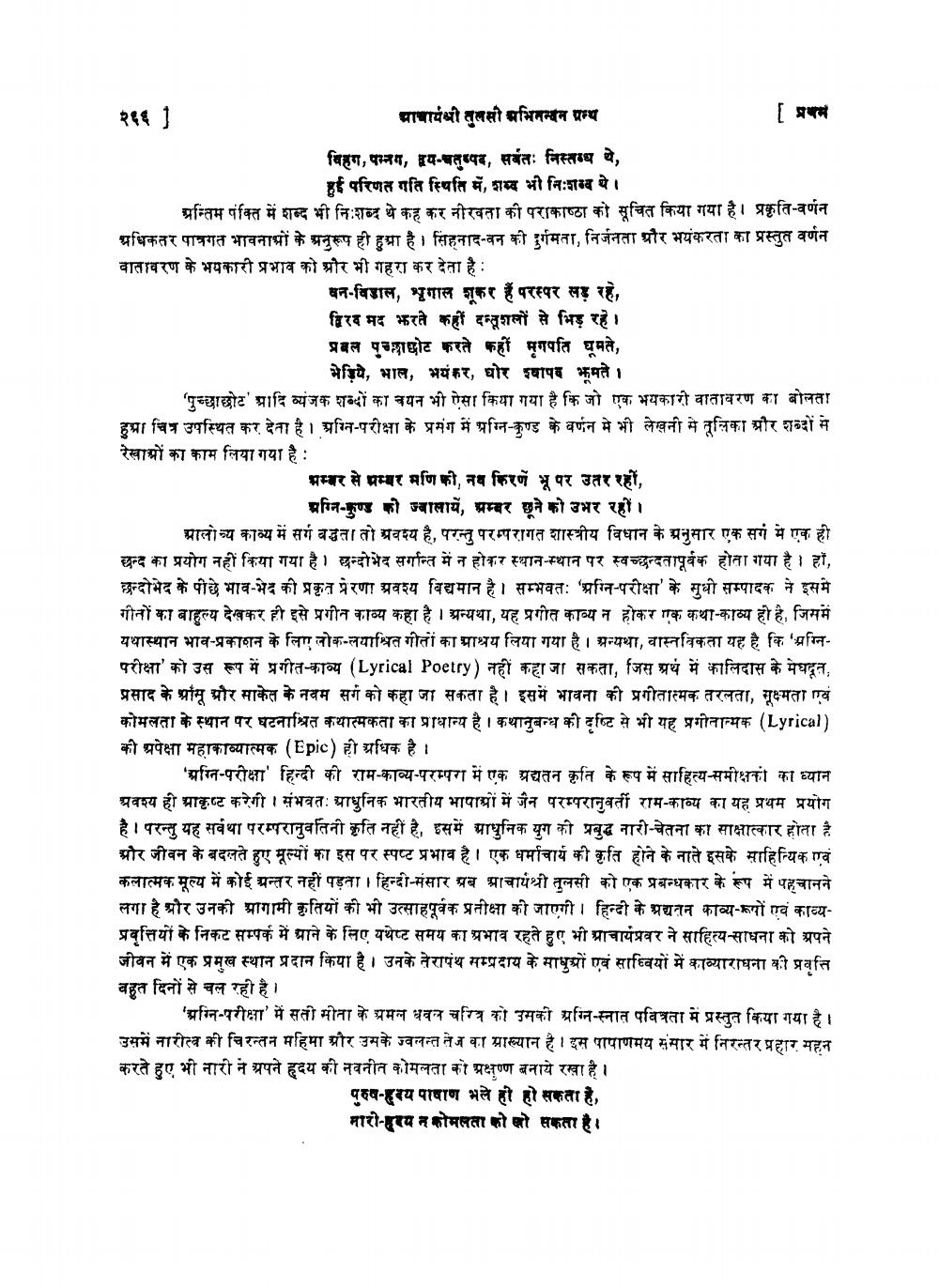________________
२६६ ]
प्राचार्यश्री तुलसी अभिनन्दन अन्य विहग, पन्नग, य-चतुष्पद, सर्वतः निस्तब्ध थे,
हुई परिणत गति स्थिति में, शम्द भी निःशम्ब थे। अन्तिम पंक्ति में शब्द भी निःशब्द थे कह कर नीरवता की पराकाष्ठा को सूचित किया गया है। प्रकृति-वर्णन अधिकतर पात्रगत भावनामों के अनुरूप ही हुआ है। सिंहनाद-वन की दुर्गमता, निर्जनता और भयंकरता का प्रस्तुत वर्णन वातावरण के भयकारी प्रभाव को और भी गहरा कर देता है :
धन-विडाल, भृगाल शूकर हैं परस्पर सड़ रहे, हिरव मद करते कहीं दन्तूशलों से भिड़ रहे। प्रबल पुण्याछोट करते कहीं मृगपति घूमते,
भेड़िये, भाल, भयंकर, घोर श्वापर झूमते । 'पुच्छाछोट' प्रादि व्यंजक शब्दों का चयन भी ऐसा किया गया है कि जो एक भयकारी वातावरण का बोलता हुमा चित्र उपस्थित कर देता है। अग्नि-परीक्षा के प्रमंग में अग्नि-कुण्ड के वर्णन मे भी लेखनी मे तूलिका और शब्दों में रेखाओं का काम लिया गया है :
अम्बर से सम्बर मणि की, नव किरणें भू पर उतर रही,
अग्नि-कुण्ड को ज्वालायें, अम्बर छूने को उभर रहीं। मालोच्य काव्य में सर्ग बद्धता तो अवश्य है, परन्तु परम्परागत शास्त्रीय विधान के अनुसार एक सगं में एक ही छन्द का प्रयोग नहीं किया गया है। छन्दोभेद सर्गान्त में न होकर स्थान-स्थान पर स्वच्छन्दतापूर्वक होता गया है। हों, छन्दोभेद के पीछे भाव-भेद की प्रकृत प्रेरणा अवश्य विद्यमान है। सम्भवत: 'अग्नि-परीक्षा' के सुधी सम्पादक ने इसमें गीनों का बाहुल्य देखकर ही इसे प्रगीत काव्य कहा है । अन्यथा, यह प्रगीत काव्य न होकर एक कथा-काव्य ही है, जिसमें यथास्थान भाव-प्रकाशन के लिए लोक-लयाश्रित गीतों का प्राश्रय लिया गया है । अन्यथा, वास्तविकता यह है कि 'अग्निपरीक्षा' को उस रूप में प्रगीत-काव्य (Lyrical Poetry) नहीं कहा जा सकता, जिस अर्थ में कालिदास के मेघदूत, प्रसाद के प्रामू और माकेत के नवम सर्ग को कहा जा सकता है। इसमें भावना की प्रगीतात्मक तरलता, मूक्ष्मता एवं कोमलता के स्थान पर घटनाश्रित कथात्मकता का प्राधान्य है । कथानुबन्ध की दृष्टि से भी यह प्रगीतान्मक (Lyrical) की अपेक्षा महाकाव्यात्मक (Epic) ही अधिक है।
'अग्नि-परीक्षा' हिन्दी की राम-काव्य-परम्पग में एक अद्यतन कृति के रूप में साहित्य-समीक्षकी का ध्यान अवश्य ही प्राकृष्ट करेगी। संभवतः आधुनिक भारतीय भापायों में जैन परम्परानुवर्ती राम-काव्य का यह प्रथम प्रयोग है । परन्तु यह सर्वथा परम्परानुवतिनी कृति नहीं है, इसमें आधुनिक युग की प्रबुद्ध नारी-चेतना का साक्षात्कार होता है और जीवन के बदलते हुए मूल्यों का इस पर स्पष्ट प्रभाव है। एक धर्माचार्य की कृति होने के नाते इसके साहित्यिक एवं कलात्मक मूल्य में कोई अन्तर नहीं पड़ता। हिन्दी-मंसार अब प्राचार्यश्री तुलसी को एक प्रबन्धकार के रूप में पहचानने लगा है और उनकी आगामी कृतियों की भी उत्साहपूर्वक प्रतीक्षा की जाएगी। हिन्दी के प्रद्यतन काव्य-रूपों एवं काव्यप्रवृत्तियों के निकट सम्पर्क में पाने के लिए यथेष्ट समय का प्रभाव रहते हुए भी प्राचार्यप्रवर ने साहित्य-साधना को अपने जीवन में एक प्रमुख स्थान प्रदान किया है। उनके तेरापंथ सम्प्रदाय के माधुओं एवं साध्वियों में काव्याराधना की प्रवृत्ति बहुत दिनों से चल रही है।
'अग्नि-परीक्षा' में सती मीता के अमन धवन चरित्र को उसकी अग्नि-स्नात पवित्रता में प्रस्तुत किया गया है। उसमें नारीत्व की चिरन्तन महिमा और उसके ज्वलन्त तेज का पाख्यान है । इस पापाणमय संसार में निरन्तर प्रहार महन करते हुए भी नारी ने अपने हृदय की नवनीत कोमलता को प्रक्षण्ण बनाये रखा है।
पुरुष-हत्य पाषाण भले ही हो सकता है, मारो-हरयन कोमलता को खो सकता है।