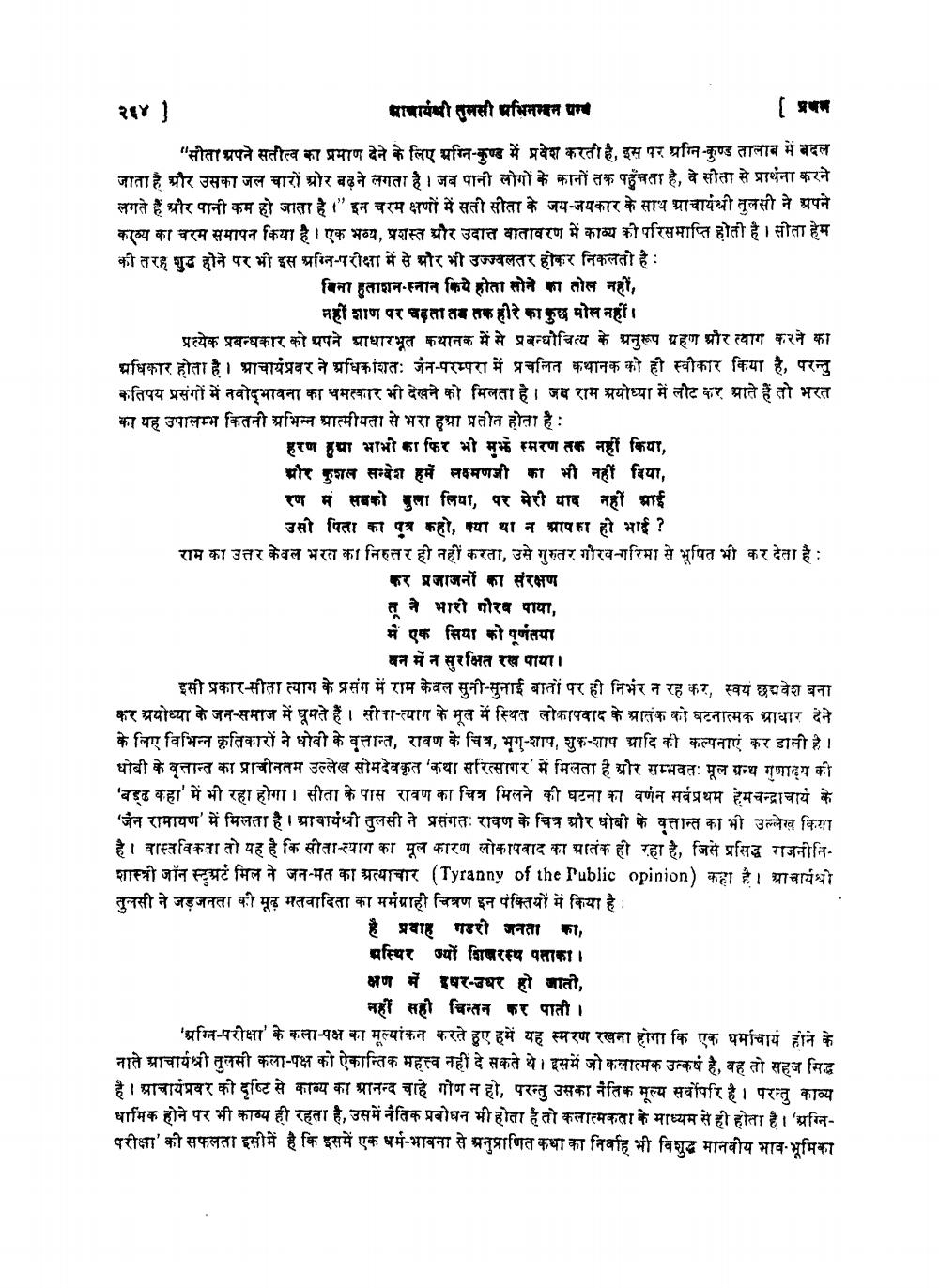________________
२६४
भाचायची तमसी अभिनन्दन पन्च "सीता अपने सतीत्व का प्रमाण देने के लिए मग्नि-कुण्ड में प्रवेश करती है, इस पर अग्नि-कुण्ड तालाब में बदल जाता है और उसका जल चारों ओर बढ़ने लगता है। जब पानी लोगों के कानों तक पहुँचता है, वे सीता से प्रार्थना करने लगते हैं और पानी कम हो जाता है।" इन चरम क्षणों में सती सीता के जय-जयकार के साथ प्राचार्यश्री तुलसी ने अपने काव्य का चरम समापन किया है। एक भव्य, प्रशस्त और उदात वातावरण में काव्य की परिसमाप्ति होती है। सीता हेम की तरह शुद्ध होने पर भी इस अग्नि-परीक्षा में से और भी उज्ज्वलतर होकर निकलती है :
बिना हुताशन-स्नान किये होता सोने का तोल नहीं,
नहीं शाण पर चढ़ता तब तक हीरे का कुछ मोल नहीं। प्रत्येक प्रबन्धकार को अपने आधारभूत कथानक में से प्रबन्धौचित्य के अनुरूप ग्रहण और त्याग करने का अधिकार होता है। प्राचार्यप्रवर ने अधिकांशतः जैन-परम्परा में प्रचलित कथानक को ही स्वीकार किया है, परन्तु कतिपय प्रसंगों में नवोभावना का चमत्कार भी देखने को मिलता है। जब राम अयोध्या में लौट कर पाते हैं तो भरत का यह उपालम्भ कितनी अभिन्न प्रात्मीयता से भरा हुआ प्रतीत होता है :
हरण हमा भाभी का फिर भी मुझे स्मरण तक नहीं किया, भोर कुशल सन्वेश हमें लक्ष्मणजी का भी नहीं दिया, रण में सबको बुला लिया, पर मेरी याद नहीं आई
उसी पिता का पुत्र कहो, क्या था न आपका हो भाई ? राम का उत्तर केवल भरत का निरुत्तर ही नहीं करता, उसे गुरुतर गौरव-गरिमा से भूपित भी कर देता है :
कर प्रजाजनों का संरक्षण तू ने भारी गौरव पाया, में एक सिया को पूर्णतया
वन में न सुरक्षित रख पाया। इसी प्रकार-सीता त्याग के प्रसंग में राम केवल सुनी-सुनाई बातों पर ही निर्भर न रह कर, स्वयं छयवेश बना कर अयोध्या के जन-समाज में घूमते हैं। सीता-त्याग के मूल में स्थित लोकापवाद के पातक को घटनात्मक प्राधार देने के लिए विभिन्न कृतिकारों ने धोबी के वृत्तान्त, रावण के चित्र, भूग-शाप, शुक-शाप आदि की कल्पनाएं कर डाली है। धोबी के वृत्तान्त का प्राचीनतम उल्लेख सोमदेवकृत 'कथा सरित्सागर' में मिलता है और सम्भवतः मूल ग्रन्थ गणाढ्य की 'बड़ढ कहा' में भी रहा होगा। सीता के पास रावण का चित्र मिलने की घटना का वर्णन सर्वप्रथम हेमचन्द्राचार्य के 'जैन रामायण' में मिलता है। प्राचार्यधी तुलसी ने प्रसंगतः रावण के चित्र और धोबी के वृत्तान्त का भी उल्लेख किया है। वास्तविकता तो यह है कि सीता-स्याग का मूल कारण लोकापवाद का अातंक ही रहा है, जिसे प्रसिद्ध राजनीनिशास्त्री जॉन स्टुअर्ट मिल ने जन-मत का अत्याचार (Tyranny of the Public opinion) कहा है। प्राचार्यश्री तुलसी ने जड़जनता की मूढ मतवादिता का मर्मग्राही चित्रण इन पंक्तियों में किया है :
है प्रवाह गरी जनता का, अस्थिर ज्यों शिखरस्थ पताका। क्षण में इधर-उधर हो जाती,
नहीं सही चिन्तन कर पाती। 'अग्नि-परीक्षा' के कला-पक्ष का मूल्यांकन करते हुए हमें यह स्मरण रखना होगा कि एक धर्माचार्य होने के नाते प्राचार्यश्री तुलसी कला-पक्ष को ऐकान्तिक महत्व नहीं दे सकते थे। इसमें जो कलात्मक उत्कर्ष है, वह तो सहज सिद्ध है। प्राचार्यप्रवर की दृष्टि से काव्य का प्रानन्द चाहे गोण न हो, परन्तु उसका नैतिक मूल्य सर्वोपरि है। परन्तु काव्य धार्मिक होने पर भी काव्य ही रहता है, उसमें नैतिक प्रबोधन भी होता है तो कलात्मकता के माध्यम से ही होता है। 'अग्निपरीक्षा' की सफलता इसी में है कि इसमें एक धर्म-भावना से अनुप्राणित कथा का निर्वाह भी विशुद्ध मानवीय भाव- भूमिका