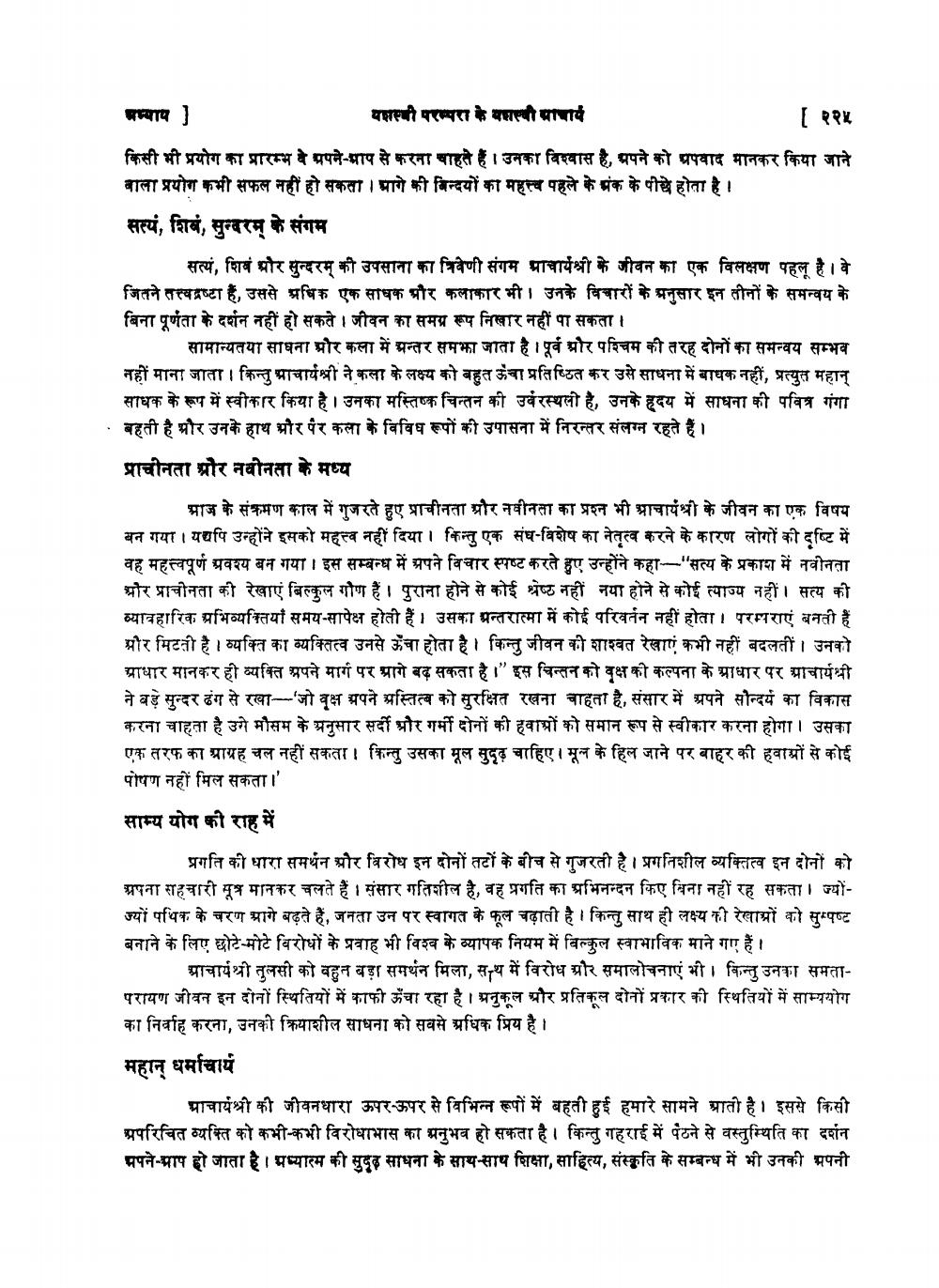________________
यशस्वी परम्परा के बारवी पाचार्य
[ २२५
किसी भी प्रयोग का प्रारम्भ वे अपने-आप से करना चाहते हैं। उनका विश्वास है, अपने को अपवाद मानकर किया जाने वाला प्रयोग कभी सफल नहीं हो सकता। मागेकी बिन्दयों का महत्त्व पहले के अंक के पीछे होता है। सत्यं, शिवं, सुन्दरम् के संगम
सत्यं, शिवं और सुन्दरम् की उपसाना का त्रिवेणी संगम प्राचार्यश्री के जीवन का एक विलक्षण पहल है। वे जितने तत्त्वद्रष्टा है, उससे अधिक एक साधक और कलाकार भी। उनके विचारों के अनुसार इन तीनों के समन्वय के बिना पूर्णता के दर्शन नहीं हो सकते। जीवन का समग्र रूप निखार नहीं पा सकता।
सामान्यतया साधना और कला में अन्तर समझा जाता है। पूर्व और पश्चिम की तरह दोनों का समन्वय सम्भव नहीं माना जाता। किन्तु प्राचार्यश्री ने कला के लक्ष्य को बहुत ऊंचा प्रतिष्ठित कर उसे साधना में बाधक नहीं, प्रत्युत महान्
साधक के रूप में स्वीकार किया है। उनका मस्तिष्क चिन्तन की उर्वरस्थली है, उनके हृदय में साधना की पवित्र गंगा • बहती है और उनके हाथ और पैर कला के विविध रूपों की उपासना में निरन्तर संलग्न रहते हैं। प्राचीनता और नवीनता के मध्य
माज के संक्रमण काल में गुजरते हुए प्राचीनता और नवीनता का प्रश्न भी प्राचार्यश्री के जीवन का एक विषय बन गया । यद्यपि उन्होंने इसको महत्व नहीं दिया। किन्तु एक संघ-विशेष का नेतृत्व करने के कारण लोगों की दष्टि में वह महत्त्वपूर्ण अवश्य बन गया। इस सम्बन्ध में अपने विचार स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा-"सत्य के प्रकाश में नवीनता
और प्राचीनता की रेखाएं बिल्कुल गौण हैं। पुराना होने से कोई श्रेष्ठ नहीं नया होने से कोई त्याज्य नहीं। सत्य की व्यावहारिक अभिव्यक्तियां समय-सापेक्ष होती हैं। उसका अन्तरात्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। परम्पराएं बनती हैं और मिटती है। व्यक्ति का व्यक्तित्व उनसे ऊँचा होता है। किन्तु जीवन की शाश्वत रेखाएं कभी नहीं बदलतीं। उनको आधार मानकर ही व्यक्ति अपने मार्ग पर आगे बढ़ सकता है।" इस चिन्तन को वृक्ष की कल्पना के आधार पर प्राचार्यश्री ने बड़े सुन्दर ढंग से रखा-'जो वृक्ष अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखना चाहता है, संसार में अपने सौन्दर्य का विकास करना चाहता है उसे मौसम के अनुसार सर्दी और गर्मी दोनों की हवाओं को समान रूप से स्वीकार करना होगा। उसका एक तरफ का आग्रह चल नहीं सकता। किन्तु उसका मूल सुदृढ़ चाहिए। मूल के हिल जाने पर बाहर की हवाओं से कोई पोषण नहीं मिल सकता।'
साम्य योग की राह में
प्रगति की धारा समर्थन और विरोध इन दोनों तटों के बीच से गुजरती है। प्रगतिशील व्यक्तित्व इन दोनों को अपना सहचारी मूत्र मानकर चलते हैं । संसार गतिशील है, वह प्रगति का अभिनन्दन किए बिना नहीं रह सकता। ज्योंज्यों पथिक के चरण आगे बढ़ते हैं, जनता उन पर स्वागत के फूल चढ़ाती है। किन्तु साथ ही लक्ष्य की रेखाओं को सुम्पष्ट बनाने के लिए छोटे-मोटे विरोधों के प्रवाह भी विश्व के व्यापक नियम में बिल्कुल स्वाभाविक माने गए हैं।
आचार्यश्री तुलसी को बहुत बड़ा समर्थन मिला, सत्थ में विरोध और समालोचनाएं भी। किन्तु उनका समतापरायण जीवन इन दोनों स्थितियों में काफी ऊँचा रहा है । अनुकूल और प्रतिकूल दोनों प्रकार की स्थितियों में साम्ययोग का निर्वाह करना, उनकी क्रियाशील साधना को सबसे अधिक प्रिय है।
महान् धर्माचार्य
प्राचार्यश्री की जीवनधारा ऊपर-ऊपर से विभिन्न रूपों में बहती हुई हमारे सामने आती है। इससे किसी अपरिचित व्यक्ति को कभी-कभी विरोधाभास का अनुभव हो सकता है। किन्तु गहराई में पैठने से वस्तुस्थिति का दर्शन अपने-आप हो जाता है। मध्यात्म की सुदृढ़ साधना के साथ-साथ शिक्षा, साहित्य, संस्कृति के सम्बन्ध में भी उनकी अपनी