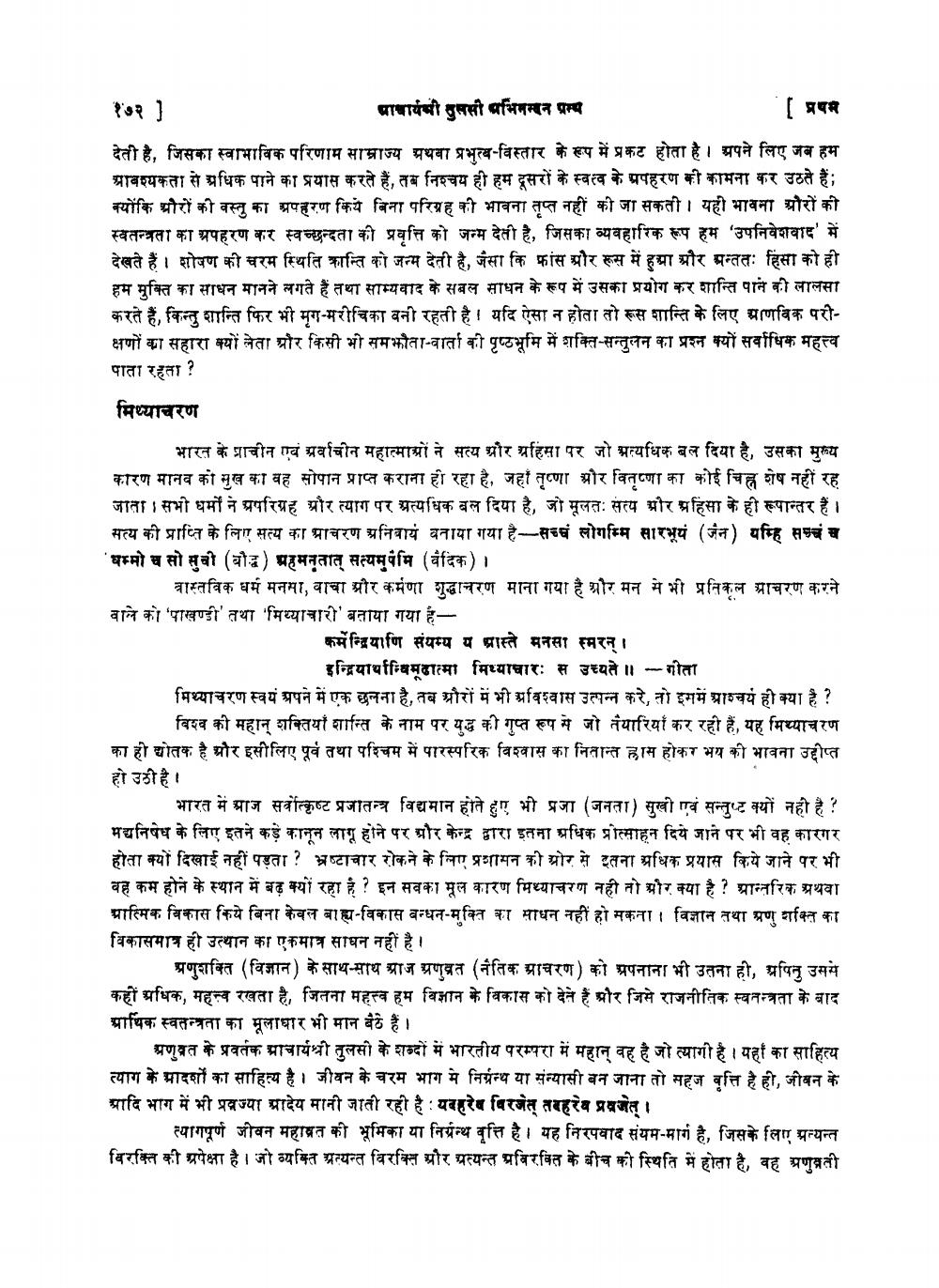________________
१७२ ]
प्राचार्यमी तुलसी अभिमम्बन मम्म
देती है, जिसका स्वाभाविक परिणाम साम्राज्य अथवा प्रभत्व-विस्तार के रूप में प्रकट होता है। अपने लिए जब हम आवश्यकता से अधिक पाने का प्रयास करते हैं, तब निश्चय ही हम दूसरों के स्वत्व के अपहरण की कामना कर उठते हैं; क्योंकि औरों की वस्तु का अपहरण किये बिना परिग्रह की भावना तृप्त नहीं की जा सकती। यही भावना औरों की स्वतन्त्रता का अपहरण कर स्वच्छन्दता की प्रवृत्ति को जन्म देती है, जिसका व्यवहारिक रूप हम 'उपनिवेशवाद' में देखते हैं। शोषण की चरम स्थिति क्रान्ति को जन्म देती है, जैसा कि फांस और रूस में हुया और पन्ततः हिंसा को ही हम मुक्ति का साधन मानने लगते हैं तथा साम्यवाद के सबल साधन के रूप में उसका प्रयोग कर शान्ति पाने की लालसा करते हैं, किन्तु शान्ति फिर भी मृग-मरीचिका बनी रहती है। यदि ऐसा न होता तो रूस शान्ति के लिए प्रमाणविक परीक्षणों का सहारा क्यों लेता और किसी भी समझौता-वार्ता की पृष्ठभूमि में शक्ति सन्तुलन का प्रश्न क्यों सर्वाधिक महत्त्व पाता रहता? मिथ्याचरण
भारत के प्राचीन एवं अर्वाचीन महात्माओं ने सत्य और अहिंसा पर जो अत्यधिक बल दिया है, उसका मुख्य कारण मानव को मुख का वह सोपान प्राप्त कराना ही रहा है, जहाँ तृष्णा और वितृष्णा का कोई चिह्न शेष नहीं रह जाता। सभी धर्मों ने अपरिग्रह और त्याग पर अत्यधिक बल दिया है, जो मूलतः सत्य और अहिंसा के ही रूपान्तर हैं। सत्य की प्राप्ति के लिए सत्य का आचरण अनिवार्य बताया गया है-सच्चं लोगम्मि सारभूयं (जैन) यहि सच्चं च 'धम्मो च सो सुची (बौद्ध) महमनतात् सत्यममि (वैदिक)।
वास्तविक धर्म मनमा, वाचा और कर्मणा शुद्धाचरण माना गया है और मन में भी प्रनिकल पाचरण करने वाले को 'पाखण्डी' तथा 'मिथ्याचारी' बताया गया है
कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यप्रास्ते मनसा स्मरन् ।
इन्द्रियान्विमहात्मा मिथ्याचारः स उच्यते॥ -गीता मिथ्याचरण स्वयं अपने में एक छलना है, तब औरों में भी अविश्वास उत्पन्न करे, तो इसमें प्राश्चर्य ही क्या है ?
विश्व की महान शक्तियाँ शान्ति के नाम पर युद्ध की गुप्त रूप में जो तैयारियां कर रही हैं, यह मिथ्याचरण का ही द्योतक है और इसीलिए पूर्व तथा पश्चिम में पारस्परिक विश्वास का नितान्त ह्रास होकर भय की भावना उद्दीप्त हो उठी है।
भारत में आज सर्वोत्कृष्ट प्रजातन्त्र विद्यमान होते हुए भी प्रजा (जनता) सुखी एवं सन्तुष्ट क्यों नही है ? मद्यनिषेध के लिए इतने कड़े कानून लागू होने पर और केन्द्र द्वारा इतना अधिक प्रोत्साहन दिये जाने पर भी वह कारगर होता क्यों दिखाई नहीं पड़ता? भ्रष्टाचार रोकने के लिए प्रशासन की ओर से इतना अधिक प्रयास किये जाने पर भी वह कम होने के स्थान में बढ़ क्यों रहा है ? इन सबका मूल कारण मिथ्याचरण नही तो और क्या है ? अान्तरिक अथवा आत्मिक विकास किये बिना केवल बाह्य-विकास बन्धन-मक्ति का साधन नहीं हो मकना । विज्ञान तथा अणु शक्ति का विकासमात्र ही उत्थान का एकमात्र साधन नहीं है।
अणुशक्ति (विज्ञान) के साथ-साथ आज अणुव्रत (नैतिक आचरण) को अपनाना भी उतना ही, अपितु उसमे कहीं अधिक, महत्व रखता है, जितना महत्व हम विज्ञान के विकास को देते हैं और जिसे राजनीतिक स्वतन्त्रता के बाद आर्थिक स्वतन्त्रता का मूलाधार भी मान बैठे हैं।
अणुव्रत के प्रवर्तक प्राचार्यश्री तुलसी के शब्दों में भारतीय परम्परा में महान् वह है जो त्यागी है। यहाँ का साहित्य त्याग के मादों का साहित्य है। जीवन के चरम भाग मे निर्ग्रन्थ या संन्यासी बन जाना तो महज वृत्ति है ही, जीवन के आदि भाग में भी प्रवज्या प्रादेय मानी जाती रही है : यवहरेव विरजेत् तरहरेव प्रवजेत् ।
त्यागपूर्ण जीवन महाव्रत की भूमिका या निर्ग्रन्थ वृत्ति है। यह निरपवाद संयम-मार्ग है, जिसके लिए अत्यन्त विरक्ति की अपेक्षा है। जो व्यक्ति अत्यन्त विरक्ति और अत्यन्त प्रविरक्ति के बीच की स्थिति में होता है, वह अणुव्रती