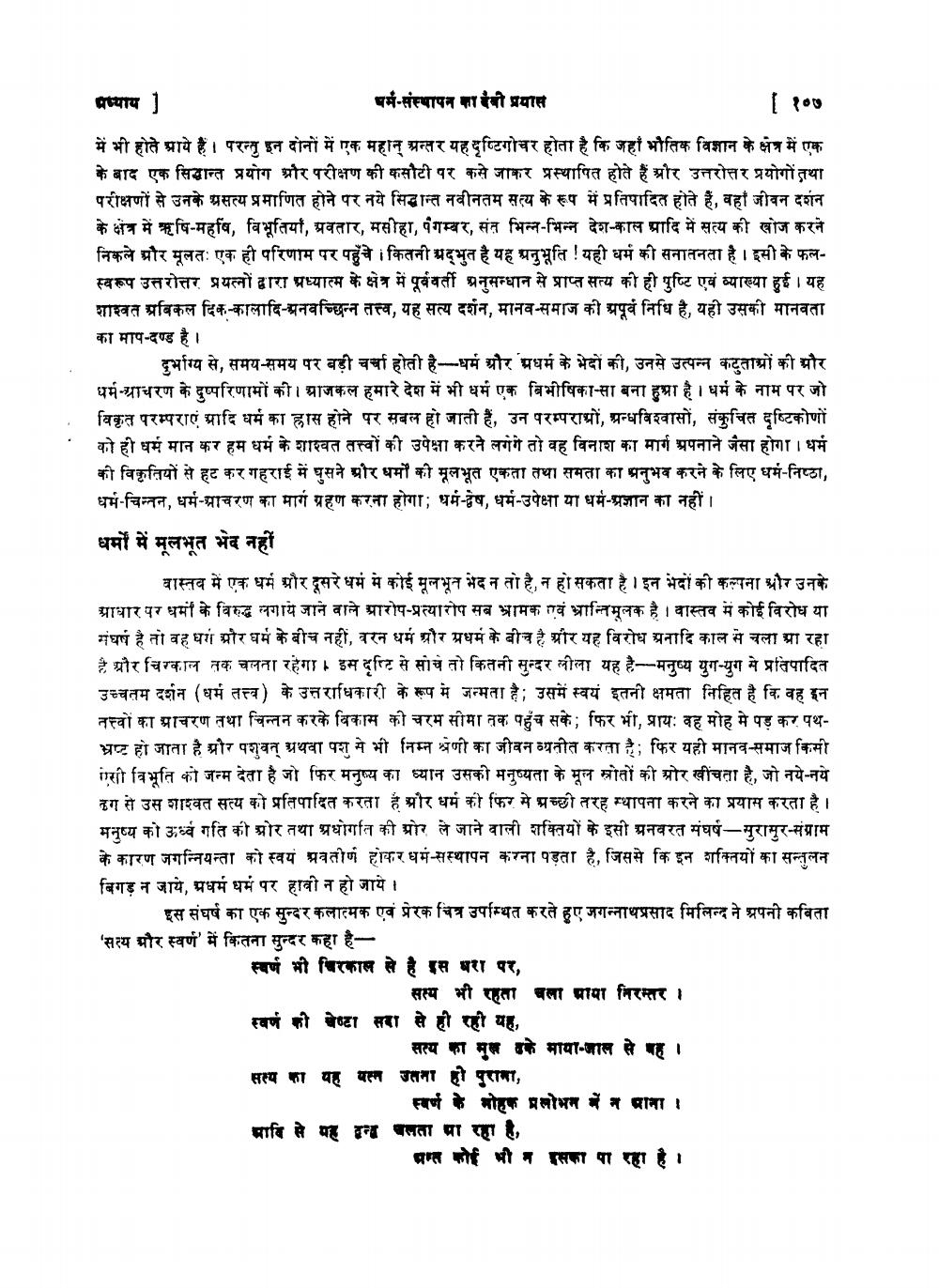________________
अध्याय ]
धर्म-संस्थापनका देवी प्रयास
[ १००
में भी होते प्राये हैं। परन्तु इन दोनों में एक महान् अन्तर यह दृष्टिगोचर होता है कि जहाँ भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में एक के बाद एक सिद्धान्त प्रयोग और परीक्षण की कसौटी पर कसे जाकर प्रस्थापित होते हैं और उत्तरोत्तर प्रयोगों तथा परीक्षणों से उनके प्रसत्य प्रमाणित होने पर नये सिद्धान्त नवीनतम सत्य के रूप में प्रतिपादित होते हैं, वहाँ जीवन दर्शन के क्षेत्र में ऋषि-महषि, विभूतियाँ, अवतार, मसीहा, पैगम्बर, संत भिन्न-भिन्न देश-काल प्रादि में सत्य की खोज करने निकले और मूलतः एक ही परिणाम पर पहुँचे । कितनी अद्भुत है यह अनुभूति ! यही धर्म की सनातनता है । इसी के फलस्वरूप उत्तरोत्तर प्रयत्नों द्वारा अध्यात्म के क्षेत्र में पूर्ववर्ती अनुसन्धान से प्राप्त सत्य की ही पुष्टि एवं व्याख्या हुई । यह शाश्वत अविकल दिक-कालादि-अनवच्छिन्न तत्त्व, यह सत्य दर्शन, मानव-समाज की अपूर्व निधि है, यही उसकी मानवता का माप-दण्ड है।
दुर्भाग्य से, समय-समय पर बड़ी चर्चा होती है-धर्म और अधर्म के भेदों की, उनसे उत्पन्न कटुताओं की और धर्म-याचरण के दुष्परिणामों की। अाजकल हमारे देश में भी धर्म एक विभीषिका-सा बना हुआ है । धर्म के नाम पर जो विकृत परम्पराएं आदि धर्म का ह्रास होने पर मबल हो जाती हैं, उन परम्पराओं, अन्धविश्वासों, संकुचित दृष्टिकोणों को ही धर्म मान कर हम धर्म के शाश्वत तत्त्वों की उपेक्षा करने लगेंगे तो वह विनाश का मार्ग अपनाने जैसा होगा । धर्म की विकृतियों से हट कर गहराई में घुसने और धर्मों की मूलभूत एकता तथा समता का अनुभव करने के लिए धर्म-निष्ठा, धर्म-चिन्तन, धर्म-आचरण का मार्ग ग्रहण करना होगा; धर्म-द्वेष, धर्म-उपेक्षा या धर्म-प्रज्ञान का नहीं। धर्मों में मूलभूत भेद नहीं
वास्तव में एक धर्म और दूसरे धर्म में कोई मूलभूत भेद न तो है, न हो सकता है । इन भेदों की कल्पना और उनके आधार पर धर्मा के विरुद्ध लगाये जाने वाले आरोप-प्रत्यारोप सब भ्रामक एवं भ्रान्तिमूलक है। वास्तव में कोई विरोध या मंघर्ष है तो वह धग और धर्म के बीच नहीं, वरन धर्म और अधर्म के बीच है और यह विरोध अनादि काल से चला आ रहा है और चिरकाल तक चलता रहेगा। इस दृष्टि से सोच तो कितनी सुन्दर लीला यह है-मनुष्य युग-युग मे प्रतिपादित उच्चतम दर्शन (धर्म तत्त्व) के उत्तराधिकारी के रूप में जन्मता है ; उसमें स्वयं इतनी क्षमता निहित है कि वह इन तत्त्वों का पाचरण तथा चिन्तन करके विकास की चरम सीमा तक पहुंच सके; फिर भी,प्रायः वह मोह मे पड़ कर पथभ्रष्ट हो जाता है और पशुवत् अथवा पश से भी निम्न श्रेणी का जीवन व्यतीत करता है ; फिर यही मानव-समाज किमी
सी विभूति को जन्म देता है जो फिर मनुष्य का ध्यान उसकी मनुष्यता के मूल स्रोतों की ओर खींचता है, जो नये-नये तुग से उस शाश्वत सत्य को प्रतिपादित करता है और धर्म की फिर से अच्छी तरह स्थापना करने का प्रयास करता है। मनुष्य को ऊर्ध्व गति की ओर तथा अधोगति की ओर ले जाने वाली शक्तियों के इसी अनवरत संघर्ष-सुरासुर-संग्राम के कारण जगन्नियन्ता को स्वयं प्रवतीर्ण होकर धर्म-सस्थापन करना पड़ता है, जिससे कि इन शक्तियों का सन्तुलन बिगड़ न जाये, अधर्म धर्म पर हावी न हो जाये।
इस संघर्ष का एक सुन्दर कलात्मक एवं प्रेरक चित्र उपस्थित करते हुए जगन्नाथप्रसाद मिलिन्द ने अपनी कविता 'सत्य और स्वर्ण' में कितना सुन्दर कहा हैस्वर्ण भी चिरकाल से है इस धरा पर,
सस्य भी रहता चला पाया निरन्तर । स्वर्ण की चेष्टा सा से हो रही यह,
सत्य का मुख ढके माया-जाल से बह । सत्य का यह बस्न उतना ही पुराना,
स्वर्ण के मोहक प्रलोभनमें न माना । मावि से मह दन चलता पा रहा है,
पन्त कोई भी इसका पा रहा है।