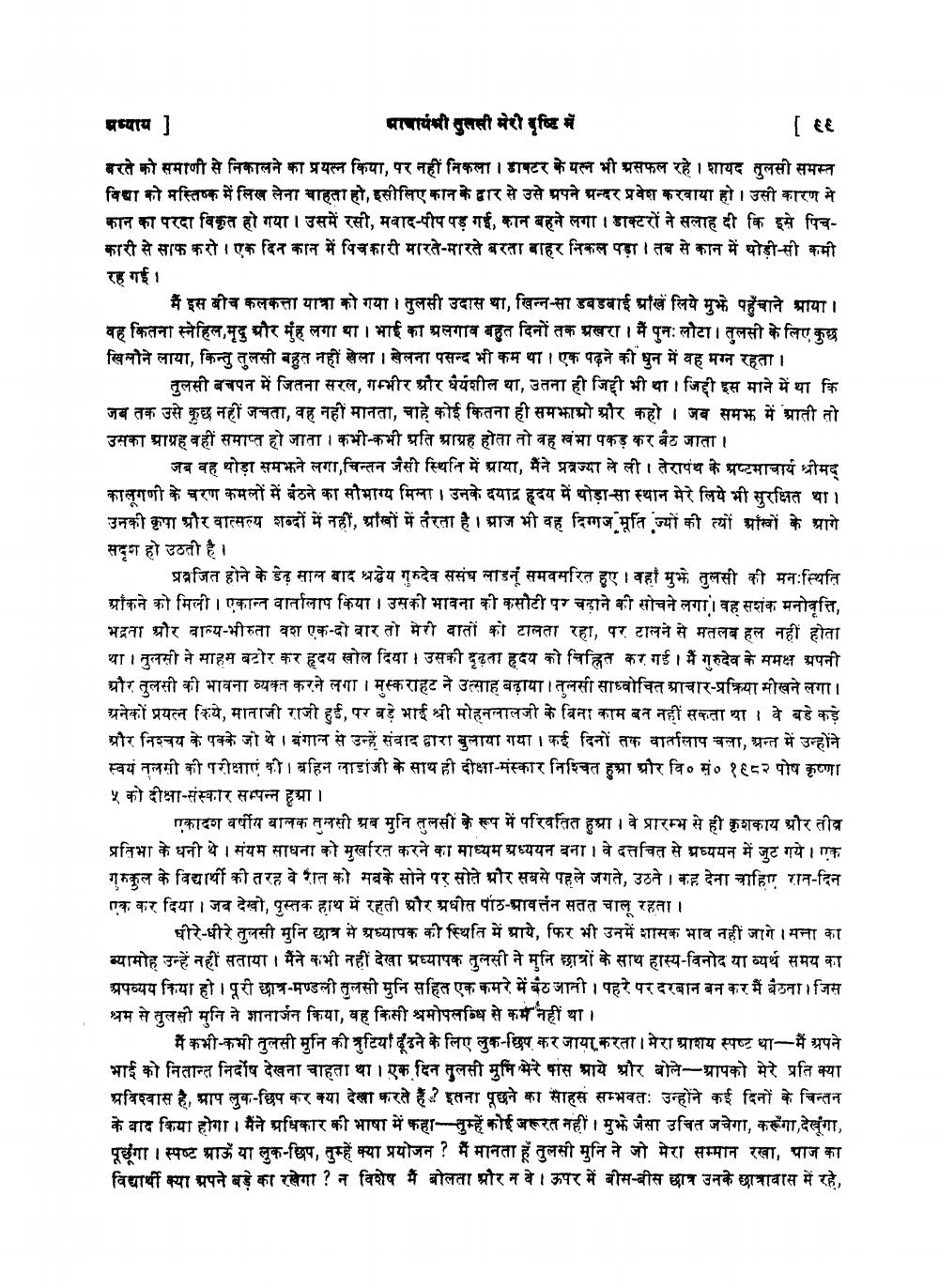________________
अध्याय ] पाचार्यश्री तुलसी मेरी दृष्टि में
[EL बरते को समाणी से निकालने का प्रयत्न किया, पर नहीं निकला । डाक्टर के यत्न भी असफल रहे । शायद तुलसी समस्त विद्या को मस्तिष्क में लिख लेना चाहता हो, इसीलिए कान के द्वार से उसे अपने अन्दर प्रवेश करवाया हो । उसी कारण मे कान का परदा विकृत हो गया। उसमें रसी, मवाद-पीप पड़ गई, कान बहने लगा । डाक्टरों ने सलाह दी कि इमे पिचकारी से साफ करो । एक दिन कान में पिचकारी मारते-मारते बरता बाहर निकल पड़ा। तब से कान में थोड़ी-सी कमी रह गई।
मैं इस बीच कलकत्ता यात्रा को गया। तुलसी उदास था, खिन्न-सा डबडबाई पाँखें लिये मुझे पहुँचाने पाया। वह कितना स्नेहिल,मृदु और मुंह लगा था। भाई का अलगाव बहुत दिनों तक अखरा । मैं पुनः लौटा। तुलसी के लिए कुछ खिलोने लाया, किन्तु तुलसी बहुत नहीं खेला । खेलना पसन्द भी कम था। एक पढ़ने की धुन में वह मग्न रहता।
तुलसी बचपन में जितना सरल, गम्भीर और धैर्यशील था, उतना ही जिद्दी भी था। जिद्दी इस माने में था कि जब तक उसे कुछ नहीं जचता, वह नहीं मानता, चाहे कोई कितना ही समझामो और कहो । जब समझ में आती तो उसका प्राग्रह वहीं समाप्त हो जाता। कभी-कभी अति प्राग्रह होता तो वह खंभा पकड़ कर बैठ जाता।
जब वह थोड़ा समझने लगा,चिन्तन जैसी स्थिति में प्राया, मैंने प्रवज्या ले ली। तेरापंथ के प्रष्टमाचार्य श्रीमद् कालगणी के चरण कमलों में बैठने का सौभाग्य मिला। उनके दयाद्र हृदय में थोड़ा-सा स्थान मेरे लिये भी सुरक्षित था। उनकी कृपा और वात्सल्य शब्दों में नहीं, आँखों में तैरता है। आज भी वह दिग्गज मूर्ति ज्यों की त्यों आँखों के आगे सदृश हो उठती है।
प्रजित होने के डेढ़ साल बाद श्रद्धेय गुरुदेव ससंघ लाडनूं समवसरित हुए। वहाँ मुझे तुलसी की मनःस्थिति प्रांकने को मिली। एकान्त वार्तालाप किया। उसकी भावना की कसौटी पर चढ़ाने की सोचने लगा। वह सशंक मनोवृत्ति, भद्रता और बाल्य-भीरुता वश एक-दो बार तो मेरी बातों को टालता रहा, पर टालने से मतलब हल नहीं होता था । तुलसी ने माहम बटोर कर हृदय खोल दिया। उसकी दृढ़ता हृदय को चिह्नित कर गई। मैं गुरुदेव के समक्ष अपनी और तुलसी की भावना व्यक्त करने लगा। मुस्कराहट ने उत्साह बढ़ाया। तुलसी साध्वोचित प्राचार-प्रक्रिया मीखने लगा। अनेकों प्रयत्न किये, माताजी राजी हुई, पर बड़े भाई श्री मोहनलालजी के बिना काम बन नहीं सकता था। वे बडे कड़े
और निश्चय के पक्के जो थे । बंगाल से उन्हें संवाद द्वारा बुलाया गया। कई दिनों तक वार्तालाप चला, अन्त में उन्होंने स्वयं तुलसी की परीक्षाएं की। बहिन लाडांजी के साथ ही दीक्षा-मस्कार निश्चित हुआ और वि० सं० १९८२ पोष कृष्णा ५ को दीक्षा-संस्कार सम्पन्न हुआ।
एकादश वर्षीय बालक तुलसी अब मुनि तुलसी के रूप में परिवर्तित हुप्रा । वे प्रारम्भ से ही कृशकाय और तीव प्रतिभा के धनी थे । संयम साधना को मुरित करने का माध्यम अध्ययन बना। वे दत्तचित से अध्ययन में जुट गये। एक गरुकुल के विद्यार्थी की तरह वे रात को मबके सोने पर सोते और सबसे पहले जगते, उठते। कह देना चाहिए रान-दिन एक कर दिया। जब देखो, पुस्तक हाथ में रहती और अधीत पाठ-प्रावर्तन सतत चालू रहता।
धीरे-धीरे तुलसी मुनि छात्र से अध्यापक की स्थिति में प्राये, फिर भी उनमें शासक भाव नहीं जागे । मना का व्यामोह उन्हें नहीं सताया। मैंने कभी नहीं देखा प्रध्यापक तुलसी ने मुनि छात्रों के साथ हास्य-विनोद या व्यर्थ समय का अपव्यय किया हो। पूरी छात्र-मण्डली तुलसी मुनि सहित एक कमरे में बैठ जाती। पहरे पर दरबान बन कर मैं बैठना। जिस श्रम से तुलसी मुनि ने ज्ञानार्जन किया, वह किसी श्रमोपलब्धि से कम नहीं था।
मैं कभी-कभी तुलसी मुनि की त्रुटियाँ ढूँढने के लिए लुक-छिप कर जाया करता। मेरा प्राशय स्पष्ट था-मैं अपने भाई को नितान्त निर्दोष देखना चाहता था। एक दिन तुलसी मुनि मेरे पास आये और बोले-पापको मेरे प्रति क्या अविश्वास है, माप लुक-छिप कर क्या देखा करते हैं ? इतना पूछने का साहस सम्भवतः उन्होंने कई दिनों के चिन्तन के बाद किया होगा। मैंने अधिकार की भाषा में कहा-तुम्हें कोई जरूरत नहीं। मुझे जैसा उचित जचेगा, करूँगा,देलूँगा, पूछगा। स्पष्ट पाऊँ या लुक-छिप, तुम्हें क्या प्रयोजन ? मैं मानता हूँ तुलसी मुनि ने जो मेरा सम्मान रखा, पाज का विद्यार्थी क्या अपने बड़े का रखेगा? न विशेष मैं बोलता और न थे। ऊपर में बीस-बीस छात्र उनके छात्रावास में रहे,